General Competition | Economics & Economy | गरीबी एवं बेरोजगारी
गरीबी उस स्थिति को कहते है जब व्यक्ति को जीवन यापन करने हेतु निम्नतम अधारभूत जरूरतें (भोजन, वस्त्र, मकान) भी उपलब्ध नही हो पाते है। यह गरीबी वर्तमान में भी भारत जैसे विकासशील देश के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है।
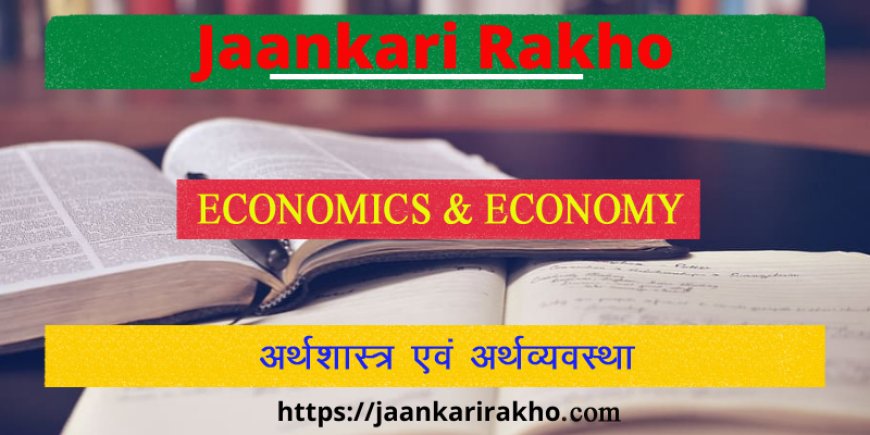
General Competition | Economics & Economy | गरीबी एवं बेरोजगारी
- गरीबी उस स्थिति को कहते है जब व्यक्ति को जीवन यापन करने हेतु निम्नतम अधारभूत जरूरतें (भोजन, वस्त्र, मकान) भी उपलब्ध नही हो पाते है। यह गरीबी वर्तमान में भी भारत जैसे विकासशील देश के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है।
- विकासशील देश के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी का अनुमान 'World Development Report 1990' में लगाया गया इस रिपोर्ट में गरीबी को निम्न तरह से परिभाषित किया गया- "गरीबी निम्नतम जीवनयापन स्तर प्राप्त करने की असर्मथता है ।
- गरीबी को यू. एन. डी. पी. (UNDP) दो प्रकार से देखता है - आय गरीबी तथा मानव गरीबी
- आय गरीबी (Income Poverty)- अगर व्यक्ति जीवन यापन हेतु आवश्यक निम्नतम वस्तु जैसे- वस्त्र, भोजन आवास भी अपने लिये उपलब्ध नही करा पाता है तो इसे आय गरीबी कहा जाता है।
- मानव गरीबी (Human Poverty) - वह व्यक्ति जिन को संतोषजनक जीवन, दीर्घ आयु, स्वस्थ रहन सहन से वंचित रहना पड़े तो इसे मानव गरीबी कहा जाता है।
- गरीबी अथवा निर्धनता के संबंध में दो धारणायें प्रचलित है अथवा गरीबी को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है - सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी ।
- सापेक्षिक गरीबी (Relative Poverty)
- सापेक्षिक गरीबी से देश के जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच में आय-विषमता का पता चलात है । सापेक्षिक गरीबी जानने हेतु देश के उच्च आय वर्ग के उच्चतम 5 - 10 प्रतिशत लोगों की आय की तुलना निम्न आय वर्ग में निम्नतम 5-10% लोगों के आय स्तर से की जाती है तथा इससे प्राप्त परिणाम सापेक्षिक गरीबी को प्रदर्शित करता है ।
- गरीबी की पाप हेतु सापेक्षिक गरीबी सिद्धांत का उपयोग प्रायः उन देशों में किया जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था काफी समृद्ध है। सापेक्षिक गरीबी मापने हेतु दो विधी प्रचलित है- लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक ।
- लारेंज वक्र (Lorenz Curve)
- लारेंज वक्र धारणा का विकास 1905 में मैक्स ओ. लारेंज ने किया । इस वक्र या प्रत्येक बिन्दु उन व्यक्ति ( अथवा परिवार ) को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय प्रतिशत के नीचे है।
- लारेंज वक्र खींचने के लिए x -अक्ष पर जनसंख्या का प्रतिशत तथा y-अक्ष पर आय का प्रतिशत लेते है । यदि 10% जनसंख्या के पास आय का 10% हो, 20% के पास आय का 20% हो अर्थात् x% जनसंख्या के पास आय का x% हो तो इसको दर्शाने वाली रेखा ग्राफ पर 45° पर होगा और इसे पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा कहते है. और यह बताता है कि . आय विषमता बिल्कुल भी नहीं है-

- पूर्ण समता रेखा वाली स्थिति प्रायः विश्व के किसी भी देश में नही पायी जाती है। लारेंज वक्र दर्शाने हेतु पहले ज्ञात किया जाता है कितने प्रतिशत जनसंख्या के हिस्से में कितने प्रतिशत आय है फिर इनसे संबंधित बिन्दु को ग्राफ पर ज्ञात कर लिया जाता है । इन बिंदु से आने वाली वक्र को ही लारेंज वक्र कहते है ।

- लारेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के जितना करीब होगा आय विषमता उतनी कम होगी तथा लारेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के जितना दूर होगा आय विषमता उनती अधिक होगी। अगर सम्पूर्ण आय किसी एक ही व्यक्ति के पास है जो इसे प्रदर्शित करने वाली रेखा AB होगा लारेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगा ।
- गिनी गुणांक (Gini Coefficient)
- सापेक्षिक गरीबी के मापन हेतु यह दूसरी तथा सबसे प्रचलित विधी है। वास्तव में गिनी गुणांक लारेंज वक्र का ही गणीतीय रूप है तथा इस गुणांक को लारेंज वक्र के सहायता से ही निकाला जाता है।
- इस गुणांक का विकास इटली के सांख्यिकी विद कोरेडो गिनी ने विकसीत किया है।
- गिनी गुणांक लारेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल को अनुपात है।
-

- गिनी गुणांक का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। अगर गिनी गुणांक शून्य है तो इसका अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को एक आय मिल रही हैं अर्थात् आय विषमता बिल्कुल भी नहीं है और अगर गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका अर्थ है एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है।
- निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty)
- जब मनुष्य अपने लिये बुनियादी आवश्यकता (जैसे- वस्त्र, भोजन, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा) प्राप्त करने में भी असर्मथ रहता है तो इसे निरपेक्ष गरीबी कहते है।
- निरपेक्ष गरीबी ज्ञात करेन हेतु सबसे पहले व्यक्ति के आदर्श जीवनयापन हेतु आवश्यक वस्तु (जैसे- अनाज, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, आवास) निश्चित की जाती है। इसके बाद आवश्यक वस्तु के मौद्रीक योग निकालकर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय निर्धारित की जाती है। प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय को सामान्यतः गरीबी रेखा कहा जाता है। जनसंख्या का जितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे होता है उसे गरीब माना जाता है।
- भारत जैसे विकासशील जैसे देशों में गरीबी मापन हेतु या गरीबी के अध्ययन के लिए निरपेक्षता सिद्धांत का ही उपयोग होता है।
- भारत में गरीबी मापन हेतु खर्च अथवा उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित किया जाता है और जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम होता है उसे गरीब मान लिया जाता है। गरीबी मापन के इस विधि को Head count Method भी कहा जाता है।
- भारत में निर्धनता रेखा परिभाषित करने के लिए योजना आयोग समय-समय पर समिति गठीतं किया। प्रमुख समिति जिनका गठन गरीबी रेखा परिभाषित करने हेतु हुआ-
- भारत में निर्धनता रेखा (गरीबी रेखा ) के निर्धारण का पहला अधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया गरीबी रेखा निर्धारण हेतु इस वर्ष एक समिति गठीत की गई।
- इस समिति के सदस्य डी. आर. गाडगिल, अशोक मेहता, बी. एन. गांगुली, पी. एस. लोकनायन, पीताम्बर पन्त, वी. के. आर. वी. राव, श्रीमन्न नारायण तथा बाला साहेब सहस्त्रबुद्धे थे।
- इस समिति ने बिना किसी आधार को स्पष्ट किये 1960-61 के प्रचलित मूल्य पर ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रू. 20 न्यूनतम उपयोग व्यय को आधार मान कर गरीबी मापन का सुझाव दिया। हालांकि समिति के इस दृष्टिकोण की तीव्र आलोचना हुई ।
- डॉ. वाई. के. अघल समिति
- योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1977 में इस समिति का गठन किया जिसने जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
- इस समिति ने 1958 के भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के न्यूनतम पोषाहार रिपोर्ट को आधार बनाकर ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र हेतु 2100 कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति से कम होगा वह गरीबी रेखा से नीचे होंगे।
- गरीबी मापन के इस प्रणाली को " भोजन ऊर्जा प्रणाली" भी कहते है।
- लकड़ावाला समिति
- योजना आयोग ने इस समिति का गठन 1989 में किया। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस समिति ने अलग-अलग राज्यों के लिए प्रचलित मूल्य के आधार पर अलग-अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया। इस समिति के सुझावो को 9 वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता की माप के लिए योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया।
- ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धनता रेखा के लिए समिति ने कृषि श्रमिको के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया तथा शहरी क्षेत्र हेतु औद्योगिक श्रमिको के उपभेक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनया।
- सुरेश तेंदुलकर समिति
- योजना आयोग ने 2005 में तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की । इस समिति के नियुक्ति करने का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारत में गरीबी घट रही है या नही तथा समिति को नयी गरीबी रेखा भी परिभाषित करने को कहा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की।
इस समिति ने उपभोग व्यय निर्धारति करने हेतु जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तु के अलावे उन वस्तु को भी शामिल किया जो जीवन की गुणवत्ता हेतु आवश्यक है। इस तरह यह समिति गरीबों के व्यापक तथा बहुआयामी रूप को स्वीकार किया।
- तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु उपयोग के लिए आवश्यक खाद्यान्न के अलावे छ: बुनियादी आवश्यकता को शामिल किया। 'ये छ :- बुनियादि आवश्यकताएँ हैं- शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादि संरचना (जैसे- सड़क, बिजली), स्वच्छ वातावरण महिलाओं को काम तथा लाभ तक व्यक्ति की पहुँच।
- तेंदुलकर समिति के सिफारिश के अनुसार गरीबी रेखा हेतु प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय तथा गरीबी की प्रतिशत-
- योजना आयोग ने 2005 में तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की । इस समिति के नियुक्ति करने का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारत में गरीबी घट रही है या नही तथा समिति को नयी गरीबी रेखा भी परिभाषित करने को कहा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की।
- भारत में निर्धनता रेखा (गरीबी रेखा ) के निर्धारण का पहला अधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया गरीबी रेखा निर्धारण हेतु इस वर्ष एक समिति गठीत की गई।

- योजना आयोग ने 2012 में रंगराजन समिति की नियुक्ति की जिसने 2014 में अपना रिपोर्ट पेश किया।
- इस समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण हेतु उसी मेथडालजी को अपनाया जिसका उपयोग डॉ. वाई. के. अघल समिति ने अपनाया था।
- यह समिति अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू. 972 तथा शहरी क्षेत्र के लिए रू. 1407 मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया।
तेंदुलकर कमेटी तथा रंगराजन कमेटी के बीच अंतर
- तेंदुलकर कमेटी (या समिति) ने राज्य स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी गरीबी रेखा निर्धारण हेतु अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा बास्केट का प्रयोग किया जबकि रंगराजन ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिए दो अलग-अलग अखिल भारत गरीबी रेखा बास्केट लिया तथा उसके आधार पर राज्य स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी गरीबी रेखा का निर्धारण किया ।
- तेंदुलकर कमेटी ने डॉ. वाई. के. अघल समिति के कैलोरी मापक सिद्धांत को नही माना जबकि रंगराजन कमेटी ने इस सिद्धांत को अपनाया।
- उपभोग व्यय संबंधी आँकड़े NSSO द्वारा एकत्रित किया जाता है। तेंदुलकर कमेटी ने NSSO के आँकड़े में आधार पर ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया परंतु रंगराजन कमेटी ने NSSO के आँकड़ों को संदिग्ध माना ।
- तेंदुलकर समिति के मेथडालजी पर आधारित गरीबी रेखा के तुलना में रंगराजन कमेटी के मेथडालजी आधार पर गरीबी का अनुमान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्रमश: 19% तथा 41% अधिक रहा ।
- तेंदुलकर कमेटी के सिफारिश के आधार पर 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी का प्रतिशत 25.7 तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत 13.7 और अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी का प्रतिशत 21.9 है। रंगराजन समिति में सिफारिश के आधार पर 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत 30.9 तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत 26.4 और अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी का प्रतिशत 29.5 है।
विभिन्न राज्यों में गरीबी का प्रतिशत (2011-12)
- योजना आयोग ने NSSO (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन) द्वारा परिवार उपभोग व्यय (2011-12) के संबंध में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 2011-12 के लिए गरीबी रेखा और गरीबी के अनुपात को अधटन किया है।
- योजना आयोग ने गरीबी रेखा निर्धारण हेतु तेंदुलकर स के सिफारिश को ही माना है। 2011-12 हेतु तेंदुलकर समिति के सिफारिश के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लिये 816 मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय और शहरी क्षेत्र के लिये रू. 1000 पर अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा निर्धारित की गई है।
- उपभोग व्यय से संम्बन्धित आँकड़े एकत्र करने की विधी-
- गरीबी से संबंधित सभी प्रकार के आँकड़ों को NSSO एकत्रित करती है। इन्ही आँकड़ो के आधार पर योजना आयोग यह सुनिश्चित करती है कि देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है।
- सर्वप्रथम पी. सी. महालनोबिस के सिफारिश पर 1958 में वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) की स्थापना की गई। 1970 में (NSS) का पुर्नगठन किया गया तथा 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई ।
- 23 मई 2019 के केंद्रीय सरकार ने NSSO तथा CSO (केंद्रीय सांख्यिकी संगठन) को मिलाकर (मर्ज करके) नेशनल स्टैटिकल ऑफिस (NSO) नाम की एक नई संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में NSO अस्तित्व में नहीं आका है।
- NSSO उपभोग व्यय संबंधित आँकड़े निम्न तरह से एकत्रित करती है।
- एकसमान संदर्भ अवधि or URP (Uniform Reference Period)
- इस विधि 30 दिनों की स्मृति अवधि के दौरान उपयोग की गई सभी वस्तुओं से संबंधित आँकड़े एकत्र किये जाते है।
- इस विधि का उपयोग NSSO 1993-94 से पहले करता था। वर्तमान में इस विधि का उपयोग नहीं होता है।
- NSSO द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए एकत्रित आँकड़ो के आधार पर अगर URP विधि का प्रयोग किया जाय तो राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुपात 27.5% प्रतिशत था जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 28.3% तथा शहरी क्षेत्र के लिए 27.3% है।
- मिश्रित संदर्भ अवधि or MRP (Mixed Reference Period)
- इस विधि पिछले 365 दिन के दौरान उपयोग की गई पाँच गैर खाद्य मदें (वस्त्र, जूता तथा चप्पल, टिकाऊ वस्तुएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा) तथा पिछले 30 दिनों में उपयोग की गई सभी वस्तुओं की माप की जाती है।
- 2004-05 के लिए एकत्रित आँकड़ो के आधार पर MRP विधि का प्रयोग किया जाय तो राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुपात लगभग 21.8 प्रतिशत आता है। ग्रामीण क्षेत्र में 21.8 तथा शहरी क्षेत्र में 21.7 प्रतिशत ।
- संसोधित मिश्रित संदर्भ अवधि or MMRP (Modified Mixed Reference Period)
- NSSO ने वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 में इस विधि को अपनाकर आँकड़े एकत्रित किये।
- इस विधि में उपयोग की जाने वाले कुछ वस्तु (जैसे- मांस-मछली, सब्जि, फल पान, तंबाकू, खाद्यन्न, शराब आदि) की माप पिछले 30 दिनों के बजाय पिछले 7 दिनों की स्मृति अवधि के लिये की जाती है तथा शेष 30 दिनों के आधार पर ही किया जाता है।
अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स (2015)
- योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग ने गरीबो में पहचान हेतु अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक कार्यदल (टास्कफोर्स) का गठन किया है। इस कार्य दल में अन्य सदस्य है- विवेक देबराय, सुरजीत भल्ला।
- अरबिन्द पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित यह कार्यदल गरीबी रेखा के अनुमान के सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाया पर आयोग ने सुझाव दिया है कि गरीबी से सम्बन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निचले 40 प्रतिशत को गरीब के रूप में माना गया।
- नीति आयोग का मानना है यदि गरीबी की संख्या जानना आवश्यक है तो ग्रामीण गरीबो का अनुमान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तथा शहरी गरीबो का अनुमान शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए ।
गरीबो के संबंध में प्रो. ए. के. सेन (Amartya Sen) का दृष्टिकोण
- प्रो. ए. के. सेन एक अर्थशास्त्री है और इन्हे 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया (प्रो. सेन ने 1973 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट) 'Poverty, Inequality and unemployment' में गरीबी मापने का एक नया दृष्टिकोण दिया।
- प्रो. सेन के अनुसार जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, वे सभी समान रूप से गरीब नही है। जो व्यक्ति गरीबी रेखा से जितना दूर होगा वह उतना ही अधिक गरीब होगा ।
- प्रो. सेन का मानना है कि अगर हमे गरीबी की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है तो गरीबी रेखा के नीचे सभी व्यक्तियों को गिनने के बजाय हमे प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में गरीबी रेखा से आय की गिरावट को देखना चाहिए। गरीबो की आय की गरीबी रेखा से गिरावट को भाकित करके गरीबो को नापा जा सकता है।
- प्रो. सेन का यह दृष्टिकोण सापेक्षिक तथा निरपेक्ष दोनों प्रकार के गरीबी मापने हेतु उपयुक्त है।
निर्धनता जाल (Poverty Trap)
- निम्नतम जीवनयापन से भी वंचित होंना गरीबी कहलाता है। अगर कोई परिवार गरीब है तो उनके साथ कई तरह के समस्या आ जाती है और समस्या उस गरीब परिवार के आने वाले पीढ़ी को प्रभावित कर देता है जिससे गरीबो में आने वाली पीढ़ी भी गरीबी के जाल में फस जाता है जिसे हम निर्धनता का दुश्चक्र या निर्धनता जाल की संज्ञा देते है।

भारत में गरीबी के कारण
- विश्व में अधिकांश गरीब भारत जैसे अर्द्ध विकसित देशों में ही निवास करते है । 1951-55 में भारत में 199 मिलियन लोग गरीब थे जो कुल जनसंख्या का 52.6% था। 1993-94 में भी लगभग 320 मिलियन लोग गरीब थे जो जनसंख्या का 36% था। योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में गरीबो की संख्या 407.1 मिलियन था जो 2011-12 में घटकर 269.3 मिलियन रह गया है। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार - (2011-12 ) गरीबी का प्रतिशत 21.9 है।
- भारत में व्यापक स्तर पर पाये जाने वाले गरीबी का निम्न कारण है-
- लम्बे समय (200 वर्ष) तक भारत का गुलाम होना ।
- जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
- कृषि का पिछड़ापन
- पूंजी का अभाव तथा धीमी गति से औद्योगिक विकास
- बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की समस्या
- आय, धन एवं संसाधनों का असमान वितरण
- प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त दोहन नहीं हो पाना
- आधारिक संरचना का अविकसित होना
- अनुकूल सामाजिक वातावरण का अभाव
- पूंजीवाद विकास पद्धति
- जब जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा गरीबी में जी रहा हो तो कई दुष्परिणाम निकल कर सामने आते है। गरीबी के प्रमुख दुष्परिणाम निम्न है-
- भुखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य की समस्या
- समाज में असमानता की वृद्धि
- जनसंख्या वृद्धि तेज होना
- अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होना
- निम्न जीवन स्तर
- अशिक्षा तथा बालश्रम की समस्या
- समावेशी विकास में बाधा
- बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएँ
भारत में गरीबी उन्मूलन के उपाय
- गरीबी दूर करने का सबसे बेहतर कारगार उपाय है कृषि का आधुनिकीकरण कर उसका तीव्र विकास की जानी चाहिए क्योंकि आज 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि पर निर्भर है।
- देश में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधन का भरपुर तथा अनुकूलतम उपयोग कर के आर्थीक विकास को तीव्र करना पड़ेगा ।
- जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना
- व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के लिए नये अवसरो का सृजन करना
- आय तथा साधनों का समान वितरण हेतु आवश्यक कदम उठाना तथा कर प्रणाली में आवश्यक सुधार लाना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करना
- बचत एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना
- गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन करना ।
बेरोजगारी (UNEMPLOYMENT)
- बेरोजगारी उस स्थिति को कहते है जब व्यक्ति को काम करने की इच्छा एवं योग्यता रहने के बावजूद उन्हे काम या रोजगार नहीं मिलता है।
- जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से या आलस्य के कारण काम नही करता है जो उसे बेरोजगार के श्रेणी में नही रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार काम करने की इच्छा है परंतु अगर उनके पास योग्यता नहीं है जिसके कारण उसे काम नही मिलता है तो इस स्थिति को भी तो बेरोजगारी नही माना जाता है।
- बेरोजगारी उस स्थिति को भी कहा जाता है जब व्यक्ति इच्छा के अनुरूप अथवा क्षमता के अनुरूप काम नहीं मिलता है या कुछ घंटो का ही काम मिल पाता है।
- नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन ने बेरोजगारी को इस तरह से परिभाषित किया है- " लाभदायक काम के अभाव के स्थिति को बेरोजगारी कहते है।" अमर्त्य सेन ने रोजगार के तीन पहलू बताये है - आय पहलू ( income aspect ), उत्पादन पहलू (Production aspect) तथा पहचान पहलू ( Recognition aspect) इसका अर्थ है कि अगर व्यक्ति रोजगार में है तो उसे आय प्राप्ति होनी चाहिए उत्पादन बढ़नी चाहिए तथा उस व्यक्ति की समाज में पहचान मिलनी चाहिए।
- शुरूआत में बेरोजगारी को सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समस्या माना जाता था परंतु वर्तमान समय में ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नही है जहाँ बेरोजगारी की समस्या नही पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होने कारण अलग-अलग होते है। विकसित देशों में जहाँ बेरोजगारी की समस्या व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है वही विकासशील तथा अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्था में बरोजगारी की समस्या विकास की धीमी गति तथा संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग न होने के कारण उत्पन्न होती है ।
बेरोजगारी के विभिन्न रूप
- ऐच्छीक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment )- जब कोई श्रमिक प्रचलित मजदूरी पर काम करना नही चाहे तो उसे ऐच्छीक बेरोजगारी कहा जाता है। परंतु इस प्रकार के बेरोजगार श्रमिक को वास्तविक रूप से बेरोजगार नही माना जाता है।
- अनैच्छीक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment )- जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार मजदूर को काम नही मिले तो इसे अनैच्छीक बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छीक बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब रोजगार की मात्रा श्रमिकों की पूर्ति से कम हो ।
- घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)- जब श्रमिक एक काम को छोड़कर दूसरे काम को पकड़ता है तो दोनों काम के बीच कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। इस तरह में बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी को संघर्षात्मक तथा अस्थिर बेरोजगारी की भी संज्ञा दी जाती है।
- घर्षणात्मक बेरोजगारी के निम्न कारण हो सकते है-
- श्रमिकों को काम की जानकारी का अभाव
- कच्चे माल की कमी
- मशीनों या यंत्रो का टूट जाना
- कार्यों का मौसमी स्वरूप
- नये कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना आदि
- घर्षणात्मक बेरोज़गारी सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था में पायी जाती है। कभी-कभी अर्थव्यवसथा के आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन के कारण भी इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है।
- घर्षणात्मक बेरोजगारी के निम्न कारण हो सकते है-
- चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment )- चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पायी जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापारं चक्र घटित होते है। व्यापारचक्र की अवस्था में जब मंदी आती है तो कई लोग बेरोजगार हो जाते है। इस प्रकार की बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है।
- संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment ) - संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था के औद्योगिक ढाँचे या संरचना में बदलाव आता है। संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्यत: दो स्थितियों में उत्पन्न होती है-
- किसी उद्योग की निर्मित वस्तुओं की मांग कम हो जाए तब उद्योग का विकास ठप पड़ जाता है। जैसे- शराबबंदी लागू होने से शराब उद्योग का बंद हो जाना। सरकार द्वारा प्लास्टीक उद्योग को बंद करा देना ।
- उत्पादन में इस्तेमाल हो रहे तकनीक में परिवर्तन होना इस कारण पुराने कारीगर बेकार हो जाते है।
- मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment ) - कुछ उद्योग अथवा व्यवसाय (जैसे- चीनी मिल, स्वेटर, जैकेट उद्योग) मौसमी प्रकृति में होते है। ये उद्योग वर्ष के कुछ महीने उत्पादन करते है शेष महीने बंद रहते है । इस तरह के उद्योग में बंद होने से उत्पन्न बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है।
- मौसमी बेरोजगारी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से पायी जाती है क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा कृषि कार्य संलग्न रहते है। कृषि कार्य मौसमी व्यवसाय है।
- अदृश्य/छिपी हुई/प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment)- जब किसी कार्य को करने हेतु जितने श्रमिक की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक उस कार्य में लगे हो तब इसे अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है । अदृश्य बेरोजगारी के स्थिति में श्रमिक काम करते तो दिखाई पड़ते है परंतु वास्तविकता यह है कि कुछ श्रमिकों हटा दिया जाए तो काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों की सीमांत आवश्यकता शून्य होती है । भारत के कृषि क्षेत्रों में इसी प्रकार के बेरोजगारी व्याप्त है।
भारत में बेरोजगारी का स्वरूप
- भारत में पाये जाने वाले बेरोजगारी को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-
- ग्रामीण बेरोजगारी
- औद्योगिक बेरोजगारी
- शिक्षित लोगों की बेरोजगारी
- ग्रामीण बेरोजगारी - भारत में बेरोजगारी की अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः दो प्रकार के बेरोजगारी पायी जाती है- मौसमी बेरोजगारी तथा छिपी हुई बेरोजगारी । ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाने वाले इस बेरोजगारी मुख्य कारण निम्न है-
- तीव्र जनसंख्या वृद्धि
- कृषि का पिछड़ापन तथा पारिवारिक कृषि जोतो का उपविभाजन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाने वाले लघु तथा कुटीर उद्योगों का पतन ।
- देश के उद्योगों का धीमी गति से विकास
- जीवन-निर्वाह कृषि
- आय बचत एवं पूंजी निर्माण का निम्न स्तर
- सरकार द्वारा चलाये जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सही ढंग से क्रियान्वयन नही हो पाना
- औद्योगिक बेरोजगारी - जब देश में उद्योगों का विकास तथा विस्तार तेजी से नही होता है तो तकनीकी एवं गैर-तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता रखने वाले लोगों को कांम नहीं मिल पाता है। तकनीकी तथा गैर-तकनीकी रूप से काम करने में सक्षम लोगों को जब काम नही मिल पाता है तो उसे हम औद्योगिक बेरोजगारी के श्रेणी में रखते है ।
औद्योगिक बेरोजगारी के निम्न कारण है-(i) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि(ii) रोजगार विहिन आर्थीक विकास(iii) उद्योगों में श्रम बचत प्रविधियो का बढ़ता हुआ प्रयोग(iv) बड़े पैमाने पर की जाने वाली कर्मचारी की छँटनी आदि ।
- शिक्षित बेरोजगारी- शिक्षित तथा प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को जब काम नही मिलता है या क्षमता के अनुसार काम नही मिलता है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते है । तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है तथा इसकी संख्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है।
शिक्षित बेरोजगारी के निम्न कारण है-
- देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण रही है। शिक्षण संस्थान डिग्रियाँ तो देते है, लेकिन रोजगार तथा पैसों से संबंधित शिक्षा का अभाव होता है।
- रोजगार तथा पैसों से संबंधित शिक्षा के अभाव के कारण लोग सफेद पोश नौकरियाँ के तरफ आकर्षित होते है और खुद रोजगार सृजन नहीं कर पाते।
- देशों में उद्योगों का विकास तथा विस्तार धीमी गति से हुआ, जिसके कारण भी शिक्षित लोगों को रोजगार नही मिल पाया।
- बढ़ती हुई जनशक्ति को कहाँ तथा कितनी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस संबंध में सरकार की नीति असफल रही है।
- देश में शिक्षा का विकास तेजी से हो रहा है परंतु उस अनुपात में रोजगार सृजन नहीं हो रहे है ।
बेरोजगारी के आधार (Basis of unemployment)
- किसी व्यक्ति को हम कब और किस आधार पर बेरोजगार कहेंगे इस संबंध में अर्थशास्त्री प्रो. राजकृष्ण ने चार कसौटियो का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है-
- समय आधार पर बेरोजगार- यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में पूर्णरोजगांरीय घंटे अथवा दिन से कम काम करता है तो उसे समय आधार पर बेरोजगार कहेंगें ।
- आय कसौटी पर बेरोजगार - यदि कोई व्यक्ति वांछित न्यूनतम स्तर से कम आय अर्जित करता है तो उसे आय कसौटी पर बेरोजगारी कहेंगें।
- इच्छुकता के आधार पर बेरोजगार- यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में लगे हुए काम से अधिक कार्य करने के लिए इच्छुक है तो उसे इच्छुकता के आधार पर बेरोजगारी कहेंगें।
- निष्पादन आधार पर बेरोजगार - यदि किसी व्यक्ति को रोजगार से निकालने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नही पड़े तो उसे निष्पादन आधार पर बेरोजगार कहेंगें।
गरीबी एवं बेरोजगारी
Objective
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







