General Competition | Science | Biology (जीव विज्ञान) | पर्यावरण प्रदूषण
पर्यावरण के अजैव घटक में होने वाला अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य तथा अन्य जीवों के लए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण कहा जाता है।
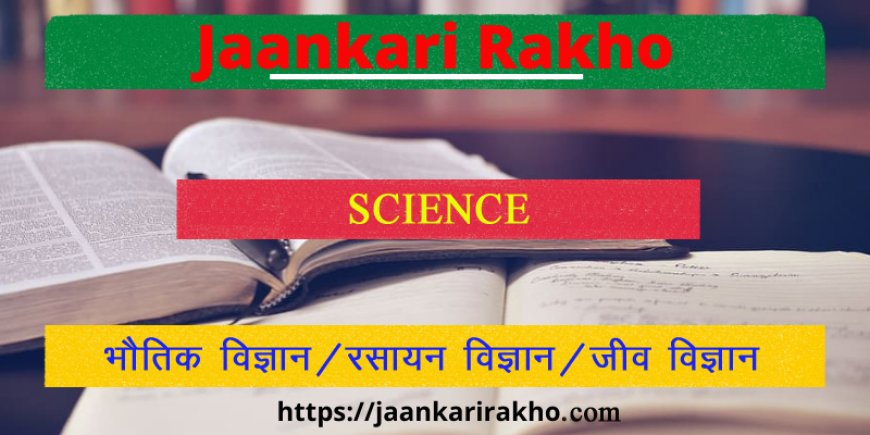
General Competition | Science | Biology (जीव विज्ञान) | पर्यावरण प्रदूषण
- पर्यावरण के अजैव घटक में होने वाला अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य तथा अन्य जीवों के लए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण कहा जाता है। ऐसे अवांछित परिवर्तन का मुख्य कारण है- मानव का अपना स्वार्थ एवं सुख । बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ती हुई औद्योगिकीकरण, बढ़ता हुआ नगरीकरण से पर्यावरण का स्वाभाविक संतुलन बदल गया है, जिससे मानव का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है।
- पर्यावरण या पारिस्थितिकी का संतुलन बिगाड़ने वाले रसायनिक या अन्य पदार्थ जो प्रदूषण के कारण बनते हैं, उसे प्रदूषक (Pollutants) कहते हैं। अपने प्रकृति के अनुसार प्रदूषकों की कई श्रेणी हैं जिसमें प्रमुख है-
- प्राथमिक (Primary) प्रदूषक- प्राथमिक प्रदूषक विभिन्न स्त्रोतों से पर्यावरण में पहुँचता हैं तथा अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं। उदाहरण:- CO, CO2, DDT आदि
- द्वितीयक (Secondary) प्रदूषक- द्वितीयक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में होनेवाली रसायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण बनते हैं। उदाहरण:- O3, NH3, PAN आदि
- जैव निम्नीकरीय (Biodegradable) प्रदूषक - ऐसे प्रदूषक पदार्थ जो पर्यावरण में उपस्थित अपघटक (Decomposers) द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। उदाहरण:- जंतुओं के मल-मूत्र, वाहत मल जल (Sewage), कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज, कपास निर्मित वस्तु, जंतु, पेड़-पौधा का मृत शरीर, लकड़ी आदि I
- जैव अनिम्नीकरणेय (Non-Biodegradable) प्रदूषक- यह प्रदूषक का जैविक अपघटन (Decompose) नहीं हो पाता है और न ही किसी अन्य प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के तुलना में यह प्रदूषक पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुँचाता है। उदाहरण: - कीटनाशी तथा पीड़कनाशी, DDT, शीशा, आर्सेनिक, ऐलुमिनियम, प्लैस्टीक, पारा, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा अन्य रसायन ।
वायु प्रदूषण (Air Pollution)
- वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाये हुए है। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% ऑर्गन, 0.03 कार्बन-डाई-ऑक्साइड तथा अन्य गैस पाये जाते हैं। वर्त्तमान समय में वायु में कई अवांछित पदार्थ (प्रदूषक) मिलकर वायु के अवयवों का संतुलन बिगाड़ दिया है जिसके कारण वायु के गुणवत्ता में निरंतर कमी आ रही है। वायु के अवयवी गैस का संतुलन बना रहना या वायु का शुद्ध रहना मनुष्य ही नहीं वरन् सभी जैविक समुदाय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है ?
- वायु प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण निम्नांकित है-
- कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रदूषक गैस है। वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसों में आधी हिस्सेदारी केवल कार्बन मोनोऑक्साइड का है। वायुमंडल में आने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत स्वचालित वाहन तथा परिवहन के अन्य साधन हैं जिनमें जैविक ईंधन का प्रयोग होता है। इसके अलावा यह गैस जैविक ईंधन के अपूर्ण दहन से, सिगरेट के धुए से, एलुमिनियम संयंत्र से वायुमंडल में आता है।
- कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है तथा सांस द्वारा अंदर जाने पर यह गैस कोई जलन भी उत्पन्न नहीं करता है। इस गैस की रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन के अपेक्षा 300 गुनी अधिक होने के कारण इसकी अल्पमात्रा भी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है जिससे श्वासवरोध (Asphyxiation) मनुष्य की मृत्यु हो जाती है
- वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से मनुष्य में शिथिलता तथा चक्कर आने लगता है। बच्चों में कम वजन का होना भी इसका एक अन्य प्रभाव है।
- कार्बन डाईऑक्साइड वायु में 0.03 प्रतिशत है। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा (0.03% ) वायु में रहना अत्यंत आवश्यक है परंतु ईंधन के जलने, कारखाने तथा यातायात के साधन बढ़ने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं जो मनुष्य एवं अन्य जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है।
- वायु में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के परिणामस्वरुप वायुमंडल के तापक्रम में वृद्धि एवं हरित घर प्रभाव, ध्रुवीय हिमखंडओं का पिघलना समुद्री जल स्तर में वृद्धि, मनुष्य में सिर दर्द, उल्टी आदि उत्पन्न होता है
- ईंधनों के दहन एवं मोटरवाहनों से न सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आते हैं बल्कि कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन जैसे- बेन्जोपायरीन, ईथीलीन, बेंजीन, एसीटिक अम्ल भी वातावरण में प्रवेश कर वायु को प्रदूषित करते हैं।
- इन हाइड्रोकार्बन की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों में समय से पहले पत्तियों एवं पुष्प कलियों में पीलापन आ जाता है एवं ये झड़ जाती हैं। मनुष्य में ऐसे हाइड्रोकार्बन फेफड़ों के कैंसर के कारण बनते हैं।
- मोटरवाहन, ,बिजली पैदा करने वाला संयंत्र, खाद्य तथा कीटनाशक उद्योग विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड निष्कासित होकर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं
- नाइट्रोजन के ऑक्साइड में मुख्यत: NO तथा NO2 है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। NO2 भूरी विषैली गैस है जिससे वायुमंडल में भूरे रंग का धुंध बनता है।
- नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण मानव रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी आती है। अम्ल वर्षा हेतु भी यह गैस उत्तरदाई है।
- बिजली पैदा करने वाले संयंत्र, उद्योग, परिष्करणशाला (Refineries), जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), सल्फर ट्राईऑक्साइड (SO3) तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आते है तथा वायु को प्रदूषित करते है।
- सल्फर के यौगिक की सांद्रता बढ़ने से मानव तथा वनस्पति दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। SO2 के प्रभाव से मुंह, गला एवं आंखों में रूखापन पैदा हो जाता है। SO2 तेज गंध वाली गैस है जो कफ पैदा करता है एवं श्वासनली को अवरुद्ध कर देता है।
- SO2 के कारण पौधों के पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, कोशिकाओं तथा उत्तकों की मृत्यु हो जाती है ।
- धुआँ में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के छोटे-छोटे कणों का बना होता है। यह धुआँ घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन, औद्योगिक संयंत्रों से वायुमंडल में मुक्त होता है।
- धुएँ में, राख, धूलकण, कालिख, हानिकारक गैस, महीन रेशे जैसे कई वायु प्रदूषक मौजूद रहते हैं जो पौधे एवं मनुष्य को विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाता है।
- धुएँ के कारण मनुष्य में दमा (Asthma), फेफड़े का कैंसर, खाती श्वसन संबंधी रोग, आंखों में जलन जैसी बीमारी होती है।
- धुएँ के प्रभाव से पौधों में पत्तियाँ काली या पीली होकर वृक्ष से झड़ जाती है।
- धुंध (Smog) दो शब्द धुआँ (Smoke ) तथा कुहरा (Fog) से मिलकर बना है। कोहरा (Fog) बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें जल के सूक्ष्मकण वायु में निलंबित रहते है। कोहरा में जब धुआँ मिलता है तो धुंध का निर्माण होता है जो शहरों के ऊपर प्राय: छाए रहते है।
- धुँध (Smog) दो प्रकार के होते हैं- सल्फ्यूरस स्मॉग तथा प्रकाश रासायनिक स्मॉग
- सल्फ्यूरस स्मॉग धुआँ, कुहरा तथा सल्फर के ऑक्साइड के मिश्रण होने से बनता है। यह स्मॉग अवकारक के तरह व्यवहार करता है तथा यह सूर्योदय के बाद ही प्रभावी होता है। सल्फ्यूरस स्मॉग को लंदन टाइप स्मॉग भी कहा जाता है।
- प्रकाश रसायनिक स्मॉग की उत्पत्ति सूर्य की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन के विघटन एवं आपसी प्रतिक्रिया के फलस्वरुप उत्पन्न होता है। यह स्मॉग ऑक्सीकारक होता है तथा इसे लॉस एंजेल्स स्मॉग भी कहते हैं।
- प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनने के विभिन्न चरण-

- प्रकाश रासायनिक स्मॉग का मुख्य अवयव ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड (NO), फार्मेल्डिहाइड, परऑक्सीएसीटल नाइट्रेट (PAN) है।
- प्रकाश रसायनिक के प्रभाव से धातु, पत्थर, रबड़, तथा रंगे हुए सतह का क्षय होता है। ओजोन तथा PAN के कारण आंखों में जलन होती है। ओजोन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड से नाक तथा गला भी प्रभावित होते हैं।
- विभिन्न प्रकार के उद्योगों से भारी धातु जैसे निकेल, शीशा, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, जिंक, बेरिलयम आदि के यौगिक वायुमंडल में निष्कासित होते रहते हैं जिनका जीवों के शरीर पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ता है।
- लैड एक विषैली धातु है । लेड धातु युक्त हवा में सांस लेने से लेड हमारे फेफड़े में एकत्र होकर लेड विषाक्तता (Lead poisoning) उत्पन्न करता है। इसके मुख्य लक्षण है- उल्टी, नींद ना आना, कब्जियत, थकावट तथा रक्त की कमी: इसके अतिरिक्त लेट से मानसिक विकृतियाँ पैदा होती है।
- पारा धातु तथा उसके यौगिक विषाक्त होते हैं। कल कारखानों के कचरे तथा खाद्यान के संरक्षण में उपयोग आने वाले कीटनाशक में पारा का यौगिक मौजूद रहता है। पारा विषाक्तता के कारण मीनामाता रोग होता है जिसमें मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है, दृष्टि और श्रवण क्षमता शिथिल पड़ जाती है, अंतत: दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है।
- कैडमियम श्वास जहर का काम करता है एवं उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों का जनक होता है।
- आजकल लोग अपने घरों में मच्छड़, चूहे, खटमल मक्खी, तिलचट्टा और दीमक जैसे कीड़ों को मारने के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। इन कीटनाशकों से में ऐल्ड्रीन, फ्लिट, गैमेक्सीन, डी.डी.टी., फिनाइल जैसे विषैले रसायन होते हैं। ये रसायन खाद्य श्रृंखला के अंग बन जाते हैं जिनका शिकार कुछ समय बाद मनुष्य स्वतः हो जाता है।
- इन विषैले रसायन के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाते हैं, लीवर तथा त्वचा रोग होने लगता है। इसके अलावे ये रासायनिक श्रृंखला का संतुलन बिगाड़ कर पारिस्थितिकी तंत्र को भी हानि पहुँचाते है।
- फ्लोराइड युक्त खनिज, मृदा, पत्थर से जहरीली गैस हाइड्रोजन फ्लोराइड उत्सर्जित होता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते रहते हैं I
- फ्लोराइड की वायु में सांद्रता बढ़ने से पत्तियों के सिरों एवं किनारों पर क्लोरोसिस तथा नेक्रोसिस उत्पन्न होता है। पशु जब ऐसे चारे खाते हैं जिनमें फ्लोरीन के यौगिक मिले तो उनमें फ्लोरोसिस हो जाता है जिससे पशु के वजन में कमी, लँगड़ापन तथा अतिसार जैसे रोग होते हैं I
- समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पाराबैगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है, परंतु वायुमंडल के कम ऊंचाई पर ओजोन का सांद्रता बढना प जीवों दोनों के लिए हानिकारक होता है।
- ओजोन की सांद्रता जब 0.01 PPM होती है तो बहुत से पौधे जैसे चीड़, सेम, टमाटर, तंबाकू आदि को क्षति पहुँचाती है। ओजोन की मात्रा बढ़ने से जीवो में श्वसन दर, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जिसके कारण DNA अणु का टूटना, मोतियाबिंद, खाँसी, आँख और छाती में जलन होने लगती है।
- एरोसॉल रसायनों का एक समूह है जो वाष्प के रूप में वायु में मुक्त होता है। वायुमंडल में । माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को भी एरोसॉल कहा जाता है। इनमें मुख्यतः फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो मिथेन आदि आते हैं। ऐरोसॉल मुख्यतः वायुयानों, एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, सुगंधियों आदि से मुक्त होते हैं।
- एरोसॉल जब वायुमंडल में कम ऊँचाई पर रहते हैं तो कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाती है परंतु जब यह समताप मंडल में फैलते हैं तो ओजोन परत को काफी हानि पहुंचाते हैं जिसके कारण फलस्वरुप पाराबैगनी किरणों की अधिक मात्रा धरती पर पहुँचकर तापमान में वृद्धि, पौधों एवं जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव तथा मनुष्यों में त्वचा कैंसर पैदा करती है।
- फ्लाई ऐस सूक्ष्म पाउडर है जिसमें मुख्यत ऐल्युमिनियम सिलीकेट, सिलिका (SiO2), कैल्शियम ऑक्साइड होते है। इसके अलावा इस पाउडर में शीशा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर जैसी धातु के सूक्ष्म कण भी होते हैं। फ्लाई ऐस का उत्सर्जन मुख्य रूप से कोयला से चलने वाले विद्युत गृह से होता है और यह दूर-दूर तक वायु में फैल जाता हैं।
- फ्लाई ऐस जीवों के श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। यह पौधे के पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर देता है।
- फ्लाई ऐस को वायुमंडल में जाने से रोकने के लिए चिमनीयों में इलेक्ट्रोस्टेटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल किया जाता है।
- 0.01 μm से 100 μm आकार के ठोस एवं द्रव कण को निलंबित कणीय पदार्थ है, जो विभिन्न औद्योगिक इकाई, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से वायुमंडल में आते हैं और वायु को प्रदूषित करते है।
- 10 μm से छोटे आकार के कण को तथा PM 10 तथा 1.5um से छोटे कण को PM 2.5 कहते है। ये सूक्ष्म कण श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़े में पहुंचकर कई प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं।
- प्राकृतिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले जहरीले गैस, परागकण, बिजाणु (Spore), धूल-कण आदि आते है।
हरित ग्रह प्रभाव और वैश्विक तापन
- हरित गृह प्रभाव को समझने से पहले हरित गृह (Green House) को जान लेना आवश्यक है। कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही विकसित होते है। उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है जिसे हरित गृह या पौधा घर कहते है। इस हरित गृह के शीशे के दीवारों द्वारा सूर्य से प्रकाश दृश्य विकिरण एवं छोटी तरंगधैर्य वाली अवरक्त विकिरण प्रवेश करती है तथा पौधा घर की सतह को तप्त कर देती है। पौधा घर की सतह तप्त होने के पश्चात मुख्यतः लंबी तरंगधैर्य वाली अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होती है जिन्हें शीशे की दीवारें परावर्तित कर देती और पौधा घर गर्म बना रहता है। पौधा घर (Green House) का गर्म वातावरण हरे पौधों के विकास के लिए अनुकूल होता है।
- वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हरितगृह जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। सूर्य के किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो दृश्य विकिरण तथा छोटे तरंगधैर्य वाली अवरक्त विकिरण हवा से होती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुँचकर उसे गर्म करती है। पृथ्वी के गर्म सतह से पुनः लंबी तरंगधैर्य वाली अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होती है जिसे वायुमंडल में स्थित CO2 पृथ्वी के सतह की ओर ही परिवर्तित कर देती है जिससे पृथ्वी गर्म हो जाती है।
- पृथ्वी को गर्म करने में जिस गैस का योगदान है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे भूमंडलीय तापन (Global Warming) कहते हैं।
- वैश्विक तापन (Global Warming) में सर्वाधिक योगदान देने वाला ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाईऑक्साइड है। इसके बाद प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) एवं क्लोरोफ्लो कार्बन (CFC) है।
- ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैस का प्रतिशत योगदान-
कार्बन डाईऑक्साइड - 60%मीथेन - 20%नाइट्रस ऑक्साइड - 6%क्लोरोफ्लोरोकार्बन - 14%
- ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होनेवाली क्रिया है जिससे धरती का तापमान एक निश्चित स्तर पर बना रहता है। अगर यह क्रिया धरती पर न हो तो इसके सतह का औसत तापमान 15°C के बजाय - 18°C हो जाएगा। परंतु ग्रीन हाउस गैस की बढ़ती सांद्रता धरती के तापमान को आवश्यकता से अधिक बढ़ा रहा है। ऐसा अनुमान है कि पिछले सौ वर्षों से पृथ्वी का ताप 05°C बढ़ा है। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि 2030 तक पृथ्वी के ताप में 2°C की वृद्धि हो सकती है।
- ग्रीन हाउस गैस के कारण उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है-
- जलवायु में अवांछनीय परिवर्तन जिनसे पूरा जैविक समुदाय प्रभावित होता है।
- पृथ्वी का ताप बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ या बर्फ के पहाड़ पिघलने लगेंगे। अतः समुद्र स्तर में वृद्धि होगी जिसके कारण तटवर्ती क्षेत्र जल में डूब जाएँगे ।
- अत्यधिक गर्मी से कृषि उत्पादन घट सकता है।
- हरित गृह प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं।
- जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग होना चाहिए ।
- वृक्षारोपण में वृद्धि करनी चाहिए तथा वनोन्मूलन में कमी लानी चाहिए।
- ऊर्जा क्षमता में सुधार लानी चाहिए।
- जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठानी चाहिए।
ओजोन अपक्षय (Ozone Depletion)
- सूर्य के किरणों में उपलब्ध पराबैंगनी (Ultraviolet) विकिरण जीवों के लिए हानिकर है। ये पराबैंगनी विकिरण मनुष्य में विभिन्न प्रकार के विमारियों जैसे- त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि को जन्म देती है। इस हानिकर पराबैंगनी से पृथ्वी के जीवों की सुरक्षा ओजोन परत करता है। ओजोन परत समताप मंडल में 16 km से 50km ऊँचाई तक के क्षेत्र में व्याप्त है। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचने से रोकती है।
- ओजोन का निर्माण समताप मंडल में ही ऑक्सीजन के अणुओं पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से होता है तथा ओजोन का निर्माण के साथ-साथ क्षय भी होते रहता है। समताप मंडल में ओजोन के निर्माण एवं क्षय के बीच एक संतुलन बना रहना आवश्यक है।

- मानव के आधुनिक जीवनशैली में कुछ रसायन जैसे - क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CCl2F2), या फ्रिऑन, मिथाइल क्लोराइड (CH3.Cl) समताप मंडल में पहुँचकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर उन्हें ऑक्सीजन के अणुओं में तोड़ देता है फलस्वरूप दिनोंदिन ओजोन परत अवक्षय हो रहा है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) के क्लोरीन के एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को विखंडित करने की क्षमता रखता है।
- ओजोन अपक्षय का सर्वाधिक असर अंटार्कटिका (दक्षिणी ध्रुव) क्षेत्र में खासकर देखा गया है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का इतना अधिक क्षय हो गया है उसे ओजोन छिद्र (Ozone hole) की संज्ञा दी जाती है।
- ओजोन छिद्र वास्तव में कोई छिद्र नहीं है बल्कि यह अंटार्कटिका के ऊपर के ओजोन की बहुत ही पतली परत है। ओजोन का मापन डॉक्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा की जाती है। एक डॉबसन यूनिट शुद्ध ओजोन की 0.01 mm मोटाई के बराबर होती है। वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण 300 डॉत्रसन यूनिट होनी चाहिए लेकिन जब ओजोन का सांद्रण 220 डॉवसन यूनिट से कम होता है तो उसे ओजोन छिद्र कहा जाता है।
- सर्वप्रथम 1974 में शेरवुड रॉलैण्ड तथा मारियो मोलिना ने यह पता लगाया की क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) के कारण समताप मंडल के ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। 1985 में जोसेफ फरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश टीम यह पता लगाया की अंटार्कटिका के ऊपर के समताप मंडल के ओजोन परत का वृहद स्तर पर क्षय हुआ है। जोसेफ फरमन के प्रमाणों के अनुसार बसंत ऋतु (सितंबर-नवंबर) में अंटार्कटिका के ऊपर के ओजोन परत में 40 प्रतिशत क्षय हो जाता है।
- ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण CFC गैस है। CFC का व्यापक उपयोग एयर कंडीशनो, रेफ्रिजरेटर, शीतलक, जेट इंजन, अग्निशामक उपकरण, गद्देदार फोम आदि में होता है। ओजोन की इस क्षति को कम करने के लिए विश्व के लगभग देश CFC का उपयोग बंद कर दिया है तथा इसकी जगह पर क्लोरीन सहित अपेक्षाकृत महँगे फ्लोरोकार्बन विकसित किए जा रहे हैं।
- गौरतलब है कि ओजोन का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा क्षोभ मंडल में व्याप्त है और ओजोन का यह हिस्सा स्मॉग व वायु प्रदूषण का निर्माण कर मानव स्वास्थ्य समेत समस्त जीवों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। क्षोभ मंडल स्थित ओजोन के इस 10 प्रतिशत हिस्से को बुरा ओजोन कहते है।
- ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ जिसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी कहते हैं क्योंकि यह कन्वेंशन (Convention) वैश्विक ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक फ्रेमवर्क का काम किया। परंतु वियना कन्वेंशन में उत्तरदायी CFC गैस के उपयोग में कमी लाने हेतु कोई बाध्यकारी नियम नहीं था।
- ओजोन अवक्षय के ओजोन अवक्षय को रोकने हेतु 1987 में मॉन्ट्रियाल (कनाडा) में एक अंतराष्ट्रीय सहमति बनी जिसे मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह संधि 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुई। मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत विकसित देशों को 2000 तक तथा विकासशील देशों को 2010 तक CFC का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है।
- भारत में ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1991 में वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया तथा मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संबंध में 1992 में हस्ताक्षर किया।
अम्लीय वर्षा (Acid Rain)
- औद्योगिक इकाई, बिजलीघर, स्वचालित वाहन तथा जैविक ईंधन के दहन से वातावरण में लगातार सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO2) मुक्त होते हैं। वर्षा के समय ये ऑक्साइड H2SO4 तथा HNO3 में परिवर्तित हो जाते हैं।

- HNO3 तथा H2SO4 जैसे अम्ल जब वर्षा जल के साथ धरती पर आते है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल (H2SO4) की मात्रा नाइट्रिक अम्ल (HNO3) की अपेक्षा अधिक होती है।
- अम्ल वर्षा के कारण निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं-
- अम्ल वर्षा से बड़ी-बड़ी इमारतों तथा ऐतिहासिक भवनों को काफी क्षति पहुंचती है। वर्षा जल के अम्ल संगमरमर या चूना पत्थर से क्रिया करके उसे संक्षारित कर देता है। जिसके कारण मकान और इमारते कमजोर हो जाती है।
- अम्ल वर्षा के कारण लोहे से बना उपकरण भी संक्षारित होने लगता है।
- अम्ल वर्षा नदियों, झीलों, तालाबों आदि को भी अम्ल बना देता है जिसके कारण मछली तथा अन्य जलीय जीव की आबादी घटने लगती है।
- अम्लीय वर्षा का जल मिट्टी के उर्वरता को नष्ट कर उसे अनुपजाऊ बना देता है। अम्लीय वर्षा के कारण पेड़-पौधों की पत्तियाँ नष्ट होने लगता है तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।
वायु प्रदूषण
- वायु प्रदूषण का नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं-
1. हानि रहित गैसों से प्रदूषक का अलग करना :
- इसके अंतर्गत जो विधि अपनाई जाती है वह प्रदूषण के कारण आकार पर निर्भर करता है ।
- 50 μm से बड़े मापी वाले प्रदूषक कणों का अलग करने हेतु गुरुत्व निःसादी टंकी (Gravity Settling Chamber) अथवा फैब्रिक फिल्टर का उपयोग किया जाता है।
- 50 μm से छोटे प्रदूषक कणों की अलग करने हेतु साइक्लोन संग्राहक (Cyclone Collector) तथा स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र (Electrostatic Precipitator) का उपयोग किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में प्रदूषक को हवा में ऑक्सीकृत करवा दिया जाता है। मोटर वाहनों में इसके लिए कैटेलिक कनवर्टर का उपयोग किया जाता है। मोटर वाहनों से निकलने वाला हानिकारक गैस एवं हाइड्रोकार्बन जब कैलिटिक कनवर्टर से गुजरते हैं तो उनका पूर्ण दहन हो जाता है और इसके बाद उत्सर्जित गैस हाइड्रोकार्बन के तुलना में कम हानिकारक होते हैं।
- कैटेलिटिक कन्वर्टर ऐसे इंजन में अच्छी तरह काम करते हैं जिसमें शीशा (lead) मुक्त पेट्रोल प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल में शीशा रहने से कैटेलिटिक कन्वर्टर में मौजूद उत्प्रेरक कुछ समय बाद कार्य करना बंद कर देते है।
- शीशा रहित एवं सल्फर रहित पेट्रोल के उपयोग के साथ-साथ इंजन से कम से कम धुआँ उत्सर्जित हो इसका उपाय करना चाहिए।
- उद्योगों और औद्योगिक प्रतिष्ठान परिष्करणशाला को आबादी से दूर खोला जाना चाहिए।
- उद्योगों की चिमनी हवा में काफी ऊपर हो एवं इसमें फिल्टर लगी होनी चाहिए ।
- डीजल इंजन का कम से कम प्रयोग होना चाहिए।
- वनारोपण करनी चाहिए तथा वन की कटाई का पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए।
- जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि यह एक मुख्य कारण है जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई है।
- इस सूचकांक की शुरुआत 6 अप्रैल 2015 को कुल 10 शहर (वर्तमान में 19 ) में रियल टाइम आधार पर वायु गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु की गई।
- इस सूचकांक में कुल 8 प्रदूषक कारी तत्व पीएम 10, पीएम 2.5, NO2, CO, SO2, NH3, O3 तथा Pb (लेड) को ध्यान में रखकर वायु की उच्च गुणवत्ता सूचकांक बनाए गए हैं। ये 6 गुणवत्ता सूचकांक है- अच्छी (0-50), संतोषजनक (51-100), सामान्य प्रदूषित ( 101-200) खराब (201-300), बहुत खराब (301-400) और गंभीर (401-500)।
- प्रत्येक शहर में प्रतिदिन 4 pm में सूचक का प्रकाशन किया जाता है।
- वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लाने हेतु यह अधिनियम संसद ने 29 मार्च 1981 को पारित किया तथा 16 मई 1981 को यह पूरे देश में लागू हुआ। अधिनियम में मुख्य रूप से मोटरगाड़ी तथा औद्योगिक इकाई से निकलने वाले धुँए एवं गंदगी के स्थान निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। आगे चलकर 1987 में इसी अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया।
- इस अधिनियम को लागू कराने का अधिकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। यह अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न केवल औद्योगिक इकाइयों की निगरानी की शक्ति देता है बल्कि प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का भी अधिकार प्रदान करता है ।
- इस बोर्ड की स्थापना जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। 1981 में इसे वायु प्रदूषण से संबंधित कार्य भी सौंप दिया गया। यह बोर्ड जिम्मेदार है- प्रदूषण स्तर का मापन, वर्गीकरण तथा उसके नियंत्रण का उपाय बताना तथा जल, वायु, ध्वनि के गुणवत्ता को तय करना । इसके अलावे यह बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है।
जल प्रदूषण (Water Pollution)
- जीवन के लिए जल अनिवार्य है साथ ही यह कृषि उद्योगों के लिए भी परम आवश्यक है। अलवण जल का वितरण असामान्य है तथा इसकी मांग दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में अगर जल प्रदूषित हो जाए तो यह एक गंभीर संकट पैदा करेगा।
- जब जल की भौतिक रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाए जिससे वह जीवों के लिए हानिकारक तथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो जाता है तो यह जल प्रदूषण कहलाता है।
- जल प्रदूषण के स्रोत दो प्रकार के होते हैं बिंदु स्रोत तथा (Point Sources) और अबिंदु स्रोत (Non-point Sources)।
- जल स्रोतों के निकट स्थित बिजलीघर, भूमिगत कोयला खदान, तेलकुआँ आदि बिंदु स्रोत के उदाहरण हैं। यह स्रोत प्रदूषक को सीधे ही जल में प्रवाहित कर देते हैं।
- जल प्रदूषण के अबिंदु स्त्रोत विभिन्न स्थानों पर फैले होते है। इसके अंतर्गत खेत, बगीचा, निर्माण स्थल, जल भराव, सड़क, गलियों से बहने वाला जल आते है।
- जल प्रदूषण के कारण :
-
- जल प्रदूषण के अनेक कारण है जिसमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है-
-
- घरेलू अपमार्जक
- लोग अपने घरों में प्रतिदिन बर्तन मांजने, कपड़ा धोने में अपमार्जक (Detergents) का प्रयोग करते है। इन अपमार्जक में फॉस्फेट, नाइट्रेट, एल्किल, बेंजीन, सल्फोनेट हानिकारक अम्ल होते है जो अंततः नदी तालाबों के जल में पहुंचकर उसे प्रदूषित करता है।
- अकार्बनिक रसायन जैसे- फॉस्फेट न नाइट्रेट का जलाशय में एकत्र होना सुपोषण (Eutrophication) कहलाता है। सुपोषण के कारण शैवालों में वृद्धि होती है और यह जलाशय के सतह पर फैल जाते है। इन शैवालों से विषैले रसायन उत्पन्न होते है जो जलाशय के अन्य जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। सुपोषण के कारण तेजी से होने वाली शैवालों की वृद्धि को जल-प्रस्फुटन (Water bloom) कहते है ।
- वाहित मल जल (Sewage)
- आजकल सभी बड़े शहरों की गंदगी, मानव अपशिष्ट नालों के द्वारा नदियों में गिरा दिया जाता है। इतने व्यापक पैमाने पर अपशिष्ट को नदियों में डालने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा BOD (Biochemical Oxygen Demand) बढ़ जाता है जिसके कारण जलीय जीव खासकर मछली मरने लगता है।
- औद्योगिक अपशिष्ट
- नदियों किनारे बड़े-बड़े व्यावसायिक नगर के कल-कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट सीधे नदियों में ही प्रभावित कर दिया जाता है। इन अपशिष्टों में लोहा, फेनॉल, क्लोरीन, तेल, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया तथा अन्य कई भारी धातु होते है जो नदियों के पानी का न सिर्फ स्वाद खराब करता है बल्कि उनसे तीव्र गंध आने लगती है।
- उर्वरक तथा पीड़कनाशी
- बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उपज अधिक-से-अधिक प्राप्त करने के लिए आज रसायनिक उर्वरक तथा पीड़कनाशी (Pesticides) का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। उर्वरक तथा पीड़कनाशी में उपस्थित खतरनाक रसायन, वर्षा जल के नदी तथा अन्य जलाशय में पहुँचकर उसे प्रदूषित कर देती है जो न सिर्फ जलीय जीवों के लिए बल्कि मनुष्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है।
- पीड़कनाशी में DDT जैसी खतरनाक रसायन पौधों के द्वारा खाद्य श्रृंखला के हर पोषी स्तर में पहुँचते है। इनकी मात्रा पहले स्तर से अगले पोषी स्तर में क्रमशः बढ़ती जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते है ।
- तापीय जल प्रदूषण
- औद्योगिक इकाई, बिजली संयंत्र, नाभिकीय रिएक्टर में इंजनों को ठंडा रखने हेतु जल का प्रयोग किया जाता है और उपयोग पश्चात् गर्म जल को ही जल स्रोतों में डाल दिया जाता है जिससे पानी का ताप बढ़ जाता है। अचानक ताप वृद्धि होने जलीय जीव एवं वनस्पतियाँ मरने लगता है।
- भारी धातुएँ
- औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट में कई भारी धातु जैसे- पारा, लेड, कॉपर, जिंक, कैडमियम आदि पाए जाते है। यह अपशिष्ट पदार्थ जब जल स्रोतों में मिलते है तो जल ना तो मनुष्य के लिए उपयोगी रहता और ना ही जलीय जीवों के लिए। भारी धातुओं का जल में सांद्रता जब लगातार बढ़ती है तो ऐसे जल का उपयोग करके कई तरह के रोग होते है ।
- पेयजल में शीशा का अधिकतम स्वीकार क्षमता 50 PPM निर्धारित किया गया है। इससे अधिक सांद्रता से शीशा विषाक्तता होती है जिससे मानव के किडनी, यकृत तथा प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है।
- पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा 50 PPM निर्धारित की गई है लेकिन 20 PPM से अधिक नाइट्रेट युक्त जल ही बच्चों के लिए हानिकारक होते है क्योंकि इससे बच्चों में मेटाहीमोग्लोबिनीमिया या बच्चों वाला नीला रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चों की त्वचा हल्के नीले रंग की हो जाती है।
- फ्लोराइड की I PPM मात्रा ही दाँतों का इनैमिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफी है। फ्लोराइड की सांद्रता 2 PPM हो जाने पर दाँत बदरंग दिखने लगते हैं और अगर फ्लोराइड की मात्रा 10 PPM से अधिक हो जाए तो दाँत तथा हड्डी से संबंधित रोग फ्लोरीसिस हो जाता है।
- जल में जब सल्फेट की सांद्रता 500 PPM पहुँच जाए तो ऐसे जल में कड़वापन आ जाता है।
- पेयजल में धातु का WHO द्वारा प्रस्तावित अधिकतम सांद्रता-
Fe - 10.2 PPMMn - 0.05 PPMcd - 0.005 PMCu - 3.0 PPMZn - 5.0 PPM
- पीने युक्त जल में निम्नलिखित तीन गुणों का होना अनिवार्य है -
- जल पारदर्शी, रंगहीन तथा गंधहीन होना चाहिए।
- जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुला हुआ होना चाहिए।
- जल हानिकारक रसायन एवं जीवाणुओं से मुक्त होना चाहिए।
- जलीय जीवों के संदर्भ में जल में घुले ऑक्सीजन (Dissolved Oxyen ) की मात्रा 8.0mg/1 से कम हो जाती है तो ऐसे जल में संदूषित कहा जाता है। जब यह मात्रा 4 mg / l से कम हो जाता है तो इसे अत्यधि क प्रदूषित कहा जाता है।
- घरेलू अपमार्जक
- जल प्रदूषण को रोकने के उपाय
- जल प्रदूषण के कई कमाण है लेकिन मुख्यतः घरेलू एवं औगोलिक पारित मल जल के कारण ही जल प्रदूषित होता है। अगर घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट को उपचार करने के बाद जल स्रोतों में प्रवाहित न करें तो काफी हद तक जल प्रदूषण को रोका जा सकता है।
- घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट या वाहित मल जल का उपचार तीन चरणों में किया जाता है-
- प्रथम चरण : इस चरण में अपशिष्ट से बड़े तथा लंबे कणों को अलग किया जाता है। इसके लिए अवसादन (Sedmentation), प्लवन (Floatation ), छानन (Screening ) आदि विधि प्रयोग में लाई जाती है।
- द्वितीय चरण: इस चरण में प्रदूषित जल को प्राथमिक उपचार ( प्रथम चरण) के बाद एक ऑक्सीकरण ताल (Oxidation Pond) में जमा किया जाता है जहाँ जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन करवाया जाता है। द्वितीय चरण में जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषक नष्ट हो जाते है और अंत में क्लोरीन का उपयोग जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है।
- तृतीय चरण: प्रदूषित जल का द्वितीयक (द्वितीय उपचार) के बाद जल फास्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य अकार्बनिक पदार्थ मौजूद रह जाते है। इन्हें दूर करने हेतु रिवर्स परासरण, ऑक्सीकरण जैसी रासायनिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम तथा द्वितीय चरण की अपेक्षा यह चरण काफी खर्चीला होता है। अतः जल को प्रदूषणरहित बनाने हेतु प्राय: दो चरण का ही उपयोग किया जाता है।
- जल प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है-
- गंगा एक्शन प्लान है : गंगा नदी बेसिन में भारत की 35 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। लेकिन यह नदी अपने अफवाह के आधे भाग में प्रदूषित हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी जिसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को प्रदूषण से पूर्णत: मुक्त करना । यह प्लान 1986 से 1993 तक चला I
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना : केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया तथा गंगा नदी से संबंधित सभी कार्य योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के अधीन कर दिया गया। इस प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना चलाया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 19 राज्यों में फैले 121 शहरों की 40 नदियों के प्रदूषित भाग को शामिल किया गया है।
- नमामि गंगे कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण को खत्म करना है। केंद्र सरकार द्वारा 2014 में 20,000 करोड़ राशि आवंटित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
- जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 : यह अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य स्तर पर प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड जल प्रदूषषकों का मानक तय करता है, प्रदूषण से संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करता है तथा सरकार को प्रदूषण रोकने के उपाय के संबंध में सलाह देता है।
विकिरण प्रदूषण (Pollution due to Radiations)
- रेडियोसक्रिय पदार्थ तथा इससे निकलने वाली अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें (विकिरण) जब वायुमंडल, जल या अन्य अजैव घटकों में पहुँचते हैं तो इसे विकिरण प्रदूषण कहा जाता है। विकिरण प्रदूषण का स्वरूप एवं प्रभाव अन्य प्रदूषण से बिल्कुल भिन्न है। विकिरण प्रदूषण के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दोनों कारण है। विकिरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है-
- विकिरण प्रदूषण में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचे अंतरिक्ष किरणों (Cosmic rays) का भी है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर यूरेनियम - 235, रेडियम- 224, थोरियम-232 जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते है जिनमें लगातार विकिरण निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते है।
- नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होने वाला नाभिकीय ईंधन भी विकिरण प्रदूषण हेतु जिम्मेवार है। नाभिकीय रिएक्टर के अपशिष्ट जहाँ पर भी फेंका जाता है वहाँ लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है।
- बहुत से रेडियो एक्टिव पदार्थ वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक्स-रे, सीटी स्कैन तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह भी विकिरण प्रदूषण हेतु जिम्मेवार है।
- वर्तमान समय विश्व के लगभग सभी समक्ष अस्त्रों का परीक्षण कर रहे है। यह परीक्षण अधिकांशत समुद्र में होता है जिसके फलस्वरूप समुद्री जल में स्ट्राशियम - 90, सीजिएम - 137, कार्बन - 14, ट्रीटियम जैसे घातक रासायनिक पदार्थों की मात्रा बहुत बढ़ गई है।
- विकिरण प्रदूषण के प्रभाव
- अपशिष्ट के रूप में फेंके गए रेडियो सक्रिय पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर स्थलीय एवं जलीय जंतु में पहुँच जाते हैं और अनेक प्रकार के बीमारी फैलाते है। अगर यह पदार्थ के उच्च मात्रा जीवों में पहुँच जाए तो जीव की तुरंत मृत्यु हो जाती है।
- अधिक समय तक बार-बार रेडियो सक्रिय पदार्थों के विकिरण से प्रभावित ने पर रक्त कैंसर (ल्यूकेमिया) हो जाता हैं।
- विकिरणों के प्रभाव से जीवों में उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि हो जाती है जिससे जीवों के जिन एवं गुणसूत्रों में परिवर्तन आ जाता है जिससे शरीर में विकृति तथा असामान्य विकास जैसे लक्षण आ जाते है।
- विकिरण प्रदूषण के कारण शारीरिक दुर्बलता, जीवन अवधि में कमी आ जाती है।
- पाराचैंगनी विकिरण में अधिक समय तक रहने पर त्वचा संबंधी रोग पिग्मेण्टोसम होता है।
- रेडियोधर्मी विकिरण (अल्फा, बीटा, गामा) से दृष्टि दोष, फेफड़ों में ट्यूमर तथा उत्तक का क्षय होता है।
- लगातार हानिकारक विकिरण वायुमंडल में अगर पहुँचते है तो इससे ओजोन परत का भी क्षरण होता है।
- विकिरण प्रदूषण का नियंत्रण
- नाभिकीय रिएक्टर, ऊर्जा घर, अनुसंधानशालाओं एवं नाभिकीय ईंधन परिवहन में रेडियो सक्रिय तत्व का रिसाव नहीं होना चाहिए।
- उन जगहों पर विकिरण प्रदूषण की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ इसका खतरा बना हुआ है।
- रेडियोधर्मी अपशिष्ट को स्टील एवं कंक्रीट से बने पात्रों में भरकर सील करना चाहिए। इसके बाद इसे पृथ्वी के काफी भीतर गाड़ देनी चाहिए अथवा समुद्र में कम से कम 100 फैदम की गहराई में छोड़ना चाहिए ।
- नाभिकीय संयंत्रों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा एवं दुर्घटना होने पर समुचित सहायता का इंतजाम पहले से होना चाहिए।
ध्वनि प्रदूषण (Sound Pollution)
- अनचाहे ऊँची आवाज को सामान्यतः शोर कहा जाता है। शोर के होने वाले हानिकारक प्रभाव को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है- यातायात के विभिन्न साधन, लाउडस्पीकर, टेलीविजन, होम थिएटर तथा आर्केस्ट्रा साउंड, कारखानों का मशीन, कई आधुनिक घरेलू उपकरण जैसे- मिक्सी, कूलर, वैक्यूम क्लीनर आदि भी ध्वनि प्रदूषण पैदा करते है ।
- भारत सरकार ने वर्ष 1987 में "वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981" में संशोधन कर वायु प्रदूषण में ही ध्वनि प्रदूषण को जोड़ दिया है।
- ध्वनि का इकाई डेसीबल है। साधारणतया 25-30 डेसीबल की ध्वनि सहन की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर 45 डेसीबल निर्धारित किया है। 80 डेसीबल की ध्वनि पर मनुष्य बेचौनी महसूस करने लगता है तथा 130 - 140 डेसीबल पर पीड़ा तथा सिर दर्द होने लगता है।
- भारत में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक निम्नलिखित है-
| क्षेत्र | दिन का समय (6 AM - 10 PM) | रात का समय (10 PM - 6 AM) |
| 1. औद्योगिक क्षेत्र | 75 डेसीबल | 70 डेसीबल |
| 2. वाणिज्यीक क्षेत्र | 65 डेसीबल | 55 डेसीबल |
| 3. आवासीय क्षेत्र | 55 डेसीबल | 45 डेसीबल |
| 4. शांत क्षेत्र (अस्पताल, शिक्षा, न्यायालय) | 50 डेसीबल | 40 डेसीबल |
- ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव निम्न है-
- लंबे समय तक तीव्र ध्वनि के प्रभाव से मनुष्य के संवेदना तथा भावनाएं छिन्न होने लगती है ।
- अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण ( 150 डेसीबल) मस्तिष्क पर इसका प्रभाव डालता है कि कभी-कभी मनुष्य पागल हो जाता है।
- बहुत शोरगुलवाले वातावरण में रहने से मनुष्य में बहरापन की समस्या आ जाती है।
- तेज ध्वनि से शरीर में हमेशा दर्द रहता है, रक्तदाब बढ़ जाता है तथा हृदय की कार्यप्रणाली अवरुद्ध होने लगता है।
- अत्यधिक तीव्र ध्वनि से मानव स्वभाव में उत्तेजना तथा क्रोध पैदा हो जाता है।
- तेज ध्वनि के कारण मानव के एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है।
- तेज आवाज से नींद में बाधा उत्पन्न होती है, आंखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती है तथा किडनी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ध्वनि प्रदूषण गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रतिकूल असर डालता है उनमें तंत्रिकीय दोष होने की संभावना बनी रहती है।
- ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं-
- ऑटोमोबाइल तथा मशीनों का उचित रख-रखाव पर ध्यान देना चाहिए उसमें समय-समय पर ग्रीस एवं तेल का उपयोग करना चाहिए।
- औद्योगिक इकाई को आबादी से दूर स्थापित की जानी चाहिए।
- हवाई जहाजों एवं यातायात के साधनों में ऐसी इंजन का प्रयोग होना चाहिए जो कम ध्वनि पैदा करता हो।
- पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है कि वह त्योहारों और उत्सवों पर गलियों में बजने वाले संगीत की तीव्रता के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। अतः लाटडस्पीकरों एवं तेज आवाज पैदा करने वाले साउंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बने कानून का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए।
- ध्वनि प्रदूषण को अपराध की श्रेणी में मानते हुए इसके नियंत्रण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 268 तथा धारा 290 का प्रयोग किया जा सकता है।
ठोस अपशिष्ट का निपटारा (Treatment of Solid waste)
- ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कूड़ा करकट भी कहा जाता है। ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत घर, पशुशाला के अपशिष्ट, अस्पतालों के अपशिष्ट, प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि आते है। अगर इन टोस अपशिष्ट को ठीक तरह से निपटारा नहीं किया गया तो इससे मृदा, वायु, जल सभी प्रदूषित हो जाते है। जिससे अंत: मानव ही प्रभावित होते है। ठोस अपशिष्ट के निपटारे हेतु प्रमुख विधि निम्नलिखित है-
- सैनिटरी लैंडफिल्स
- इस विधि से में ठोस अपशिष्ट को गड्ढा में डाला जाता है एवं प्रतिदिन कुछ मिट्टी से ढक दिया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल टोस अ अपशिष्ट के निपटारे हेतु एक सस्ता तथा आसान विधि है परंतु इससे समस्या का समुचित निदान संभव नहीं है क्योंकि बड़े शहरों में अपशिष्टओं की मात्रा इतनी अधिक होती है कि गई तुरंत भर जाते है।
- सैनिटरी लैंडफिल्स पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है क्योंकि अपशिष्ट में उपस्थित रासायनिक पदार्थ रिसकर भौम जल को प्रदूषित कर देते हैं।
- भस्मीकरण (Incineration)
- यह विधि थोड़ी महंगी विधि है इसमें ठोस अपशिष्ट को 1000°C पर जलाया जाता है जिससे टोस अपशिष्ट राख, गैस व ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। खतरनाक कचड़ा तथा अस्पतालों के अपशिष्ट को प्राय: इसी विधि द्वारा निपटाया जाता है।
- जैविक पुनर्प्रसंस्करण (Biological Reprocessing)
- जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट निपटारे हेतु यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट को एक कंटेनर में तब तक रखा जाता है जब तक कि वह अपघटित ना हो जाए। अपघटित होने के बाद अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते है जिससे जैविक खाद्य का भी निर्माण किया जा सकता है।
- समुद्री डंपिंग
- नाभिकीय कचड़े, खतरनाक रसायन जैसे ठोस अपशिष्ट को इस विधि से निपटाया जाता है। अपशिष्ट को सुरक्षित पैकेट में अच्छी तरह से भरकर सील कर दिया जाता है और समुंद्र में कम से कम 1000 फैदम की गहराई में छोड़ दिया जाता है।
- ठोस अपशिष्ट को नियंत्रित करने में 3R (Reduce, Reuse, Recycle) भी एक बेहतर विकल्प है। मानव को कम-से-कम या आवश्यकता अनुसार ही पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। पुर्नचक्रण (Recycle) के माध्यम से पदार्थों को नए उत्पाद में बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा सामानों को फेंकने के बजाय इन का पुन: उपयोग करना चाहिए।
- प्लाज्मा आर्क
- यह एक महंगी प्रौद्योगिकी है जिसका इस्तेमाल खतरनाक एवं रेडियोसक्रिय वाले कचड़े के निपटान हेतु किया जाता है। इस विधि में कचड़ा पूरी तरह नष्ट हो जाता है तथा प्रदूषण भी बहुत कम हो जाता है। इस विधि में नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस नहीं बनते है।
- सैनिटरी लैंडफिल्स
अभ्यास प्रश्न
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







