General Competition | Science | Physics (भौतिक विज्ञान) | प्रकाश
प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हमारी आँख कोई महत्व नहीं है ।
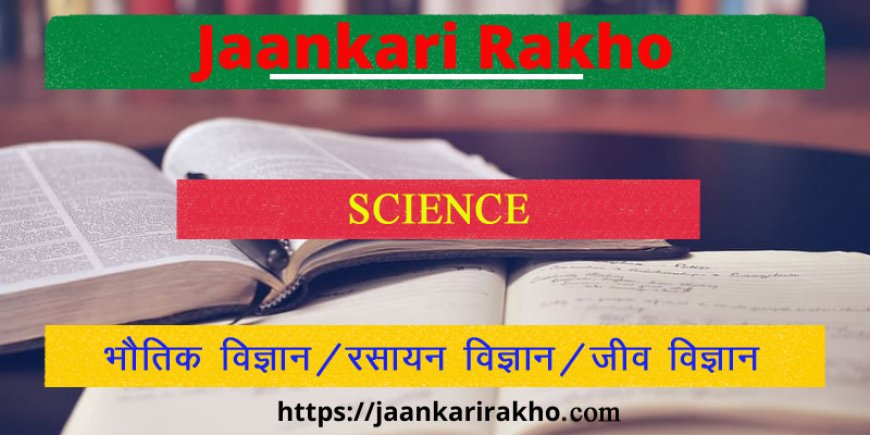
General Competition | Science | Physics (भौतिक विज्ञान) | प्रकाश
- प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हमारी आँख कोई महत्व नहीं है ।
- प्रकाश अयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश ऊर्जा को, ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- श्वेत प्रकाश (सूर्य से आनेवाला प्रकाश) विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश तरंगों का मिश्रण है। इन प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्ध्य . 4 × 10-7 m से 8 × 10-7 m तक होता है।
- प्रकाश का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग शून्य (निर्वात) में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 108 m/s होता है। अन्य सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग निर्वात से कम होता है। हवा में प्रकाश का वेग, निर्वात में, प्रकाश के वेग के बराबर ही माना जाता है।
- प्रकाश तरंग को प्रारंभ में अतिसूक्ष्म कण माना गया बाद में इसे तरंग (अनुप्रस्थ) माना गया । आधुनिक क्वाटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों स्वभाव रखता है। किसी माध्यम से गमण करते व्यक्त प्रकाश तरंग स्वभाव को दर्शाता है तथा पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया (interaction) करते समय, कण स्वभाव को दर्शाता है ।
- किरण (Ray)– प्रकाश स्त्रोत से निकलकर प्रकाश सरल रेखीय मार्ग से होकर सभी दिशाओं में गमण करता है। किसी भी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं । करण को तीर का चिन्ह देकर दर्शाया जाता है ।

- प्रकाश पुंज (Beam of light)- किसी निश्चित दिशा में जा रहे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाशपुंज तीन प्रकार के होते हैं ।
- समांतर किरण - पुंज (Parallel Beam)- यदि प्रकाश पुंज की किरणें परस्पर एक-दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर प्रकाशपुंज कहा जाता है। बहुत दूर के प्रकश स्त्रोत (सूर्य, तारा इत्यादि) से आ रही प्रकाशपुंज को समांतर प्रकाश-पुंज माना जाता है।

- संसृत (अभिसारी) किरण पुंज (Convergent Beam ) - जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिन्दु पर मिलती है तब इसे संसृत या अभिसारी किरण - पुंज कहते हैं।

- अपस्तत (अपसारी) किरण पुंज (Divergent Beam) - यदि प्रकाश पुंज की किरणें किसी बिन्दु से निकलकर बढ़ने के साथ फैलती जाती है तब इसे अपस्तत या अपसारी किरण पुंज कहते हैं।

- समांतर किरण - पुंज (Parallel Beam)- यदि प्रकाश पुंज की किरणें परस्पर एक-दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर प्रकाशपुंज कहा जाता है। बहुत दूर के प्रकश स्त्रोत (सूर्य, तारा इत्यादि) से आ रही प्रकाशपुंज को समांतर प्रकाश-पुंज माना जाता है।
- पारदर्शी पदार्थ (Transpoarent Matter)- वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी कहलाता है।
उदा० - काँच, पानी, हवा आदि ।
- पारभासी पदार्थ (Translucent)- जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का बहुत कम भाग ही आर-पार जा सके पारभासी पदार्थ कहलाता है।
उदा० - घिसा हुआ काँच, तेल लगा कागज, रक्त, दूध आदि ।
- अपारदर्शी पदार्थ (Opaque Matter)- जिनसे होकर प्रकाश आर-पार नहीं जा सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है ।
उदा०- लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा आदि ।NOTE:- हवा तथा निर्वात को छोड़कर, अन्य सभी माध्यम का मोटाई ही निर्धारित करता है कि वह पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी होगा। जैसे - काँच का पतला भाग पारदर्शी होता है, कुछ और मोटा काँच पारभासी होता है जबकि बहुत मोटा काँच अपारदर्शी होता है ।
- प्रदीप्त वस्तु (Luminous Body )- यदि वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती है जो उसे प्रदीप्त कहा जाता है। जैसे- सूर्य, तारा, जलता बल्व ।
- अप्रदीप्त वस्तु (Non-luminous body)- जब कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती है तो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं जैसे- पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह, पत्थर, आदि ।
- प्रकाशिकी (Optics)-- भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुण प्रकृति तथा प्रतिबिम्ब के बनने का अध्ययन किया जाता है प्रकाशिकी कहलाता है ।
- किसी माध्यम से चलती हुई प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्त्तन कहलाता है।
- प्रकाश जिस माध्यम के सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्त्तक सतह कहते हैं । परावर्त्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्त्तन दो तरह से हो सकता है ।
- नियमित परावर्त्तन- जब प्रकाश की किरणें बहुत ही चिकनी, समतल और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे कुछ निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित होता है। ऐसे परावर्त्तन को नियमित परावर्त्तन कहते हैं ।
- अनियमित परावर्त्तन- जब प्रकाश की किरणें रूखड़ी तथा चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश अनियमित रूप से परावर्तित होती है। ऐसे परावर्त्तन अनियमित परावर्त्तन कहलाता है ।

-
- प्रकाश के नियमित परवर्तन के दो नियम हैं-
- आपतीत किरण, परावर्तीत किरण तथा आपतन बिन्दु पर डाला गया लम्ब तीनों एक ही तल में होते हैं ।
- आपतन कोण तथा परावर्त्तन कोण एक-दूसरे के बराबर होते हैं ।
- प्रकाश के नियमित परवर्तन के दो नियम हैं-
- प्रकाश की किरण अगर परावर्त्तक सलह पर लंबवत है तो प्रकाश की किरण परावर्त्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है इस स्थिति में आपतन कोण तथा परावर्त्तन कोण का मान शून्य होता है ।
- जब किसी वस्तु से निकला हुआ किरण-पुंज परावर्त्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिन्दु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो यह दूसरा बिन्दु पहले बिन्दु का प्रतिबिम्ब कहलाता है। वस्तु के प्रत्येक बिन्दु का प्रतिबिम्ब बनता है और "प्रतिबिम्ब के समूह वस्तु का प्रतिबिम्ब कहते हैं।
- प्रतिविम्ब दो प्रकार के होते हैं-
- वास्तविक प्रतिबिम्ब (Real Image)- जब किसी बिन्दु से निकला हुआ किरण-पुंज परावर्तन या अपवर्त्तन के बाद जिस बिन्दु पर वास्तव में मिलती है उस बिन्दु को वास्तविक प्रतिबिम्ब कहते हैं।
- वास्तविक प्रतिबिम्ब हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है।
- आभासी या काल्पनिक प्रतिबिम्ब (Virtual image )- जब किसी बिन्दु से निकला हुआ किरण - पुंज परावर्त्तन या अपवर्त्तन के बाद जिस बिन्दु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिन्दु को आभासी प्रतिबिम्ब कहते हैं।
- आभासी प्रतिबिम्ब हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है।
- वास्तविक प्रतिबिम्ब (Real Image)- जब किसी बिन्दु से निकला हुआ किरण-पुंज परावर्तन या अपवर्त्तन के बाद जिस बिन्दु पर वास्तव में मिलती है उस बिन्दु को वास्तविक प्रतिबिम्ब कहते हैं।
- समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब अभासी वस्तु के आकार के बराबर तथा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है।
- वस्तु का प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु दर्पण से जितना आगे रहता है, प्रतिबिम्ब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है ।
- समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब का पाि उत्क्रमण (Lateral inversion) होता है अर्थात् प्रतिबिम्ब पलटा हुआ प्रतीत होता है।
- वस्तु तथा प्रतिबिम्ब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लम्बवत होता है ।
- समतल दर्पण से परावर्त्तन के बाद प्रत्येक आपतीत किरण में 180 - 2i (π - 2i ) का विचलन होता है। ( i = आपतन कोण = परावर्त्तन कोण) ।
- अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिम्ब समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण की ऊँचाई वस्तु की ऊँचाई का आधा होना आवश्यक है ।
- यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष V चाल से गतिमान हो तो वस्तु और प्रतिबिम्ब के सापेक्ष गति 2v होगी।
- अगर दो समतल दर्पण एक-दूसरे θ कोण पर हो तो उनके बीच रखी गयी किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब की संख्या

- समतल दर्पण में प्रतिबिम्ब की ऊँचाई वस्तु की ऊँचाई के बराबर होती है । प्रतिबिम्ब वस्तु के अपेक्षा सीधी होती है। फलतः इसका आवर्धन '+1' होता है।
- समतल दर्पण का सर्वाधिक प्रयोग आइने के रूप में किया जाता है ।
- इस दर्पण का उपयोग परिदर्शी (Periscope) तथा बहुदर्शी (Kaleidoscope) बनाने में किया जाता है।
- व्यस्त मार्ग पर बहुत अधिक मोड़नेवाले स्थान पर इसे लगाया जाता है जिससे चालक दूसरी ओर की गाड़ी को देख सके।
- समतल दर्पण का उपयोग बाल काटने वाले सैलून में किया जाता है ताकि लोग सिर के पीछे के भागों को देख सके ।
- यदि दर्पण का परावर्त्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो तो वैसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं ।
- गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं-
- अवतल दर्पण (Concave Mirror ) - वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्त्तन उसके दबे भाग की ओर से होता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं।
- उत्तल दर्पण (Convex Mirror)- उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्त्तन उसके उभरे भाग से होता है। इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं।

- ध्रुव (Pole ) - गोलीय दर्पण के परावर्त्तक सतह के मध्य बिन्दु को ध्रुव कहते हैं। इसे P अक्षर से दर्शाया जाता है ।
- वक्रता केन्द्र (Centre of Curvature) - जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है, उसे खोखले गोले के केन्द्र को वक्रता केन्द्र कहते हैं ।
- मुख्य अक्ष (Principal axis) - दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केन्द्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं । मुख्य अक्ष दर्पण के सतह पर लम्ब होती है और दर्पण के मध्य बिन्दु से होकर गुजरती है।
- वक्रता त्रिज्या (Radius of Curvature) ध्रुव और वक्रता केन्द्र के बीच दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ।
- द्वारक (Aperture)– दर्पण के परावर्त्तक सतह के क्षेत्र को उसका द्वारक कहते हैं। इसका मान गोलीय दर्पण के घेरे द्वारा या उसके वक्रता केन्द्र पर बने ठोस कोण या घेरे के व्यास से ज्ञात किया जाता है।
- मुख्य फोकस (Principle Focus )- मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्त्तन के बाद जिस बिन्दु पर मिलती है (अवतल दर्पण में), या जिस बिन्दु पर मिलती हुई प्रतीत होती है (उत्तल दर्पण में), उस बिन्दु को मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं।
- अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक तथा उत्तल दर्पण का फोकस अभासी होता है।
- फोकसान्तर (Focal length )- ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसान्तर या फोकस दूरी कहते हैं I
- आवर्धन (Magnification ) - प्रतिबिम्ब के ऊँचाई तथा वस्तु के ऊँचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं।

- स्थिति I - जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब अवतल दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिम्ब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है ।
- स्थिति II – जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब अनंत ( बहुत दूर) पर बनता हैयह प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के तुलना में बहुत बड़ा होता है।
- स्थिति III - जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केन्द्र और फोकस के बीच हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब वक्रता केन्द्र और अनंत के बीच बनता है । यह प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है ।
- स्थिति IV – जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केन्द्र हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब वक्रता केन्द्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है ।
- स्थिति V - जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केन्द्र और अनंत के बीच हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब वक्रता केन्द्र और फोकस के बीच बनता है । यह प्रतिबिम्ब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है ।
- स्थिति VI – जब वस्तु अनंत (बहुत दूर) पर हो- इस स्थिति में प्रतिबिम्ब फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के तुलना में बहुत छोटा होता है।
- स्थिति VII – जब वस्तु ध्रुव पर हो- इस स्थिति में प्रतिबिम्ब ध्रुव पर ही बनता है। यह प्रतिबिम्ब अभासी, सीधा तथा वस्तु -बराबर होता है।
- उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रखने पर प्रतिबिम्ब हमेशा सीधा अभासी और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिम्ब सदा दर्पण के पीछे ही बनता है।
- स्थिति I – जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर हो- इस स्थिति में प्रतिबिम्ब ध्रुव पर ही बनता है। प्रतिबिम्ब अभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता I
- स्थिति II - जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच हो - इस स्थिति में प्रतिबिम्ब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है । प्रतिबिम्ब अभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है ।
- स्थिति III - जब वस्तु अनंत पर हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है । यह प्रतिबिम्ब अभासी, सीधा और वस्तु के तुलना में बहुत छोटा होता है।
- अवतल दर्पण का उपयोगं सोलर कुकर या सौर भट्ठी • प्रकाश को अभिसरित (Converged) करने में किया जाता है।
- कान, नाक तथा गले के डॉक्टर आंतरिक भाग का जाँच करने हेतु अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ।
- बाल-दाढ़ी बनाने वाले सैलून में व्यक्ति का बड़ा प्रतिबिम्ब बनाने हेतु अवतल दर्पण का उपयोग होता है।
- दंत चिकित्सक दाँत को स्पष्ट देखने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ।
- हेडलाइट, टॉर्च, टेबुल लैम्प का परावर्त्तक अवतल दर्पण के ही बने होते हैं ।
- परावर्त्तन दूरदर्शी बनाने हेतु अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ।
- प्रदर्शन-कक्ष (Show-room) में विभिन्न आकार के प्रतिबिम्ब बनाने हेतु अवतल दर्पण ही उपयोग में लाये जाते हैं।
- उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र (Field of Vision)- काफी विस्तृत होता है। इस दर्पण से पीछे के बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। इस कारण से उत्तल दर्पण का प्रयोग स्कूटर, मोटरकार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है।
- सड़कों तथा गलियों के बल्व के ऊपर का परावर्त्तक उत्तल दर्पण का बना होता है ।
- प्रदर्शन कक्ष (Show-room) में छोटे-छोटे प्रतिबिम्ब बनाने हेतु उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
- समतल दर्पण का परावर्त्तक सतह समतल, अवतल का दबा हुआ तथा उत्तल का उभरा हुआ होता है ।
- समतल तथा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिम्ब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है जबकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिम्ब दर्पण के आगे भी बनता है तथा पीछे भी ।
- 3. समतल तथा उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है जबकि अवतल दर्पण से काल्पनिक (आभासी) एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिम्ब बनता है ।
- समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है जबकि अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मापने लायक होती है।
- अगर दर्पण के बना प्रतिबिम्ब सीधा एवं वस्तु के ऊँचाई का बनता है और वस्तु को आगे पीछे करने पर भी प्रतिबिम्ब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो, यह दर्पण समतल दर्पण है।
- अगर दर्पण में बना प्रतिबिम्ब सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु को दर्पण से थोड़ा दूर करने पर प्रतिबिम्ब का आकार बढ़ता है तो, यह दर्पण अवतल दर्पण है ।
- अगर दर्पण में बना प्रतिबिम्ब सीधा एवं वस्तु से छोटा है और वस्तु को दर्पण से दूर करने पर प्रतिबिम्ब का आकार घटता - है तो, यह दर्पण उत्तल दर्पण है।
- गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी (u) प्रतिबिम्ब की दूरी (v) और फोकस दूरी (f) के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं।

- गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन
 NOTE:- उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा धनात्मक (+) होता है । अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिम्ब के लिए आव नि ऋणात्मक (-) तथा आभासी प्रतिबिम्ब के लिए आवर्धन धनात्मक (+) होता है।
NOTE:- उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा धनात्मक (+) होता है । अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिम्ब के लिए आव नि ऋणात्मक (-) तथा आभासी प्रतिबिम्ब के लिए आवर्धन धनात्मक (+) होता है।
- दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब का स्थान निर्धारण करने के लिए दूरियों की चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिबिम्ब की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके-

- अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या (R) तथा फोकस दूरी (f) ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या (R) तथा फोकस दूरी (f) धनात्मक होता है ।
- जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में तिरछी आपतीत होती है तो प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो जाती है तथा कुछ भाग दूसरे माध्यम में प्रारंभिक पथ से कुछ मुड़ कर प्रवेश करती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश के किरण के पथ बदलने की घटना प्रकाश का अपवर्त्तन कहलाता है ।
- प्रकाश के अपवर्त्तन का कारण- प्रकाश के अपवर्त्तन का करण है, विभिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग-अलग होना। सघन माध्यम (Optically dencer) में प्रकाश की चाल कम तथा विरल माध्यम (Optically rare) में प्रकाश की चाल अधिक होती है ।
- आपतित किरण- दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़नेवाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं ।
- आपतन बिन्दु– जिस बिन्दु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिन्दु कहते हैं।
- अभिलंब— किसी सतह के किसी बिन्दु पर खींचे गये लंब को उस बिन्दु पर का अभिलंब कहते हैं।
- आवर्तित किरण- दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं।
- आपतन कोण- आपतित किरण, अभिलब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं ।
- अपवर्त्तन कोण- अपवर्तित किरण, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्त्तन कोण कहते हैं ।

- जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो -
- प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
- प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है ।
- जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो वह बिना मुड़े अर्थात् बिना अपवर्त्तन के सीधे निकल जाती है ।
- अपवर्त्तन के नियम- अपवर्तन के दो नियम है-
- आपतीत किरण, आपतन बिन्दु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं I
- किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या ( Sine) और अपवर्त्तन कोण की ज्या (Sine) का अनुपात एक नियतांक (Constant) होता है। यदि आपतन कोण । तथा अपवर्त्तन कोण r हो तो

- इस नियतांक (onstant) की माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्त्तनांक भी कहते हैं । इस नियम को पहली बार स्नेल ने निकाला था इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं ।
- किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्त्तनांक कहते हैं।
- किसी माध्यम का अपवर्त्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल (c) तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को कहते हैं I

- प्रमुख पदार्थ (माध्यम) का अपवर्त्तनांक

- सबसे कम अपवर्तनांक वाली माध्यम निर्वात है तथा सबसे अधिक अपवर्त्तनांक वाला माध्यम हीरा है।
- जिस माध्यम का अपवत्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है।
- पानी के सतह पर रखी छड़ मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है।
- पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है ।
- वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्त्तन होने से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं।
- वायुमंडलीय अपवर्त्तन के कारण ही सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ते हैं।
- जल से भरे बर्त्तन में अवस्थित सिक्का ऊपर उठा दिखाई पड़ता है।
- जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब वह विशेष आपतन कोण जिसके संगत का अपवर्त्तन कोण 90° होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है।
- जब क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है, तब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाकर उसी माध्यम में परावर्त्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है।
- जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब प्रकाश की किरण का दूसरे माध्यम में अपवर्त्तन नहीं होता है और प्रकाश की किरण उसी माध्यम में प्रकाश के परावर्त्तन के नियम का पालन करते हुए लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन कहते हैं।
- पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना हेतु निम्न शर्त का पूरा होना अनिवार्य है-
- प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए ।
- जिस विरल माध्यम में प्रकाश जा रही हो उस विरल माध्यम के लिए सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए ।
- पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन तथा परावर्तन में अंतर-
| पूर्ण आंतरिक परावर्तन | परावर्तन |
| 1. प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। | 1. प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए। |
| 2. आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। | 2. आपतन कोण का मान कुछ भी हो सकता है। |
| 3. यहाँ पर किरण का अपवर्त्तन या अवशोषण नहीं होता है । | 3. यहाँ पर किरण का अपवर्तन एवं अवशोषण संभव है। |
| 4. यह बहुत अधिक तीक्ष्ण (intense) होती है । | 4. यह कम तीक्ष्ण होती है। |
| 5. इसमें आपतीत किरण पूर्णतः लौट आती है। | 5. इसमें आपतीत किरण अंशतः ही लौटती है । |
- क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध-

- जिस माध्यम का अपवत्तनांक अपेक्षाकृत अधिक होता है उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है तथा जिस माध्यम का अपवर्त्तनांक अपेक्षाकृत कम होता है उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है।
उदा०- एक माध्यम का क्रांतिक कोण 60° है उस माध्यम का अपवर्त्तनांक क्या होगा ?

- कुछ प्रमुख पदार्थ का अपवर्त्तनांक एवं क्रांतिक कोण

- पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन के कारण होनेवाली घटना
- पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई पड़ता है ।
- मरीचिका (Mirage)-- मरीचिका एक धोखे की वस्तु या प्रकाशीय भ्रम है। गर्म क्षेत्रों में यात्री को यह आभास जलाशय का भ्रम उत्पन्न करता है।
- पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन के कारण तेज धूप में समतल चिकनी सड़क झिलमिलाते दिखाई पड़ता है और लगता है कि सड़क भींगा हुआ है ।
- ठंडे क्षेत्र में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दूर से आता जहाज उठता हुआ दिखाई पड़ता है। यह भी एक प्रकार दृष्टि भ्रम ( मरीचिका) है। इस दृष्टि भ्रम को लूमिंग (Looming) कहते हैं ।
- पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन के कारण तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है। बिना तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन नहीं कर पाता है ।
- पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन के कारण तेज गर्मी वाले दिन में मरीचिका दिखाई पड़ता है ।
- लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है ।
- लैंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लेन्टीन (Lentil ) से हुई है । लेंस का आकार हमारे देश में होने वाले मसूर दाल के दाने की तरह होता है ।
- लेंस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व बढ़ गया है। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, दूरदर्शी, प्रोजेक्टर सभी में लेंस का प्रयोग किया जाता है।
- लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-
- उत्तल या अभिसारी लेंस (Convex Lens)
- अवतल या अपसारी लेंस (Cocave Lens)
- उत्तर लेंस- उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस निम्न प्रकार के हो सकते हैं-
- अवतल उभयोत्तल (Biconvex )- इस लेंस का दोनों तल उत्तल होता है।
- समतलोत्तल (Plano-Convex ) - इस लेंस का एक तल समतल दूसरा तल उत्तल होता है।
- अवतलोत्तल (Cancavo-Convex)- इस लेंस का एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल होता है।
- अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है I अवतल लेंस निम्न प्रकार के हो सकते हैं।
- उभयावत्तल (Biconvex )- इसका दोनों तल अवतल होता है ।
- समतलावतल (Plano - convave ) - इसका एक तल समतल तथा दूसरा तल अवतल होता है ।
- उत्तलावतल (Convexo-concave)- इस लेंस का एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल होता है।
- उत्तर लेंस- उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस निम्न प्रकार के हो सकते हैं-
- वक्रता केंद्र (Centre of Curvature)- लेंस का गोलीय पृष्ठ वृहद गोला का भाग होता है, उस गोले के केन्द्र को वक्रता केन्द्र कहते हैं । लेंस में दो वक्रता केन्द्र होते हैं जिसे C1 तथा C2 से दर्शाया जाता है ।
- मुख्य अक्ष (Principal Axis )- किसी लेंस के दोनों वक्रता केन्द्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं ।
- प्रकाशिक केंद्र (Optical Centre)- लेंस का केन्द्र बिन्दु को प्रकाशिक केन्द्र कहते हैं। इसे 0 अक्षर से दर्शाया जाता है। प्रकाशिक केन्द्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलन के निर्गत हो जाती है।
- मुख्य फोकस (Focus )- मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिन्दु पर मिलती है (उत्तल लेंस में) या जिस बिन्दु पर मिलती हुई प्रतीत होती है (अवतल लेंस में) उस बिन्दु को मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस में दो फोकस होता है जिसे F1 तथा F2 द्वारा दर्शाया जाता है ।
- फोकसांतर या फोकस दूरी (Focal len प्रकाशिक केन्द्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं । इसे f द्वारा दर्शाया जाता है।
- द्वारक (Aperature)- किसी गोलीय लेंस की वृत्ताकारं भाग का प्रभावी व्यास उस गोलीय लेंस का द्वारक कहलाता है ।
- स्थिति I - जब वस्तु अनंत (बहुत दूर) पर हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है । यह प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के तुलना में बहुत छोटा होता है।
- स्थिति II - जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो - इस स्थिति में प्रतिबिम्ब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होता है। यह प्रतिबिम्ब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है ।
- स्थिति III - जब वस्तु फोकस पर हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिम्ब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बडा होता है।
- स्थिति IV – जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो - इस स्थिति में प्रतिबिम्ब 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिम्ब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से होता है।
- स्थिति V - जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो - इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब 2F2 पर बनता है । यह प्रतिबिम्ब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है।
- स्थिति VI - जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच हो - इस स्थिति में प्रतिबिम्ब F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है।
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिम्ब का बनना
- अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिम्ब ही बनता है चाहे वस्तु किसी भी स्थिति पर क्यों न रखी जाए ।
- स्थिति I- जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच हो - इस स्थिति में प्रतिबिम्ब लेंस तथा F2 के बीच बनता है । "यह प्रतिबिम्ब अभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है ।
- स्थिति II- जब वस्तु अनंत पर हो- इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिम्ब F2 पर बनता है । यह प्रतिबिम्ब अभासी, सीधा तथा वस्तु के तुलना में बहुत छोटा होता है।
- लेंस के लिए वस्तु—दूरी (u) प्रतिबिम्ब दूरी (v) तथा फोकस दूरी (f) के बीच संबंध एक सूत्र द्वारा बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं।

-

- m का मान धनात्मक होने पर प्रतिबिम्ब अभासी होगा तथा m का मान ऋणात्मक होने पर प्रतिबिम्ब वास्तविक होगा ।

- उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
- मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है लेकिन जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद फोकस से होकर हीं गुजरती है, तो इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं।
- लेंस को बारी-बारी से पुस्तक के एक पृष्ठ के समीप लाने पर-
- यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर अक्षर बड़ा दिखाई पड़े तो यह लेंस उत्तल होगा।
- यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर अक्षर अपने वास्तविक अकार का दिखे तो वह लेंस नहीं है, वह एक काँच का टुकड़ा होगा ।
- यदि पृष्ठ में छपे अक्षर को लेंस से देखने पर अक्षर छोटा दिखाई पड़े तो यह अवतल लेंस होगा ।
- किसी लेंस की क्षमता या शक्ति, लेंस के उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों को एकत्रित करता है या फैलाता है ।
- अधिक फोकस - दूरी का लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को कम एकत्रित करता है या फैलाता है जबकि कम फोकस दूरी वाला लेंस प्रकाश के समांतर किरणों का अधिक एकत्रित करती है या फैलाती है।
- किसी लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त की जाती है-

- लेंस की क्षमता का मात्रक डाइऑप्टर (D) ।1 डाइऑप्टर (1D) उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी । m हो ।
- लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी की होती है अर्थात् उत्तललेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती हैं ।
- अगर भिन्न क्षमता वाले लेंस को एक-टूकरे के सम्पर्क में रखा जाए तो - सम्पर्क में रखे लेंस के निकाय की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक-पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है ।
उदा०- 1. चार लेंस जिनकी क्षमता क्रमशः +2D, -3D, + 4.5D, −0.5D है, इन्हें एक दूसरे के सम्पर्क में रखा गया है । इस लेंस की संयोजन क्षमता क्या होगा ?पूरेलेंस निकाय का संयोजन शक्ति= +2D + (−3D) + 4.5D + (−0.5D)= +2D – 3D + 4.5D – 0.5D= +3D2. दो पतले लेंस की क्षमता +3.5D तथा - 2.5D है । इन्हें एक - दूसरे के संपर्क में रखा गया है। इस लेंस की संयोजन क्षमता क्या होगा ?संयोजन क्षमता= +3.5D + (−2.5 D )= ID
- जिस प्रकाश में विभिन्न तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्तियों के प्रकाश का मिश्रण रहता है उसे संयुक्त या बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश संयुक्त प्रकाश है।
- जिस प्रकाश में केवल एक रंग का प्रकाश होता है उसे एकवर्णी प्रकाश (Monochromic light) कहते हैं । जैसे- पीला रंग का प्रकाश, हरा रंग का प्रकाश ।
- प्रकाश के सभी रंगों का तरंगदैर्ध्य एवं आवृत्ति भिन्न-भिन्न होता है । परन्तु सभी रंगों के आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य का गुणनफल 3 × 1018 m/s ही होता है अर्थात् निर्वात में सभी प्रकाश का वेग 3 × 108 m/s ही होता है।
वेग = आवृत्ति × तरंगदैर्ध्य
- किसी संयुक्त प्रकाश का विभाजित होकर अपने अवयवी रंगों के प्रकाश में अलग हो जाना ही उस संयुक्त प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण कहलाता है।
- सर्वप्रथम न्यूटन ने सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर विभिन्न रंगों में विभाजित किया था।
- श्वेत प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण कराने हेतु एक प्रिज्म की आवश्यकता होती है तथा प्रिज्म के दूसरी ओर एक श्वेत पर्दा रखा जाता है I
- जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब श्वेत पर्दा पर सात रंगों का एक रंगीन पट्टी (धब्बा की तरह ) दिखाई पड़ता है। पर्दे पर प्राप्त रंगीन पट्टी को वर्णपट ( Spectrum) कहते हैं।
- अशुद्ध वर्णपट (Impure Spectrum ) - जब श्वेत प्रकाश का पतली किरणपुंज को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो पतली किरण पुंज के सभी किरणें सात रंगों में विभक्त हो जाती है, जिससे प्राप्त वर्णपट पर सभी रंग एक-दूसरे पर चढ़ जाते हैं। इसे वर्णपट को अशुद्ध वर्णपट कहते हैं I
- शुद्ध वर्णपट (Pure Spectrum)- शुद्ध वर्णपट वह वर्णपट है जिसमें श्वेत प्रकाश के सातों रंग स्पष्ट अलग हो । शुद्ध वर्णपट प्राप्त करने हेतु स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
- श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने से जो स्पेक्ट्रम (वर्णपट) प्राप्त होता है उसमें नीचे से ऊपर की ओर निम्न रंग क्रमानुसार. होते हैं-
- बैगनी (Violet)
- जामुनी (Indigo)
- नीला (Blue)
- हरा (Green)
- पीला (Yellow)
- नारंगी (Orange)
- लाल (Red)
इन रंगों को संक्षेप में बेनीआहपीनाला कहते हैं तथा अंग्रेजी में VIBGYOR कहते हैं।
- कुछ लोग Indigo को नीला तथा Blue को आसमानी बोलते हैं। कुछ विद्वान Indigo और Blue के बदले मात्र एक रंग Blue का ही प्रयोग करते हैं और सात रंग के जगह छह रंग का प्रयोग कहते हैं।
- किसी भी प्रकार का रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। श्वेत प्रकाश के अवयवी सातों रंग का तरंगदैर्ध्य अलग-अलग होता है। निर्वात में विभिन्न रंगों का तरंगदैर्ध्य-

- हमलोगों का आँख भी विभिन्न रंगों का पहचान उसके तरंगदैर्ध्य के आधार पर ही करता है।
- बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है तथा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होता है ।
- किसी सघन माध्यम में बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है जिसके कारण प्रिज्म द्वारा इस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है जिसके कारण प्रिज्म द्वारा इसका न्यूनतम विचलन होता है।
- जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति यथावत रहती है परंतु उसका तरंगदैर्ध्य तथा वेग परिवर्तित हो जाता है। काँच में श्वेत प्रकाश के लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का वेग सबसे कम होता है ।
- पीला रंग को स्पेक्ट्रम (वर्णपट ) का माध्य रंग (Mean Colour) कहा जाता है।
- काँच या अन्य माध्यम में प्रकाश के विभिन्न रंगों का वेग भिन्न-भिन्न होता है। प्रत्येक रंग के किरणों का अपवर्त्तन कोण खास आपतन कोण के लिए भिन्न-भिन्न होता है। इसलिए विभिन्न रंग एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं।
- इन्द्रधनुष एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के दिनों में, आकाश में सूर्य के विपरित दिखाई देते हैं।
- इन्द्रधनुष बनने में वर्षा की बूँदे प्रिज्म की भूमिका निभाता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश जब वर्षा के बूँदे में प्रवेश करता है तो निम्न प्रक्रिया के फलस्वरूप इन्द्रधनुष बनता है-
- सबसे पहले श्वेत प्रकाश का अपवर्त्तन तथा वर्ण-विक्षेपण होता है ।
- पुनः वर्ण-विक्षेपित किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्त्तन होता है ।
- और जब श्वेत प्रकाश वर्षा में बूँद से बाहर निकलती है एक बार फिर अपवर्तन होता है ।
- कभी-कभी आकश में दो इन्द्रधनुष एक साथ दिखते हैं, इनमें एक चमकीला होता है, जबकि दूसरे पहले के अपेक्षा थोड़ा धुँधला होता है ।
- चमकीले इन्द्रधनुष को प्राथमिक इन्द्रधनुष कहते हैं। इसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है तथा बैगनी रंग अन्दर की ओर होता है।
- धुँधला इन्द्रधनुष को द्वितीयक इन्द्रधनुष कहते हैं इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग अन्दर की ओर होता है ।
- किसी कण पर पड़कर प्रकाश का एक भाग का विभिन्न दिशाओं में छितराने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है ।
- प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा उसक तरंगदैर्ध्य के चतुर्थघात के व्युतक्रमानुपाती होता है।
![]()
- उपर्युक्त संबंध के अनुसार जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। यही कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
- प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें निम्न परिघटना देखने को मिलता है-
- आकाश का रंग दिन के समय नीला दिखाई पड़ता है।
- अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर वह नीला न दिखाई देकर काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकीर्णन नहीं हो पाता है I
- सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है I
- दोपहर के समय सूर्य अपने वास्तविक रंग में दिखाई पड़ता है क्योंकि दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है।
- खतरे का संकेत लाल रंग होते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होगा और यह ज्यादा दूर तक दिखाई देगा।
- अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन का अध्ययन सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक सी. वी. रमण द्वारा किया गया था । इस कार्य हेतु उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ।
- प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक रंग या मूल रंग कहा जाता है क्योंकि इन तीनों रंगों से प्रकाश के अन्य सभी रंग को प्राप्त किया जा सकता है।
- तीनों प्राथमिक रंग (लाल + हरा + नीला) मिलकर श्वेत प्रकाश (सूर्य प्रकाश जैसा) बनाते हैं ।
- प्राथमिक रंग आपस में मिलकर निम्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करते हैं-
लाल + नीला = मेजेन्टानीला + हरा = स्यान (Cyan)लाल + हरा = पीला
- मेजेन्टा, सायन तथा पीला रंग के प्रकाश को प्रकाश का द्वितीयक रंग कहते हैं ।
- प्रकाश का द्वितीयक रंग, प्रकाश के प्राथमिक रंग के साथ मिलकर श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते है, जो निम्न है -
नीला + पीला = श्वेतहरा + मेजेंटा = श्वेतलाल + सयान = श्वेत
- जिन दो रंगों के प्रकाश से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, उन दोनों रंगों के प्रकाश को एक-दूसरे का सम्पूरक या पूरक रंग (Complementry Colours) कहते हैं, अर्थात्-
- नीला का पूरक रंग पीला है या पीला का पूरक रंग नीला है।
- हरा का पूरक रंग मेंजेटा है य मेजेंटा का पूरक रंग हरा है ।
- लाल का पूरक रंग सयान है या सयान का पूरक रंग लाल है। ।
- श्वेत प्रकाश में हम वस्तु को जिस रंग में देखते हैं वास्तव में वह वस्तु उस रंग का होता नहीं है बल्कि वस्तु दिखने वाले रंग को परावर्तित करता है और परावर्तित रंग ही हमारे आँखों तक पहुँचता है।
- लाल गुलाब श्वेत प्रकाश में लाल दिखता है इसका कारण है- लाल गुलाब श्वेत प्रकाश के अन्य छह रंग को अवशोषित कर सिर्फ लाल रंग को ही परावर्तित करता है ।
- जब वस्तु अपने ऊपर आपतीत होने वाले सभी प्रकाश परावर्तित कर दे तो वह श्वेत दिखाई देता है तथा वस्तु अपने ऊपर आपतित होने वाले सभी प्रकाश अवशोषित कर ले तो वह काला दिखाई देता देगा।
- लाल रंग की वस्तु सिर्फ श्वेत या लाल प्रकाश में ही लाल रंग में दिखेगा अन्य किसी रंग के प्रकाश में वह काला दिखाई देगा क्योंकि अन्य सभी रंगों के प्रकाश को वह पूर्णतः अवशोषित कर लेगा।
- श्वेत (उजला) रंग की वस्तु श्वेत प्रकाश के श्वेत रंग का दिखाई देगा। अन्य सभी रंग के प्रकाश में श्वेत वस्तु उसी रंग में दिखेगा जो रंग प्रकाश का है क्योंकि श्वेत रंग की वस्तु सभी रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है।
- मानव नेत्र ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अद्भुत प्रकाशिय यंत्र है। यही कारण है कि आँख का अध्ययन प्रायः प्रकाशिकी (Optics) के अंतर्गत किया जाता है, परन्तु आँख एक मानव अंग है अतः इसका अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत ही मुख्य रूप से होता है।
- हमारा आँख लगभग गोलीय है और नेत्र - गोलक का व्यास लगभग 2.3 cm होता है। नेत्र के निम्न महत्वपूर्ण भाग होते हैं-
- श्वेत पटल (Sclerotic ) - नेत्र गोलक का सबसे बाहरी भाग जो सफेद और मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है श्वेत पटल कहलाता है।
- कॉर्निया (Cornea)– श्वेत पटल का अग्र भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है इसे कॉर्निया कहते है।
- कोराइड (Choroid)- श्वेत पटल के ठीक नीचे की परत जो गहरे भूरे रंग की होती है कोराइड कहलाता कोराइड परत आगे आकर दो परतों में विभाजित हो जाती है-
- कोराइड के आगे वाले अपारदर्शी परत जिसमें सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है उसे आइरिस (परितारिका) कहते हैं ।
- आइरिस के ठीक पीछे के भाग को सिलियसी मांसपेशी कहलाता है इसी. मांसपेशी के द्वारा नेत्र लेंस जुड़ा होता है।
- पुतली (Pupi)- आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं।
- नेत्र-लेंस (Eye Lens)- मानव का नेत्र लेंस लगभग-लगभग उत्तल होता है । यह लेंस प्रोटीन का बना होता है I
- दृष्टिपटल (Retina)– नेत्र का सबसे भीतरी परत दृष्टिपटल कहलाता है। रेटिना में दृक्तंत्रिका (Optic Nerves) होते हैं। जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है।
- जलीय द्रव (Aqueous humour)- आँख के कॉर्निया तथा लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे जलीय द्रव कहते हैं।
- काचाभ द्रव (Vitenous humour)— नेत्र-लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा रहता है उसे काचाभ द्रव कहते हैं ।
- प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर आँख के कॉर्निया और जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ता है। नेत्र लेंस उस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिम्ब रेटिना पर बनाता है।
- रेटिना पर जब प्रतिबिम्ब बनने की संवेदना उत्पन्न होती है तो यह संवेदना विद्युत सिग्नल में परिणत हो जाता है। यह विद्युत सिग्नल रेटिना से जुड़े Optic Nerves द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है। मस्तिष्क विद्युत सिग्नल का व्याख्या करता है और इसी व्याख्या के अनुरूप हम वस्तु को देख पाते हैं।
- आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस द्वारा होता है। मंद प्रकाश में आइरिस पुतली के छिद्र को बड़ा कर देता ताकि अधिक से अधिक प्रकाश आँख में प्रवेश कर सके तथा तीव्र प्रकाश में आइरिस पुतली के छिद्र को छोटा कर देता है. जिससे कम प्रकाश आँख में प्रवेश कर सके। यही कारण है कि एकाएक तीव्र प्रकाश में जाने पर कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है ।
- समायोजना (Accomodation)- सिलियसी मांसपेशी नेत्र- लेंस का फोकस दूरी को बदलते रहता है ताकि पूरी स्पष्ट प्रतिबिम्ब रेटिना पर बन सकें। इसी गुण को समायोजना कहते हैं।
- अंघ बिन्दु (Blind Spot)- वह स्थान जहाँ Optic Nerves रेटिना को छिद्रित कर मस्तिष्क में जाती है, अंध बिन्दु कहलाता है। अंध बिन्दु प्रकाश के लिए सं संवेदनशील नहीं है। अगर रेटिना के अंध बिन्दु पर किसी वस्तु तु का प्र प्रतिबिम्ब बनता है तो मस्तिष्क इस प्रतिबिम्ब का स्ष्ट व्याख्या नहीं कर पाता है और वह वस्तु हमें धुँधला नजर आता है।
- पीत बिन्दु (Yellow Spot)- नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिन्दु पर काटता है उसे पीत बिन्दु कहते हैं । पीत बिन्दु पर बना प्रतिबिम्ब पूर्णतः स्पष्ट होता है।
- बिना चश्मे की मदद से एवं बिना किसी तनाव के कम-से-कम जितनी कम दूरी की वस्तु को आँख स्पष्ट देख सकता है, उस दूरी को आँख का निकट बिन्दु कहते हैं । सामान्य आँख के लिए यह दूरी 25 cm होती है परन्तु बच्चा 25 cm से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 25 cm को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं।
- बिना चश्मे की मदद से एवं बिना किसी तनाव के अधिक-से-अधिक जिनती दूरी तक की वस्तु को आँख स्पष्ट देख सकती है, उस दूरी को आँख का दूर बिन्दु कहते हैं । सामान्य व्यक्ति के यह दूरी अनंत होती है।
- रेटिना पर दो प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिका होते हैं- दण्ड (Rods) तथा शंकु ( Cones) कोशिका ।
- शंकु कोशिका तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदनशील है जबकि मंद प्रकाश में यह कोशिका सक्रिय नहीं होता है। तीव्र प्रकाश में आँख शंकु कोशिका के मदद से ही देखता है।
- प्रकाश के रंग की पहचान भी शंकु कोशिका द्वारा होता है। विभिन्न रंगों की पहचान हेतु अलग-अलग प्रकार के शंकु कोशिका होती है ।
- मक्खी के रेटिना में पाराबैगनी रंग के पहचान के लिए भी शंकु कोशिका होती है जिससे मक्खी पाराबैगनी रंग का भी पहचान कर सकता है । परन्तु मनुष्य में यह शंकु कोशिका नहीं होता है।
- दण्ड कोशिका मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है तीव्र प्रकाश के लिए बहुत कम । मंद प्रकाश में हम किसी वस्तु को दण्ड कोशिका की मदद से ही देखते हैं।
- मंद प्रकाश में हम वस्तु की पहचान कर लेते हैं परन्तु उनके रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि मंद प्रकाश में रंगों की पहचान करने वाला शंकु कोशिका सक्रिय नहीं रहता है।
- जब आँख किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिम्ब रेटिना पर बनता है । वस्तु को आँख के सामने से हटा लेने पर 1/10 Sec. तक उस वस्तु को देखने की संवेदना रेटिना पर रहती है, इसे दृष्टि निर्बन्ध कहते हैं।
- दृष्टि निर्बंध के कारण ही जलते हुए गोले को तेजी से घुमाया जाता है तो वह जलते हुए वलय के रूप में दिखाई देता है।
- चलचित्र (फिल्म) भी दृष्टि निर्बंध सिद्धान्त पर बनाया जाता है। चलचित्र में वास्तव में किसी चीज के चलने का आभास स्थायी चित्रों की एक श्रृंखला से होती है। ऐसी श्रृंखला में प्रत्येक चित्र आने वाले चित्र से लगभग सटा रहता है।
- चलचित्र कैमरे द्वारा खींचे गये चित्रों में दृश्यो के क्रम को किसी परदे पर 24 प्रतिबिम्ब प्रति सेकेण्ड या इससे भी अधिक दर से प्रक्षेपित किया जाता है और व्यक्ति को प्रतिबिम्ब का क्रमागत प्रभाव एक-दूसरे से मिला प्रतीत होता है ।
- निकट दृष्टि दोष ( Short Sightedness or Myopia)
- निकट दृष्टि दोष वाले आँख निकट की वस्तु को देख पाता है, परन्तु दूर (अनंत) की वस्तु को साफ-साफ नहीं देख पाता है। ऐसे आँख के लिए दूर बिन्दु अनंत से कम होता है।
- निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण हैं-
- आँख का नेत्र गोलक का लम्बा होना जिससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है ।
- नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या नेत्र लेंस का वक्रता अत्यधिक हो जाना जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है।
- नेत्र के इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है।
- दूर दृष्टि दोष (Long Sightedness or Hypermetropia)
- दूर दृष्टि दोष वाला आँख दूर (अनंत) की वस्तु को साफ-साफ देख सकता है परन्तु नजदीक (25 cm) की वस्तु को साफ-साफ नहीं देख पाता है। ऐसे आँख के लिए निकट बिन्दु 25 cm से अधिक होता है ।
- दूर दृष्टि दोष होने के दो कारण हैं-
- आँख का नेत्र - गोलक छोटा होना
- नेत्र - लेंस की फोकस - दूरी बढ़ जाना
- नेत्र के इस दोष को दूर करने हेतु उचित क्षमता का उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है ।
- जटा दृष्टि दोष (Presbyopia)
- यह दोष बुढ़ापे में प्रायः होता है । इस दोष में व्यक्ति का आँख दूर दृष्टि एवं निकट दृष्टि दोनों दोष से प्रभावित हो जाता है ।
- इस दोष का मुख्य कारण है आँख के सिलयरी मांसपेशी का कमजोर हो जाना जिससे नेत्र लेंस की लोचकता कम हो जाती है I
- इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस की नीचे में उत्तल लेंस होता है तथा ऊपर में अवतल लेंस होता है।
- अबिन्दुकता (Astigmatism)
- इस दोष वाला आँख एक ही ऊँचाई की क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को एक लम्बाई की क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को एक लम्बाई में नहीं देख सकती है।
- इस दोष का मुख्य कारण है कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना ।
- इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है।
- Note:- उपर्युक्त आँख के चारों दोष को दूर करने के लिए आजकल कॉन्टेक्ट लेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
- मोतियाबिंद (Cataract)
- अधिक आयु के व्यक्ति का नेत्र - लेंस दूधिया तथा धुँधला हो जाता है जिससे व्यक्ति को अंशतः या पूर्णतः दिखाई नहीं पड़ता है। इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है ।
- शल्य चिकित्सा (Surgery) द्वारा मोतियाबिंद का सफल एवं सुरक्षित उपचार संभव है ।
- वर्णान्धता (Colour Blindness)
- नेत्र के रेटिना में अगर लाल एवं हरे रंग की पहचान करने वाला शंकु कोशिका नहीं होता है, तो ऐसे नेत्र लाल एवं हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। नेत्र के इस दोष को वर्णान्धता कहते हैं।
- नेत्र में यह दोष एक प्रकार के जीन के आधार पर होता है और इसका उपचार संभव नहीं है।
- प्रख्यात वैज्ञानिक एवं प्रथम परमाणु मॉडल देने वाले जॉन डाल्टन भी वर्णान्धता से पीड़ित थे । इस कारा इस रोग को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है ।
- वर्णान्धता वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान नहीं किये जाते हैं ।
Note:-
- नेत्रदान करते समय आँख का केवल अग्र भाग कॉर्निया ही दान किया जाता है।
- आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है । आइरिस का रंग जलवायु एवं स्थान के अनुसार बदला हुआ पाया जाता है ।
- आँख द्वारा देखने की क्रिया ठीक उसी प्रकार होती हैं जिस तरह फोटो कैमरा से फोटो खींचने की ।
- कैमरा में आगे लेंस होता है और पीछे फोटो-फिल्म ठीक उसी प्रकार आँख के आगे लेंस होता है और पीछे रेटिना I
- कैमरा में जो काम शटर का होता है ठीक ऐसा ही काम आँख का पलक करता है।
- कैमरा में जो काम (प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करना) डायफ्राम करता है ठीक वैसा ही काम आँख का पुतली करता है।
- मानव का आँख एक सर्वप्रमुख संवेदी अंग (ज्ञानेन्द्रीय) है जिसकी मदद से प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखा जा सकता है। कैमरा मानव निर्मित यंत्र है जिससे वस्तु का प्रतिबिम्ब उतारा जा सकता है।
- नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिम्ब बनता है जबकि कैमरा में फोटोफिल्म या फोटोग्राफीक पलेट पर प्रतिबिम्ब बनता है ।
- आँख में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नियत रहती है। कैमरा में लेंस और फोटोफिल्म की दूरी आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है।
- नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब अस्थाई होता है जबकि कैमरा में बना प्रतिबिम्ब सथाई होता है।
- देखे जाने वाली वस्तु आँखों पर जितना बड़ा कोण बनाती है, उसे उस वस्तु का दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहते हैं I
- वस्तु बड़ा है तो दर्शन कोण बड़ा बनता है। छोटी वस्तु का दर्शन कोण छोटा बनता है। लेकिन वस्तु की आँख से दूरी बढ़ने पर दर्शन कोण घटते जाता है ।
- किसी वस्तु का आँख पर जितना बड़ा दर्शन कोण बनेगा वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी जैसे यंत्र में वस्तु का दर्शन कोण आभासी रूप से जाता है जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है ।
- सूक्ष्मदर्शी निकट स्थित सूक्ष्म वस्तु को बड़ा कर स्पष्ट दिखलाता है जबकि दूरदर्शी दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखलाता है।
- सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। इसके द्वारा छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। इस सूक्ष्मदर्शी में लेंस के चारों प्लास्टिक अथवा टीन का फ्रेम लगा होता है तथा इस फ्रेम को पकड़ने के लिए एक हैण्डिल लगा रहता है ।
- इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटे वस्तु को देखने हेतु वस्तु को सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस के प्रकाश केन्द्र और फोकस दूरी के बीच रखा जाता है जिससे वस्तु का बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिम्ब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होता है।
- सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता-

- सरल सूक्ष्मदर्शी का फोकस दूरी जितना कम रहता है आवर्द्धन उतना ही अधिक होता है-
- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेन्स होते हैं। दोनों उत्तल लेंस को एक नली में इस प्रकार लगया जाता है ताकि दोनों लेन्स का मुख्य अक्ष एक ही हो ।
- सूक्ष्मदर्शी का जो लेंस वस्तु के समीप होता है उसे अभिदृश्यक (Objectlens) कहते हैं तथा जोलेंस आँख के समीप होता है उसे नेत्रिका (Eyelens) कहते हैं ।
- अभिदृश्यक लेंस का घेरा ( Aperture) तथा फोकस दूरी छोटा होता है तथा नेत्रिका का घेरा तथा फोकस दूरी दोनों बड़ा होता है ।
- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंस इस प्रकार फीट रहता है कि अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिम्ब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है, जिसका प्रतिबिम्ब और बड़ा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (25 cm) पर बनता है ।
-

-


- आवर्द्धन तथा आवर्द्धन क्षमता में निम्न अंतर है-

- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्द्धन अधिक होने के-
- अभिदृश्यक की फोकस - दूरी कम होनी चाहिए ।
- नेत्रिका की फोकस - दूरी कम होना चाहिए ।
- सूक्ष्मदर्शी की नली (जिसमें दोनों लेंस फीट रहते हैं) की लंबाई अधिक होनी चाहिए ।
- खगोलीय दूरबीन
- इस दूरबीन से आकाशीय पिण्ड जैसे - ग्रह, तारा का स्पष्ट प्रतिबिम्ब बनाकर देखा जाता है ।
- खगोलीय दूरबीन में भिन्न त्रिज्या की दो खोखली नली होते हैं। बड़ी त्रिज्या वाले नली के अन्दर बाहर छोटी त्रिज्या वाले नली को खिसकाया जा सकता है।
- बड़े त्रिज्या वाले नली के बाहरी छोर पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो वस्तु के तरफ रखा जाता है इसे अभिदृश्यक कहते हैं ।
- छोटी त्रिज्या वलो नली के बाहरी किनारे पर कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है । इसे नेत्रिका कहते हैं ।
- खगोलीय दूरबीन में प्रतिबिम्ब देखने हेतु इसका दो प्रकार से समयोजन किया जाता है।
- सामान्य समायोजन - अगर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस का समायोजन इस प्रकार से किया जाए कि अनंत पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिम्ब भी अनंत पर बने तो इसे सामान्य समायोजन कहते हैं । इस तरह से बना प्रतिबिम्ब बड़ा तो होता है परन्तु उल्टा होता है।
- सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन का

- दूरबीन के नली की आवश्यक लंबाई
L = fo + fefo = अभिदृश्यक की फोकस दूरी fe = नैत्रिका की फोकस दूरी
- सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन का आवर्द्धन क्षमता अधिक होने के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक तथा नैत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए।
- सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन का
- स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजना- अगर खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका को इस प्रकार समायोजन किया जाए कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिविम्व आँख से 25 cm की दूरी पर बने तो इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजना कहते हैं। इस स्थिति में भी वस्तु का प्रतिबिम्ब उल्टा ही बनता है।
- स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर खगोलीय दूरबीन का आवर्द्धन क्षमता

- इस समायोजना हेतु खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई

- स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर खगोलीय दूरबीन का आवर्द्धन क्षमता
- सामान्य समायोजन - अगर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस का समायोजन इस प्रकार से किया जाए कि अनंत पर स्थिर वस्तु का प्रतिबिम्ब भी अनंत पर बने तो इसे सामान्य समायोजन कहते हैं । इस तरह से बना प्रतिबिम्ब बड़ा तो होता है परन्तु उल्टा होता है।
- पार्थिव दूरबीन
- खगोलीय दूरवीन में बना प्रतिविम्व उल्टा होता है। अगर इस दूरवीन में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाए कि बना प्रतिविम्व सीधा हो तो वह पार्थिव दूरबीन बन जाएगा ।
- पार्थिव दूरबीन तीन उत्तल लेंस होता है एक अभिदृश्यक (उत्तल लेंस), एक नेत्रिका (उत्तल लेंस) तथा इन दोनों के बीच एक और उत्तल लेंस होता है जिसका मुख्य प्रायोजन होता प्रतिबिम्ब को सीधा करना ।
- पार्थिव दूरबीन का भी खगोलीय दूरवीन के तरह दोनों प्रकार से समायोजना हो सकता है।
- जब प्रतिविम्ब अनन्त पर बनता है, तब
-

- दूरवीन के नली की लंबाई = fo + 4f + fe
f = बीच वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी
-
- जब प्रतिबिम्व स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूर पर बनता हो, तब
-
- जब प्रतिविम्ब अनन्त पर बनता है, तब
Note :- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, विभिन्न प्रकार के दूरवीन का विस्तृत अध्ययन करने हेतु देखे- NCERT PHYSICS (वर्ग - 12 ) | अगर आप NDA तथा CDS के परीक्षा देते हैं तो अनिवार्य रूप से पुस्तक अध्ययन करें।
- जब दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश की तीव्रता, उन तरंगों के अलग—अलग तीव्रता के योग से भिन्न होता है। कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक पायी जाती है जबकि कुछ बिन्दुओं पर बिल्कुल अँधेरा रहता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतीकरण कहते हैं।
- माध्यम के जिस बिन्दु पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, उन बिन्दुओं पर हुए व्यक्तिकरण को संपोषी व्यतिकरण (Constructive Interferance) कहते हैं ।
- माध्यम के जिस बिन्दु पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है अर्थात् अँधेरा रहता है, उस बिन्दु पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण (Distructive interference) कहते हैं।
- व्यतिकरण प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग द्वारा व्यतिकरण के घटना को दिखाया।
- व्यतिकरण की घटना हेतु माध्यम से संरचरण करने वाले प्रकाश तरंग की आवृत्ति समान होनी चाहिए।
- व्यतिकरण के कारण निम्न परिघटना हमें देखने को मिलता है-.
- साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना।
- सीडी (CD) का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ना।
- जल की सतह पर फैले तेल का परत का रंगीन दिखाई पड़ना ।
- प्रकाश तरंग के संरचण मार्ग में अगर प्रकाश के तरंगदैर्ध्य (400 nm - 800 nm ) कोटि का कोई अवरोध रखा जाए तो, प्रकाश उस अवरोध के किनारे से टकराकर मुड़ जाता है अथवा अपने सरलरेखीय पथ से विचलित हो जाता है और प्रकाश वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ पूरी तरह अन्धकार होनी चाहिए । प्रकाश की यह घटना विवर्तन कहलाता है।
- प्रकाश का विर्वन भी प्रकाश के तरंग सिद्धान्त की पुष्टि करता है।
- जब प्रकाश की तरंगे प्रकाश स्त्रोत से निकलक सभी संभव दिशाओं में गतिमान होता है तो इसे प्रकाश तरंग को अध्रुवी प्रकाश कहते हैं।
- सूर्य से आने वाली प्रकाश, विद्युत बल्व, मोमबत्ती, ट्यूब लाईट आदि के प्रकाश अध्रुवीय प्रकाश है।
- प्रकाश के तरंगों के कम्पन को किसी एक दिशा में, लाने की क्रिया को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं । ध्रुवण का अर्थ होता है- एक दिशा में लाना ।
- ध्रुवीत प्रकाश प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल या पोलराइडो का प्रयोग किया जाता है।
- ध्रुवण की घटना यह पूष्टि करता है कि के प्रकाश की तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ है।
अभ्यास प्रश्न
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here








