General Competition | Science | Physics (भौतिक विज्ञान) | ध्वनि
जब शांत जल में पत्थर के छोटे टकड़े को फेंका जाता है तो जल में जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ एक Disturbance (विक्षोभ ) उत्पन्न होता है जो विक्षोभ एक घेरे के रूप में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है ।
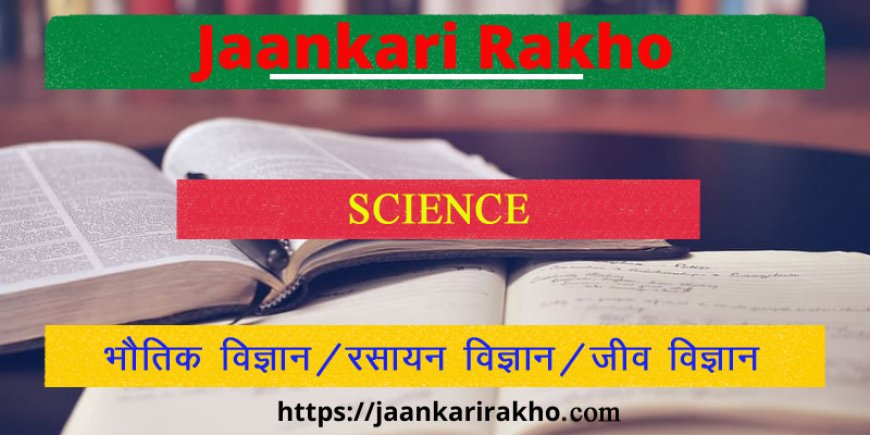
General Competition | Science | Physics (भौतिक विज्ञान) | ध्वनि
- जब शांत जल में पत्थर के छोटे टकड़े को फेंका जाता है तो जल में जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ एक Disturbance (विक्षोभ ) उत्पन्न होता है जो विक्षोभ एक घेरे के रूप में निश्चित चाल से आगे बढ़ता है ।
- इसी प्रकार के विक्षोभ को यांत्रिक तरंग (Mechanical Wave) कहते हैं तथा उसके आगे बढ़ने की प्रक्रिया को Wave Motion कहते हैं ।
- Wave दो प्रकार के होते हैं-
- Transverse Wave (अनुप्रस्थ तरंग)
- Longitudinal Wave (अनुदैर्ध्य तरंग)

- अनुप्रस्थत तरंग के उदाहरण:-
- तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है।
- रस्सी को दिवार में बांधकर एक सिरे को पकड़कर ऊपर नीचे हिलाने पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है।
- अनुप्रस्थ तरंग किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तब उत्पन्न होता है तब वह माध्यम दृढ़ (Rigid ) हो । गैस में Rigidity (दृढ़ता) नहीं होती है अतः गैस में अनुप्रस्थत रंग उत्पन्न नहीं होता है।
- द्रव के ऊपरी सतह पर ही अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है । द्रव के भीतर नहीं ।
- अनुप्रस्थ तरंग से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को Crest ( श्रृंग) तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को Trough (गर्त ) कहते हैं।
- अनुदैर्ध्य तरंग उदाहरण:-
- वायु और गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है I
- स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य होती है ।
- यदि किसी छड़ को बीच में कसकर उसके एक सिरे को भींगे कपड़े से लंबाई की दिशा में रगड़े तो छड़ में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है।

- अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न (Compression) तथा विरलन (Rarefaction) के रूप में आगे बढ़ती है।
- y-ray ( मामा किरण)
- तरंग दैर्ध्य 6x10-4 to 1x10-11 m
- आवृत्ति 5x1022 to 3x1019 Hz
- y-rays के खोज का श्रेय वैकुरल को है।
- X-ray.
- तरंग दैर्ध्य 1x10-11 to 3×10-8 m
- आवृत्ति 3 x 1019 to 1x1016 Hz
- X-rays के खोज का श्रेय रॉन्जन को है ।
- X-rays का उपयोग
- X-rays की सहायता से मनुष्य के शरीर को आर पार देखा जा सकता है। X-ray के उपयोग शल्य चिकित्सा (Surgery) में होता है।
- क्षय-रोग (TB) के उपचार में भी X-rays का उपयोग होता है ।
- X-rays का उपयोग कैन्सर के इलाज में भी होता है।
- X-rays के प्रयोग से कुछ पदार्थों के क्रिस्टल रचना का अध्ययन किया जाता है।
- X-rays की सहायता से नकली और असली मूल्यवान पदार्थ की जाँच की जाती है।
- शरीर के अंदर छीपी वस्तु का पता भी X-rays से लगाया जाता है ।
- पुल, गटर के दरार का पता भी X-rays की सहायता से लगाया जाता है ।
- पारा बैंगनी
- तरंग दैर्ध्य 6 x 10-10 to 4x10-7 m
- आवृत्ति 5x1017 to 8x1014 Hz
- पाराबैगनी किरण की खोज रिटर ने किया था ।
- पारावे ग्नी का उपयोग:-
- पाराबैगनी किरण में प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने का गुण होता है। इस गुण का उपयोग खनिज नमूनों के जाँच में होता है ।
- पाराबैगनी शरीर पर कम मात्रा में पड़कर विटामिन-D उत्पन्न करता है।
- फैक्ट्री या प्रयोगशाला के वायुमंडलल से बैक्टीरिया हटाने में पाराबैगनी का उपयोग होता है ।
- किमती पत्थर के पहचान में भी पाराबैंगनी किरण का उपयोग होता है।
- दस्तावेज के जालसाजी की जाँच भी पाराबैंगनी किरण की सहायता से की जाती है।
- दृश्य प्रकाश
- तरंग दैर्ध्य 4x10-7 to 8x10-7 m
- आवृत्ति 8x1014 to 4x1014 Hz
- दृश्य प्रकाश के खोज का श्रेय न्यूनटन को है ।
- अवरक्त किरण
- तरंग दैर्ध्य 8x10-7 to 3x10-5 m
- आवृत्ति 4 x 1014 to 3x1013 Hz.
- अवरक्त विकिरण का खोज विलियन हर्शेल ने किया था ।
- अवरक्त विकिरण का उपयोग-
- मांसपेशी के तनाव के उपचार में
- कृत्रिम उपग्रह को सौर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा देने में
- धुँध, कुहासा, बादलों वाली स्थिति में फाटोग्राफी करने में ।
- पौधा घरों में पौधा को गर्म रखने में
- सौर-कुकर में
- मौसम - विज्ञान में
- उष्मा विकिरण
- तरंग दैर्ध्य 10-5 to 10-1 m
- आवृत्ति 3×1013 to 3×109 Hz
- माइक्रो तरंग
- तरंग दैर्ध्य 10-3 to 0.3.m
- आवृत्ति 3×1011 to 1×109 Hz
- रेडियो-तरंग
- तरंग दैर्ध्य 10 to 104.m
- आवृत्ति 3x107 to 3x104 Hz
- रेडियो तथा माइक्रो तरंग विकिरण का प्रयोग रेडियो तथा TV संचार पद्धति में होता है ।
- आयाम (Amplitude) :- माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक-से-अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को आयाम कहते ।

- आवर्त्तकाल (Time Period) :- माध्यम के किसी कण को एक कम्पन या एक दोलन में जितना समय लगता है, उसे तरंग का आवर्त्तकाल कहते हैं। इसे T से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक सेकेण्ड है।
- आवृत्ति (Frequency ) :- माध्यम का कोई कण एक सेकेण्ड में जितना कम्पन करता है वही उस तरंग की आवृत्ति कहलाता है। इसे प्रायः n से सुचित किया जाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है।
यदि माध्यम के किसी कण की आवृत्ति और आवर्त्तकाल क्रमश: n और T हो तो

- तरंगदैर्ध्य (Wavel Length) :- दो समीपवर्ती श्रृंग और गर्त्त (अनुप्रस्थ तरंग में) अथवा समीप वाले संपीड़न और विरलन के केन्द्र के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं । अथवा एक आवर्त्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे 2 (लेम्डा) से सूचित किया जाता है इका मात्रक मीटर होता है।
- तरंग वेग (Wave Valocity ) :- एक सेकेण्ड तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग - वेग कहते हैं। इसे प्रायः V से सूचित किया जाता है।
- तरंग दैर्ध्य, तरंग चाल तथा आवृत्ति में संबंध :-

प्रगामी तरंग (Progessive Wave)
अप्रगामी तरंग ( Stationary Wave)
- अप्रगामी तरंग, तरंग नहीं है बल्कि एक कंपन है क्योंकि इसमें विक्षोभ का संचरण नहीं होता है।
उदा० :- 1. स्वरमापी (Sonometer) में दो सेतुओं के बीच तने तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है।2. Organ pipe में अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग उत्पन्न होता है।
ध्वनि तरंग
- ध्वनि एक प्रकार अनुदैर्ध्य तरंग है I
- ध्वनि तरंग के आवृत्ति परिसर-
- Audible Wave (श्रव्य परास) :- सामान्य मनुष्य को ध्वनि की संवेदना कंपन की आवृत्ति के एक निश्चित परास के बीच होती है। यह परास 20 Hz - 20,000 Hz के बीच रहता है। 20 Hz - 20,000 Hz के बीच के तरंग को Audible Wave कहते हैं। मनुष्य ने तो 20 Hz से कम और न ही 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति के ध्वनि तरंग को सुन सकता है।
- Infrasonic Wave ( अपश्रव्य तरंग ):- 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को अपश्रव्य तरंग कहते हैं ।
- हाथी, ह्वेल जैसे जानवर 20 Hz से कम की ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है।
- • ज्वालामुखी उद्भेदन तथा भूकंप होने पर 20 Hz से कम आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है।
- Ultrasonic Wave:- जिस तरंग की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है उसे पयश्रव्य तरंग कहते हैं ।
- आजकल आधुनिक विधियों द्वारा 5 × 105 KHz (5000 × 105 Hz) आवृत्ति तक का पराश्रव्य तरंग उत्पन्न किया जा सकता है ।
- चमगादड़ के अलावे कुत्ता, बिल्ली, चिड़ियाँ सूँस (डॉलफीन के समान जलीय जीव) कुछ कीड़े-मकोड़े पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं और उसे सून भी सकते हैं।
- पराश्रव्य तरंग में अत्यधिक ऊर्जा रहने तथा तरंदैर्ध्य बहुत छोटा होने के कारण इस तरंग का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है।
प्रमुख उपयोग निम्न है-
- द्रवों में पराश्रव्य तरंग की चाल ज्ञात कर द्रव की रसायनिक संरचना, सांद्रण, अवशोषण, संपीडयता आदि का पता लगाया जाता है।
- समुद्र की गहराई मापने हेतु भी पराश्राव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है।
- स्कंदन (Coagulation) प्रक्रिया में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है।
- स्कंदन (Coagulation) :- यदि किसी द्रव में ठोस के सूक्ष्म कण तैर रहें हो, तो उस द्रव में पराश्रव्य तरंगों को भेजने पर ये कण आपस में मिलकर बड़े होने लगते है । और नीचे बैठ जाते हैं। यह क्रिया स्कंदन कहलाता है।
- पराश्रव्य तरंग का उपयोग धातु के भीतर के दरारों का पता लगाने में किया जाता है ।
- छोटे-छोटे जीव (चूहा, मछली, मेढ़क ) पर पराश्रव्य तरंग डालकर उन्हें अंगहीन बनाया जाता पराश्रव्य तरंग से बैक्टीरिया को भी खत्म किया जाता है । अथवा भार डाला जाता है।
- Ultrasonography, Echocardiography गुर्दे के पत्थर तोड़ने में, मोतियाबिंद हटाने में पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है।
ध्वनि का चाल
- विभिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंग की चाल भिन्न-भिन्न होती है। यह चाल ठोस में अधिकतम, द्रवों में उससे कम और गैस में न्यूनतम होती है ।
- 20°C पर विभिन्न माध्यमों को ध्वनि की चाल-

ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाला कारक:-
- ताप के स्थिर रहने पर हवा में ध्वनि की चाल हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता है यानि दाब के बदलने पर ध्वनि के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 1°C ताप के बढ़ने से हवा में ध्वनि की चाल 0.61 m/s बढ़ जाती है।
- आई हवा (जलवाष्पयुक्त) में ध्वनि की चाल शुष्क हवा ( जलवाष्प रहित ) में ध्वनि की चाल से अधिक होती है ।
- ध्वनि तरंग की चाल माध्यम के वेग का भी प्रभाव पड़ता है। यदि माध्यम की गति तरंग-गति के दिशा में हो तो ध्वनि-तरंग की चाल बढ़ जाती है तथा इसकी दिशा विपरित होने पर तरंग की चाल घट जाती है।
- प्रघाती तरंग में इतनी अधिक ऊर्जा रहती है कि इसके प्रभाव से मकान के खिड़की, दरवाजे के काँच टूट जाते हैं कभी कभी पूरा इमारत क्षतिग्रस्त हो जाता है, अगर व्यक्ति के कान तक यह तरंग पहुँचता है तो व्यक्ति के श्रवण शक्ति खत्म हो जाती है।
- मैक संख्या = किसी माध्यम से ध्वनि की चाल / उसी माध्यम में ध्वनि की चाल
- मैक संख्या 1. से तात्पर्य है वस्तु ध्वनि के चाल से चल रहा है। मैक संख्या 2 से तात्पर्य है वस्तु ध्वनि के चाल से दुगुणी चाल से चल रहा है।
- मैक संख्या 1 से अधिक चाल को Supersonic तथा मैक संख्या 5 (ध्वनि के चाल का पाँच गुणा ) से अधिक चाल को Hypersonic कहते हैं।
- तारत्व (Pitch)
- तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है।
- मोटी ध्वनि की तारत्व निम्न होता है जबकि पतली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है ।
- तारत्व आवृत्तिर पर निर्भर करता है अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक तथा कम तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है ।
- पुरूष की आवाज से स्त्रियों की आवाज पतली होती है क्योंकि स्त्रियों के आवाज का तारत्व उच्च होता है। बच्चों के आवाज की उच्च तारत्व का होता यही कारण है कि बच्चों का आवाज भी पतला होता है।
- तारत्व का मापन संभव नहीं इसे हम मस्तिष्क से सिर्फ अनुभव कर सकते हैं।
- प्रबलता (Loudness)
- ध्वनि की प्रबलता वह गुण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है ।
- अधिक प्रबलता वाली ध्वनि अधिक ऊर्जा होती है तथा ध्वनि तरंग का आयाम अधिक होता है। कम् प्रबलता की ध्वनि में कम ऊर्जा रहती है और इसका आयाम कम होता है ।
- ध्वनि जैसे-जैसे ध्वनि-स्त्रोत से दूर होते जाता है उसकी प्रबलता तथा आयाम दोनों घटते जाता है।
- साधारण बातचित में ध्वनिका आयाम 10-9 होता है।
- ध्वनि की प्रबलता (Loundness) तथा ध्वनि की तीव्रता (Intensity) दोनों एक-दूसरे से भिन्न हैं ।
- ध्वनि की प्रबलता कानों की संवेदनशीलता की माप है जबकि तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेण्ड गुजरने वाली ऊर्जा है। समान तीव्रता वाली ध्वनि को भी हमारा कान एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल सुन सकता है।
- ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसीबल (dB) में मापा जाता है।
- प्रमुख ध्वनि स्त्रोत एवं उनकी तीव्रताः-
- साधारण बातचीत - 30-40 dB
- जोर से बातचीत - 50-60 dB
- ट्रक-ट्रैक्टर - 90-100 dB
- साइरन - 110-120 dB
- जेट विमान - 140-150 dB
- मिसाइल - 180 dB
- WHO के अनुसार मानव के सर्वोत्तम ध्वनि 45 dB की होती है। 75 dB की अधिक की ध्वनि मानव कान को हानि पहुँचा सकता है। मनुष्य अधिकतम 130 dB की ध्वनि सुन सकता है लेकिन 85 dB से अधिक तीव्रता की ध्वनिसे मनुष्य बहरा हो सकता है जबकि 150 dB की अधिक ध्वनि की तीव्रता से मनुष्य पागल हो सकता है।
- गुणता (Timber)
- गुणता ध्वनि को वह लक्षण है जिससे हमारा कान समान तारत्व एवं समान तीव्रता की विभिन्न ध्वनि में अंतर कर सकता है।
- अगर एक साथ हारमोनियम तथा तबला समान तारत्व और समान तीव्रता की ध्वनि निकाल रहा है तो हमारा कान गुणता के आधार पर यह जान जाता है कि कौन-सी ध्वनि हारमोनियम का है और कौन-सी ध्वनि तबला का ।
- एक विशेष आवृत्ति की ध्वनि को tone का जाता है तथा विभिन्न tone से उत्पन्न ध्वनि को स्वरक हा जाता है।
- ध्वनि का परावर्त्तन (Reflection of Sound)
- ध्वनि तरंग का किसी परावर्त्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को ध्वनिका परावर्तन कहते हैं ।
- प्रकाश छोटी परावर्त्तक सतह से भी परावर्तित हो सकता है परन्तु ध्वनि को परावर्तित करने के लिए परावर्त्तक सतह अपेक्षाकृत बड़ी होनी चाहिए ।
- ध्वनि के परावर्त्तन के लिए परावर्त्तन का समतल होना आवश्यक नहीं है।
- ध्वनि का परावर्त्तन उन्हीं नियमों के अनुसार होता जो प्रकाश के परावर्त्तन के नियम हैं ।
- ध्वनि के परावर्त्तन के होने वाली महत्वपूर्ण घटना :-
- प्रतिध्वनि (Echo)
- किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनिका टकराकर परावर्तित होने से उस ध्वनि का पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि या Echo कहते हैं ।
- हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 sec तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम-से-कम 0. 1 sec का समय - अंतराल होनी आवश्यक है।
- 0.1 sec में ध्वनि (344 m/s x 0.1 sec = 34.4m) 34.4m की दूरी तय करती है अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्त्रोत से न्यूनतम दूरी 17.2 m अवश्य होनी चाहिए ।
- प्रतिध्वनि के व्यवहारिक उपयोगः-
- प्रतिध्वनि का उपयोग कर ध्वनि के चाल को मापा जाता है ।
- चमगादड़ प्रति ध्वनि का उपयोग कर अपने रास्ते में पड़ने वाले अवरोध का पता लगा लेते हैं और बचकर निकल जाते हैं ।
- प्रतिध्वनि का उपयोग मेडिसीन के क्षेत्र में Echo Cardiography तथा Ultrasonography जैसे उपकरण में होता है।
- अनुररण (Reverberation)
- किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दिवारों से बारबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है अब तक यह इतनी कम न हो जाये क यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबर परावर्त्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध (Persistance of Sound) होता है जिसे अनुरणन कहते हैं ।
- अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छत और दिवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाये जाते हैं।
- ध्वनि के बहुलित परावर्त्तन (Multiple Reflection) के उदाहरणः-
- मेघगर्जन की धवन जो धीरे-धीरे मंद होकर समाप्त होती है इसका कारण हैं मेघगर्जन की धवन का बादल के परतों द्वारा कई बार परावर्त्तन होता है और एक-एक कर हमारे कानों तक पहुँचता है।
- डॉक्टरी स्टेथोस्कोप में भी ध्वनि के बहुलित परावर्त्तन सिद्धान्त का उपयोग होता है।
- हॉर्न, बिगुल, मेगाफोन, लाउडस्पीकर जैसे यंत्र इस प्रकार बनाये जाते हैं की प्रारंभ में इनकी ध्वनि सभी दिशाओं में नहीं फैलती है। पहले इस यंत्र के नली वाली संरचना में ध्वनि का कई बार परावर्त्तन होता है और सभी ध्वनि एकजुट होकर यंत्र के शंकुनुमा चौड़े मुँह से प्रबलता के साथ निकलता है।
- प्रतिध्वनि (Echo)
- ध्वनि का अपर्त्तन (Refraction of Sound)
- जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं।
- ध्वनि के अपवर्त्तन के कारण ही ध्वनि दिन के समय कम क्षेत्र तक ही सुनी जा सकती है जबकि रात के समय ध्वनि दूर-दूर तक सुनाई देती है।
- प्रणोदित कम्पन (Forced Vibration)
- कम्पन करने की क्षमता रखने वाली वस्तु पर जब बाहर से कोई आवर्त्त बल लगाया जाता है तो वस्तु लगाये जाने वाले बल के आवर्त्तकाल से कम्पन करने लगता है। वस्तु के इस प्रकार के कम्पन को प्रणोदित कम्पन कहते हैं । प्रणोदित कम्पन का आयाम हमेशा समान रहता है ।
- मंदित कम्पन (Dansped Vibration) :- किसी भी प्रकार के कम्पन करने वाली वस्तु पर v क प्रतिरोधक बल लगता है। यह प्रतिरोधक बल या को माध्यम के घर्षण के कारण उत्पन्न होता है या फिर कम्पीत वस्तु के आंतरिक घर्षण के कारण । इस तरह से कम्पीत वस्तु पर प्रतिरोधक बल के काम करने से वस्तु का आयाम घटता है और अन्त में समाप्त हो जाता है। ऐसा कम्पन मंदिन कम्पन कहलाता है ।
सरल दोलक के लोलक का कम्पन मंदि कम्पन के उदाहरण हैं।
- अनुनाद (Resonace ) :- जब किसी कम्पन करने वाली वस्तु पर कोई ऐसा बल कार्य करता है जिसका आवर्त्तकाल वस्तु आवर्त्तकाल से भिन्न हो तो वस्तु का आयाम बहुत ही कम होता है परन्तु जब वस्तु पर क्रियाशील बल का आवर्त्तकाल वस्तु के आवर्त्तकाल के बराबर हो तो वस्तु का आयाम अधिकतम होता है । प्रणोदित कम्पन की इसी स्थिति को अनुनाद कहते हैं ।
- अर्थात् अनुनाद प्रणोदित कम्पन की वह स्थिति है जिसमें वस्तु और उसपर क्रियाशील बल का आवर्त्तकाल बराबर होता है।
- अनुनाद के उदाहरणः-
- जब मेज पर रेडियो या अन्य बाध यंत्र बनते हैं जो मेज पर रखे गिलास प्लेट खड़-खड़ करने लगता है इसका कारण अनुनाद है। यानि वर्त्तन की आवृत्ति संगीत ध्वनि के आवृत्ति के बराबर होने पर दोलन का आयाम बढ़ जाता है और वे लड़खड़ाने लगते हैं।
- तार-वाद्य यंत्र जैसे- सितार अनुनाद के सिद्धान्त पर ही कार्य करता है। इस यंत्र में मुख्यतार के बगले में कई तार लगे होते । मुख्य तार को बजाते हैं तो बगले वाले तार अनुनादित हो जाते हैं और स्वर की तीव्रता बढ़ जाती है।
- अनुनाद के कारण ही खाली वर्त्तन में जल भरने पर उससे निकलने वाली ध्वनि का स्वर बदलते रहता है।
- रेडियो भी अनुनाद के सिद्धान्त पर काम करता है ।
- ध्वनि का व्यतिकरण (Interference of Sound)
- अध्यारोपण (Super imposition)— जब दो ध्वनि तरंग एक साथ एक रेखा पर चलती है तो एक तरंग को दूसरी तरंग से मिलने की क्रिया को अध्यारोपण कहते हैं ।
- जब दो ध्वनि तरंग एक-दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो परणामी ध्वनि की तीव्रता कही पर महत्तम तथा कहीं पर न्यूनतम होती है इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं।
- जहाँ पर ध्वनि तरंग की तीव्रता महत्तम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण तथा जहाँ पर ध्वनि तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं ।
- दो ध्वनि तरंग के व्यतिकरण हेतु आवश्यक शर्तें:-
- तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए ।
- तरंगों का अयाम बराबर होनी चाहिए ।
- किसी बिन्दु पर दोनों तरंगों के कारण विस्थापन एक ही रेखा पर होनी चाहिए ।
- कुहरे वाली रात में जाज को संकेत देने हेतु सायरन का इस्तेमाल होता है। सायरन की ध्वनि निकट और दूर तक सुनी जाती है । परन्तु बीच के कुछ क्षेत्र में साइरन की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। इसका कारण व्यतिकरण है।
- ध्वनि का विवर्त्तन (Diffraction of Sound)
- ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य लगभग 1 m का होता है। जब तरंग दैर्ध्य कोटि का अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्त्तन कहते हैं ।
- विवर्त्तन के कारण ही बाहर से आने वाली ध्वनि, दरवाजा, खिड़की से टकराकड़ मुड़ती है और हमारे कानों तक पहुँचती है।
- बाहरी कान:- मनुष्य के बाहरी कान में कर्ण पल्लव (Pinnal) तथा कर्णनलिका (ear canal) होता है। बाहरी कान बाहर से खुला रहता है और परिवेश से ध्वनि तरंग को एकत्रित कर मध्य कान में भेजने का कार्य करता है।
- मध्य कान:- Ear Canal से कसकर बँधी एवं तनी हुई झिल्ली होती है जिसे Eardrum (कर्णपट ) कहते हैं। Eardrum द्वारा ही बाहरी कान तथा मध्य कान से अलग होता है। मध्य कान में तीन हड्डी होती है- hammer, anivl तथा Strirrup | मध्य कान ध्वनि तरंग को आंतरिक कान में संचरित कर देता है ।
- आंतरिक कान:- आंतरिक कान में द्रव से भरी एक नली होती है जिसे Cochlea (कर्णावर्त) कहते हैं। इसका आकार घोंघा की तरह होता है। इसका आकार घोंघा की तरह होता है। यह नली Stirrup हड्डी से जुड़ा रहता है। Cochlea में विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से रहता है ।
- SONAR - समुद्री जहाज, समुद्र गहराई मापने या समुद्र में छिपे वस्तु का पता लगाने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग करता है। इस तकनीक को SONAR (Sound Navigation and Ranging) कहते हैं ।
अभ्यास प्रश्न
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







