General Competition | Science | Physics (भौतिक विज्ञान) | विद्युत
Electricity शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द Electron से हुई है। Electron का शाब्दीक अर्थ होता है ऐम्बर ।
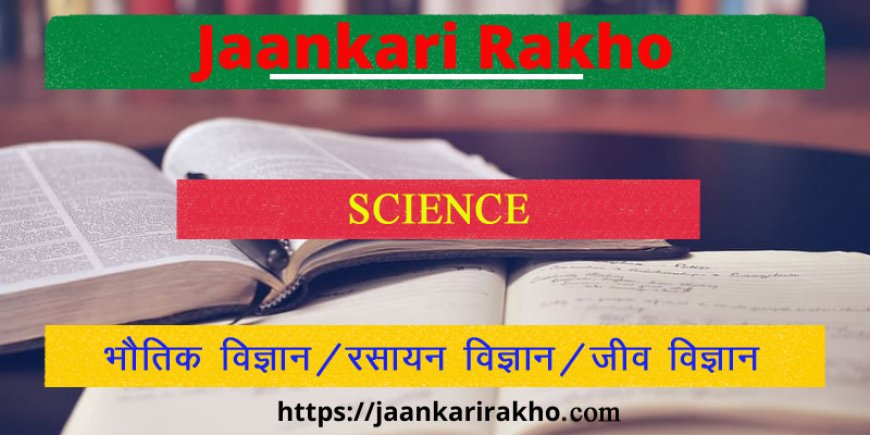
General Competition | Science | Physics (भौतिक विज्ञान) | विद्युत
- Electricity शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द Electron से हुई है। Electron का शाब्दीक अर्थ होता है ऐम्बर । सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने ही बताया था कि - ऐम्बर को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर ऐम्बर में आकर्षण का गुण आ जाता है ।
- विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं-
- धन आवेश (Positive Charge)- काँच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश काँच पर होता है उसे धन आवेश कहते हैं ।
- ऋण आवेश (Negative Charge)- ऐबोनाइट के छडको ऊन से रगड़ने पर जो आवेश ऐबोनाइट पर होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं।
- आवेश उत्पन्न होने के कारणः- आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण है: पदार्थ के परमाणु का इलेक्ट्रॉन। जब दो वस्तु को आपस में रगडा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, निकलकर दूसरी वस्तु है कर दूसरी वस्तु में चला जाता है।
- जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वह घन आवेशित हो जाता है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है।
- जब भी दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो दोनों आवेश एक साथ उत्पन्न होते हैं और उनका परिमाण एक-दूसरे के बराबर होता है ।
- आवेश का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नाश। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांन्त कहते हैं ।
- समान आवेश के बीच विकर्षण बल तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है।
- आवेश का SI मात्रक कूलॉम है । 1 कूलॉम आवेश 6.25 x 1018 इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होते हैं। संसार में सबसे कम परिमाण का आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6x10-19C (ऋण आवेश) होता है ।
- आवेश की विमा [AT] है जहाँ A धारा तथा T समय की विमा है ।
- कूलम्ब के दो आवेश के बीच कार्य करने वाले भाषण तथा विकर्षण बल के संबंध में दो नियम प्रतिपादित किये हैं-
- दो आवेश के बीच कार्य करने वलो तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती है ।
F ∝ a1 × a2
- दो आवेश के बीच कार्य करने वाले आकर्षण तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
 k नियतांक (constant) है जिनका मान उस माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है जिस माध्यम में आवेश रखा है।
k नियतांक (constant) है जिनका मान उस माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है जिस माध्यम में आवेश रखा है।
- दो आवेश के बीच कार्य करने वलो तथा विकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती है ।
- कूलम्ब का नियम न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण नियम के समान है। दोनों नियम सिर्फ एक मुख्य अंतर है- गुरूत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है जबकि वैद्युत बल में आकर्षण एवं विकर्षण दोनों होता है ।
- जब निर्वात में IC का दो आवेश (विपरित आवेश या समान आवेश) के बीच की दूरी 1 m हो तो उन दोनों आवेश के बीच 9 × 109 न्यूटन का विकर्षण (या आकर्षण) बल लगता है ।
- जब दो आवेश के बीच की दूरी 10-14m से कम हो तब यहाँ कूलम्ब का नियम का पालन नहीं होता है। जब दो आवेश के बीच की दूरी 10-14m से कम होता है तो उनके बीच लगने वाले बल को नाभकीय बल कहते हैं ।
- एकांक धनात्मक अविश को अनन्त से किसी बिन्दु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिन्दु का विभव कहते । विभव अदिश राशि है तथा उसका SI मात्रक वोल्ट (v) है ।
- अगर 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिन्दु पर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिन्दु का विभव 1 वोल्ट होगा ।

- अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है। धन आवेशित वस्तु विभव धनात्मक होता है तथा ऋण आवेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना गया है।
- विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिन्दुओं के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं । विभवांतर भी अदिश राशि है और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है ।
- 1C आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक लाने में । जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिन्दुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा ।
- विभवांतर, कार्य तथा आवेश के बीच संबंध से निम्न सूत्र प्राप्त होते हैं-

- विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युतधारा कहते हैं ।
- जब चालक तार को दो भिन्न-भिन्न विभवों के आवेशों से या विद्युत स्त्रोत से जोड़ा जाता है तब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के धारा के विपरित बहने वाली धारा को ही विद्युतधारा कहा जाता है ।
- निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉनिक धारा बहती है तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा बहती है ।
- विद्युत धारा के प्रवाह हेतु दो बिन्दु के विभव का अंतर होना अनिवार्य है। अगर दो बिन्दु का विभव समान है तो उनके बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा ।
- विद्युत धारा अदिश राशि है इसका SI मात्रक ऐम्पीयर (A ) है । विद्युतधारा का परिमाण छोटा रहने पर मिली ऐम्पीयर (aM) तथा माइक्रो एम्पीयर का भी प्रयोग होता है।

- चालक (Conductors)– जिस पदार्थ से होकर विद्युत सुगमतापूर्वक गमन कर सकता है उसे चालक कहते हैं। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन (विलयन में) पाये जाते हैं।
उदा०— ताम्बा, चाँदी, ग्रेफाइट, अम्ल क्षार या लवण युक्त जलीय विलयन ।
- कुचालक (Insulators)– जिस पदार्थ से होकर विद्युत आसानी से गमन नहीं कर सकता है उसे कुचालक या विद्युतरोधी कहते हैं। ऐसे पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या नगण्य मात्रा में होते हैं।
उदा०– रबड़, काँच, प्लास्टिक, अबरख, आसुत जल ।
- अर्द्धचालक (Semi-conductor)- अर्द्धचालक वह पदार्थ है जिसमें सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं परन्तु विशेष अशुद्धि मिलाने पर या गर्म करने पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती हैं और वे चालक की तरह व्यवहार करते हैं।
उदा० - सिलिकॉन, जरमेनियम
- जिस पथ से होकर विद्युतधारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ से जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो वह बंद विद्युत परिपथ कहलाता है।
- विद्युत परिपथ को दर्शाने हेतु कुछ प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है-

- गैल्वेनोमीटर (Galvanometer)
- गैल्वेनोमीटर एक नाजुक विद्युतीय उपकरण है। इसका उपयोग विद्युत आवेश की उपस्थिति, आवेश की प्रकृति, धारा की उपस्थिति, धारा का दिशा मापने हेतु किया जाता है।
- ‘गैल्वोनोमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है।
- गैल्वोनोमीटर में शंट (एक प्रकार प्रतिरोधक तार ) जोड़कर इसे ऐमीटर तथा वोल्टमीटर में बदला जा सकता है।
- ऐमीटर (Ammeter)
- ऐमीटर द्वारा ऐम्पीयर में धारा का प्रबलता का मापन किया जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है।
- ऐमीटर को विद्युत परिपथ का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
- गैलवोनोमीटर की कुंडली (Coil) में समांतर क्रम में शंट जोड़कर एमीटर बनाया जाता है ।
- वोल्टमीटर (Voltmeter)
- वोल्टमीटर द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। इसका प्रतिरोध काफी अधिक होता है।
- वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ जाता है।
- गैल्वोनोमीटर के कुंडली में श्रेणीक्रम में शंट जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है।
- जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, उनके सिरों के बीच का विभवांतर तथा चालक के प्रतिरोध के संबंध में एक नियम दिया जो ओम का नियम कहलाता है।
- ओम का नियम:- यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है।

- ओम के नियम से प्राप्त महत्वपूर्ण सूत्र -

- प्रतिरोध का SI मात्रक ओम के नाम पर ओम रखा गया है जिसका संकेत Ω होता है ।
- अंतराष्ट्रीय ओम (International Ohm)- यदि 0.0144521 kg शुद्ध पारे के स्तम्भ की लंबाई 1.063 मीटर और उसके एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 10-10 m2 हो तब 0°C पर उसका प्रतिरोध एक अंतर्राष्ट्रीय ओम होता है।
- ओम नियम की सीमाएँ:-
- ओम का नियम धातु चालक तथा अन्य कुछ चालकों पर ही लागू होता है। सभी चालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता है।
- रेडियो बाल्व, ट्रांजिस्टर, दिष्टकारी ( Rectifiers ) गैसों से जब विद्युत धारा गमन होता है तो यहाँ ओम का नियम लागू नहीं होता है।
- प्रतिरोध (Resistance) तथा प्रतिरोधक (Resistor) का अर्थ अलग-अलग होता है-
- प्रतिरोध:- प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है।
- प्रतिरोधकः - प्रतिरोोक एक वस्तु जिसका अपना प्रतिरोध होता है ।
- वे पदार्थ जो विद्युत का चालक होते हैं, उनका प्रतिरोध अत्यंत निम्न होता है। वे पदार्थ जो विद्युत का कुलाचक होते हैं, उनका प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता है ।
- चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक-
- चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है-
- तार की लंबाई दुगुणा बढ़ा देने पर उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा और लंबाई आधा कर देने पर प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा।
- चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थकाट के क्षेत्रफल (Area of Cross Section) के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

- अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगुणा कर दिया जाए तो प्रतिरोध घट कर आधा हो जाएगा या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़कर दुगुणा हो जाएगा।
- किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात् तार का व्यास बढ़ा दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध घटकर पहले का एक-चौथाई हो जाएगा या तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़कर पहले का चार गुणा हो जाएगा।
- चालक का प्रतिरोध उस पदार्थ पर भी निर्भर करता है जिस पदार्थ से चालक बना होता है।
- समान लंबाई के नाइक्रोम का प्रतिरोध, कॉपर तार के प्रतिरोध के लगभग 60 गुणा अधिक होता है।
- ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर चालक तार का प्रतिरोध, घटता है।
- कुछ मिश्रधातु (मैगनिन, कान्स्टनटन, नाइक्रोम) का प्रतिरोध ताप से अप्रभावित रहता है।
- चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है-
- विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है । इच्छा के अनुरूप विद्युत धारा प्राप्त करने के हेतु दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है।
- प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो विधि से किया जाता है-
- श्रेणीक्रम संयोजन (Series Cobination)
- जब एक प्रतिरोधकों का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोधक तार के पहले सिरे से, दूसरा प्रतिरोधक तार का दूसरा सिरा तीसरे प्ररितोधक तार के पहले से जोड़कर यहीं क्रम आगे बढ़ता है तो यह संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है ।
- श्रेणीक्रम में जितने भी प्रतिरोधक जुड़े होते हैं उन सभी में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान समान होता है।
- श्रेणीक्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर अलग-अलग होता है।
- श्रेणीक्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों का समतुल्य प्ररितोध सभी प्रतिरोधकों के अलग-अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं।
अगर चार प्रतिरोधकों का प्रतिरोध क्रमश: R1, R2, R3 तथा R4 हो तो इन सभी का समतुल्य प्रतिरोध (R)R = R1 + R2 + R3 + R4
- समांतर क्रम संयोजन (Parallel Combination)
- जब दो यो दो से अधिक प्रतिरोधकों के एक सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरा को एक साथ जोड़कर प्रतिरोध का संयोजन किया जाता है, तो यह संयोजन समान्तर क्रम संयोजन कहा जाता है।

- समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधकों में प्रवाहित होनेवाले विद्युत धारा का मान अलग-अलग होता है।
- अलग चार प्रतिरोधक जिनता प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 हो और यह समांतर क्रम में जुड़ा हो तो परिपथ का समतुल्य (R) निम्न सूत्र से प्राप्त किया जाता है-

- घरेलू विद्युत उपकरण समांतरक्रम में ही जोड़ा जाता है, इसके निम्न कारण हैं-
- समांतर क्रम से जुड़े विद्युत उपकरण में कोई एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी विद्युत उपकरण सामान्य रूप से काम करते रहते हैं जबकि श्रेणीक्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता है।
- समांतर क्रम से जुड़े सभी विद्युत उपकरण के लिए अलग-अलग स्विच होता है, जबकि श्रेणीक्रम से जुड़े सभी विद्युत उपकरण के लिए एक ही स्विच होता है।
- समांतर क्रम से जुड़े सभी विद्युत उपकरण को समान विभवांतर ( 220V) मिलता है जबकि श्रेणीक्रम से जुड़े सभी विद्युत उपकरण को समान विभवांतर नहीं मिल पाता है ।
- घरेलू विद्युत उपकरण में अलग-अलग परिमाण का विद्युत धारा की आवयकता होती है। जैसे हीटर को अधिक विद्युत धारा चाहिए बल्व को कम । विद्युत उपकरण की यह आवश्यकता केवल समांतर क्रम करके ही पूरा किया जा सकता है।
- जब दो यो दो से अधिक प्रतिरोधकों के एक सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरा को एक साथ जोड़कर प्रतिरोध का संयोजन किया जाता है, तो यह संयोजन समान्तर क्रम संयोजन कहा जाता है।
- मिश्रीत संयोजन (Mixed Combination)
- प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिनमें श्रेणीक्रम तथा समांतर क्रम संयोजन एक साथ रहता है, मिश्रीत संयोजन कहलाता है-

- प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिनमें श्रेणीक्रम तथा समांतर क्रम संयोजन एक साथ रहता है, मिश्रीत संयोजन कहलाता है-
- श्रेणीक्रम संयोजन (Series Cobination)
- सेल का विद्युत वाहक बल जूल में ऊर्जा का वह परिणाम है जो सेल सहित विद्युत परिपथ में एक कूलॉम विद्युत आवेश प्रवाहित होने में• सेल द्वारा आपूर्ति की जाती है।
- यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो, सेल से जुड़े विद्युत परिपथ का प्रतिरोध R हो और सेल द्वारा । विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित किया जाता हो तब सेल का विद्युत वाहक बल
E = Ir + IR
- सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेल के विभवांतर से निम्न अंतर है-
- सेल का विद्युत वाहक बल (E) = Ir + IR · होता है जबकि सेल का विभवांतर (V) = IR होगा ।
- सेल का विद्युत वाहक बल सेल के विभवांतर से बड़ा होता है ।
- सेल का विद्युत वाहक बल का मान नियत होता है, जबकि सेल जैसे-जैसे पुराना होते जाता है उसका विभवांतर घटता जाता है।
- खुले परिपथ (जब सेल से धारा नहीं बहती है।) में सेल के दोनों सिरों के बीच लगा वोल्ट मीटर द्वारा मापा गया परिमाण सेल का विद्युत वाहक बल होगा और बंद परिपथ (जब धारा प्रवाहित हो) में वोल्टमीटर द्वारा मापा गया परिमाण सेल का विभवांतर होगा।
- जब दो भिन्न विभवों के बीच आवेश का गमन होता है तब विद्युतीय कार्य सम्पन्न होता है । विद्युत कार्य का भी SI मात्रक जूल है।
- विद्युतीय कार्य = विभवांतर x आवेश
या W = VQ .......(i)

- किसी विद्युत परिपथ प्रति सेकण्ड किये गये कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं । शक्ति का SI मात्रक वाट है।

- विद्युत कार्य के सूत्र से विद्युत शक्ति का प्राप्त सूत्र

- वाट शक्ति का छोटा मात्रक है । शक्ति का बड़ा मात्रक है-
- 1 KW (किलोवाट) = 1000 W
IHP (हॉर्स पॉवर) = 746 W
- घरों में जो विद्युत ऊर्जा खर्च होता है उसे जूल में नहीं मापा जाता है क्योंकि जूल ऊर्जा छोटा मात्रक है।
- घरों में खर्च विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा (KWh) में मापा जाता है। KWh को ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक या वोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या केवल यूनिट कहते हैं।
1 Unit = 1KWh= 1000 Wh= 3600000Ws= 3.6 × 10 106J
- घरों में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा के लिये सूत्र-

- विद्युतधारा के प्रवाह से किसी प्रतिरोधक या चालक में उष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युतधारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं ।
- विद्युतधारा के उष्मीय प्रभाव के संबंध में जूल ने तीन नियम प्रतिपादित किये हैं-
- किसी निश्चित समय में किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है I
H ∝ I2 R तथा t = Cons tan t
- किसी निश्चित समय में निश्चित विद्युतधारा से चालक में उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है।
H ∝ R I तथा t = Cons tan t
- किसी निश्चित विद्युतधारा से किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उस समय के समानुपाती होता है जितने समय तक चालक में धारा प्रवाहित होती है।
H ∝ t I तथा R = Cons tan t
- किसी निश्चित समय में किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है I
- जूल के तीनों नियम को मिलाने पर
H ∝ I2 RtH = cons tan t × I2 RtSI मात्रक में constnat का मान 1 होता है ।अतः उत्पन्न ऊष्मा (H) = I2 Rt
- विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करनेवाले विद्युत उपकरण है- विद्युत बल्व, ट्यूब लाईट, हीटर, विद्युत इस्त्री (आयरन), आर्क लैम्प, फ्यूज, ऐमीटर, वोल्टमीटर, विद्युत विकिरण (Electric Radiator), टेस्टर ।
- विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित प्रमुख उपकरण-
Electric Lamp (विद्युत बल्व )
- विद्युत बल्व विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है ।
- बल्व का फिलामेंट टंग्सटन का बना होता है जिसका गलनांक 3380°C है जिसके कारण यह पिघलता नहीं है ।
- बल्व के भीतर निर्वात के स्थान पर अक्रिय गैस- नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर दिया जाता है ताकि उच्च ताप पर टंग्सटन का ऑकसीकरण न हो ।
- बल्व की शक्ति वाट के रूप बल्व पर अंकित रहता है। अधिक वाट के बल्व का प्रतिरोध कम तथा कम वाट के बल्व का प्रतिरोध अधिक होता हैं।
- बोल्टेज को बढ़ाने पर बल्व की शक्ति बढ़ती है परंतु बल्व के फ्यूज होने की संभावना बढ़ जाती है।
Electric-heater (हीटर)
- हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है ।
- हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोधकता तथा गलनांक बहुत ही उच्च होता है। नाइक्रोम को Heating element भी कहते कहते हैं।
- विद्युतधारा बहने पर नाइक्रोम का तार गर्म होकर बहुत अधिक उष्मा देता है। इसमें प्रकाश की मात्रा कम होती है क्योंकि नाइक्रोम का तार गर्म होकर लाल रहता है जिससे अवरक्त किरण उत्सर्जित होता है ।
- फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित एक सुरक्षा-व्यवस्था है ।
- कभी-कभी परिपथ में विद्युत धारा का मान अचानक बढ़ जाता है जिससे परिपथ में आग लग सकती है तथा विद्युत उपकरण नष्ट हो सकते हैं। इसी स्थिति से बचने हेतु फ्यूज का इस्तेमाल होता है। फ्यूज अधिक धारा प्रवाहित होने पर विद्युत परिपथ को भंग कर देता है।
- विद्युत परिपथ में अचानक धारा का मान बढ़ जाने का दो कारण है ।
- Over loading- घरेलू वायरिंग एक खास लोड पर की जाती है। जब भी इस लोड से अधिक विद्युत धारा ली जाती है तो उसे Overloading कहते हैं।
- Short-circutting- जब कभी संयोग से या गलत संयोजन करने से गर्म तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाता है तो विद्युत परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है जिससे धारा का मान बढ़ जाता है।
- फ्यूज कम द्रवणांक तथा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का एक पतला तार है ।
- फ्यूज को हमेशा गर्म तार से श्रेणीक्रम में लगाया जाता है।
- अच्छा फ्यूज टिन का बना होता है। सस्ता फ्यूज टीन एवं तांबे के मिश्रधातु का बना होता है। कुछ फ्यूज टीन, ताँबे तथा के मिश्रधातु का भी बना होता है। इसके अलावे फ्यूज एलुमिनियम, कॉपर, आयरन तथा लेड का भी हो सकता है।
- चुम्बक में उत्तर - दक्षिण दिशा बतलाने का गुण होता है। दैशिक गुण के कारण ही इसे Lode - Stone कहा जाता है।
- ध्रुव (Pole)– स्वतंत्रतापूर्वक झूलते चुम्बक हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा में आकर रूकता है। चुम्बक के जो सिरा उत्तर दिशा में रूकता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा जो सिरा दक्षिण दिशा में रूकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं ।
- चुंबक के समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है।
- चुबंकीय याम्योत्तर (Magnetic Meridian ) - पृथ्वी के किसी स्थान पर स्वतंत्र रूप से लटके चुबंक के उत्तर - दक्षिण ध्रुव से जाते उदग्र काल्पनिक तल को उस स्थान का चुबंकीय याम्योत्तर कहते हैं ।
- भौगोलिक याम्योत्तर (Geographical Meridian ) - पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर-दक्षिण ध्रुव से जाते उदग्र काल्पनिक तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं ।
- पृथ्वी के चुबंकीय अक्ष– पृथ्वी भी एक विशाल चुबंक है। पृथ्वी के चुम्बकीय उत्तर-दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी का चुबंकीय अक्ष कहते हैं ।
- पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर–दक्षिण ध्रुवों को मिलानेवाली रेखा को पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के केन्द्र पर चुबंकीय तथा भौगोलिक अक्ष का कोण 15° होता है।
- किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुम्बक के प्रभाव का अनुभव किया, जा सके चुबंकीय क्षेत्र कहलाता है।
- चुम्बक के इस प्रभाव को चुबंकीय क्षेत्र की तीव्रता से मापा जाता है जिसे संक्षेप में चुबंकीय क्षेत्र भी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है।
- चुबंकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक Weber / m2 या टेसला है ।
- चुंबकीय क्षेत्र को चुबकीय क्षेत्र के रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता हैं। चुबकीय क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र रेखाओं का गुण-

- किसी चुंबक के चुबंकीय क्षेत्र में क्षेत्र - रेखाएँ एकसतत बंद वक्र (continuous closed curved ) की तरह रहता है। ये रेखाएँ चुबंक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से हो हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है।
- ध्रुव के निकट क्षेत्र - रेखाएँ बहुत घनी होती है और जैसे-जैसे ध्रुव से दूरी बढ़ती है उसका घनत्व कम होता जाता है ।
- क्षेत्र-रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है ।
- जहाँ-जहाँ क्षेत्र-रेखा एक दूसरे के निकट रहते हैं वहाँ चुबंकीय क्षेत्र प्रबल होता है । चुबंक के ध्रुव के निकट चुबंकीय क्षेत्र प्रबल होता है।
- चुबंकीय क्षेत्र - रेखाएँ एक-दूसरे को काटती नहीं है।
- क्षेत्र - रेखाएँ एक ही दिशा में गमण करते हैं तथा एक-दूसरे को विकर्षित करते हैं।
- 1820 ई० में Hanse Christian Oerested ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया की जहाँ कहीं विद्युत आवेश गमण करता है उसके आस-पास चुबंकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
- धारावाही तार (Current Carrying Wire) से धारा बहने से आस-पास चुबंकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटनाओं को विद्युत धारा का चुबंकीय प्रभाव कहते हैं ।
- सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुबंकीय क्षेत्र की दिशा दाये हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। यदि धारावाही तार को दाएँ हाथ से इस प्रकार पकड़े की अंगूठा तार से प्रवाहित धारा दिशा बताये तो मुड़ी हुई अंगुली चुबंकीय बल रेखा की दिशा को बतलाता है ।

- परिनालिका (Solenoid)- जब कुचालक पदार्थ के खोखली और बेलनाकार नली के ऊपर विद्युतरोधी चालक तार को सपल रूप से लपेटा जाता है तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं ।

- जब परिनालिका से धारा बहती है तो परिनालिका छड़ चुम्बक की तरह व्यवहार करता है यानि पारिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है ।
- परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुबंकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दॉये हाथ के नियम से प्राप्त होता है— यही परिनालिका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि उँगलियाँ धारा की दिशा में हो तो अॅगूठे की दिशा चुबंकीय क्षेत्र की दिशा होगी ।

अभ्यास प्रश्न
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







