General Competition | Science | Biology (जीव विज्ञान) | पौधों और मानव में पोषण
पोषण, ऐसा जैव प्रक्रम (Life Process) है जिसमें सजीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करते है।
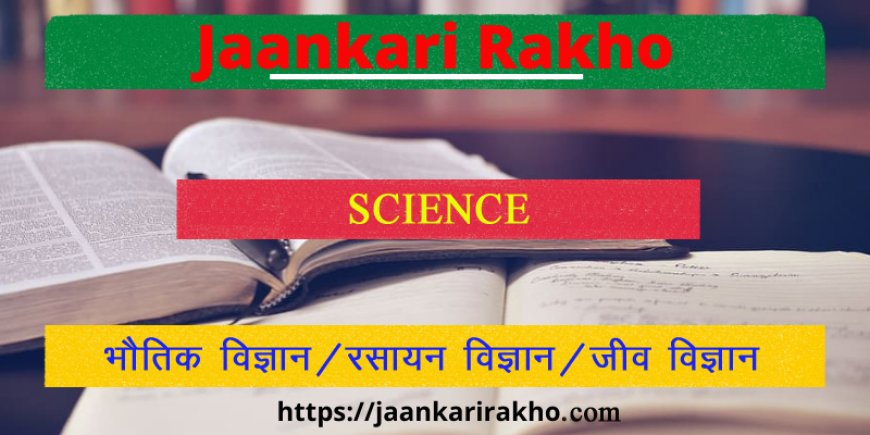
General Competition | Science | Biology (जीव विज्ञान) | पौधों और मानव में पोषण
- सजीवों को अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवनपर्यंत भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, जिससे जीवन की सभी उपापचयी (Metabolic) क्रिया संचालित होती है। इसके अतिरिक्त भोजन से प्राप्त ऊर्जा सजीवों के शरीर के निर्माण, वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है।
- पोषण, ऐसा जैव प्रक्रम (Life Process) है जिसमें सजीव भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करते है।
- विभिन्न प्रकार के सजीवों में पोषण दो प्रकार से होता है-
- स्वपोषण (Autotrophic Nutrition ) : पोषण की वह विधि जिसमें सजीव भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहे, स्वपोषण कहलाता है तथा जिस सजीव में स्वपोषण होता है उसे स्वपोषी (Autotrophs) कहते है।
- 'Autotrophs' दो ग्रीक शब्द Auto तथा troph के मेल से बना है। Auto शब्द का अर्थ स्वतः (Salf) होता है तथा troph का अर्थ पोषण (Nutrition) होता है।
- स्वपोषण के भी दो प्रकार होते हैं-
- प्रकाशीय स्वपोषण (Photo-autotrophism): एक कोशिकीय जीव तथा सभी हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज (भोजन) का निर्माण करते है। यह प्रकाशीय स्वपोषण है जो प्रकाश-संश्लेषण भी कहलाता है।
- रसायनिक स्वपोषण : इस प्रकार का स्वपोषण कुछ जीवाणु जैसे- फेरोमोनास, सल्फोमोनास, बिगियाटोआ आदि में पाया जाता है। यह लौह--योगिकों तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
- परपोषण या विषम पोषण otrophic : पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते एवं पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण कहलाता है। ऐसे जीव जिनमें परपोषण होता वं परपोषी (Heterotrophs) कहलाते है।
- 'Heterotroph' 'भी दो ग्रीक शब्द Hetero तथा troph से मिलकर बना है। Hetero का अर्थ विषम या भिन्न होता है तथा troph का अर्थ पोषण होता है।
- परपोषण के तीन प्रकार है-
- मृतजीवी पोषण (Saprophytic Nutrition) : मृतजीवी पोषण में जीव अपना भोजन, मृत जंतु और पौधे के शरीर से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी, मृत जन्तु तथा पौधों में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिक को अपने शरीर में उपस्थित एंजाइम की मदद से तरल (घुलित) कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर उसे अवशोषित कर लेते है। भोजन को तरल रूप से अवशोषित करने के कारण मृतजीवी पोषण को अवशोषक पोषण (Absorptive Nutrition ) भी कहा जाता है।
- यह पोषण कवक, जीवाणु तथा कुछ प्रोटोजोआ में होता है। ये मृतजीवी (Saprophytes ) अपघटक भी कहलाते है।
- परजीवी पोषण (Parasitic Nutrition ) : परजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें एक जीव अपना भोजन दूसरे जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे, प्राप्त करता है। जीव जो भोजन प्राप्त करता है परजीवी (Parasite) कहलाता है और जीवधारी जिसके शरीर से भोजन प्राप्त किया जाता है परपोषी (Host) कहलाता है।
- परजीवी, परपोषी (Host ) से भोजन तो प्राप्त करता है परन्तु परपोषी को कोई लाभ नहीं पहुचाता है बल्कि परपोषी को प्रायः हानि ही पहुँचाता है। परपोषी पौधा और जन्तु हो सकता है। परजीवी का भोजन भी प्रायः तरल ही होता है।
- रोग फैलाने वाले सभी सूक्ष्मजीव, कवक कुछ पौधे (अमरबेल ) में परजीवी पोषण होता है।
- प्राणिसम पोषण (Holozoic Nutrition ) : इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन का अन्तर्ग्रहण करता है, फिर भोजन को पचाता है इसके बाद पचित भोजन जीव के कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है।
- प्राणिसम पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है। मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, मेढ़क, मछली, अमीबा आदि में इसी प्रकार का पोषण होता है।
- मृतजीवी पोषण (Saprophytic Nutrition) : मृतजीवी पोषण में जीव अपना भोजन, मृत जंतु और पौधे के शरीर से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी, मृत जन्तु तथा पौधों में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिक को अपने शरीर में उपस्थित एंजाइम की मदद से तरल (घुलित) कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर उसे अवशोषित कर लेते है। भोजन को तरल रूप से अवशोषित करने के कारण मृतजीवी पोषण को अवशोषक पोषण (Absorptive Nutrition ) भी कहा जाता है।
- स्वपोषण (Autotrophic Nutrition ) : पोषण की वह विधि जिसमें सजीव भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहे, स्वपोषण कहलाता है तथा जिस सजीव में स्वपोषण होता है उसे स्वपोषी (Autotrophs) कहते है।
पौधों में पोषण (Nutrition in Plant)
- पौधे स्वपोषी होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे, जिनमें क्लोरोफील पाया जाता है, मृदा से जल तथा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं एवं ऑक्सीजन को वायुमंडल में उप-उत्पाद (By Product) के रूप में निकालते हैं। पौधों में स्वपोषण की यह प्रक्रिया 'प्रकाश संश्लेषण' कहलाता है।
- प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपने लिए भोजन तैयार करते हैं लेकिन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राणिजगत (Animal kingdom) को भी भोजन की प्राप्ति होती है।
प्रकाश संश्लेषण (Photo Synthesis)
- प्रकाश संश्लेषण एक जटिल रसायनिक प्रतिक्रियाओं का श्रृंखला है जो कोशिका के हरितलवक में स्थित क्लोरोफील सूर्य के विकिरण ऊर्जा के कोशिका के अंदर सम्पन्न होता है। पादप अवशोषित करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा पत्तियों में स्थित जल दो भाग ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विभक्त हो जाता है। ऑक्सीजन पत्तियों के रंध्र से बाहर वायुमंडल में आ जातें हैं तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाते है।
- अतः “प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्लोरोफील की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके, कार्बन डाइआक्साइड और जल से अपना भोजन (ग्लूकोज) बनाते हैं।"

- प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रसायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा, रसायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं। यह रसायनिक ऊर्जा ग्लूकोज के अणुओं में संचित रहते है।
- प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु बनने में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु भाग लेते हैं तथा इसी दौरान ऑक्सीजन के भी 6 अणु मुक्त होते है, जिस कारण पहले यह अनुमान लगाया गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के विभक्त होने से बनता है। लेकिन, अब यह प्रमाणित हो चुका है कि बाहर मुक्त होने वाले ऑक्सीजन का स्त्रोत जल (H2O) है न कि कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक
- सर्वप्रथम जोसेफ प्रीस्टले ने यह सिद्ध किया था कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है।
- प्रीस्टले के बाद जॉन इंगेन हौज ने यह सिद्ध किया कि हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध (ऑक्सीजन) बना सकता है। जॉन इंगेज हॉज के प्रयोग से पता चला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफील तथा सूर्य का प्रकाश दोनों जरूरी है।
- एण्टनी लेवांजियर (Antony Lavoisier) यह साबित किया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहाण करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं।
- रॉबर्ट मायर ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट किया, वे अपने प्रयोगों से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी पोधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफील द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रसायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते है।
- प्रोफेसर ब्लैकमैन ने यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण न केवल प्रकाश रसायनिक क्रिया है, बल्कि यह जीव रसायनिक (Biochemical) क्रिया भी है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य पदार्थ
- प्रकाश संश्लेषण हेतु चार पदार्थों की आवश्यकता होती है। इनमें किसी एक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। यह चार पदार्थ निम्नलिखित हैं-
- कार्बन डाइऑक्साइड : प्रकाश संश्लेषण हेतु पौधे CO2 वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। पोधे के पत्तियों में पाये जानेवाले रंध्र (Stomata) के द्वारा CO2 वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है। जलीय पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण न कर जल में घुले बाइकार्बोनेट से CO2 ग्रहण करते है।
- जल : जल प्रकाश संश्लेषण हेतु अनिवार्य है परंतु प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं में भी पौधों को जल की आवश्यकता होती है। जल, पौधा मृदा से जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जड़ों द्वारा सोखा गया जल जाइलम उत्तक के द्वारा पौधों के पत्तियों तक पहुँचता है।
- सूर्य का प्रकाश : प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में अथवा अंधरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। कोई भी कृत्रिम प्रकाश जिससे विकिरण ऊर्जा निकलती है, उस प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है।
- क्लोरोफील : प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफील एक महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य घटक है जो हरितलवक में पाया जाता है। क्लोरोफील ही सूर्य के प्रकाश ऊर्जा (या विकिरण ऊर्जा) की टैप कर उसे रसायनिक ऊर्जा में बदलते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएँ (Phases of Photosynthesis)
- प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है, जो दो चरणों (Phase) में सम्पन्न होता है-
- प्रकाश अभिक्रिया (Light Reaction )
- यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरितलवक के ग्राना वाले भाग में होता है। इस अभिक्रिया की खोज हिल (Hill) नामक वैज्ञानिक ने की थी जिसके कारण इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया में निम्नलिखित क्रियाएँ क्रमिक रूप से होती है-
- सर्वप्रथम क्लोरोफील, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते है। क्लोरोफील एक अणु है जो परमाणुओं से बना है। सूर्य प्रकाश के फोटॉन द्वारा क्लोरोफील परमाणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते है।
- इसके बाद जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल के प्रकाशिक अपघटन से H तथा OH आयन बनते है। OH आयन से पुन: O2 तथा H2O का निर्माण होता है। O2 वातावरण में मुक्त हो जाता है।

- जल के प्रकाशिक अपघटन से निकले Ht को विशेष प्रकार के हाइड्रोजन ग्राही विटामिन NADP+ (Nicotinamide Adeuine Dinucleotide Phosphate) ग्रहण कर लेता है।
4H+ + 4e- + 2NADP → 2NADH2
- इसके बाद पौधे में पाये जाने वाले ADP (Adenosine diphosphate) तथा फॉस्फोरस आपस में मिलकर ATP नामक यौगिक का निर्माण करते है। ATP बनने की प्रक्रिया को प्रकाश फॉस्फेटीकरण (Photophosphorylation) कहा जाता है।
- प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में NADPH, एवं ATP का निर्माण होता है। NADPH 2 तथा ATP का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था या अप्रकाशिय अभिक्रिया (Dark Reaction) में होता है।
- यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरितलवक के ग्राना वाले भाग में होता है। इस अभिक्रिया की खोज हिल (Hill) नामक वैज्ञानिक ने की थी जिसके कारण इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया में निम्नलिखित क्रियाएँ क्रमिक रूप से होती है-
- अप्रकाशिक अभिक्रिया (Dark Reaction)
- इसे अप्रकाशिक (Dark) अभिक्रिया इसलिए नहीं कहते हैं कि यह अँधेरे ( प्रकाश की अनुपस्थिति) में होता है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि इस अभिक्रिया हेतु प्रकाश की जरूरत नहीं है।
- अप्रकाशीय अभिक्रिया हरितलवक के स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश अभिक्रिया में बने NADPH2 तथा ATP की सहायता से सम्पन्न होता है।
- अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मेल्विन कालविन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस कार्य के लिए 1961 में कालविन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रकाशिक अभिक्रिया को Calvin-cycle भी कहा जाता है। Calvin-cycle तीन चरणों में पूर्ण होता है-
- कार्बोक्सिलीकरण : Calvin-cycle के दौरान हरित लवक के स्ट्रोमा में दो रसायन RuBP (Ribolose biphosphate) तथा रूबिस्को एंजाइम मौजूद रहता है। रूबिस्को एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में CO2 का RuBP से संयोजन कार्बोकिसलीकरण कहा जाता है। CO2 तथा RuBP के संयोजन से PGA (Phosphoglyceric Acid) का निर्माण होता है। PGA प्रकार संश्लेषण के कालविन चक्र का प्रथम स्थायी यौगिक है।
- अपचयन (Reduction ) : यह अभिक्रियाओं अणुओं से मिलकर फॉस्फोग्लीसेरलडीहाइड की एक श्रृंखला है। इस क्रिया में PGA, ATP है। बनाता है, जो ग्लूकोज का निर्माण करता है।
- पुनर्जनन ( Regneration) : इस क्रिया RuBP के अणु का निर्माण पुनः हो जाता है जिसका उपयोग कार्बोक्सिलीकरण में हुआ था । RuBP के पुनः निर्माण होने से Calvin-cycle बिना किसी बाधा के निरंतर जारी रहता है।
- Calvin-cycle में CO2 के प्रत्येक अणु के स्थिरिकरण के लिए ATP के तीन अणु तथा NADPH2 के दो अणु की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु Calvin-cycle से 6 चक्कर की आवश्यकता होती हैं जिससे 6 अणु CO2 के स्थिरिकरण या ग्लूकोज में बदलने हेतु 18 ATP तथा 12 NADPH2 का जरूरत पड़ती है । सम्पूर्ण अप्रकाशिक अभिक्रिया या Calvin-cycle को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है-
6RuBP + 6CO2 + 18ATP + 12 NADPH2→ 6 RuBP + C6H12O6 + 18 ADP + 18P + 12 NADP
- प्रकाश अभिक्रिया (Light Reaction )
प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक
- प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बाह्य कारक तथा आंतरिक कारक । ताप, प्रकाश, CO2 तथा जल बाह्य कारक है तथा क्लोरोफील की मात्रा, जीवद्रव्य, कोशिका में संचित भोजन की मात्रा और पत्ती की आंतरिक संरचना आंतरिक है।
- ताप : लगभग 30°C से 35°C ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। इससे अधिक ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। गर्म प्रदेशों में 5°C से नीचे ताप पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है।
- प्रकाश : पत्तियों तक जो प्रकाश पहुँचता है उसका 80 प्रतिशत पत्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है, शेष प्रकाश परावर्तित हो जाते है। लेकिन पत्तियों द्वारा अवशोषित प्रकाश का मात्र 0.5 से 3.5 प्रतिशत ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है।
- प्रकाश की तीव्रता : प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है परंतु प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ने से प्रकाश-संश्लेषण रूक जाती है।
- प्रकाश के गुण: प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य में होती है। पौधे लाल तरंगदैर्ध्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं जबकि नीली तरंगदैर्ध्य दूसरे स्थान पर रहती है। पीली और हरी तरंगदैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है।
- प्रकाश का अवधि : प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रतिदिन 10 से 12 घंटे का प्रकाश पर्याप्त होता है। इससे अधिक देर तक प्रकाश की उपलब्धता पर प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- कार्बन डाइऑक्साइड : कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक (limiting factor) कहा जाता है। CO2 की 0.03% मात्रा प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्याप्त है। इसकी मात्रा में वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण उसी दर से बढ़ जाती है परंतु CO2 की मात्रा लगातार बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण के दर में कमी आती है।
- जल : पौधे द्वारा अवशोषित जल का मात्र 1 प्रतिशत ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। पौधे को अगर जल की कमी हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है।
मानव शरीर में पोषण Nutrition in Human Body
- मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में प्राणिसम पोषण (Holozoic क्रियाओं-अन्तर्ग्रहण (Ingestion), पाचन (Digestion), अवश अवशोषण utrition) होता है। प्राणिसम जीवों में पोषण पांच (Absorption), स्वांगीकरण (Assimilation) तथा बहिष्करण या मल त्याग (Egestion) द्वारा सम्पन्न होती है। मनुष्य में भी ये सभी क्रियाएँ होती है।
- पोषण के पाँच क्रियाओं में पाचन सबसे महत्वपूर्ण है। पाचन की क्रिया में ठोस, जटिल बड़े-बड़े अघुलनशील भोजन- अणु विभिन्न एंजाइम की सहायता से तरल सरल, छोटे-छोटे अणुओं में विभक्त हो जाते है।
- मनुष्य में पाचन हेतु एक विकसित पाचन तंत्र (Digestive system) पाया जाता है। यह पाचन तंत्र आहारनाल (Alimentary Canal) एवं इससे संबंधित विभिन्न पाचक ग्रंथि से मिलकर बना है। मनुष्य का आहारनाल 8 से 10 मीटर तक की होती है।
- मनुष्य के आहारनाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है-
- मुख गुहा (Buccal Cavity )
- मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान है जो मुँह के रास्ते से खुलता है तथा जबड़े तथा होठो के माध्यम से बंद होता है। मनुष्य के दो जबड़े में निचला जबड़ा गतिशील होते हैं। मुखगुहा के अंदर के ऊपर वाले हिस्से तालु (Palate) कहलाता है तथा पार्श्व (lateral) के मांसल भाग को गाल कहते है।
- मुखगुहा के भीतर तीन प्रमुख संरचनाएँ- दाँत (Teeth), जीभ (Tongue) तथा लार ग्रंथि (Salivary gland) मौजूद है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- दाँत (Teeth)
- मनुष्य के दाँत को तीन हिस्सों में बाँटा गया है। दाँत का वह भाग जो मसूढ़े के ऊपर निकला रहता है, सिर (Crown) कहलाता है तथा मसूढ़े के अंदर रहने वाले भाग को जड़ (Root) कहे हैं। सिर तथा जड़ के बीच दाँतों के पतले भाग को ग्रीवा (Neck) कहते है।
- दाँतों के संरचना में मज्जा गुहा (Pulp cavity) दंतास्थि (Dentine ) तथा इनामेल आते है। दाँतों के सबसे भीतरी संरचना मज्जा गुहा से बना होता है, इस भाग में रू रवाहिनी तथा तंत्रिका - सूत्र भरे होते हैं। मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्थित आते है। दंतास्थि ही दाँतों के अधिकांश भाग को तैयार करते है। दंतास्थि एक उत्तक है जो हड्डी से भी ज्यादा कड़ा तथा हल्के पले रंग का होता है । दाँत के सिर (Crown) वाले भाग के ऊपर इनामेल (Enamel) का परत चढ़ा रहता है । दाँत इनामेल के कारण ही देखने में श्वेत प्रतीत होते है।
- दाँतों का इनामेल कैल्सियम फॉस्फेट से बनता है जो जल में अविलेय है, किन्तु मुँह का pH 5.5 से कम हो जाने पर इनामेल का क्षय होने लगता है। दाँतों का यह इनामेल मानव शरीर का सबसे कड़ा भाग है।
- मनुष्य के पूरे जीवन काल में दाँत दो बार निकलते हैं। जन्म के बाद जो दाँत निकलते हैं उसे दूध दाँत (Milk Teeth) कहते है। दूध दाँत की संख्या 20 होती है 10 ऊपरी जबड़े में और 10 नीचले जबड़े में। 6 से 7 वर्ष उम्र के बाद दूध दाँत एक-एक करके टूटने लगते हैं तथा तथा उसके स्थान नये दाँत आ जाते है। इस नये दाँत को स्थायी दाँत कहते है। स्थायी दाँत 32 होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े तथा 16 निचले जबड़े में।
- स्थायी दाँत (Permanent Teeth) चार प्रकार के होते है-
Incisor ( कर्तनक) : यह दाँत पकड़ने तथा काटने के काम आते है। ऊपरी तथा # नीचले जबड़े में इसकी संख्या 4-4 होती है।Canine (भेदक) : यह दाँत फाड़ने के काम आते है। ऊपरी तथा नीचले जबड़ में इसकी संख्या 2-2 होते है ।Premolar : यह कुचलने वाले दाँत है। ऊपरी तथा नीचले जबड़े में इसकी संख्या 4-4 होती है।Molar : यह चबाने वाले दाँत हैं। ऊपरी तथा नीचले जबड़े में इसकी संख्या 6-6 होती है।
- बच्चों के दूध दाँत में प्रीमोलर तथा अंतिम मोलर दाँत का अभाव रहता है। मनुष्य के पूरे जीवनकाल में कुल 52 दाँत निकलते है।
- जन्म के बाद मनुष्य में दो बार दाँत निकलते है, इस अवस्था को Diphyodont कहा जाता है। मनुष्य में चार प्रकार के दाँत पाये जाते हैं, ऐसे दाँत वाले प्राणी Heterodont कहलाते हैं।
- जीभ (Tongue)
- जीभ एक मांसल सांचना है, निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जाते हैं-
- यह लार ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले लार (Saliva) को भोजन के साथ मिलाता है।
- जीभ के द्वारा भोजन का स्वाद ग्रहण किया जाता है, जिसके बाद हमें स्वाद की अनुभूति होती है।
- यह दाँत की भीतरी सतहों को साफ एवं चिकना रखती है।
- भोजन निगलने में जीभ मदद देती है।
- जीभ हमें बोलने में मदद करती है।
- जीभ की सतह पर तीन प्रकार रोएंदार रचनाएँ पाई जाती है, जिन्हें पैपिला (Papilla) कहा जाता है। पैपिला में स्वाद कलिकाएँ (Taste Bud) पाये जाते है जो स्वाद ग्रहण का कार्य करती है।
- जीभ के ऊपरी बीच वाली सतह पर जो पैपिला होते हैं, उसे फिलीफॉर्म पैपिला कहा जाता है। इस पैपिला में कोई स्वाद कलिकाएँ मौजूद नहीं रहता है।
- जीभ के दाँये तथा बाएँ किनारे-किनारे फैले पैपिला को फंगीफॉर्म पैपिला कहते हैं। इस पैपिला में नमकीन मीठा तथा खट्टा स्वाद ग्रहण करने वाली स्वाद नलिकाएँ पायी जाती है।
- जीभ के पिछले सतह पर सरकमभैलेट पैपिला पाया जाता है जिसमें तीखा स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पायी जाती है।
- जीभ एक मांसल सांचना है, निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जाते हैं-
- लार ग्रंथियाँ (Salivary glands) -
- मनुष्य के मुख-गुहा में कुल तीन जोड़ी लार ग्रंथि पायी जाती है। इस ग्रंथि में नली (Duct ) पायी जाती है, अतः यह बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है।
- तीन जोड़ी लार-ग्रंथि में पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है जो दोनों कान के पास पायी जाती है। एक जोड़ी सबलिंगुल ग्रंथि जीभ के दोनों बगल में तथा एक जोड़ी सबमेडिबुलर थि जबड़े के नीचे पाये जाते है।
- सभी लार ग्रंथियाँ लार को स्त्रवित करता है। प्रतिदिन मानव में 1-11/2 लीटर लार (Saliva) स्त्रावित होता है। लार एक क्षारीय तरल पदार्थ है। लार में 99.2 प्रतिशत जल पाये जाते है। जल के अतिरिक्त लार में Na+, K+, Cl- म्यूकस तथा दो प्रकार के एंजाइम टायलिन (Ptylin) तथा लाइसोजाइम ( Lysozyme) पाये जाते है।
- लार में उपस्थित टायलीन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड ( Starch) को डेक्सट्रीन तथा माल्टोजम में परिवर्तित कर देता है।

- इस तरह भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शरू हो जाता है तथा सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट (Starch) का पाचन होता है। भोजन में उपस्थित लगभग 30 प्रतिशत स्टार्च का ही पाचन मुखगुहा में हो पाता है।
- लार भोजन को नरम तथा लसदार बनाता है एवं घुलनशील पदार्थ को घुलाकर स्वाद का बोध कराता है। लार का लाइसोजाइम एंजाइम के प्रभाव से भोजन के साथ मुखगुहा में आये जीवाणु नष्ट हो जाते है।
- दाँत (Teeth)
- ग्रसनी (Pharynx)
- मुखगुहा के पीछले हिस्से को ग्रसनी कहते है । ग्रसनी में दो छिद्र होते है - Gullet तथा Glottis / Gullet आहार नाल के अगले भाग ग्रासनली में खुलता है। भोजन Gullet छिद्र से होकर ग्रासनली में आ जाता है।
- Glottis छिद्र श्वासनली ( Trachea ) में खुलता है। भोजन तथा पानी Glottis छिद्र में प्रवेश न करे, इस हेतु Glottis के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसे Epiglottis कहते है । ग्रसनी में जब भोजन तथा पानी आते है Epiglottis, glottis को बंद कर देता है, पुनः उसे खोल देता है। इस तरह Glottis से होकर कंवल हवा ही प्रवेश कर पाता है।
- ग्रासनली (Oesophagus)
- ग्रसनी के बाद आहार नाल का अगला भाग ग्रासनली है। भोजन ग्रसनी से gullet छिद्र द्वारा ग्रासनली में आ जाता है। भोजन का ग्रसनी से ग्रासनली में आना निगलना कहलाता है।
- भोजन जैसे ही ग्रासनली में पहुँचता है वैसे ही इसकी भित्ति में एक गति उत्पन्न होती है। इस गति को क्रमानुकुंचन गति (Peristaltic Waves) कहते है। इस गति के कारण भोजन ग्रासनली से अमाशय में आ जाते है।
- ग्रासनली की लंबाई लगभग 10-12 इंच होता है तथा इसमें भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है।
- अमाशय (Stomach)
- अमाशय एक चौड़ी थैली के समान संरचना है जो उदर गुहा (Abdominal cavity) के बाएँ भाग में मौजूद रहता है। मनुष्य का अमाशय तीन हिस्सों में बँटी रहती है। अमाशय के अग्र भाग कार्डिएक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। कार्डिएक तथा पाइलोरिक भाग के बीच वाले भाग को फुण्डिक भाग कहते है।
- अमाशय के भीतरी दिवारों पर स्तंभाकार एपीथीलिक उत्तक के कोशिकाएँ धँसकर जठर ग्रथि (Gastric gland) का निर्माण करता है।
- जठर ग्रंथि में तीन प्रकार के कोशिकाएँ मौजूद रहती है। ये कोशिकाएँ है- म्यूकस कोशिकाएँ, अम्लजन कोशिकाएँ (Parital cell) तथा जाइमोजेन कोशिकाएँ। जठर ग्रंथि की तीनों कोशिकाएँ से प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस (Gastric Juice) का स्त्रावण होता है।
- जठर रस में जल 0.4 प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजन एंजाइम तथा म्यूकस मौजूद रहते है।
- जठर रस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCI) टायलीन एंजाइम की क्रिया को रोक देता है, भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है।
- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से जठर रस में मौजूद पेप्सिनोजेन एंजाइम सक्रिय पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करते है। पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओजेज में परिवर्तित कर देता है।

- अमाशय प्रोटीन पांचन का प्रमुख स्थान है। सर्वप्रथम प्रोटीन का पाचन इसी भाग में होता है। परंतु अमाशय में प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहा बालक आशक पाचन ही होता है।
- जठर रस के साथ स्त्रावित होने वाला म्यूकस अमाशय की दिवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन एंजाइम के प्रभाव से बचाये रखता है।
- कभी-कभी जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव अधिक हो जाता है जिससे म्यूकस का स्त्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के दिवारों को क्षतिग्रस्त कर उसमें घाव उत्पन्न कर देता है। इस घाव को अल्सर कहते है ।
- ऐसे व्यक्ति को अल्सर ( Peptic Ulcer) होने की संभावना ज्यादा रहता है जो लंबे समय तक भूखे ही रह जाते है।
- अमाशय के प्रोटीन के अतिरिक्त वसा का भी आंशिक रूप से पाचन शुरू हो जाता है। वसा पचाने हेतु अमाशय से गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम स्त्रावित होता है जो वसा को वसा अम्ल (Fatty Acid) तथा ग्लिसरॉल (Glycerol) से परिवर्तित कर देता है।

- शिशु के अमाशय के जठर ग्रंथि से प्रोरेनिन एंजाइम का स्त्राव होता है। प्रोरेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है।
- अमाशय में भोजन चार से पाँच घंटे तक रहता है जिससे भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई के समान हो जाता है, भोजन के इस स्वरूप को काइम (Chyme) कहते हैं। काइम आहारनाल के अगले भाग छोटी आँत में प्रवेश कर जाता है।
- जिस रास्ते से भोजन ग्रासनली से अमाशय में प्रवेश करता है उसे कार्डिएक ऑरिफिश कहते है तथा जिस रास्ते से भोजन अमाशय से छोटी आँत में प्रवेश करता है उसे पायलोरिक ऑरिफिश कहते है।
- छोटी आँत ( Small Intestine)
- छोटी आँत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह 6 मीटर लम्बी तथा 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। शाकाहारी जीवों का छोटी आँत मांसाहारी जीवों के तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी होती है।
- मनुष्य का छोटी आँत के तीन भाग होते है। छोटी आँत का अग्रभाग ग्रहणी (Duodenum) कहलाता है। ग्रहणी के बाद छोटी आंत के दो भाग क्रमशः जेजुनम तथा इलियम होता है।
- छोटी आँत का सबसे बड़ा तथा प्रधान भाग इलियम है। इसी भाग में अधिकतर भोजन का पाचन होता है। ग्रहणी छोटी आँत का सबसे छोटा भाग है।
- छोटी आँत के ग्रहणी वाले भाग में आहारनाल के प्रमुख पाचक ग्रंथि यकृत तथा अग्न्याशय की नली आकर खुलती है। भोजन जैसे ही ग्रहणी में पहुँचता है, सबसे पहले यकृत का पित्त रस तथा उसके बाद अग्न्याशय के अग्न्याशयी रस भोजन में आकर मिलते है तथा भोजन का पाचन करते हैं।
- यकृत (Liver)
- यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत के कोशिकाओं द्वारा पित्त रस (Biole Juice) तैयार होता है जो यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय (Gall bladder) में जमा रहते हैं ।
- पित्त रस गाढा तथा हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसमें 86 प्रतिशत जल शेष पित्त लवण तथा पित्त कणिकाएँ पाये जाते हैं। पित्त रस में भोजन को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है।
- भोजन जैसे ही छोटी आँत के ग्रहणी में आता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलकर नली द्वारा ग्रहणी में आ जाते हैं। पित्त रस के दो प्रमुख कार्य होते हैं-
- यह अमाशय से आये अम्लीय भोजन (Chyme) को क्षारीय बनाता है ताकि अग्न्याश्य का अग्न्याशयी रस भोजन को पचा सके।
- यह वसा अणुओं को तोड़कर, उसका पायसीकरण (Emulsification) करते हैं ताकि वसा का पाचन हो सके। बिना पायसीकरण का आहारनाल में वसा का पाचन संभव नहीं है।
- यकृत का प्रमुख कार्य है- पित्त रस का निर्माण करना। इसके अतिरिक्त यकृत अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जो निम्न है-
- यह विटामिन A का संश्लेषण करता है तथा उसे संचित रखता है।
- विटामिन A के अतिरिक्त यकृत कई कार्बनिक यौगिकों का संग्रह करता है। यह लाल रक्त कण (RBC) के निर्माण हेतु लोहे (Fe) का भी संचय करता है।
- यकृत शरीर में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रखता है।
- यकृत में बड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। रक्त स्कंदन में काम आने वाला फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण यकृत में ही होता है।
- यकृत में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा से कॉलेस्टेरॉल का भी निर्माण होता है।
- यकृत शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है।
- अग्न्याश्य (Pancreas)
- अग्न्याशय अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। अग्न्याशय बाह्य स्त्रावी तथा अत:स्त्रावी दोनों ग्रंथि के समान कार्य करता है, जिस कारण इसे मिश्रीत ग्रंथि भी कहा जाता है।
- अग्न्याशय मुख्य रूप से एसीनर कोशिकाएँ का बना होता है। इन कोशिकाओं से अग्न्याशयी रस (Pancreatic Juice) स्त्रावित होता है जिसमें कई प्रकार के पाचन एंजाइम होते है। एसीनर कोशिकाओं के बीच-बीच में a, B तथा y नाम की छोटी-छोटी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, जिसे लैंगरहैंस द्वीपिका (Islet's of Langerhens) कहते है। लैंगर हैंस द्वीपिका से हार्मोन का स्त्राव होता है।
- अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा स्त्रावित अग्न्याशयी रस में भोजन के सभी अवयवों का पाचन करने वाला एंजाइम मौजूद होता है, जिस कारण अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक एंजाइम (Complete Digestive Enzyme) कहते है ।
- ग्रहणी में पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस की क्रिया होने के बाद भोजन जेजुनम और अंततः इलियम में आ जाता है। इलियम में भोजन के आते ही छोटी आंत की दिवारों पर स्थित ग्रंथि से क्षारीय आंत्र रस या सक्कस एंटेरीकस का स्त्राव होता है।, जो भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है।
- आंत्र-रस (Succus entericus) में पाये जाने वाले एंजाइम तथा उनके द्वारा होने वाले प्रतिक्रिया निम्न है-
- पेप्टाइडेज एंजाइम पेप्टोन को एमीनो अम्ल में बदल देते हैं।
- लाइपेस एंजाइम बचा हुआ वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते है।
- माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोस में परिवर्तित कर देते है।
- लैक्टेज एंजाइम लेक्टोज को ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में बदल देते है।
- इनवर्टेस एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज तथा प्रक्टोज में परिवर्तित करते है।
- इरेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड (प्रोटीन के भाग) को एमीनो अम्ल में बदल देता है।
- मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर आंत्र रस स्त्रावित होता है। आंत्र रस के प्रतिक्रिया के बाद भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में सम्पन्न हो जाता है।
- भोजन के पूर्ण पाचन होने के बाद प्रोटीन से अमीनो अम्ल, वसा से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट (स्टार्च, ग्लाइकोजेन) से सरल कार्बोहाइड्रेट (ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज) बनते है।
- छोटी आँत के इलियम वाले भाग में न सिर्फ भोजन का पूर्ण पाचन होता है बल्कि पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है जो इलियम के कोशिकाओं में मौजूद रसाकुर ( Villi) द्वारा विसरण विधि से होता है।
- अवशोषण के उपरांत भोजन इलियम के रसाकुर में स्थित रूधिर वाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं तथा रूधिर - संचार द्वारा शरीर के समस्त अंगों के कोशिकाओं में वितरित हो जाते है।
- छोटी आंत में पचन के उपरांत भोजन तरल रूप में परिवर्तित हो जाते है। भोजन के इस स्वरूप को चाइल (Chyle) कहते है ।
- यकृत (Liver)
- बड़ी आँत (Large Intestine)
- छोटी आँत आहारनाल के अगले भाग बड़ी आँत में खुलती है। बड़ी आँत आहारनाल का अंतिम भाग है। बड़ी आंत छोटी आँत के तुलना में अधिक चौड़ी, परंतु लंबाई में छोटी होती है।
- बड़ी आँत के दो भाग होते हैं- कोलन (Colon) तथा मलाशय (Rectum)। छोटी आँत में पाचन तथा अवशोषण के उपरांत बचे अपचा तथा अवशिष्ट भोजन बड़ी आँत के कोलन में आ जाता है। कोलन में अवशिष्ट भोजन का जल अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन रेक्टम में संचित हो जाता है, जहाँ से यह समय-समय पर मलद्वार (Anus) के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है।
- छोटी आँत तथा बड़ी आँत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, जिसे सीकम (Caecum) कहते है। सीकम के शीर्ष पर एक अँगुली जैसी रचना होती है जिसे ऐपेंडिक्स (Appendix ) कहते है। सीकम तथा ऐपेंडिक्स दोनों ही मानव शरीर के अवशेषी अंग है।
- बड़ी आँत में किसी प्रकार का एंजाइम स्त्राव नहीं होता है। इस भाग में बिना पचे हुए भोजन का कुछ समय के लिए संग्रह होता है।
- मुख गुहा (Buccal Cavity )
आहारनाल में स्त्रावित होने वाला हॉर्मोन
- आहारनाल के विभिन्न भागों में कुछ हॉर्मोन का भी स्त्राव होता है जो भोजन के पाचन पर नियंत्रण रखता हैं आहारनाल में स्त्रावित होने वाला प्रमुख हॉर्मोन निम्न है-
- गैस्ट्रीन (Gastrin ) : यह हॉर्मोन अमाशय के दिवार से स्त्रावित होता है। यह हॉर्मोन अमाशय के जठर-ग्रंथि से जठर रस का स्त्राव करवाता है।
- कोलीसिस्टोकाइनीन (Cholecystokinin ) : यह हॉर्मोन पित्ताशय को उत्तेजित करता है जिससे पित्ताशय से पित्त रस निकलकर ग्रहणी में प्रवेश करते है ।
- सेक्रेटिन (Secretin): यह अग्न्याशय को उत्तेजित करता है, जिसके फलस्वरूप अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलकर ग्रहणी में आते है।
- इंटेरोगेस्टेरोन (Enterogesterone) : यह हॉर्मोन गैस्ट्रीन हॉर्मोन की सक्रियता को रोकता है ताकि अमाशय के जठर ग्रोथ से ज्यादा जठर रस नहीं स्त्रावित हो ।
अभ्यास प्रश्न
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







