General Competition | Science | Biology (जीव विज्ञान) | पौधों और मानव' में श्वसन
सजीवों के शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शरीर में श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है।
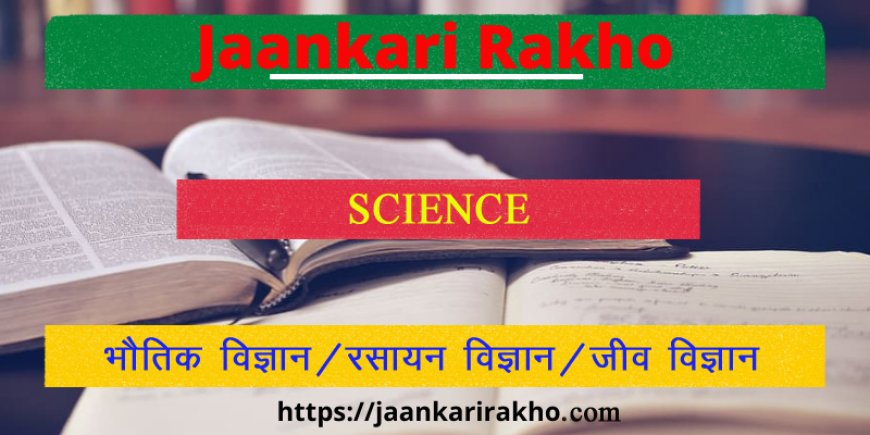
General Competition | Science | Biology (जीव विज्ञान) | पौधों और मानव' में श्वसन
- सजीवों के शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए अनवरत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शरीर में श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है।
- श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के भीतर भोजन (glucose) का ऑक्सीजन तथा एंजाइम के मदद से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है।
- श्वसन की प्रक्रिया शरीर के कोशिकाओं में होता है, जिसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है-
भोजन (glucose) + ऑक्सीजन → कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊर्जा
- श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन अपशिष्ट के रूप बनते हैं जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन के उपरांत जल भी बनते हैं परंतु जल को श्वसन-अपशिष्ट नहीं कहा जाता है क्योंकि जल शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते है।
- श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का कोशिकाओं द्वारा तुरन्त उपयोग नहीं होता है, बल्कि यह ऊर्जा कोशिका में ही ATP अणुओं के रूप में संचित हो जाता है और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ATP अणु टूटकर ऊर्जा निर्मुक्त कर देते है।
- श्वसन के दौरान बने समस्त ऊर्जा ATP अणु के रूप में परिवर्तित हो जाते है। कोशिकाओं के भीतर ATP का निर्माण हेतु ADP तथा फॉस्फेट अणुओं की आवश्यकता होती है, जो कोशिका में मौजूद रहता है।
ADP + फॉस्फेट + ऊर्जा (श्वसन से बना ) → ATP
- कोशिका के भीतर जब ऊर्जा की जरूरत होती है, जल के सहायता से ATP अणु को विखंडित कर दिया जाता है-
ATP → ADP + फॉस्फेट + ऊर्जा
- श्वसन में इस्तेमाल होने वाले भोजन (glucose) को कोशिकीय ईंधन कहते तथा श्वसन के दौरान बने ATP (Adenosine Di-Phosphate) को ऊर्जा-करेंसी कहते है।
श्वसन के प्रकार (Types of Respiration)
- कोशिकाओं में होने वाला श्वसन दो प्रकार के होते हैं- वायवयी (ऑक्सी) श्वसन तथा अवायवीय (अनॉक्सी) श्वसन ।
- यदि कोशिका में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर ATP बनता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते है।
- अगर कोशिका में माइटोकॉण्ड्रिया नहीं हो तो उस स्थिति में भी अवायवीय श्वसन ही होते है। प्रोकैरोयोटीक कोशिका से बने जीव जैसे- जीवाणु में माइटोकॉण्ड्रिया नहीं होते हैं, उन जीवों में अवायवीय श्वसन ही होती है।
- जीवाणु तथा पौधे के कोशिका में अवायवीय श्वसन होने पर इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2ATP अणु का निर्माण होता है।

- जीवाणु के कोशिका में माइटोकॉण्ड्रिया नहीं होते हैं, अतः इसमें हमेशा अवायवीय श्वसन ही होता है। पौधे के कोशिका में अवायवीय श्वसन उस स्थिति में होता है जब पौधों के कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
- जंतुओं तथा मानव के कोशिका में भी जब कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, तब कोशिका में अवायवीय श्वसन शुरू हो जाता है। जंतुओं तथा मानव में अवायवीय श्वसन होने पर लैक्टीक अम्ल तथा 2ATP ऊर्जा उत्पन्न होते है।

- जब व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करता है अथवा जल्दी-जल्दी कार्य करता है, इस स्थिति में पेशी कोशिकाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन शुरू के कारण पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनता है जो पेशीय जकड़न या ऐंठन उत्पन्न करता है।
- वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसके अतिरिक्त वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉण्ड्रिया का होना अनिवार्य है।
- वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉण्ड्रिया के मदद से सम्पन्न होता है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 38ATP अणु का निर्माण होता है।

श्वसन अभिक्रिया (Respiration Reactions)
- कोशिका में दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बाद श्वसन सम्पन्न होता है। सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होती है उसके बाद क्रेब्स चक्र अभिक्रिया होता है।
- श्वसन के दौरान सर्वप्रथम गलाइकोलाइसिस होता है। यह अभिक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में सम्पन्न होता है।
- ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप पायरूत्रिक अम्ल तथा 2ATP ऊर्जा बनता है।
C6H12O6 →2C3H4O3 +4[H] + 2ATP
- ग्लाइकोलाइसिस में चार हाइड्रोजन परमाणु भी बनते है। यह H - परमाणु माइटोकॉण्ड्रिया में जाकर GATP ऊर्जा बनाने में सक्षम होता है परन्तु माइटोकॉण्ड्रिया कोशिका में नहीं रहने पर यह H - परमाणु इथाइल ऐल्कोहॉल या लैक्टिक अम्ल बनने में खर्च हो जाता है।
- इस अभिक्रिया की खोज हेन्स क्रेब्स ने किया था जिसके कारण इसे क्रेव्स साइकिल कहा जाता है। यह अभिक्रिया या साइकिल कोशिका के माइटोकॉण्ड्रिया में होता है। माइटोकॉण्ड्रिया की अनुपस्थिति में क्रेब्स - साइकिल नहीं हो सकता है।
- क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने पायरूवेट अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा प्रत्येक पायरूविक अम्ल से 15ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
- एक ग्लूकोज अणु से दो अणु पायरूविक अम्ल ग्लाइकोसिस के दौरान बना है था । अतः क्रेब्स - साइकिल में दो पायरूत्रिक अम्ल से 30ATP ऊर्जा का निर्माण होता है।
- ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेव्स साइकिल के उपरांत श्वसन सम्पन्न हो जाता है और 1-glucose अणु से 38ATP ऊर्जा का निर्माण होता है।
वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर
(Difference between Aerobic and Anaerobic Respiration)
- वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉण्ड्रिया का होना अनिवार्य है जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका के कोशिकाद्रव्य में ही सम्पन्न हो जाती है।
- वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
- वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज इथाइल ऐल्कोहॉल या लैक्टिक अम्ल बनाते है।
- वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु 38ATP ऊर्जा निर्माण कर सकता है जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से केवल 2ATP ऊर्जा का ही निर्माण होता है।
- वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल दोनों होते हैं जबकि अवायवीय श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है।
श्वसन- भागफल (Respiratory Quotient)
- श्वसन क्रिया में निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक कहते है।
श्वसन गुणांक = निष्कासित CO2 का आयतन / अवशोषित O2 का आयतन
- श्वसन प्रक्रिया में जब कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है तब श्वसन भागलफल का मान 1 होता है लेकिन जब प्रोटीन तथा वसा का इस्तेमाल होता है तब श्वसन भागलफल 1 से कम होता है। श्वसन प्रक्रिया में कभी भी शुद्ध वसा तथा प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होता है।
बाह्य श्वसन (External Respiration)
- पौधों तथा जन्तु में मुख्य रूप से वायवीय श्वसन पाये जाते है। वायवीय श्वसन में साँस लेने तथा साँस छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। बाह्य श्वसन पौधे तथा जन्तुओं में अलग-अलग तरीके से होते है ।
- पौधो में बाह्य श्वसन-
- पौधों में श्वसन गैसों का आदान-प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधे विसरण विधि द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते है। पौधों का सभी भाग अलग-अलग श्वसन करते है।
- पौधे की जड़े में पाया जाने वाला मूलरोम मिट्टी के कणों से बीच फँसे वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में ही छोड़ देते है।
- जलीय पौधे जल में घुले ऑक्सीजन को विसरण विधि द्वारा प्राप्त करते है तथा जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर देते है।
- बड़े पौधे के तना या शाकीय पौधे के पाये जाते है। श्वसन गैस (O2 तथा CO2) का आदान-प्रदान हेतु वातरन्ध्र (lenticels) पाये जाते है। छोटे तना में वातरंध्र का अभाव होता है, इन पौधों के तना में गैसीय आदान-प्रदान हेतु रंध्र (Stomata) पाये जाते है।
- पौधों की पत्तियों में श्वसन गैसों का आदान-प्रदान रंध्र (Stomata) के द्वारा होता है ।
- पौधा की पत्तियाँ दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है क्योंकि दिन में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होते रहता है, लेकिन पत्तियाँ रात में श्वसन हेतु वातवरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होने ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है।
- पौधों में होने वाले बाह्य श्वसन की तीन प्रमुख विशेषताएँ-
- पौधों के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती अलग-अलग श्वसन करते है।
- पौधों में श्वसन गैसों का विसरण नहीं होता है, इसके विपरित जंतुओं या मानव में श्वसन गैसों का विसरण होता है।
- पौधों को जीवन-यापन हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है।
विभिन्न प्रकार के जंतुओं में बाह्य श्वसन
- मोनेरा तथा प्रोटिस्टा समुदाय के एक कोशिकृति जीवों में इस गम (O2 तथा CO2) का आदान-प्रदान कोशिका झिल्ली से श्वसन 2 विसरण विधि द्वारा होता है। मोनेरा समुदाय के जीवों में केवल अवायवीय श्वसन होता है, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है।
- पोरीफेरा (स्पंज) तथा सीलेंटेरेटा / निडेरिया (हाइड्रा) संघ के जीवों में भी श्वसन गैसों का आदान-प्रदान शरीर के सतह से विसरण विधि द्वारा होता है।
- कीट तथा मकड़ी वर्ग के जीवों में श्वसन गैसों का आदान-प्रदान हेतु विशेष अंग पाये जाते हैं जिसे ट्रेकिया (Trachea) कहते है। ट्रेकिया एक नली (Tube) समान रचना होती है जिसका एक सिरा शरीर के अंदर सीधे उत्तकों से जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा शरीर के सतह पर एक छिद्र आकार के संरचना के रूप में खुलती है। इस छिद्र को श्वासरंध्र (spiracle) कहते है। श्वासरंध्र छिद्र से ही वायुमंडलीय गैस ट्रेकिया में प्रवेश करते हैं तथा सीधे उत्तकों की कोशिका में पहुँचते है।
- मछली जैसे जलीय जीवों में बाह्य - श्वसन हेतु क्लोम (gills) नामक संरचना होती है। गिल्स, जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करत है। गिल्स केवल जलीय श्वसन हेतु उपयुक्त है, इस संरचना द्वारा जीव वायुमंडलीय गैसों का उपयोग नहीं कर सकते है।
- कीचड़ युक्त तलाबो में रहने वाले कुछ मछलियाँ, जैसे- गरई, सिंधी, कवई, मांगुर आदि में गिल्स के अतिरिक्त, सहायक श्वसन अंग पाये जाते है। सहायक श्वसन अंग से ये मछली वायुमंडल ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सक्षम होता है और यही कारण है ये मछलियाँ ज्यादा समय तक पानी के बाहर जिंदा रहती है।
- स्तनधारी (Human) में बाह्य श्वसन को सम्पन्न कराने हेतु एक विकसित श्वसन तंत्र (Respiratory system) पाये जाते हैं, जिससे फेफड़े (lungs) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
मनुष्य का श्वसन - तंत्र (Respiratory system of Human Body)
- मानव के श्वसन तंत्र का प्रारंभ एक जोड़े नासिक रंध्र (Nostril or Nares) से होता है। नारिक रंध्र मुख के ठीक ऊपर लगभग गोलाकार आकृति की होती है ।
- दोनों ही नासिका रंध्र भीतर की ओर अलग-अलग नासिका वेश्म (Nasal chamber) में खुलती है। दो नासिका वेश्म के बीच एक लंबी अस्थि होती है जिसे नासा - अस्थि (Nasal septum) कहते है ।
- नासिका वेश्म (Nasal chamber) के अग्र भाग में रोमयुक्त त्वचा ( hariy skin) पाये जाते हैं जिसमें श्लेषा (mucous) लगे होते है। नासिका वेश्म की यह रोम युक्त त्वचा हवा के धूलकण को हवा से छानकर अलग कर देती है।
- नासिका वेश्म के पीछले भाग में संवेदी कोशिका पाये जाते हैं जिनके द्वारा हवा के सुगंध द्वारा दुर्गंध का पता चलता है। इस क्षेत्र को घ्राण क्षेत्र (Olfactory region) तथा श्वसन क्षेत्र (Respiratory region) भी कहा जाता है।
- नासिका वेश्म मुखगुहा के पीछे ग्रसनी (Pharynx) में खुलता है। ग्रसनी से श्वसन मार्ग का प्रारंभ कंठ द्वारा (glottis) से शुरू होता है। ग्लोटिस के ऊपर एपीग्लाटिस नाम का ढ़क्कन पाया जाता है। जैसे ही हवा ग्रसनी में पहुँचता है, एपीग्लाटिस, ग्लोटिस के ऊपर से हट जाता है तथा हवा ग्लांटिस से होकर श्वसन मार्ग के अगले हिस्से में पहुँच जाती है।
- ग्लोटिस, उपास्थि (Cartilage) की बनी संरचना हैं जो गले पर उभार की तरह दिखती है। गले के इस उभार को एडम्स ऐपल (Adma's (apple) कहा जाता है। एडम्स ऐपल नर मानव (Male Human) में ही वयस्क होने के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देते है ।
- ग्लोटिस के पीछे स्वर तंत्र (Larynx) पाया जाता है, जिसमें ध्वनि की उत्पत्ति हेतु कंपनशील स्वर झिल्ली (Vocal card) पाया जाता है। मनुष्य का आवाज लैरिंक्स से ही निकलता है। इस संरचना को मानव का Sound Box कहा जाता है ।
- लैरिक्स पीछे की ओर श्वासनली ( Trachea ) में खुलता है। मानव का ट्रैकिया लगभग 12 cm लंबी होती है और इसका व्यास लगभग 16 mm होता है।
- ट्रेकिया नली की दिवार पतली तथा कमजोर होती है, इसे मजबूती देने हेतु ट्रेकिया की पूरी लंबाई में उपास्थि के बने अर्धवलय संरचना पायी जाती है।
- ट्रेकिया, गर्दन को पार कर छाती वाले हिस्से में पहुँचकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, इन दोनों भाग को ब्रॉकाई (Bronchi) कहते है। ब्रॉकाई के ऊपर उपास्थि के बने पूर्ण वलय उपस्थित रहते है। दोनों ही ब्रोकाई बाएँ - दाँय हिस्सों में बँटकर फेफड़ा (lungs) में प्रवेश कर जाती है।
- फेफड़ा मनुष्य के बक्षगुहा (Thoracic cavity) में स्थित स्पंजी, गुलाबी तथा थैलीनुमा संरचना है। फेफड़ों की संख्या दो होती है, बायीं ओर की ओर फेफड़ा दो थैलियों से युक्त और दायी ओर एक बड़ी और दो छोटी थैली युक्त संरचना में बँटी रहती है।
- फेफड़ा वक्षगुहा के जिस भाग में स्थित होती उसे प्लूरल गुहा (Plural cavity) कहते हैं। प्लूरल गुहा के चारों ओर झिल्लीयों का पतला आवरण रहता है जिसे पेराइटल प्लूरा (Parietal pleura) कहा जाता है।
- ब्रोंकाई (Bronchi) फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक छोटी नलियों में विभक्त हो जाती है जिसे ब्रौंकिओल्स (Bronchiloes) कहते है । पुनः बौंकिओल्स कई शाखाओं में विभक्त होती है जिन्हें वायुकोष्ठ वाहिनी (Alveolar duct) कहते है । प्रत्येक वायुकोष्ठ वाहिनी वायुकोष (airsac or Alveoli) पर आकर समाप्त हो जाती है।
- श्वसन मार्ग के प्रारंभ नासिका रंध्र से होता है तथा वायुकोष्ठ पर आकर समाप्त जाता है। दोनों फेफड़ों में 3x108 वायुकोष पाये जाते हैं तथा फेफड़ों में 400 से 800 वर्गफीट सतह श्वसन गैसों (O2 तथा CO2) के आदान-प्रदान के लिए उपलब्ध रहता है।
- फेफड़ों के प्रत्येक वायुकोष्ठ के चारों ओर बहुत ही महीन रक्त वाहिकाओं (Blood Capillaries) मौजूद रहती है, जिनमें रक्त भरा रहता है। वायुकोष्ठ में ही हवा का ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करते हैं तथा रक्त का कार्बनडाइऑक्साइड, रक्त से बाहर निकल आते है।
- वायुकोष्ठ तथा अशुद्ध रक्त (CO2 युक्त रक्त) के बीच श्वसन गैसों का आदान-प्रदान विसरण विधि द्वारा होती है। विसरण क्रिया श्वसन गैसों के दावों में अंतर होने के कारण सम्पन्न होता है-

श्वसन की क्रियाविधि (Mechanism of Respiration)
- श्वसन या बाह्य श्वसन की पूरी प्रक्रिया दो अवस्थाओ में सम्पन्न होती है। यह दो अवस्थाएँ है- प्रश्वास ( Inspiration) तथा उच्छ्वास (Expiration)
- इस प्रक्रिया में हवा नासिका रंध्र से वायु-मार्ग होते हुए वायुकोष्ठ में पहुँचती है।
- साँस लेत समय डायफ्राम पीछे की ओर खिसकता है तथा पसलियों के बीच पाये जाने वाले अन्तर्कोशी मांसपेशी (Intercostal Muscles) में संकुचन होता है जिससे सभी पसलियाँ फैल जाती है।
- डायफ्राम के पीछे खिसकने तथा पसलियों के फैलने के कारण फेफड़ा भी फैल जाता है जिससे फेफड़ों में मौजूद वायु का दाब वायुमंडल में मौजूद वायु के दाब से कम हो जाता है। फलस्वरूप वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है।
- इस अवस्था में श्वसन के पश्चात् वायु उसी पथ के द्वारा बाहर निकल कर वायुमंडल में आती है, जिस पथ से वह फेफड़ों में प्रवेश किया था।
- उच्छृवास के दौरान डायफ्राम तथा पसलियाँ पुनः अपने स्थान पर आ जाती है जिससे फेफड़ा सिकुड़ जाती है।
- फेफड़ों में स्वयं फैलने तथा सिकुड़ने का गुण नहीं होता है। फेफड़ों के ऊपर स्थित पसलियाँ एवं डायफ्राम के फैलने-सिकुड़ने से ही फेफड़ा फैलता - सिकुड़ता है।
- बाह्य - श्वसन की दो अवस्था प्रश्वास तथा उच्छ्वास को सम्मिलित रूप से 'Breathing' कहते है।

फेफड़े में की मात्रा (Volume of Air in the lungs)
- सामान्य श्वसन के दौरान आधा लीटर हवा साँस के द्वारा खींची एवं छोड़ी जाती हैं हवा के इस आयतन को लहरी आयतन (Tidal volume) कहते है। सामान्य स्थितियों में वयस्क मानव 15 से 18 बार प्रति मिनट सॉस लेता और छोड़ता है।
- टायडल आयतन (500ml) का दो-तिहाई हिस्सा ही फेफड़ों के वायु कोष्ठ तक पहुँच पाता है। शेष एक-तिहाई हिस्सा वायु-मार्ग में ही रह जाते हैं।
- यदि खूब दम लगाकर साँस ली जाए तो दो लीटर अतिरिक्त हवा खींची जा सकती है, हवा के इस आयतन को प्रश्वसन का संरक्षित आयतन (Inspiratory reserve volume) कहा जाता है। अगर खूब दम लगा कर साँस छोड़ा जाता है तो 1½ लीटर अतिरिक्त हवा छोड़ी जा सकती है, हवा के इस आयतन को उच्छश्वसन का संरक्षित आयतन (Expiratory reserve Volume) कहते हैं।
- इस तरह खूब दम लगाकर साँस खींचने और साँस छोड़ने पर लगभग 4 लीटर हवा खींची और छोड़ी जा सकती है। इसे श्वसन की जैविक क्षमता (Vital capacity of Respiration) कहते है।
- फेफड़े में अधिकतम 5.4 लीटर से 6 लीटर हवा भर सकता है, लेकिन सामान्यतः फेफड़े के अंदर लगभग तीन लीटर हवा भरी रहती है, जिसे क्रियाशील अपशिष्ट आयतन (Functional Residual Volume) कहते है।
- अगर पूरे दम लगाकर भी साँस को छोड़ा जाए, तो भी फेफड़ों में मौजूद संपूर्ण हवा को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। खूब दम लगाकर साँस छोड़ने पर भी 1½ लीटर फेफड़ों में मौजूद ही रहता है, इसे अपशिष्ट आयतन (Residual Volume) कहते है।
मानव शरीर में गैसों का परिवहन (Transport of Gases)
- फेफड़े के वायु कोष्ठ (Alveoli) में पहुँचा हवा से ऑक्सीजन निकलकर रक्त में आ जाता है। ऑक्सीजन रक्त के लाल रुधिर कोशिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन से जुटकर ऑक्सी- हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाते है तथा रुधिर - परिसंचरण के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुँच जाते है।
- रुधिर के लाल रक्त कोशिका (RBC) में स्थित हीमोग्लोबिन एक अद्वितीय जटिल रसायनिक यौगिक है, इसके अभाव में श्वसन-क्रिया नहीं हो सकती है, यही कारण हीमोग्लोबिन को श्वसन - वर्णक (Respiratory Pigment) कहा जाता है।
- हीमोग्लोबिन की रचना दो भागों से मिलकर होती है। हीमोग्लोबिन का 5 प्रतिशत भाग हीमेटीन अथवा हीम कहलाता है, इसी भाग में लौह (Fe) परमाणु पाया जाता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का 95 प्रतिशत भाग ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 13 ml ऑक्सीजन का परिवहन करने में सक्षम होता तथा प्रति 100 ml रुधिर में 19-20 ml ऑक्सीजन उपस्थित रहते है।
- कोशिकीय श्वसन के उपरांत बने कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी रुधिर - संरचरण के माध्यम से होता है, परन्तु केवल 10- 20 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुटकर कार्बोक्सीहिमोग्लोबिन बनाते है तथा इसी रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते है।
- लगभग 85 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा के जल में घुलकर बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं तथा इसी रूप में फेफड़े के वायुकोष्ठ में पहुँच कर पुनः रक्त से अलग हो जाते हैं, अंतत: शरीर के बाहर निकल जाते है।
अभ्यास प्रश्न
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







