विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान
प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
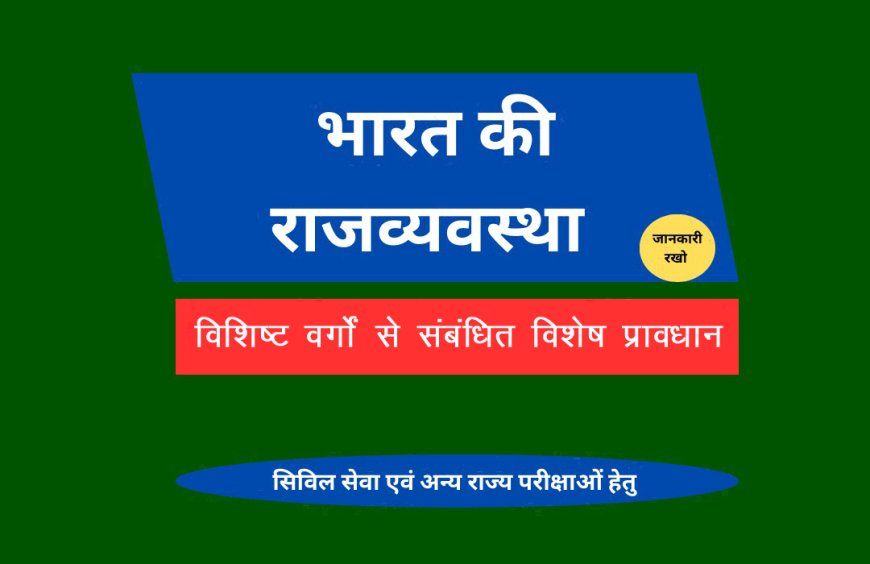
विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान
विशेष प्रावधान का औचित्य
वर्गों का आधार
विशेष प्रावधान के अंग
- विधायिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्वः आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा।
आंग्ल- भारतीय समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इसी तरह राज्य की विधानसभा में इस समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं।मूल रूप से आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के ये दोनों प्रावधान सिर्फ दस वर्षो (यानी 1960 तक) के लिए किए गए थे। लेकिन उसके बाद इसकी अवधि लगातार हर बार दस-दस वर्षों के लिए बढ़ाई जाती रही हैं। 2009 के 95वें संशोधन के अनुसार यह दोनों प्रावधान अब 2020 तक लागू रहेंगे।95वे वां संशोधन विधेयक, 2009 द्वारा आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व के दो प्रावधानों के विस्तार के कारण निम्नवत् हैं :(i) संविधान की धारा 334 के अनुसार संविधान का प्रावधान, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल- भारतीय समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, संविधान लागू होने के 60 साल बाद अप्रभावी हो जाएगा दूसरे शब्दों में 25 जनवरी, 2010 में ये प्रावधान खारिज हो जाएंगे यदि इन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया तो ।(ii) हालांकि पिछले 60 वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों ने काफी तरक्की की है, फिर भी जिन कारणों से संविधान सभा ने सीटों के आरक्षण तथा सीटों पर नामांकन का प्रावधान किया था, वे कारण अभी भी मौजूद हैं। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन करना 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए।आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का यह प्रावधान निम्न कारण से किया गया है, “आंग्ल- भारतीय धार्मिक, सामाजिक और साथ ही साथ भाषायी रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ऐसे में यह प्रावधान जरूरी था, वरना संख्या के हिसाब से एक बहुत ही छोटा समुदाय होने और पूरे भारत में छितराये रहने के कारण आंग्ल-भारतीय चुनावों के जरिए विधायिकाओं की एक सीट भी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। "
- नौकरी एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा केंद्र और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि 2000 के 82वें संशोधन अधिनियम में केंद्र या राज्यों के सरकारी पदों पर बहाली की किसी परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन के मापदंड घटाने का प्रावधान है।
- आंग्ल- भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान तथा शिक्षा अनुदान : आजादी के पहले केंद्र की रेलवे, आबकारी, डाक एवं तार सेवा के कुछ पद आंग्ल- भारतीयों के लिए आरक्षित थे। इसी तरह आंग्ल- भारतीयों के शिक्षण संस्थानों को केंद्र एवं राज्यों से विशेष अनुदान मिला करता था। संविधान के तहत इन सुविधाओं को क्रमिक रूप से कम करते हुए जारी रखा गया और अंततः 1960 में यह सुविधा समाप्त हो गयी।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग: अनुसूचित जाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और यह आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा (धारा 338 ) । इसी तरह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा (धारा 338 ए)। राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्टों को इन पर की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष रखेंगे। पहले संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2003 के 89वें संशोधन के जरिए इस संयुक्त आयोग को दो स्वतंत्र निकायों के रूप में बांट दिया गया । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लिए जो काम करेगा वही काम वह आंग्ल- भारतीयों के लिए भी करेगा। दूसरे शब्दों में, आयोग आंग्ल-भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। बाद में 102 वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए, संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। उसी के अनुरूप राष्ट्रपति को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है जो कि इन वर्गों के संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों का अनुसंधान करके तत्संबंधनी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों तथा कृत कार्यवाही संबंधी ज्ञापन संसद में प्रस्तुत करेंगे।
- अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण: अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। वे ऐसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन संविधान लागू होने के दस वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। इस तरह 1960 में आयोग का गठन हुआ। यू.एन. ढेबर इसके अध्यक्ष बनाए गए और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। चार दशक बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू कराने के लिए राज्यों को निर्देश देने का कार्यपालक अधिकार केंद्र के पास है।
- पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्तिः सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट उस पर की गई कार्रवाइयों की जानकारी के साथ संसद में रखी जाएगी।
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







