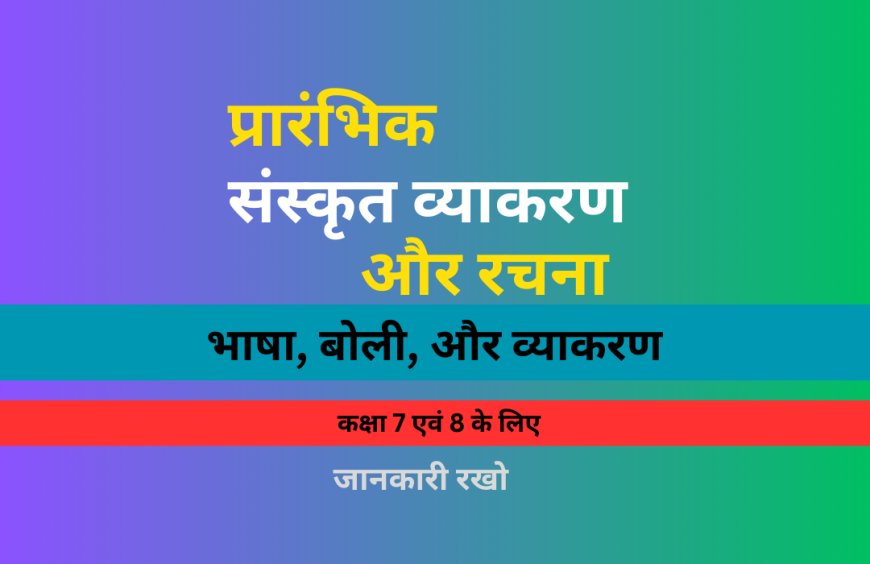संस्कृत व्याकरण
संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का स्थान सर्वोपरि है। बिना व्याकरण के न्याय, साहित्य, मीमांसा, वेदान्त इत्यादि किसी भी शास्त्र का सम्यक् ज्ञान नहीं हो सकता। व्याकरण का अर्थ ही होता है, जिससे शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो - 'व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्'।
व्याकरण में भाषा-संबंधी नियम रहने के कारण भाषा मर्यादित एवं परिष्कृत रहती है। अतएव व्याकरण का महत्त्व अक्षुण्ण है।
व्याकरण के मुख्य रूप से तीन भाग हैं— वर्ण, पद और वाक्य | वर्णों से पद और पदों से वाक्य बनते हैं।
जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं— स्वर और व्यञ्जन ।
स्वर वर्ण
जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर के उच्चारण में अन्दर से आनेवाली ध्वनि में किसी तरह की रुकावट नहीं होती है। स्वर 13 हैं— अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ऌ, ए, ऐ, ओ, औ
स्वर के तीन भेद हैं— ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत
ह्रस्व स्वर- - ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये पाँच हैं— अ, इ, उ, ऋ और लृ । ह्रस्व को मूल ध्वनि या मूल स्वर भी कहते हैं ।
दीर्घ स्वर - दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व के उच्चारण से कुछ अधिक जोर लगाना पड़ता है। दीर्घ स्वर आठ हैं — आ, ई, ऊ, ॠ, ए, ऐ, ओ और औ ।
प्लुत स्वर — प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर लगाना पड़ता है। इसका प्रयोग सम्बोधन वगैरह में होता है। जैसे— हे कृष्ण !
व्यञ्जन वर्ण
जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो, उसे व्यञ्जन वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं।
कवर्ग - क ख ग घ ड.
चवर्ग - च छ ज झ ञ
टवर्ग - ट ठ ड ढ ण
तवर्ग - त थ द ध न
पवर्ग - प फ ब भ म
अन्त:स्थ - य र ल व ऊष्म - श ष स ह
अनुस्वार और विसर्ग – वर्णों के अंतर्गत अनुस्वार (.) और विसर्ग (:) की गणना नहीं होने पर भी ये वर्णों की तरह कार्य करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से तथा विसर्ग का उच्चारण आधा 'ह' के समान होता है।
स्पर्श – क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं ।
अन्तःस्थ – य, र, ल और व को अन्तःस्थ वर्ण कहते हैं।
ऊष्म – श, ष, स और ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं।
घोष – वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह घोष होते हैं।
अघोष – वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, ष, स अघोष होते हैं।
अल्पप्राण – वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम तथा य, र, ल, व वर्ण अल्पप्राण होते हैं।
महाप्राण – वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा श, ष, स, ह वर्ण महाप्राण होते हैं।
अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः – अ, आ, कवर्ग, ह् और विसर्ग का उच्चारण-स्थान कण्ठ है। इसलिए ये कण्ठ्य वर्ण कहलाते हैं।
इचुयशानां तालुः – इ, ई, चवर्ग, य् और श् का उच्चारण - स्थान तालु है, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं।
ऋटुरषाणां मूर्द्धा — ऋ, ॠ, टवर्ग, र् और ष् का उच्चारण - स्थान मूर्द्धा है, इसलिए ये मूर्द्धन्य वर्ण कहलाते हैं ।
लृतुलसानां दन्ताः – लृ, तवर्ग, ल् और स् का उच्चारण दाँत से होता है, इसलिए ये दन्त्य वर्ण कहलाते हैं।
उपूपध्मानीयानामोष्ठौ — उ, ऊ और पवर्ग का उच्चारण - स्थान ओष्ठ है, इसलिए ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं।
एदैतो: कण्ठतालुः – ए और ऐ का उच्चारण-स्थान कण्ठ और तालु है, इसलिए इन्हें कण्ठ्य-तालव्य कहते हैं।
ओदौतोः कण्ठौष्ठम्—ओ और औ का उच्चारण कण्ठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें कण्ठ्यौष्ठ्य वर्ण कहते हैं ।
वकारस्य दन्तोष्ठम् – वकार का उच्चारण दन्त और ओष्ठ से होता है, इसलिए ये दन्त्यौष्ठ्य कहलाते हैं।
ञमङणनानां नासिका च -ञ्, म्, ङ्, ण् और न् का उच्चारण स्थान कण्ठ, तालु आदि के अतिरिक्त नासिका भी है। अनुस्वार का भी उच्चारण - स्थान नासिका है।
व्याकरण में प्रत्याहार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। दो वर्ण वाले प्रत्याहार अनेक वर्णों का बोध कराते हैं। प्रत्याहार का मुख्य आधार निम्नलिखित माहेश्वर सूत्र हैं।
1. अइउण् 2. ऋलृक् 3. एओङ् 4. ऐऔच् 5. हयवरट् 6. लण् 7. ञमङणनम् 8. झभञ् 9. घढधष् 10. जबगडदश् 11. खफछठथचटतव् 12. कपय् 13. शषसर् 14. हल्
ये चौदह माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों के आधार पर ही अण्, अक् आदि प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इनके अंतिम वर्ण ण्, क्, ङ् आदि हलन्त होते हैं। दो वर्ण वाले प्रत्याहार की रचना में पहला वर्ण इन्हीं सूत्रों से लिया जाता है जो हलन्त नहीं होता। दूसरा अंतिम वर्ण हलन्त होता है जो इन्हीं सूत्रों के अंतिम हलन्त वर्णों से लिया जाता है। अपेक्षित प्रत्याहार के अंतर्गत इन्हीं दोनों वर्गों के बीच पड़नेवाले वर्णों की गणना की जाती है। इस गणना में हलन्त वर्णों को छोड़ दिया जाता है, किन्तु प्रत्याहार का पहला वर्ण जोड़ा जाता है।
उदाहरण के लिए, ‘अण्' प्रत्याहार को ही लिया जाए। इसमें उपर्युक्त नियमानुसार अ, इ, उ ये तीन वर्ण आते हैं। 'अक्' प्रत्याहार में अ, इ, उ, ऋ एवं लृ ये पाँच वर्ण होते हैं। नीचे कुछ प्रमुख प्रत्याहार दिए जा रहे हैं -
अण्— अ, इ, उ
अक्— अ, इ, उ, ऋ, लृ
अच्—अ, इ, उ, ऋ, ऌ, ए, ओ, ऐ, औ
अट्— अ, इ, उ, ऋ, ऌ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र
इक् – इ, उ, ऋ, ऌ
एङ्– ए, औ
एच् – ए, ओ, ऐ, औ
ऐच्— ऐ, औ
खर्—ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स
जश् — ज, ब, ग, ड, द
झय् – झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प
झश्— झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द
यण्— य, व, र, ल
हश्—ह, य, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द
इनके अतिरिक्त भी अश्, अल्, हल् आदि कुछ प्रत्याहार और हैं।
1. वर्ण किसे कहते हैं तथा उसके कितने भेद हैं ?
2. मूल स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं ? सोदाहरण बताएँ।
3. स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं?
4. तालु से कौन-कौन वर्ण उच्चरित होते हैं? बताएँ।
5. स्वर वर्ण और व्यञ्जन वर्ण में क्या अंतर है ?
6. निम्नलिखित वर्गों में स्वर वर्णों को रेखांकित करें।
ख, अ, क, ई, प, आ, श, ऊ, ए, ध, औ, ह, ऐ, ग, श, ओ, इ, व
7. अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं ?
8. महाप्राण में कौन-कौन वर्ण हैं?
9. पवर्ग का उच्चारण-स्थान बताएँ।
10. वकार का उच्चारण किस-किस स्थान से होता है ? बताएँ ।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..