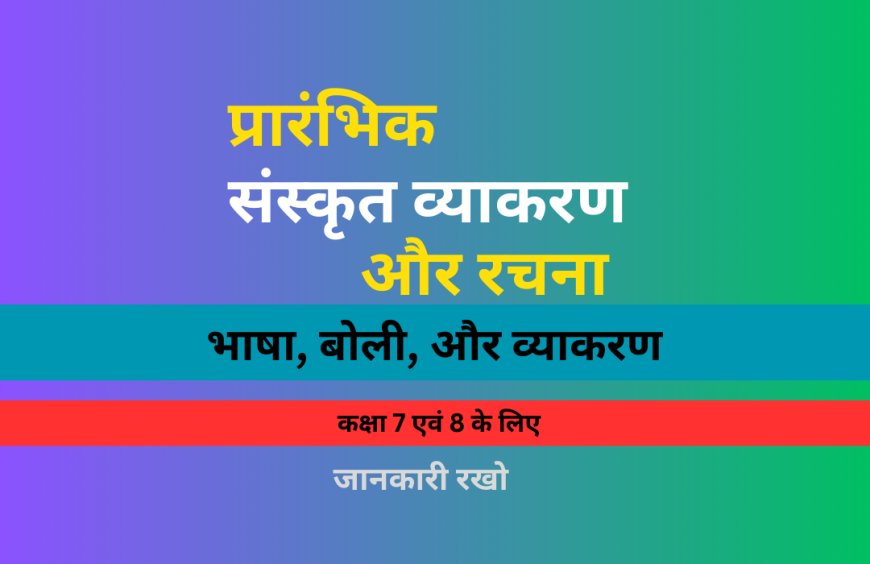कारक और विभक्ति
क्रियान्वयिकारकम् - क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो, उसे कारक कहते हैं। जैसे—‘बालकः पठति' (लड़का पढ़ता है) — इस वाक्य में 'पठति’ क्रिया का प्रत्यक्ष सम्बन्ध ‘बालकः’ से है, इसलिए 'बालकः' कर्ताकारक हुआ।
संस्कृत में कारक के छह भेद माने गए हैं— कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण। क्रिया के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहने के कारण सम्बन्ध और सम्बोधन को कारक नहीं माना जाता है। जैसे— रामस्य अश्वः धावति (राम का घोड़ा दौड़ता है)। इस वाक्य में ‘धावति' क्रिया का सम्बन्ध 'अश्वः' से है, न कि 'रामस्य' से; इसलिए ‘अश्वः' में कर्ताकारक हुआ और रामस्य में कोई कारक नहीं । 'अश्व' (घोड़ा) का सम्बन्ध चूँकि ‘राम’ से है, इसलिए 'राम' शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई |
विभक्ति—जिसके द्वारा कारक और वचनविशेष का बोध हो, उसे विभक्ति कहते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी और सप्तमी - ये सात विभक्तियाँ हैं। प्रत्येक विभक्ति में तीन वचन होते हैं।
कर्ताकारक में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, सम्प्रदान में चतुर्थी, अपादान में पञ्चमी, सम्बन्ध में षष्ठी तथा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है।
कर्ताकारक
स्वतन्त्रः कर्ता—क्रिया के सम्पादन में जो स्वतन्त्र हो, उसे कर्ताकारक कहते हैं। कर्ताकारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे— लड़का पुस्तक पढ़ता है—बालकः पुस्तकं पठति। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया बालक कर रहा है, इसलिए ‘बालकः’ कर्ताकारक हुआ।
प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा – शब्दार्थमात्र, संख्या, परिमाण, लिङ्ग या वचन मात्र का बोध होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे—
शब्दार्थ मात्र में— उच्चैः, रामः, फलम्
संख्या मात्र में— द्वौ बालकौ, त्रीणि फलानि
परिमाण मात्र में— द्रोणो व्रीहिः (धान्य)
लिङ्ग मात्र में — तटः, नदी, तीरम्
वचन मात्र में—बालकः (एकवचन), बालकौ (द्विवचन), बालकाः (बहुवचन)
सम्बोधने च - सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे— हे कृष्ण ! पुस्तक लाओ (हे कृष्ण! पुस्तकम् आनय) । इस वाक्य में 'हे कृष्ण' सम्बोधन है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। इसी तरह, 'हे सीते!', 'हे मुने!' आदि में समझना चाहिए।
कर्मकारक
कर्तुरीप्सिततमं कर्म – कर्ता को क्रिया के द्वारा जो अत्यंत अभीप्सित हो, उसे कर्मकारक कहते हैं। जैसे— बच्चा चन्द्रमा को देखता है (बालः चन्द्रं पश्यति) । इस वाक्य में ‘बालः' कर्ता को 'पश्यति' क्रिया के द्वारा अभिलषित चन्द्रमा है, इसलिए 'चन्द्रं' कर्मकारक हुआ।
कर्मणि द्वितीया—कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे— सीता रोटी खाती है (सीता रोटिकां खादति) । इस वाक्य में 'रोटिकां' कर्मकारक है, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति हुई।
क्रियाविशेषणे च – क्रियाविशेषण में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे— 1. कछुआ धीरे-धीरे चलता है-कच्छपः मन्दं-मन्दं चलति । 2. मोहन मीठी बात करता है - मोहनः मधुरं वदति।
उपर्युक्त प्रथम वाक्य में 'मन्द-मन्दं' तथा दूसरे वाक्य में 'मधुरं' क्रियाविशेषण हैं, इसलिए इनमें द्वितीया विभक्ति हुई ।
सर्वत:, परितः, अभितः (चारों ओर), उभयत: (दोनों ओर), प्रति, निकषा (समीप), धिक्, अनु, यावत् शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे -
गाँव के चारों ओर खेत हैं— ग्रामं सर्वतः क्षेत्राणि सन्ति ।
घर के दोनों ओर पेड़ हैं — गृहम् उभयतः वृक्षाः सन्ति।
नदियाँ समुद्र के पास जाती हैं - नद्यः समुद्रं प्रति गच्छन्ति।
विद्यालय के निकट नदी है – विद्यालयं निकषा नदी अस्ति ।
राष्ट्र के अभक्त को धिक्कार है— राष्ट्रस्य अभक्तं धिक् !
वह पुस्तक की नकल करता है— स पुस्तकम् अनुकरोति।
राम घर तक जाएगा — रामः गृहं यावत् गमिष्यति।
दुह्, याच्, प्रच्छ् आदि धातुओं के योग में दो कर्म होते हैं, और दोनों में द्वितीया जैसे - विभक्ति होती है।
रमेश गाय दुहता है— रमेशः गां दुग्धं दोग्धि।
किसान से अन्न माँगता है – कृषकम् अन्नं याचते।
छात्र शिक्षक से पाठ पूछता है- -छात्रः शिक्षकं पाठं पृच्छति।
करणकारक
साधकतमं करणम्—क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक हो, उसे करणकारक कहते हैं। जैसे- - राधा कलम से लिखती है (राधा कलमेन लिखति ) । इस वाक्य में लिखना क्रिया का सहायक ‘कलम' है, इसलिए यह (कलम) करणकारक हुआ।
कर्तृकरणयोस्तृतीया - अनुक्त कर्ता, अर्थात् कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तथा करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे -
कर्मवाच्य में – राम चन्द्रमा को देखता है — रामेण चन्द्रः दृश्यते ।
भाववाच्य में - मदन हँसता है— मदनेन हस्यते ।
करणकारक में— हरिण को बाण से बेधता है – मृगं बाणेन विध्यति।
उपर्युक्त प्रथम वाक्य में कर्मवाच्य का कर्ता 'रामेण' है तथा दूसरे वाक्य में भाववाच्य का कर्ता ‘मदनेन’ है, इसलिए दोनों में तृतीया विभक्ति हुई ।
तीसरे वाक्य में ‘बाणेन' करणकारक है, इसलिए इसमें भी तृतीया विभक्ति हुई |
अपवर्गे तृतीया – कार्य-समाप्ति या फल-प्राप्ति के अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है | यथा – मासेन गणितं शिक्षितम् (एक मास में गणित सीख लिया)। त्रिक्रोशेन उत्तररामचरितं पठितम् (तीन कोस जाते-जाते उत्तररामचरित पढ़ लिया) ।
सहयुक्तेऽप्रधाने – सह, साकं, सार्द्धं (साथ) आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे- - राम के साथ सीता वन गई — रामेण सह सीता वनम् अगच्छत्। यहाँ ‘सह' शब्द के योग में 'रामेण' में तृतीया विभक्ति लगी। इसी तरह साकं, सार्द्धं के योग में समझना चाहिए।
येनाङ्गविकार: – जिस अंग में विकार का ज्ञान हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे— पीठ का कुबड़ा – पृष्ठेन कुब्जः, पाँव से लँगड़ा – पादेन खञ्जः, कानों से बहरा – कर्णाभ्यां बधिरः । इन वाक्यांशों में क्रमशः ‘पृष्ठेन', 'पादेन' तथा 'कर्णाभ्यां अंगसूचक शब्दों में विकार रहने के कारण तृतीया विभक्ति हुई |
प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् – प्रकृति, जाति, आकृति, नाम आदि कई शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे— प्रकृत्या शूरः ( स्वभाव से वीर), जात्या ब्राह्मणः (जाति से ब्राह्मण), आकृत्या सुन्दरः (आकृति से सुन्दर), नाम्ना सुरेशः (नाम से सुरेश), सुखेन शेते (आराम से सोता है) इत्यादि ।
इत्थंभूत लक्षणे – जिस लक्षण से कोई व्यक्ति या पदार्थ पहचाना जाए, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे – जटाभिः तापसः (जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है), शिखया हिन्दुः (चोटी से हिंदू मालूम पड़ता है), पुस्तकैः छात्रः (पुस्तकों से छात्र ज्ञात होता है)।
घोड़ा वहाँ दौड़ता है — अश्वः तत्र धावति ।
हे रमेश ! श्याम यहाँ है— रमेश ! श्यामः अत्र अस्ति।
नरेश और महेश खेलते हैं – नरेशमहेशौ खेलतः ।
हाथी नहीं दौड़ते हैं — गजाः न धावन्ति।
राम अखबार पढ़ता है. - रामः समाचारपत्रं पठति ।
सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं— मार्गम् उभयतः वृक्षाः सन्ति।
लक्ष्मण ने राम से कहा - लक्ष्मणः रामं प्रति अवदत् ।
खरहा तेजी से दौड़ता है - शशकः वेगेन धावति ।
पुत्र के साथ पिता जाता है — पुत्रेण सह पिता गच्छति।
बैल को डंडे से पीटता है — वृषभं दण्डेन ताडयति।
वह आँखों का अन्धा है—स नेत्राभ्याम् अन्धः अस्ति।
दिनेश सरल स्वभाव का है – दिनेशः प्रकृत्या सरलः ।
कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् – जिसको दिया जाए, उसे सम्प्रदानकारक कहते हैं। जैसे- - ब्राह्मण को वस्त्र देता है (ब्राह्मणाय वस्त्रं यच्छति) । इस वाक्य में ब्राह्मण को वस्त्र देने की बात कही गई है, इसलिए 'ब्राह्मणाय' सम्प्रदानकारक हुआ।
चतुर्थी सम्प्रदाने – सम्प्रदानकारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे— छात्र को पुस्तक देता है (छात्राय पुस्तकं ददाति) । इस वाक्य में छात्र सम्प्रदानकारक है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर 'छात्राय' हुआ।
नमः, स्वस्ति आदि शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे— राम को प्रणाम—रामाय नमः, शारदा को प्रणाम – शारदायै नमः लोगों का कल्याण हो — जनेभ्यः स्वस्ति ।
रुच्यर्थानां प्रीयमाण: - रुच् धातु तथा उसके समानार्थक अन्य धातुओं के योग में प्रसन्न होनेवाले में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे— बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है- बालकाय मोदकं रोचते।
अपादानकारक
ध्रुवमपायेऽपादानम् – जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु अलग हो, उसे अपादानकारक कहते हैं। जैसे— 'पेड़ से पत्ते गिरते हैं. - वृक्षात् पत्राणि पतन्ति'। इस वाक्य में पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, इसलिए 'वृक्षात्' अपादानकारक हुआ।
अपादाने पञ्चमी - अपादान में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे— 'घर से लड़का जाता है’—गृहात् बालकः गच्छति'। इस वाक्य में ‘गृहात्' अपादानकारक है, इसलिए इसमें पञ्चमी विभक्ति हुई।
जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो, उसमें भी पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे - रस से रक्त उत्पन्न होता है— रसात् रक्तम् प्रजायते।
बहिः (बाहर), आरात् (समीप), ऋते (बिना), दिशा, देश वाचक आदि शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे -
गाँव के बाहर विद्यालय है— ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति।
घर के समीप खेत है— गृहात् आरात् क्षेत्रम् अस्ति।
परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है— परिश्रमात् ऋते विद्या न भवति।
गाँव से उत्तर तालाब है – ग्रामात् उत्तरस्यां तडागः अस्ति।
भारत से पश्चिम इंगलैंड है— भारतात् पश्चिमायाम् आंग्लदेशः।
भीत्रार्थानां भयहेतुः—भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में भय का जो कारण रहता है उसमें पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे— वह साँप से डरता है — सः सर्पात् बिभेति। सिपाही बदमाशों से लोगों की रक्षा करते हैं – राजपुरुषाः दुष्टेभ्यः जनान् रक्षन्ति।
पृथग्विनाभ्यां द्वितीयातृतीये च – पृथक् (अलग) और बिना शब्दों के योग में पञ्चमी, तृतीया और द्वितीया तीनों विभक्तियाँ होती हैं। जैसे— आँवले के तेल से अलग यह तेल है—आमलकी तैलात् (तैलेन, तैलं) पृथक् इदम् तैलम्— धर्म के बिना सुख नहीं मिलता—धर्मात् (धर्मेण, धर्मं) बिना सुखं न मिलति।
अन्यार्थैः– अन्य, इतर, अतिरिक्त, भिन्न आदि अन्यार्थक शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है। जैसे – मित्र के सिवा दूसरा कौन सहायक हो सकता है—मित्रात् अन्यः कः सहायकः भवति? सरकार से अलग यह संघ है— सर्वकारात् भिन्नः अयं संघः ।
सम्बन्धकारक
षष्ठी शेषे– कर्तादि कारकों से भिन्न ‘शेष', अर्थात् स्व-स्वामिभावादि सम्बन्धकारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे- - राम का दूत-रामस्य दूतः । यहाँ राम और दूत में स्वस्वामिभाव सम्बन्धकारक है। देवदत्त का बेटा – देवदत्तस्य पुत्रः – यहाँ जन्य-जनकभाव सम्बन्ध है। इसी तरह, किसी भी प्रकार के सम्बन्धकारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे – विद्यालय का छात्र- - विद्यालयस्य छात्रः, माता का हृदय – मातुः हृदयम्, राष्ट्र का नेता – राष्ट्रस्य नेता आदि ।
दूरम् अन्तिकम् (समीप), कुशलम्, हितम् आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। दूरम् और अन्तिकम् के योग में पञ्चमी विभक्ति भी होती है। जैसे—
गाँव से दूर विद्यालय है - ग्रामस्य (ग्रामात्) दूरं विद्यालयः अस्ति।
विद्यालय के समीप कुआँ है— विद्यालयस्य (विद्यालयात्) अन्तिकं कूपः अस्ति।
आपका कल्याण हो - भवतः कुशलं भवेत्।
समाज की भलाई करनी चाहिए – समाजस्य हितं कुर्यात् ।
तुल्यार्थैस्तृतीया च— तुल्य, सम आदि समानार्थबोधक शब्दों के योग में षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियाँ होती हैं। जैसे— सत्य के समान तप नहीं है— सत्यस्य (सत्येन) तुल्यं तपः नास्ति।
अधिकरणकारक
आधारोऽधिकरणम् – क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे– 'विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं — विद्यालये छात्राः पठन्ति'। इस वाक्य में छात्रों के पढ़ने का आधार ‘विद्यालय’ है, इसलिए 'विद्यालये' अधिकरणकारक हुआ।
सप्तम्यधिकरणे- अधिकरणकारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे— 'पेड़ पर कौआ है—वृक्षे काकः अस्ति । इस वाक्य में 'वृक्षे' अधिकरणकारक है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति हुई ।
निर्धारणे षष्ठी – अनेक में से यदि किसी एक वस्तु की महत्ता बताई जाए, तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। जैसे— पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है— पर्वतेषु (या पर्वतानां) हिमालयः श्रेष्ठः । कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं — कविषु ( या कवीनां) कालिदासः श्रेष्ठः।
राजा गरीब को धन देता है - राजा निर्धनाय धनं ददाति ।
श्रीकृष्ण को प्रणाम — श्रीकृष्णाय नमः ।
राम विद्यालय से आता है — रामः विद्यालयात् आगच्छति।
गाँव से बाहर बगीचा है – ग्रामात् बहिः उद्यानम् अस्ति।
वह बाघ से डरता है. -सः व्याघ्रात् बिभेति।
विज्ञान से भिन्न साहित्य है – विज्ञानात् भिन्नं साहित्यम् अस्ति।
रमेश का घोड़ा चरता है – रमेशस्य अश्वः चरति।
घर के समीप पेड़ हैं — गृहस्य अन्तिकं वृक्षाः सन्ति ।
राष्ट्र का हित करना चाहिए – राष्ट्रस्य हितं कुर्यात् ।
ऑफिस में किरानी हैं— कार्यालये लिपिकाः सन्ति ।
क्या इस गाँव में सज्जन नहीं हैं— किम् अस्मिन् ग्रामे सज्जनाः न सन्ति ?
पण्डितों में जगन्नाथ श्रेष्ठ थे – पण्डितेषु जगन्नाथः श्रेष्ठः आसीत्।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..