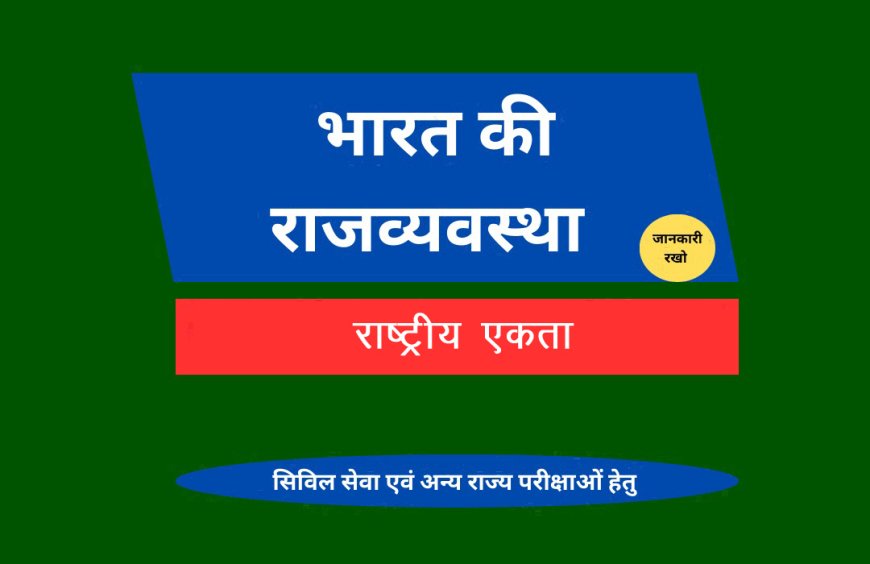राष्ट्रीय एकता
भारत धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, नस्ल, क्षेत्र आदि के रूप में एक विस्तृत विभिन्नता वाला देश है। अत: देश के चतुर्दिक विकास एवं संपन्नता के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय
राष्ट्रीय एकता की परिभाषा एवं कथन:
"राष्ट्रीय एकता का अर्थ है- देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना तथा समाज में राष्ट्रीय एवं लोकहित धारणा फैलाना, जो संकीर्ण हितों से परे हो । " (मायरोन वेनर)
"राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिससे लोगों के दिल में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता और समग्र विकास की भावना पैदा होती है। एक समान नागरिक बोध या राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना उनके बीच बढ़ती है।' (एच. ए. गनी)
"राष्ट्रीय एकता ईंट एवं गारे से बन सकने वाला एक घर नहीं है। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। इसके विपरीत एकता एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। यह एक चेतना है जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए।” (डॉ. एस. राधाकृष्णन)
"राष्ट्रीय एकता का अर्थ लोगों के भिन्न वर्गों से बने राजनीतिक समुदाय या राज्य की समग्रता से है न कि एकरूपता से है; एकता से है न कि समानता से; पुनर्मेल से है न कि मेल से; एकत्र करने से है न कि समागीकरण से।" (रशीदुद्दीन खान)
सार रूप में राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम एवं उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं।
राष्ट्रीय एकता में निम्न बड़े अवरोध शामिल हैं:
1. क्षेत्रवाद
क्षेत्रवाद का अर्थ उप-राष्ट्रवाद और उप-क्षेत्रवाद निष्ठा से है। यह किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए राष्ट्र की तुलना में अधिक लगाव को इंगित करता है। इसमें उप-क्षेत्रीयतावाद है, जिसके अंतर्गत किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र हेतु अधिक लगाव होता है।
क्षेत्रवाद “भारत में राजनीतिक एकता की एक अनुषंगी प्रक्रिया है। यह उन शेष घटकों के लिए घोषणा है, जिनका राष्ट्रीय राजनीति एवं राष्ट्रीय संस्कृति में वर्णन नहीं होता और जो नयी राजनीति के केंद्र में सम्मिलित नहीं हैं। इन्हें राजनीतिक असंतुष्टता एवं राजनीतिक बहिष्करण के रूप में व्यक्त किया गया है।
क्षेत्रवाद एक देशव्यापी तथ्य है जो स्वयं को निम्न छह तरीकों से स्थापित करता है:
- भारतीय संघ के कुछ राज्यों (जैसे-खालिस्तान, द्रविडनाडु, मिजो, नागा और अन्य) के लोगों द्वारा अलग होने के लिए मांग।
- कुछ क्षेत्र के लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग (जैसे-तेलंगाना, बोडोलैंड, विदर्भ, गोरखालैंड तथा अन्य ) |
- कुछ केंद्रशासित क्षेत्रों के लोगों द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग (जैसे-पुडुचेरी, दिल्ली, दमन और दीव आदि) ।
- अन्तर - राज्यीय सीमा विवाद (जैसे- चंडीगढ़ और हरियाणा ) तथा नदी जल विवाद (जैसे- कावेरी, कृष्णा, रावीव्यास तथा अन्य ) ।
- क्षेत्रीय उद्देश्य के लिए संगठनों का गठन, जो कि अपने नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुसरण के लिए आतंकी गतिविधियों की वकालत करें (जैसे- शिवसेना, तमिल सेना, हिंदी सेना, सरदार सेना, लक्षित सेना तथा अन्य ) |
- जो स्थानीय लोगों की सरकारी पदों, निजी नौकरियों, आज्ञा पत्रों एवं अन्य में प्राथमिकता की वकालत करते है। उनका नारा असम असामियों के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए होगा।
2. सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता का अर्थ है- किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम को राष्ट्र पर प्राथमिकता देना तथा किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर अपने सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देना। इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन में भी थीं जहां 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में मुस्लिम, सिख व अन्य को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था।
सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण से बढ़ावा मिला है। इसके विभिन्न परिणाम निम्न हैं:
- धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन (जैसे- अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, शिव सेना आदि)
- धर्म के आधार पर प्रभावशाली समूहों का उभरना (जैसे- आर.एस.एस., विश्व हिंदू परिषद, जमात-ए-इस्लामी, एंग्लो-इंडियन क्रिश्चियन संघ तथा अन्य )
- सांप्रदायिक दंगे ( हिंदू-मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू-ईसाई तथा आदि के बीच बनारस, लखनऊ, मथुरा, हैदराबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, मुरादाबाद और अन्य कई स्थान सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए हैं।
- धार्मिक आकारों पर मतभेद, जैसे- मंदिर, मस्जिद और अन्य (अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मतभेद जहां 6 दिसंबर, 1992 को कार सेवकों ने विवादास्पद ढांचे को नष्ट किया था ) |
सांप्रदायिकता की समस्या धार्मिक मुस्लिमों की रूढ़िवादिता और पाकिस्तान की भूमिका से है और साथ ही हिंदू कट्टरवाद, सरकारी जड़त्व, राजनीतिक दलों व अन्यों की भूमिका, चुनावी अनिवार्यता, सांप्रदायिक मीडिया, सामाजिक-आर्थिक कारकों आदि से भी।
3. जातिवाद
जातिवाद का अर्थ सामान्य राष्ट्रीय हित की अपेक्षा किसी जाति वर्ग के प्रति निजी प्रेम से है। यह मुख्य रूप से जाति के राजनीतिकरण का परिणाम है। इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में शामिल हैं:
- जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन (जैसे-मद्रास में जस्टिस पार्टी, डी.एम.के., केरल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य )
- दबाव समूहों का जाति के आधार पर उभरना (जैसे - नादर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा और अन्य )
- चुनाव के दौरान पार्टी टिकटों का आवंटन तथा राज्य में जाति आधार पर मंत्रियों की परिषद का गठन।
- विभिन्न राज्यों में ऊंची तथा निम्न जातियों या प्रभावशाली जातियों के बीच जाति मतभेद, जैसे- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य।
- आरक्षण नीति पर हिंसक मतभेद तथा विरोध प्रदर्शन।
बी. के. नेहरू ने इस बात पर ध्यान दिया कि, "सांप्रदायिक निर्वाचन (ब्रिटिश समय से) अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के रूप में मौजूद है। वे जाति के उत्थान पर बल देते थे तथा लोगों को उनकी जाति के प्रति जागरूक करते थे। यह राष्ट्रीय एकता के लिए अनुकूल नहीं है । "
राज्य स्तर पर, राजनीति मूल रूप से अधिसंख्यक जाति तथा वर्ग के बीच का विवाद है, जैसे-आंध्र प्रदेश में कामा बनाम रेड्डी, कर्नाटक में लिंगायत बनाम बोकालिग्गा, केरल में नायर बनाम इझावा, गुजरात में बनिया बनाम पातीदार, बिहार में भूमिहार बनाम राजपूत, हरियाणा में जाट बनाम अहीर, उत्तर प्रदेश में जाट बनाम राजपूत, असम में कालिता बनाम अहोम तथा अन्य |
4. भाषावाद
भाषावाद का अर्थ किसी भी भाषा के प्रति प्रेम तथा अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से घृणा है। भाषावाद का विषय भी क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता या जातिवाद की तरह राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसके दो आयाम हैं-(अ) भाषा के अधार पर राज्यों का पुनर्गठन (ब) संघ की राजभाषा का निर्धारण।
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की देशव्यापी मांग के कारण आंध्र प्रदेश राज्य 1953 में तब मद्रास से बना। परिणामस्वरूप, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-1955 ) द्वारा दिए सुझावों के आधार पर राज्यों का भाषा के आधार पर विस्तृत रूप से पुनर्गठन हुआ। इसके बावजूद, भारत का राजनीतिक नक्शा लोक समर्पित दबाव एवं राजनीतिक दशा के कारण लगातार बदलता रहा। जिसके परिणामस्वरूप मुंबई, पंजाब, असम को बांटा गया। 2000 के अंत तक, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 1956 के 14 तथा 6 से क्रमश: 28 तथा 7 हो चुकी थी।
राजभाषा भाषा अधिनियम, 1963 के कानून द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा भाषा के रूप में दर्जा देने से दक्षिण भारत एवं पं. बंगाल में हिंदी विरोधी आंदोलनों ने जन्म लिया। तब, केंद्रीय सरकार ने आश्वासन दिया कि गैर-हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य जब तक चाहें अंग्रेजी को एक सहायक राजभाषा भाषा के रूप में जारी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल तंत्र के लिए त्रिभाषा सूत्र (अंग्रेजी, हिन्दी और एक क्षेत्रीय भाषा) को तमिलनाडु' द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप हिन्दी भारत की समग्र संस्कृति की लोकभाषा के रूप में नहीं उभर सकी है। जैसी की संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पना की गई थी।
भाषावाद की परेशानी हाल के समय में कुछ क्षेत्रीय दलों के बढने के साथ और भी बढ़ी है, जैसे-टीडीपी, एजीपी, शिवसेना तथा इसी प्रकार के अन्य दल।
राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC) का गठन 1961 में अनेकता में एकता' के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, यू.जी.सी. का चेयरमैन, 2 शिक्षाशास्त्री, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आयुक्त तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। परिषद को निर्देशित किया गया कि वह राष्ट्रीय एकता से संबंधित परेशानियों का परीक्षण करे और इससे निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दे। परिषद ने राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। हालांकि ये सुझाव केवल कागज पर रहे तथा इसे लागू करने हेतु केंद्र और राज्यों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।
1968 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन की। इसका आकार 39 से 55 सदस्यों तक बढ़ाया गया। उद्योग, व्यापार तथा मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया। परिषद की बैठक श्रीनगर में हुई तथा इसमें राष्ट्रीय अखंडता की जड़ों को कमजोर करने वाली सभी प्रवृत्तियों की भर्त्सना संबंधित एक प्रस्ताव स्वीकारा गया। इसने राजनीतिक दलों, संगठनों एवं प्रेस से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता हेतु समाज के सृजनात्मक बलों से आग्रह किया। इसने क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता तथा भाषावाद पर रिपोर्ट देने हेतु तीन समितियों का गठन भी किया। हालांकि, वास्तविक रूप में, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।
1980 में, केंद्र सरकार ने पुनः राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया, जो पूर्णत: अप्रचलित हो चुकी थी। इसकी सदस्यता को और विस्तृत किया गया। इसके ऐजेंडा में चर्चा के लिए तीन विषय थेरू सांप्रदायिक सद्भाव की समस्या, उत्तर पूर्व क्षेत्र में अशांति तथा नए शिक्षा निकायों की आवश्यकता परिषद ने राष्ट्रीय एकता पर सांप्रदायिक तथा अन्य विभाजित बलों के प्रहार पर नियमित नजर रखने हेतु एक स्थायी समिति गठित की।
1986 में राष्ट्रीय विकास परिषद पुनर्गठित किया गया तथा इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। इसमें पंजाब में आतंकवाद को राष्ट्र की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर हमला माना। इस संबंध में इसने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। परिषद ने नियमित आधार पर कार्यवाही के लिए एक 21 सदस्यीय समिति का भी गठन किया। परिषद से सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया।
1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने वी. पी. सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया। इसकी सदस्य संख्या 101 तक बढ़ाई गई। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के नेता, महिला, उद्योग व्यापार, शैक्षिक, पत्रकार एवं सार्वजनिक व्यक्तित्व के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें चर्चा के लिए बने कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दे थे, जैसे- पंजाब तथा कश्मीर की समस्याएं, अलगाववादियों द्वारा हिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव तथा अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद समस्या लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।
2005 में, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा सरकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षा में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया। 103 सदस्यीय इस परिषद की बैठक 1992 के 12 वर्ष उपरांत आयोजित हुयी। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही परिषद में राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों, प्रसिद्ध लोगों, उद्योगपतियों, मीडिया, श्रमिक तथा महिलाओं आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करता है। यह परिषद राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों की ओर ज्यादा प्रभावी तरीके से ध्यान दे रही थी तथा उनके क्रियान्वयन पर बराबर नजर रख रही थी और सिफारिशें कर रही थी।
राष्ट्रीय एकता परिषद की 14वीं बैठक, ओडीशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में सांप्रदायिक दंगों के बीच वर्ष 2008 में संपन्न हुयी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यों के साथ ही अन्य सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कारक, क्षेत्रीय, जातीय तथा धार्मिक असमानता को दूर करना, अतिरेकवाद का निषेध, अल्पसंख्यकों के बीच धार्मिक सहिष्णुता एवं सुरक्षा एवं सतत् विकास आदि मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गयी।
प्रधानमंत्री बनाए गए। राष्ट्रीय एकता परिषद के 147 सदस्य हैं जिनमें केन्द्रीय मंत्री, लोकसभा एवं राज्य सभा के विपक्ष के नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, प्रमुख पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व, व्यवसाय तथा महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाना है।
अक्टूबर 2010 में सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की एक स्थाई समिति भी गठित की। इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, जबकि 4 केन्द्रीय मंत्री, 9 मुख्यमंत्री तथा रा.ए.प. के 5 सहयोजित सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। यह समिति रा.ए.प. की बैठकों का एजेंडा निर्धारित करती है।
रा.ए.प. की 15 वीं बैठक सितम्बर 2011 में हुई। बैठक के ऐजेंडा में साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के उपाय, सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर दृष्टिकोण, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उपाय, भेदभाव समाप्त करने के उपाय विशेषकर अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ, नागरिक अशांति की स्थिति में राज्य तथा पुलिस के कर्तव्य तथा धर्म और जाति के नाम पर युवाओं में अतिवाद को रोकने आदि विषय सम्मिलित थे।
एनआईसी (NIC) की सोलहवीं बैठक 23.09.2013 को हुई जिसमें एक संकल्प पारित कर हिंसा की भर्त्सना की गई है। सभी समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए सभी उपाय करने, लोगों के बीच सभी तरह के भेदों एवं विवादों का समाधान कानूनी ढांचे के अंतर्गत करने, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों का अत्याचार की निंदा यौन दुर्व्यवहार की निंदा और महिलाओं को समान अवसरों के साथ अपने सामाजिक-आर्थिक विकास की पूरी आजादी, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी समय उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर राय बनी।
साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन
साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन (NFCH) की स्थापना 1992 में हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय है। यह साम्प्रदायिक सौहार्द, भाईचारा तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।
एन. एफ. सी. एच. की दृष्टि एवं लक्ष्य निम्नलिखित हैं:
- वृष्टि: भारत साम्प्रदायिक तथा हर प्रकार की हिंसा से मुक्त हो । जहाँ हर नागरिक, विशेषकर युवा एवं बच्चे, शांति और सौहार्द के साथ रहें ।
- लक्ष्यः साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अखण् डता को सुदृढ़ करना तथा सामूहिक सामाजिक प्रयासों तथा जागरुकता कार्यक्रमों से विविधता में एकता को प्रोत्साहित करना, हिंसा प्रभावित लोगों विशेषकर बच्चों तक पहुंचना, भारत की साझी सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए अंतर- आस्था संवाद को बढ़ावा देना।
एन.एफ. सी. एच. की गतिविधियों में सम्मिलित हैं:
- सामाजिक हिंसा से प्रभावित बच्चों को उनकी देखभाल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जिससे कि उनका पुनर्वास किया जा सके, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- अपने स्तर पर अथवा शिक्षा संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि के सहयोग से ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले।
- अध्ययन संचालित करना तथा संस्थाओं/ अध्येताओं को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- साम्प्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करना।
- राज्य सरकारों / संघीय क्षेत्र में प्रशासकों, औद्योगिकी वाणिज्यिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को संलग्न कर फाउण्डेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना।
- इस विषय पर सूचना सेवाएं प्रदान करना तथा मोनोग्राफ एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..