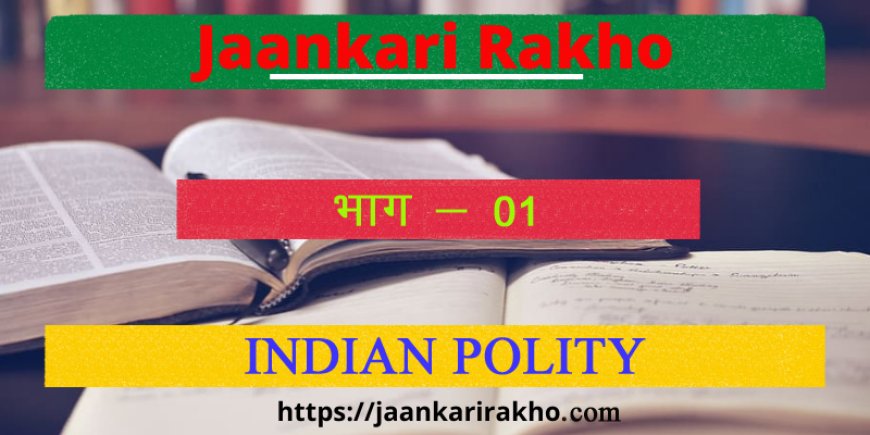General Competition | Indian Polity | मूल अधिकार
मैलिक अधिकार के विषय में जानकारी में भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12-35 प्राप्त कराता है ।
विशेषता:
(1) मौलिक अधिकार की सुरक्षा एवं गारंटी में भारत का उच्चतम न्यायलय प्रदान करता है ।
(2) मौलिक अधिकार के हनन / उल्लंघन के स्थिति में न्यायपालिका इसे बहाल करवाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार न्यायोचित या वाद योग्य है ।
(3) मौलिक अधिकार असीमित है।
(4) मौलिक अधिकार में संसोधन संसद कर सकती है।
(5) मौलिक अधिकार देश के भीतर राजनैतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है ।
मैग्नाकार्टाः-
सर्वप्रथम ब्रिटेन का राजा जॉन किंग ने 1215 ई. में सामंतों के दवाब में आकर ब्रिटेन के आम नागरिकों के लिए जो अधिकारों की घोषणा की है, उसे ही मैग्नाकार्टा कहा गया। भारतीय संविधान का भाग-3 हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिस कारण भारतीय संविधान के भाग-3 को मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
- कांग्रेस ने अपने 1931 के करांची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की माँग की जिसका प्रारूप · पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था ।
- मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। जिसमें संपति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता था लेकिन भारतीय संसद ने 44वाँ संविधान संसोधन 1978 के तहत् संपति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया तथा अनुच्छेद- 31 को निरस्त कर दिया । जिस कारण वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो निम्न है-
(1) समता / समानता का अधिकार (14-18)
(2) स्वतंत्रता का अधिकार (19-22)
(3) स्वषण के विरूद्ध अधिकार (23-24)
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28)
(5) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार (29-30)
(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)
नोट- वर्तमान समय में संपति के अधिकार को 300 (क) में रखा गया है जिसके तहत् संपति का अधिकार एक विधिक/ कानूनी अधिकार है।
अनुच्छेद-12
इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत संसद, विधानमंडल तथा संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था भी आता है ।
अनुच्छेद-13
यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि या संविधान लागू होने के बाद बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है तो वह विधि मान्य नहीं होगा ।
न्यायिक पुर्नाविलोकन (Judicial Review):-
यह मूलतः अमेरिका संविधान की विशेषता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 13, 32, और 226 में की गई है। भारत में शक्ति के पृथ्ककरण का सिद्धांत को लागू किया गया है।
कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान के अनुरूप है या नहीं इसकी जाँच करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है, इसे ही न्यायिक पुर्नाविलोकन कहते हैं। यह प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है तथा कार्यपालिका और विधायिका मनमानी ना कर सकें ।
♦ समता का अधिकारः
अनुच्छेद- 14
विधि के समक्ष समानता का अधिकार
अनुच्छेद- 15
सामाजिक (जाति, धर्म, लिंग, स्थान) समानता का अधिकार
अनुच्छेद- 16
लोक नियोजन में समानता
अनुच्छेद- 17
अस्पृश्यता का अंत (छुआ-छूत)
अनुच्छेद- 18
उपाधि का अंत |
इसमें तीन क्षेत्र (सेना क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र तथा पुलिस क्षेत्र) में छुट दिया गया है।
विधि के समक्ष समानता:-
इसका अर्थ होता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान है चाहें वो अमीर हो या गरीब । अनुच्छेद-14 में विधि का शासन तथा विधियों के समान संरक्षण की चर्चा है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ।
भारत में अधिकारः
(1) मौलिक अधिकारः-
भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12-35 में जिस अधिकार की चर्चा है वो सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते है।
(2) संवैधानिक अधिकार:-
भारतीय संविधान के भाग-3 तथा अनुच्छेद 12-35 के अलावे जो अनुच्छेद हमें अधिकार देते हैं संवैधानिक अधिकार कहलाता है।
जैसे- अनुच्छेद-301 (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकार )
(3) कानूनी या विधिक अधिकार:-
वैसे अधिकार जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है लेकिन भारत की संसद या विधान मंडल कानून बनाकर प्रदान करती है कानूनी अधिकार कहलाता है।
जैसे - मातृत्व अवकास का अधिकार
(4) मानव अधिकार:-
वे अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है मानवाधिकार कहलाता है।
(5) सुचना का अधिकारः-
संसद ने 2005 ई. में कानून बनाकर सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमें यह अधिकार प्रदान किया जिस कारण हम इसे कानूनी अधिकार मान सकते हैं।
(6) मतदान का अधिकार:-
मतदान के अधिकार की चर्चा स्पष्टता पूर्वक भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत् धारा 62 में किया गया है और यह अधिनियम भारतीय संसद ने बनाया है। जिस कारण इसे कानूनी या विधिक की श्रेणी में रखते है ।
(7) संपत्ति का अधिकारः-
मूल संविधान में यह एक मौलिक अधिकार था लेकिन संसद ने 44वाँ संविधान संसोधन 1978 के तहत् अनुच्छेद- 300 (क) में इसे शामिल किया ।
♦ अपवाद: SC, ST और OBC
मूल संविधान में SC और ST को आरक्षण का प्रावधान किया गया लेकिन OBC को आरक्षण का प्रावधान नहीं था। OBC वर्ग के लोगों का आरक्षण V. P मंडल आयोग के सिफारिस पर प्रधामंत्री विश्वनाथ सिंह के द्वारा 1 प्रदान किया गया । OBC वर्ग के लोगों को 27% तक आरक्षण प्रदान किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का - गठन 1953 ई. में काका कालेकर की अध्यक्षता में हुआ, वहीं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 ई. में V. P मंडल की अध्यक्षता में हुआ ।
♦ क्रिमीलेयर:
इन्दिरा सहनी केस 1992 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमीलेयर का सिद्धांत दिया। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वैसे लोग जिनका वर्तमान में सलाना आय 8 लाख रूपया या उससे अधिक हो वे क्रिमीलेयर श्रेणी में आते हैं।
ओ.बी.सी. वर्ग के वैसे लोग जो क्रिमीलेयर की श्रेणी में आते हैं उन्हें 27% आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है।
स्वतंत्रता का अधिकार (19-22) :
अनुच्छेद-19
वर्तमान में यह अनुच्छेद 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है ।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ( बोलने की, पुतला जलाने की, झण्डा फहराने की सुचना का अधिकार)
- सभा करने का अधिकार (हथियार वर्जित)
- चारों ओर भ्रमण करने का अधिकार (भारत में)
- भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता
- संपत्ति का अधिकार (अर्जित)
- व्यवसाय करने का अधिकार
नोट- संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया जिसे सरकार छीन सकती है।
अनुच्छेद- 20
दोष सिद्धि से संरक्षण
★ यह अनुच्छेद दोषी को तीन प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है ।
(1) अपराधी जिय समय अपराध करता है उसे उसी समय के कानून के हिसाब से सजा दिया जायेगा ।
(2) अपराधी को एक गलती की एक ही सजा दिया जायेगा ।
(3) अपराधी स्वयं के खिलाफ गवाहीं नहीं दे सकता है।
अनुच्छेद-21
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
★ यह अनुच्छेद हमें गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार व्रदान करता है। इस अनुच्छेद को व्यापक रूप मेनका गाँधी वाद 1978 के द्वारा प्रदान किया गया। इस अनुच्छेद के तहत् निम्न अधिकारों को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।
प्राण की स्वतंत्रता
(1) हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं।
(2) हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता है ।
(3) हम पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं।
(4) अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना
दैहिक स्वतंत्रता
(1) हम अकेला रह सकते हैं। (एकांतवास)
(2) विदेश जाने की स्वतंत्रता
(3) निजता का अधिकार
(4) व्यभिचार (Adualty) ( शादी होने के बाद भी हम किसी से संबंध रख सकते हैं।- लड़के-लड़कियाँ के स्वेच्छा पूर्वक)
नोट - (1) पिरथीनाथ बनाम भारत संघवाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने आत्म हत्या के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया ।
(2) ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य वाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि आत्म हत्या करना मौलिक अधिकार नहीं है। लोगों को अपने जीवन जीने पर जोर देनी चाहिए ।
आत्महत्याः
भारतीय दंड संहिता धारा 309 के तहत् आत्म हत्या करना दण्डनीय अपराध है ।
अनुच्छेद - 21 (क)
यह मूल संविधान में नहीं था । इसे 86वाँ संविधान संसोधन 2002 के तहत् शामिल किया गया तथा यह कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जायें अर्थात, हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद - 21 (क) के तहत् शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।
अनुच्छेद- 22
गिरफ्तारी के विरूद्ध संरक्षण
यह अनुच्छेद गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को तीन प्रकार का संरक्षण देता है-
(1) गिरफ्तारी का कारण जान सकें ।
(2) गिरफ्तार होने के 24 घंटा के भीतर जज के समक्ष ले जाया जायें |
(3) अपना मनपसंद वकील रख सकता है।
नोट- अनुच्छेद- 22 दो प्रकार के लागों को प्राप्त नहीं होता है-
(1) शत्रु देश के विदेशी नागरिक को
(2) निवारक निरोध कानून के तहत् जिसे गिरफ्तार किया जाता है।
निवारक निरोध क़ानूनः-
वैसा कानून जिसके तहत्- अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि, अपराध ना हो । यह कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है जिस कारण इस पर नियम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों बना सकती है। इस कानून को रॉलेट एक्ट की संज्ञा दी जाती है तथा इस कानून को भारतीय संविधान की आवश्यक बुराई भी कहा जाता है । इस कानून के तहत् किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर अधिकतम 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है। इसमें अधिकतम समय तक नज़रबंद रखने हुतू सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। अगर सलाहकार परिषद सिफारिस करता है तब ही 3 माह से अधिक समय तक नज़रबंद किया जा सकता है ।
मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आपातः-
अनुच्छेद- 352 के तहत् जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात लागू होने से मालिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद- 352 लागू होता है तो अनुच्छेद- 358 स्वतः लागू हो जाते हैं तथा हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद- 19 निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद- 19 के अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित करने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद- 359 के तहत् करते हैं।
- 44वाँ संविधान संसोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि अपातकाल के दौरान में अनुच्छेद- 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। अर्थात ये दोनों ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं।
शोषण के विरूद्ध अधिकार ( 23-24 )
अनुच्छेद- 23
मानव के र्दुव्यवहार और बलातश्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
नोट- अनुच्छेद- 23 के प्रावधानों को प्रभावी तरीका से लागू करने के लिए ही बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया ।
अनुच्छेद- 24
14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या किसी भी खतरनाक काम में शामिल नहीं किया जायें।
बचपन बचाओ आंदोलन:-
यह आंदोलन कैलाश सत्यर्थी के द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन के द्वारा कैलाश सत्यर्थी ने कारखाना में काम कर रहें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुक्त कराकर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का काम किया।
इस कार्य के लिए ही कैलाश सत्यर्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ( 25-28)
अनुच्छेद- 25
यह अनुच्छेद हमें अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने, उसके अनुरूप आचरण करने तथा अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है । इस अनुच्छेद के प्रावधानों के कारण ही सिख धर्म के लोग कृपान रखते हैं ।
♦ बौद्ध, जैन तथा सीख हिन्दु धर्म का अंग है ।
अनुच्छेद- 26
धार्मिक कार्यो का प्रबंधन
अनुच्छेद- 27
किसी भी के वृद्धि या पोषण में जो व्यय किये जाएगें उसपर "कर" नहीं लगेगा।
अनुच्छेद- 28
सरकारी धन से चल रहें संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा ।
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार (29 - 30)
अनुच्छेद- 29
यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाकर रख सकता है ।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यकों को भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाकर रखने का अधिकार है।
नोट- भारत में अल्पसंख्यक होने का आधार धार्मिक तथा भाषायी है।
- भारत में हिंदु बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावे अन्य सभी समुदाय जैसे- मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इत्यादि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं ।
अनुच्छेद- 30
यह अनुच्छेद् अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को यह अधिकार देता है कि वह अपना शैक्षणिक संस्थान खोलकर वहाँ शासन-प्रशासन भी चला सकता है I
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (32)
अनुच्छेद- 32
अनुच्छेद- 32 यह कहता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसे बहाल करवाने के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसे ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद- 32 को माना जाता है।
- मौलिक अधिकार हनन होने की स्थिति में अगर हम अनुच्छेद- 32 के सुप्रीम कोर्ट जाते है, तो वही अनुच्छेद- 226 के तहत्ं हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट याचिका (Writ) जारी करता है ।
याचिका (Writ) 5 प्रकार का होता है जो निम्न है -
1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण 2. परमादेश 3. अधिकार पृच्छा लेख 4. प्रतिशेधं लेख 5. उत्प्रेषण
सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के रिट जारी करने में अंतर-
|
सुप्रीम कोर्ट |
|
हाई कोर्ट |
| 1. |
सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत वर्ष के लिए रिट जारी करता है। |
1. |
हाई कोर्ट संबंधित राज्य के लिए रिट जारी करता है । जैसे- पटना हाई कोर्ट बिहार के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तरप्रदेश के लिए | |
| 2. |
सिर्फ मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है । |
2. |
हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का हनन, कानूनी अधिकार का हनन, संवैधानिक अधिकार का हनन इत्यादि में रिट जारी करता है । |
| 3. |
सुप्रीम कोर्ट के विरूद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। |
|
|
1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण ( हवियस कर्पस):
इसका शाब्दिक अर्थ 'सशरीर प्रस्तुत करना होता है। इस रिट के माध्यम से न्यायलय गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर न्यायलय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस रिट के माध्यम से अनुच्छेद - 21 और 22 (मौलिक अधिकार) की रक्षा होती है ।
2. परमादेश (मेंडामस):
इसका शाब्दिक अर्थ 'हम आदेश देते हैं' होता है। यदि लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तब यह रिट / याचिका जारी किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्राइवेट व्यक्ति को लेकर यह स्टि जारी नहीं किया जाता है ।
3. अधिकार पृच्छा - लेख (को-वेरेन्टो):
इसका शाब्दिक अर्थ 'किस अधिकार से' होता है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक महत्व के पद पर बैठे पदाधिकारी के पद की वैधानिकता की जाँच की जाती है। यह रिट प्रसाद-प्रयत्न के पद को लेकर जारी नहीं होता है । यह रिट राष्ट्रपति को लेकर जारी हो सकता है लेकिन राज्यपाल को लेकर जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद - प्रयत्न पद हैं।
4. प्रतिशेध (प्रोहिविशन):
इसका शाब्दिक अर्थ 'रोकना' होता है। यह एक न्यायिक रिट है। यह रिट उपर के न्यायलय नीचे के न्यायलय को लेकर तब जारी करता है जब सुनवाई (निर्णय) नहीं हुआ हो ।
5. उत्प्रेषण (सरटियोरी):
इसका शाब्दिक अर्थ 'प्रमाणित करना होता है। यह भी एक प्रकार का न्यायिक रिट है । यह रिट उपर के न्यायलय नीचे के न्यायलय को लेकर तब जारी करता है जब निर्णय हो गया हो ।
नोट- पोस्टमार्टम की संज्ञा उत्प्रेशन रिंट को दिया जाता है ।
नोट- न्यायिक रिट हमेशा उपर के न्यायलय नीचे के न्यायलय को लेकर जारी करता है
अनुच्छेद- 33
खुफिया बल, पुलिस बल, सुरक्षा एजेंसी, सशस्त्र पुलिस बल, इत्यादि के बीच अनुशासन बनायें रखनें को लेकर इन लोगों के मौलिक अधिकारं पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद- 34
अगर देश के किसी क्षेत्र में मार्सल लॉ (सेना का कानून ) लागू हो और उस क्षेत्र के लिए सेना ने कोई आदेश दण्डादेश पारित किया हो तो संसद को स्वीकृति देनी होती है ।
अनुच्छेद- 35
यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार को अधिक से अधिक प्रभावी बना सकता है।
मौलिक अधिकार को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच होने वाले विवाद -
(1) सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के माध्यम से यह कहा है कि संसद मौलिक अधिकार में संसोधन नहीं कर सकती है।
(2) भारतीय संसद ने 24वाँ संविधान संसोधन 1971 के द्वारा यह प्रावधान किया कि मौलिक अधिकार में संसद संसोधन कर सकती है l
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..