General Competition | Science | Biology (जीव विज्ञान) | ऊतक विज्ञान
समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक सामान्य कार्य करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। उत्तक कोशिका का समूह है, एक उत्तक की सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है ।
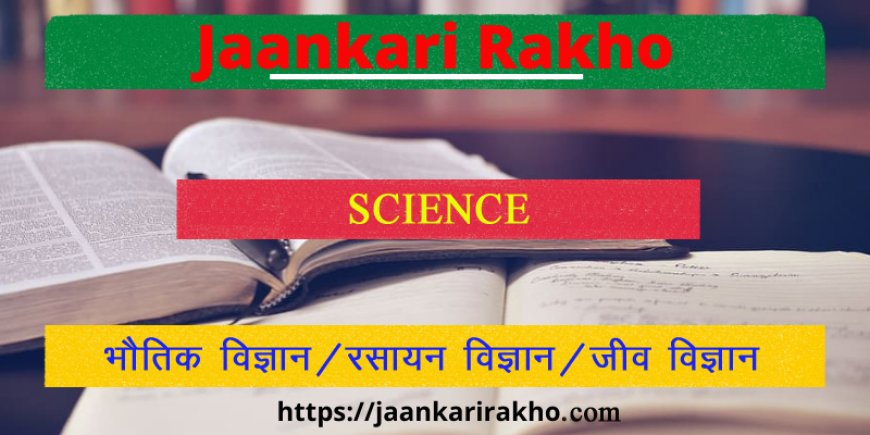
General Competition | Science | Biology (जीव विज्ञान) | ऊतक विज्ञान
- समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक सामान्य कार्य करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। उत्तक कोशिका का समूह है, एक उत्तक की सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान होती है ।
- पौधा तथा जंतु की कोशिका लगभग समान होते हैं परंतु पौधा तथा जंतु के उत्तक अलग-अलग होते हैं।
- पौधों को उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बाँटा गया है-
- विभज्योतकी उत्तक (Meristematic Tissue) तथा 2. स्थायी उत्तक ( Parmanent Tissue)
- विभज्योतकी उत्तक-
- यह उत्तक ऐसी कोशिका की बनी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है । उत्तक की कोशिकाएँ गोल, अंडाकार या बहुभुजी होता है।
- इस उत्तक के कोशिका के बीच खाली जगह (Intercellular Space) नहीं होता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य प्रचुर मात्रा में भरी रहती है परन्तु इन कोशिका में रिक्तिता (Vacuoles) छोटी होती है अथवा नहीं होती है।
- स्थिति के आधार पर विभाज्योतिकी उत्तक को तीन भागों में बाँटा गया है।
- Apical Meristem ( शीर्षस्थ विभाज्योतिकी) - यह उत्तक तने के अग्र भाग में रहते हैं। इस उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप ही पौधा लंबाई में बढ़ते हैं। पौधा की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि (Primary Growth) कहलाता है।
- Lateral Meristem (पार्श्व विभाज्योतिकी) — ये उत्तक तने और जड़ों के किनारे में होते है। इस उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप पौधा का मोटाई बढ़ता है। पौधा का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक को कैम्बियम (Cambium) भी कहते हैं ।
- Intercalary Meristem (अंतर्वेशी विभाज्योतिकी)- ये शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक के ही भाग है जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। यह उत्तक प्रायः पत्तियों के आध र पर तनों के पर्व (Inter Node) तथा पर्वसंधि (Node) के पास पाये जाते हैं। यह उत्तक शीघ्र ही स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं ।
- Parmanent Tissue (स्थायी उत्तक)
- विभाज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएँ लगातार विभाजित होकर स्थायी उत्तक बनाता है ।
- स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं- (i) साधारण स्थायी उत्तक (Simple parmanent Tissue) तथा -(ii) जटिल स्थायी उत्तक (Complex Parmant Tissue)
(i) साधारण उत्तक (Simple Tissue)
-
-
- इस उत्तक में समान आकार के कोशिका पाये जाते हैं तथा सभी कोशिका मिलकर समान कार्य करती है ।
- साधारण स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं।
-
- पेरेनकाइमा उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। इस उत्तक की कोशिका प्रायः गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होता है। इन उत्तक के कोशिका के बीच खाली स्थान (Intercellular Space) पाये जाते हैं।
- यह उत्तक पौधों के सभी कोमल भाग में पाये जाते हैं। यह उत्तक जाइलम और फ्लोएम के मिर्माण में भी भाग लेते हैं।
- इस उत्तक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थों को जमा करके रखना है।
- कुछ पेरेनकाइमा उत्तक में क्लोरोप्लास्ट भी पाये जाते हैं जिसके कारण यह उत्तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जिस पेरेनकाइमा उत्तक में क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसे हरित उत्तक (Chlorenchyma) कहते हैं ।
- जलीय पौधा का पेरेनकाइमा उत्तक वायुतक (arenchyma) में बदल जाता है । वायुतक जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है।
- यह उत्तक भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है लेकिन कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होते हैं I
- इस उत्तक की कोशिका लंबी, गोल अनियमित ढंग से कोणों पर मोटी होती है। सेलुलोज के अधिकता के कारण इस कोशिका की कोशिका मित्ती (Cellwall) मोटी होती है।
- यह उत्तक केवल कमजोर पौधों में ही पाये जाते हैं तथा पौधों को प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों में इस उत्तक का अभाव रहता है।
- कभी-कभी इस उत्तक में हरित लवक (Chloroplast) भी पाये जाते हैं। जिससे कुछ मात्रा में यह प्रकाशसंश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं।
- यह उत्तक मृत कोशिका के बने होते हैं। इस उत्तक की कोशिका लम्बी, सँकरी तथा मोटी कोशिका भित्ती वाले होते हैं।
- इस उत्तक के कोशिका के बीच कोई खाली जगह नहीं होता है। इस उत्तक के कोशिकाओं में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है, यह रसायन कोशिका को काफी मजबूत बना देता है।
- यह उत्तक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधों से प्राप्त जूट, सनई, पटवा, दृढ़उत्तक है।
- यह उत्तक पौधा को यांत्रिकी सहायता पहुँचाते हैं तथा पौधा के आंतरिक भाग को सुरक्षा देते हैं।
(ii) जटिल उत्तक (Coplex Parmanent Tissue)
- जटिल उत्तक विभिन्न आकार की कोशिका के बने होते हैं परन्तु सभी कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं।
- जटिल उत्तक दो प्रकार के हैं- A. Xylem तथा B. Phloem. Am
- जाईलम उत्तक चार प्रकार के कोशिकाओं का बना होता जाइलम उत्तक पूरे पौधे में पाया जाता है जिसका सर्वप्रमुख काम है जल का संवहन करना। इसके अलावे जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता देता है तथा भोजन संग्रह भी करता है ।
- जाइलम जिस चार प्रकार के कोशिकाओं के बने हैं वे है- वाहिनीकाएँ ( Tracheids), वाहिकाएँ (Vessels), जाइलम तंतु (Xylem Fibres) तथा जलाइम मृदुतक (Xylem Parenchyma).
- वाहिनिकाएँ का मुख्य काम है जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुँचाना। वाहिकाएँ तथा जाइलम तंतु पौधों का यांत्रिकी सहायता देता है तथा जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह करता है ।
- जाइलम उत्तक के जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित रहता है बाकी सभी कोशिका मृत होती है।
- जाइलम के तरह फ्लोएम भी चार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये चार कोशिकाएँ हैं- चालनी नालिका (Sieve Tubes), सहकोशिका (Campanion Cells), फ्लोएम तंतु ( Phloem Fibres), फ्लोएम मृदुतक (Phloemparchchyma).
- फ्लोएम में फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका है बाकी सभी जीवित कोशिका है।
- फ्लोएम उत्तक जाइलम के साथ-साथ पौधे के सम्पूर्ण भाग में पाये जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में पहुँचाना।
- रक्षी उत्तक के अंतर्गत बाह्य त्वचा (Epidermis ) तथा कॉर्क (Cork) आते हैं।
A. बाह्य त्वचा ( Epidermis )
- एपिडर्मिस की कोशिका पौधा के सभी भाग (जड़, तना, पत्ती) की रक्षा करता है। यह उत्तक पौधों को जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के अघातों से बचाता है।
- मरूस्थलीय पौधों के एपिडर्मीस में क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है, जो पौधों में जल-हानि को रोकता है।
- जड़ों के एपीडर्मिस के मूलरोम ( Root hairs) पाये जाते हैं जो भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं।
- समय के साथ-साथ जब जड़ तथा तना पुराने होते जाते हैं, तब तने के एपीडर्मिस का स्थान पर कॉर्क कैंबियम आ जाता हैं यही कॉर्क कैंबियम (पार्श्व विभाज्योतिकी) की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क (छाल) का निर्माण करता है।
- कॉर्क के सभी कोशिका मृत होती है। कॉर्क का मुख्य काम है- पौधों को सुरक्षा देना ।
- कॉर्क में सुबेरीन नामक रसायन रहता है जिसके कारण कॉर्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता है।
- कॉर्क का इस्तेमाल बोतल के कॉर्क बनाने, में खेल का समान बनाने में होता है। व्यापारिक कॉर्क क्वेकर्स सुबेर नामक पौधा से प्राप्त होता है ।
- वार्षिक वलय (Annual rings)
- विभिन्न ऋतुओं में मौसम बदलने के कारण कैम्बीयम (पार्श्व विभाज्योजिकी) की सक्रियता में परिवर्तन होता है। इस कारण पौधो में स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण होता है ।
- वार्षिक वलय पौधा के एक वर्ष के वृद्धि को दर्शाता है। पौधा में जितने वार्षिक वलय होते हैं पौधा की आयु उतनी ही मानी जाती है।
- ऐसा क्षेत्र जहाँ सालोभर मौसम के समान होता है, वहाँ के पौधा में वार्षिक वलय नहीं बनते । समुद्र के आस-पास उगने वाले पौधा में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि समुद्र के आस-पास सालोभर मौसम समान रहता है।
- वार्षिक वलय (Annual rings)
- जंतु में चार प्रकार के उत्तक पाये जाते हैं।
- Epithelium Tissue (उपकला उत्तक)
- Connective Tissue (संयोजी उत्तक)
- Muscular Tissue (पेशी उत्तक)
- Narvous Tissue (तंत्रिका उत्तक)
- Epithelium Tissue ( उपकला उत्तक)
- एपीथीलीयम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। इस उत्तक के कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है।
- एपीथीलीयम उत्तक का मुख्य कार्य अंगों का सुरक्षा प्रदान करना है। यह उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थ के विसरण, स्त्रवण (Secretion) तथा अवशोषण में सहायता करते हैं ।
- एपीथीलीयम उत्तक को चार भागों में बाँटा गया है-
- शल्की एपीथीलीयम ( Squamous epithelium)
- यह उत्तक की आकृति फर्श या दिवार पर लगी चपटी ईट की तरह होती है।
- त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी उत्तक से होता है। इसके अलावे यह उत्तक रक्तवाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं ।
- स्तंभाकार एपीथीलीयम (Columnar epithelium)
- इस उत्तक की कोशिका लंबे होते हैं तथा कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रो विलाई होते हैं।
- यह उत्तक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहाँ अवशोषण या स्त्रवण का काम होते हैं। जैसे- आंत, अमाशय, पित्ताशय ।
- घनाकार एपीथीलीयम (Cuboidal epithelium)
- इस उत्तक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। यह उत्तक के द्वारा शरीर में ग्रंथि (glands) का निर्माण होता है।
- प्रमुख ग्रंथि-
- स्वेद ग्रंथि (Sudoriferous Gland )- यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत (Epidermis) में पाये जाते हैं। इनके द्वारा पसीने का स्त्राव होता है ।
- लैक्राइमल ग्रंथि (Lachrymal Glands)- यह ग्रंथि आँख में पायी जाती है, जिससे आँसू का स्त्राव होता है। आँसू में लाइसोजाम नामक विशेष इंजाइम पाये जाते हैं जिससे प्रभाव से आँख में आये हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं।
- मिस ग्रंथि (Ceruminous Glands) - यह स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाया जाता है। इस ग्रंथि मोम के समान पदार्थ स्त्रावित होता है ।
- सीबम ग्रंथि (Sebum gland)- यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस (मीतरी परत ) में पायी जाती है। यह ग्रंथि एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्त्रावित करती है जिसे सीबम कहते हैं जो त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है।
- पक्ष्माभी उपकला (Ciliated epithelium)-
- इस उत्तक की कोशिका लम्बी होती है तथा इसमें सिलिया (Cilia) पाये जाते हैं। यह उत्तक ट्रैकिया के भितरी सतह में, अंडवाहिनी (oviduct) गर्भाशय में पाये जाते हैं ।
- यह उत्तक अंगों द्वारा स्त्रावित पदार्थ को सिलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थों को एक ही दिशा में जाने मदद करता है I
- शल्की एपीथीलीयम ( Squamous epithelium)
- Connective Tissue (संयोजी उत्तक)
- संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों तथा उत्तकों को जोड़ने का काम करता है।
- संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है ।
- उत्तक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं इसे मैट्रीक्स कहते हैं । विभिन्न संयोजी उत्तक के मैट्रीक ठोस, जेली के समान, सघन, कठोर या तरल हो सकते हैं।
- संयोजी उत्तक के प्रमुख प्रकार-
- अवकाशी उत्तक (Areolar Tissue)
- यह उत्तक रक्तवाहिनीयों (Blood Vessels) तथा तंत्रिकाओं (Nerves Cells) के चारों तरफ घेरा बनाता है।
- एरियोलर उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी या दो मांसपेशी को आपस में जोड़ता है।
- मास्ट कोशिका - यह एरियोलर उत्तक में पाई जाने वाले कोशिका है। यह कोशिका रूधिर वाहिनी के चारों तरफ पायी जाती है। इस कोशिका द्वारा हिस्टामिन (प्रोटीन), हिपैटीन (कार्बोहाइड्रेट) तथा सीरोटोनीन (प्रोटीन) स्त्रावित होता है।
- हिस्टामिन रूधिर वाहिनी को फैलाता है। हिपैरीन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है तथा सिरोटोनीन रूधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है।
- एरियोलर उत्तक के श्वेत तंतु कोशिका (White Fibres cells) द्वारा कॉलेजन प्रोटीन तथा पीला तंतु कोशिका (Yellow Fibres Cells) द्वारा एलास्टीन प्रोटीन स्त्रावित होता है।
- वसा संयोजी उत्तक (Adipose Connective Tissue)
- यह उत्तक वसा कोशिका (Fat cells) से बनी होती है, इन कोशिका में वसा छोटी-छोटी बूँदी के रूप में भरी रहती है।
- यह उत्तक वसा को संचित करके रखता है। यह शरीर के ताप को बनाये रखता है ।
- शरीर के वसा कोशिका के अधिकता से मोटापा का सामना करना पड़ता है।
- कंडरा (Tendon)
- यह संयोजी उत्तक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। यह उत्तक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लीचीले होते हैं ।
- स्नायु (Ligament)
- यह उत्त हड्डीयों (अस्थि) को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। यह उत्तक अत्यधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं।
- उपास्थि उत्तक (Cartilage)
- यह उत्तक कोंड्रियो ब्लास्ट कोशिका के बने होते तथा इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में कोंड्रीन प्रोटीन पाया जाता है।
- उपास्थि अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है। ये उत्तक बाह्यकर्ण, नाक, श्वासनली (ट्रेकिया), स्टरनम जैसे अंगों में पाये जाते हैं।
- अस्थि (Bone)
- यह काफी मजबूत संयोजी उत्तक हैं क्योंकि इस उत्तक के मैट्रीक्स कैल्शियम तथा फॉस्फोरस लवण से बना होता है। अस्थि के मैट्रीक्स में ओसीन नामक प्रोटीन होता है।
- लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा (Marrow cavity) कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडीपोज उत्तक (वसा उत्तक) भरा रहता है तो उस मज्जा गुहा को अस्थिमज्जा (Bone Marrow) कहते हैं ।
- अस्थिमज्जा दो तरह के होते (अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा तथा बीच वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा पायी जाती है।
- लाल अस्थि मज्जा में RBC ( लाल रक्त कण ) तथा पीली अस्थि मज्जा में WBC (श्वेत रक्त कण ) का निर्माण होता है।
- स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान रचना होता है जिसे हैवर्सियन नलिका कहते हैं । हैवर्सियन नलिका की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण है।
- रक्त (Blood)
- रक्त तरल संयोजी उत्तक है क्योंकि इस उत्तक के मैट्रीक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं ।
- रक्त के तरल भाग या मैट्रीक्स को प्लाज्मा कहते हैं तथा प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती रहती है।
- रक्त का 50% भाग प्लाज्मा का बना होता है शेष 45% रूधिर कोशिका होता है।
- प्लाज्मा का 90% भाग जल से बना होता है शेष में 7% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
- रक्त में तीन प्रकार की कोशिका होती है-
(i) लाल रक्त कण (RBC), (ii) श्वेत रक्त कण (WBC) तथा (iii) प्लेटलेट्स (Platelets)
- लसीका (Lymph)
- लसीका, रक्त के समान ही तरल संयोजी उत्तक है । लसीका में केवल श्वेत रक्त कण (WBC) होते हैं। इसमें लाल रक्त कण तथा प्लेटलेट्स का अभाव होता है।
- लसीका की कोशिका एंडीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकता है।
- लसीका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थों का भी परिवहन होता है।
- अवकाशी उत्तक (Areolar Tissue)
- Muscular Tissue ( पेशी उत्तक)
- इस उत्तक की कोशिका लंबी-लंबी होती है तथा इन कोशिका में एक प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं, इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं ।
- यह उत्तक का मुख्य काम जीवों को प्रचलन में मदद करना है।
- पेशी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं-
- आरेखित या अनैच्छीक पेशी (Unstriped Muscles)
- इस पेशी में होनेवाला संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता है, यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छीक पेशी कहते हैं।
- यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरीस में, वृषण (Testes ) में, मूत्र वाहिनी तथा मूत्राशय में, रक्तवाहिनीयों में पायी जाती है।
- रेखित पेशी या ऐच्छीक पेशी (Striped Muscles)
- यह पेशी जीव के कंकाल (हड्डी) से जुड़ी होती है तथा इनमें प्रसार तथा संकुचन जीवों के इच्छा के अनुरूप होता है।
- यह पेशी शरीर के बाहु पैर, गर्दन आदि में पायी जाती है एवं इस पेशी का कुल भार शरीर कुल भार का 50 प्रतिशत होता है।
- हृदय पैशी (Cardiac Muscles)
- हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं । हृदय पेशी की रचना रेखित पेशी के समान होता है।
- यह पेशी स्वभाव से अनैच्छीक होती है तथा जीवनभर इसमें प्रसार तथा संकुचन होते रहता है।
- आरेखित या अनैच्छीक पेशी (Unstriped Muscles)
- Narvous Tissue (तंत्रिका उत्तक)
- जीवों के मस्तिष्क, मेरूरज्जु (Spinal cord) तथा सभी तंत्रिकाएँ (Nerves) इसी उत्तक के बने होते हैं।
- तंत्रिका उत्तक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कहते हैं।
- यह उत्तक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इन उत्तक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है।
अभ्यास प्रश्न
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







