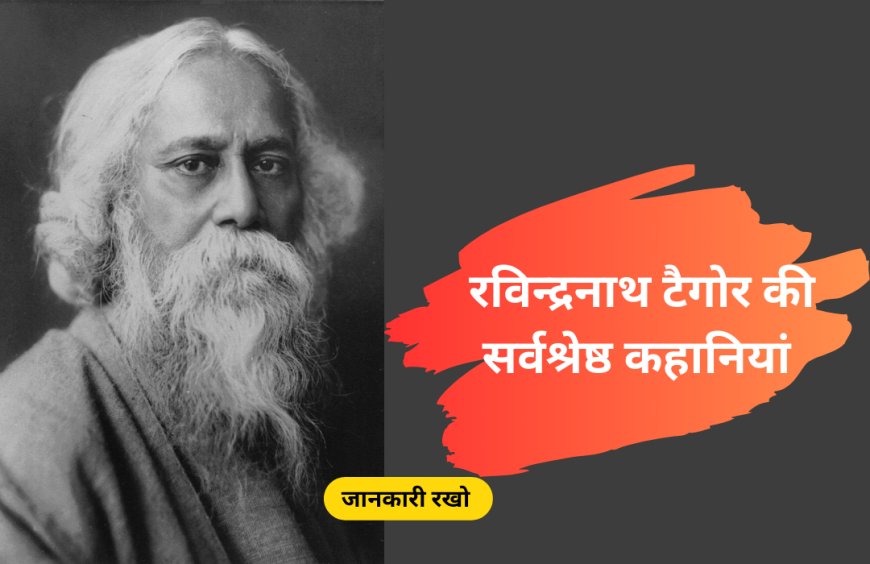गूंगी
कन्या का नाम जब सुभाषिणी रखा गया था, तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इससे पहले, उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेसिनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिणी। अब केवल सब उसे 'सुभा' ही कहकर बुलाते हैं ।
बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके थे। अब छोटी कन्या सुभा माता-पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती, वह सब कुछ अनुभव कर सकती है। यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुभा के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह-तरह की चिंताफिक्र की बातें किया करते हैं, किंतु स्वयं सुभा इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है । इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी । वह मन-ही-मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाएं तो अच्छा हो, लेकिन जहां पीड़ा है, उस समय पीड़ा की तरह जीती-जागती बनी रहती है ।
विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर, उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है । शुभा के पिता वाणीकंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, परंतु माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है ।
सुभा को बोलने की जुबान नहीं है, लेकिन उसकी लम्बी-लम्बी पलकों में दो बड़ी-बड़ी काली आंखें अवश्य हैं और उसके ओष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप-कांप उठते हैं।
वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, उनको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है। बस, कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए और वह हर समय ठीक भी नहीं होता, ताकत की कमी से बहुधा उसमें भूल हो जाती है, लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन अपने-आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते और कभी सिकुड़ते हैं। कभी-कभी आंखें चमक-चमककर जलने लगती हैं और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ-सी जाती हैं, कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती हैं तो कभी चंचल दामिनी की तरह, ऊपर-नीचे, इधर-उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं और विशेषकर मुंह के भाव के सिवाय जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं, उसकी आँखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती ही है। करीब-करीब साफ-सुथरे नील-गगन के समान।
उन आंखों को उदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, छवि-लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जिहाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है और यही कारण है कि साधारण लड़के-लड़कियों को उसकी ओर से किसी-न-किसी प्रकार का भय-सा बना रहता है, उसके साथ कोई खेलता नहीं । वह नीरव दुपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासिनी बनी रहती ।
गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी-सी सरिता है। गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है। उसको तनिक भी आलस्य नहीं, वह अपनी इकहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक-न-एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव हैं और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं। जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने-आपको भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्न- चित्त असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जा रही है।
वाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय - घर, भुसे का ढेर, आम, कटहल और केलों का बगीचा हरेक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घर में, आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में, उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं, मालूम नहीं, किंतु काम-धंधे से ज्योंही उसे तनिक फुरसत मिलती, त्योंही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती।
प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है। नदी की स्वर - ध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़-पौधों की मर्मर ध्वनि, यह सब मिलकर चारों ओर के गमना-गमन आंदोलन और कम्पन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिर-स्तब्ध हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट-फूट पड़ती हैं। प्रकृति के यह अनोखे शब्द और अनोखे गीत—यह भी तो गूंगी की ही भाषा है, बड़ी बड़ी आंखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिणी की जो भाषा है, उसी का मानो. वह विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झींगुरों की झिनझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर शब्दातीत नक्षत्र - लोक तक केवल इंगित, संगीत, क्रंदन और उच्छवास भरी पड़ी हैं।
दोपहर को नाविक और मछुए, खाने के लिए अपने-अपने घर जाते, गृहस्थ और पक्षी आराम करते, पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती, जन-समाज अपने सारे काम-धंधों को बीच में रोककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करते। उस समय रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने-सामने चुपचाप बैठी रहतीं । एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे-से वृक्ष की छाया में ।
सुभाषिणी की कोई सहेली ही नहीं थी । गोशाला में दो गाएं हैं। एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती । ये नाम सुभाषिणी के मुंह से उन गार्यो ने कभी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली-भांति पहचानती हैं। सुभाषिणी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है, जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लाड़ करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती। इन बातों को उसकी ‘सारो’ और ‘पारो’ इंसान से कहीं अधिक और भली-भांति समझ जाती हैं।
सुभाषिणी गोशाला में घुसकर अपनी दोनों बांहों से जब 'सारो' की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती है, तब 'पारो' स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई, उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिणी दिन-भर में कम-से-कम दो-तीन बार तो नियम से गोशाला में जाया करती । इसके सिवाय अनियमित आना-जाना भी बना रहता । घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता । सुभाषिणी के सहनशील और विषाद- शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान-शक्ति में उसकी बांहों पर सींग घिस घिसकर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करतीं।
इसके सिवाय, एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुभाषिणी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब-तब सुभाषिणी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। सुभाषिणी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता, मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है ।
ऊंची श्रेणी के प्राणियों को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके बोलने की जिह्वा है और वह गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं है ।
वह था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप । प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता-पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई काम-काज करके घर-गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा।
निकम्मों के लिए एक बड़ा सुभीता यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहें, पर बाहरी जनों के लिए वे प्रायः स्नेहपात्र होते हैं। इसका कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिलकियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एक-आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांवों में दो-चार निठल्ले- निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है। काम-धंधे में, हास - परिहास में और जहां कहीं भी एक-आध की कमी देखी, वहीं वे चट-से हाथ के पास ही मिल जाते हैं ।
प्रताप की विशेष रुचि एक ही है । वह है मछली पकड़ना। इससे उसका बहुत-सा समय आसानी से कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के किनारे पर बहुधा वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिणी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है, अतः प्रताप, सुभाषिणी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिणी को ‘सुभा' कहते, किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुभा को ‘सू' कहकर पुकारता ।
सुभाषिणी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता- जल में कांटा डालकर उसकी ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगाकर लाती । शायद, बहुत देर तक बैठे-बैठे, देखते-देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे उसके किसी काम में सहारा दे। उसके मन में ऐसा आता था कि किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और न वह कुछ कर ही सकती थी। वह मन-ही-मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वह जादू-मंतर से चट से कोई ऐसा चमत्कार दिखा सके, जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे — 'अच्छा! 'सू' में यह करामात ! मुझे क्या पता था ?'
मान लो, सुभाषिणी यदि जल-परी होती और धीरे-धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे-से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत-प्रसाद में स्वर्ण-जड़ित शय्या पर कौन बैठी है? और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता—‘अरे! यह तो अपने वाणीकंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है ‘सू’। मेरी ‘सू’ आज मणियों से जटिल, गम्भीर, निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जल-परी बनी बैठी है ।'
तो! क्या यह बात हो ही नहीं सकती, क्या यह नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी, 'सू’ प्रजा- शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणीकंठ के घर पैदा हुई है और इसीलिए वह आज ‘गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती।'
सुभाषिणी की अवस्था दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी । धीरे-धीरे मानो वह अपने आपको अनुभव कर रही है। मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वर - सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भर-भर देता है। अब मानो वह अपने आपको देख रही है। अपने विषय में कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती।
पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे-से कक्ष के झरोखे को खोलकर, भय से ग्रस्त अवस्था में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा । देखा कि पूर्णिमा-प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है। वह भी यौवन के उन्माद से, आनंद से, विषाद से, असीम नीरवता की अंतिम परिधि तक, यहां तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। मानो इस स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो ।
इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता-पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यहां-वहां निंदा कर रहे हैं। यहां तक कि जाति- विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है । वणीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते-पीते आराम से हैं और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है।
स्त्री-पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह-मशविरा हुआ। कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर परदेश चले गए।
अंत में, एक दिन लौटकर पत्नी से बोले – “चलो, कोलकाता चलें?”
कोलकाता जाने की तैयारियां पूरे जोर-शोर से होने लगीं। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुभा का सारा अंतःकरण आंसुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भावी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों से मूक पशु की तरह लगातार अपने माता-पिता के साथ रहती और अपने बड़े-बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखती मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती, पर वे उसे, कोई भी बात समझाकर बताते ही नहीं थे ।
इसी बीच में एक दिन, शाम के समय तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते-हंसते पूछा – “क्यों री 'सु' मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है । तू विवाह करने कोलकाता जा रही है। देखना, कहीं हम लोगों को भूल मत जाना।” इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा ।
तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की ओर ताकती और आंखों-ही-आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती है 'मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ।'
सुभा ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा । उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी | वाणीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे। सुभा उनके चरणों में पास बैठकर उनके मुख की ओर देखते हुए रोने लगी। अंत में बेटी को दिलासा और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर आंसू की दो बूंदें ढुलक पड़ीं। कल कोलकाता जाने का शुभ मुहूर्त है। सुभा गोशाला में अपनी चिर-संगिनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से सहलाकर गले में बाहें डालकर, वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी-भरकर उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बांध को न रोक सके।
उस दिन शुक्ला- द्वादशी की रात थी । सुभा अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने-पहचाने सरिता-तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई । मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बांहों को लिपटाकर कहना चाहती है— 'तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर मां ! मेरे समान तू मुझे अपनी बांहों में पकड़े रख, कहीं मत विदा कर ।'
कोलकाता के एक किराए के मकान में एक दिन सुभा की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया। उसका जूड़ा बांधा, उसमें जरी का फीता लपेट दिया। आभूषणों से लादकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुभा के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे। नेत्र कहीं सूख न जाएं, इस भय से माता ने उसे समझाया-बुझाया और अंत में फटकारा भी, परंतु अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की ।
उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया । कन्या के माता-पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे । मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों । अंदर से बहुत डांट-फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया।
निरीक्षकों ने बहुत देर के उपरांत कहा – “ऐसी कोई बुरी भी नहीं है । "
विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है । फिर हिसाब लगाकर देखा गया कि जो हृदय आज माता-पिता के विछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है। अंत में कल वह उन्हीं के काम आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगीं। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा।
पात्र देखकर, खूब अच्छे मुहूर्त में सुभा का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता-पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी । सुभा का पति पछांह की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया ।
एक सप्ताह के अंदर ही सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, परंतु इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं है। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थीं, लेकिन कोई उसे समझ न सका । अब वह चारों ओर निहारती रहती है। उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे । उसके जन्म से परिचित थे। वे चेहरे उसे यहां दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित हो उठा और सृष्टिकर्ता के सिवाय और कोई उसे सुन ही न सका ।
अब की बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया ।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..