BPSC TRE 2.0 SOCIAL SCIENCE CLASS 9TH GEOGRAPHY NOTES | प्राकृतिक वनस्पति
प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है, जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं।
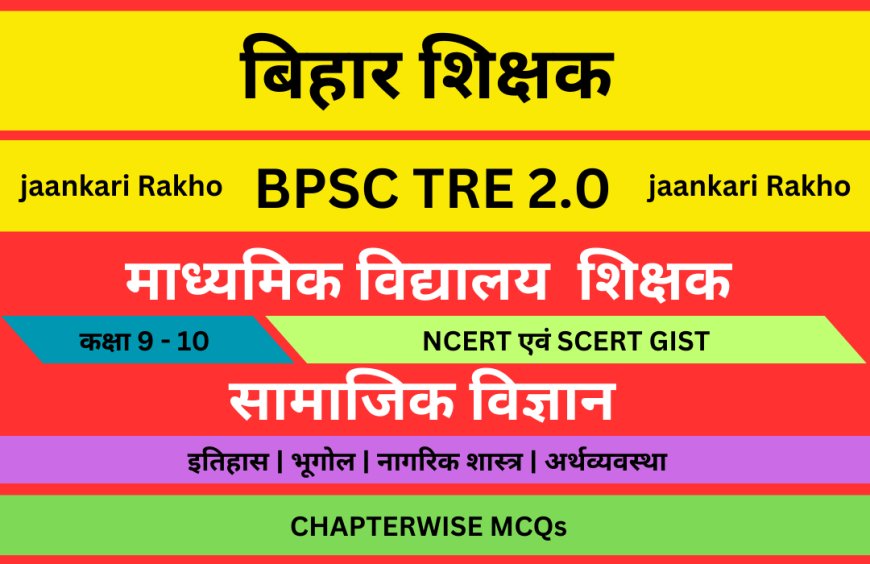
BPSC TRE 2.0 SOCIAL SCIENCE CLASS 9TH GEOGRAPHY NOTES | प्राकृतिक वनस्पति
- प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है, जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं।

- हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में दसवें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है।
- भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6 प्रतिशत है।
- इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं जैसे कि फर्न, शैवाल (एलेगी) तथा कवक (फंजाई) भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2021
- भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2021 जारी की।
- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), देहरादून को देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने का काम सौंपा गया था। देश में वनों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने का चलन वर्ष 1987 से शुरू हुआ था। इस प्रकार से 2021 में जारी हुई यह रिपोर्ट अपनी तरह की 17वीं रिपोर्ट है।
- भारत उन कुछ चुनिन्दा देशों में है जो अपने वन क्षेत्र की स्थिति पर एक वैज्ञानिक अध्ययन करते आया है। जिसके तहत भारत में वन क्षेत्र का आकार, घनत्व, आरक्षित और संरक्षित वनों की श्रेणी में वनाच्छादित भू-भाग की स्थिति और इनके बाहर वनाच्छादित भू-भाग की स्थिति पर भी एक आंकलन प्रस्तुत करता है।
- देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर हैं जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62 प्रतिशत है।
- 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें से वनावरण में 1,540 वर्ग किमी और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किमी की वृद्धि पाई गई है।
- वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है, उसके बाद यह बहुत घने जंगल में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी), इसके बाद तेलंगाना (632 वर्ग किमी) और ओडिशा (537 वर्ग किमी) हैं।
| 1- आंध्र प्रदेश | 647 वर्ग किलोमीटर, |
| 2. तेलंगाना | 632 वर्ग किलोमीटर, |
| 3. ओडिशा | 537 वर्ग किलोमीटर, |
| 4. कर्नाटक | 155 वर्ग किलोमीटर |
| 5. झारखंड | 110 वर्ग किलोमीटर |
अधिकतम वन क्षेत्र / आच्छादन वाले राज्य
- क्षेत्रफल के हिसाब से, मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।
| राज्य | वन क्षेत्र |
| मिजोरम | 84.53% |
| अरुणाचल | 79.33% |
| मेघालय | 76.00% |
| मणिपुर | 74.34% |
| नागालैंड | 73.90% |
इन राज्यों में 75 फीसदी से ज्यादा वन क्षेत्र
- पांच राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं।
- 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, असम, ओडिशा में वन क्षेत्र 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच है।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2021 में देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किमी है। 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है।
- मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य ओडिशा (8 वर्ग किमी), इसके बाद महाराष्ट्र (4 वर्ग किमी) और कर्नाटक (3 वर्ग किमी) हैं।
- देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2021 में काष्ठ भंडार को लेकर भी आंकड़े मुहैया कराये गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में काष्ठभंडार की क्षमता 6,167.50 मिलियन क्यूबिक मीटर है।
- जिसमें 4388.50 मिलियन क्यूबिक मीटर वन क्षेत्र के अंदर और 1779.35 मिलियन क्यूबिक मीटर वन क्षेत्र की सीमा से बहार मौजूद वन क्षेत्र में मौजूद है।
- बांस उत्पादन को लेकर इस रिपोर्ट में दिये गए आंकड़े भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बांस उत्पादन परियोजना के लिए निराशाजनक हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बांस उत्पादन का कुल क्षेत्रफल 1,49,443 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 10,594 वर्ग किलोमीटर की गिरावट 2019 की तुलना में दर्ज की गयी है।
- कार्बन भंडार जो एक नयी आर्थिक परियोजना के रूप में भी आकार ले रहा है उसके आंकड़े हालांकि थोड़ा उत्साहजनक हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र में कार्बन का भंडार 1204 मिलियन टन आँका गया है। यहाँ 79.4 मिलियन टन की वृद्धि पिछली रिपोर्ट की तुलना में दर्ज की गयी है।
- लगभग 39.7 मिलियन टन की वृद्धि हुई है जो 146.6 मिलियन टन कार्बन डाई आक्साइड के समतुल्य है।
- आग से प्रभावित या आग लाग्ने के मामले में संवेदनशील वनों की शिनाख्त भी इस रिपोर्ट में की गयी है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रों का 22.77 प्रतिशत जंगल ऐसे हैं जो आग की परिस्थितियों को लेकर अति संवेदनशील हैं।
- क्लाइमेट हॉट-स्पॉट्स आंकलन के निष्कर्ष भी इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं जो भविष्य में आसन्न परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2030, 2050 और 2085 के लिए किए गए दूरगामी आंकलन से यह तस्वीर सामने आती है कि इन वर्षों में लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य तापमान में वृद्धि होगी।
- इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश में बहुत कम या न के बराबर तापमान वृद्धि हो सकती है।
- पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में इसके संदर्भ में बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों और ऊपरी मालाबार समुद्री तटों में बेतहाशा बारिश बढ़ेगी जबकि पूर्वोत्तर के ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्व-पश्चिम के लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश की गति में मामूली या न के बराबर परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2021 पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं जो हिंदुस्तान में जैव विविध तता के लिए जाने जाते हैं और इसी रूप में वर्गीकृत भी किए जाते है।
- रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल 169521 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है जो इस क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें 0.60 प्रतिशत यानी 1,020 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गयी है।
- 140 पहाड़ी जिलों में कुल 283,104 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दर्ज किया गया है जो इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 17 प्रतिशत है। मौजूदा आंकलन के मुताबिक इसमें भी 902 वर्ग किलोमीटर (0.32 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गयी है।
- आदिवासी बाहुल्य जिलों को जिन्हें इस रिपोर्ट में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स या आदिवासी जिले कहा गया है और जिनकी संख्या 218 है, वहाँ कुल वन क्षेत्र 422296 वर्ग किलोमीटर है जो इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53 प्रतिशत है।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ भी 622 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में गिरावट आयी है। हालांकि ये गिरावट अभिलेखों में दर्ज वन क्षेत्र (रिकोर्डेड फॉरेस्ट एरिया) और हरित क्षेत्र (ग्रीन वाश) के दायरे में मौजूद वन क्षेत्र के लिए है। लेकिन अगर इन्हीं 218 जिलों में इन दो श्रेणियों से बाहर पैदा हुए वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 600 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है।
टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण
- वर्तमान ISFR 2021 में, है ने भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया है। इस संदर्भ में, टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण में बदलाव पर यह दशकीय मूल्यांकन वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों और प्रबंधन के प्रभाव का आकलन करने में मदद करेगा।
- इस दशकीय मूल्यांकन के लिए प्रत्येक टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ISFR 2011 (डेटा अवधि 2008 से 2009) और वर्तमान चक्र (ISFR 2021, डेटा अवधि 2019-2020) के बीच की अवधि के दौरान वन आवरण में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है।
- इसमें FSI की नई पहल के तहत एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसमें 'जमीन से ऊपर बायोमास' का अनुमान लगाया गया है।
- FSI ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC), इसरो, अहमदाबाद के सहयोग से सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) डेटा के एल-बैंड का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर जमीन से ऊपर बायोमास ( AGB) के आकलन के लिए एक विशेष अध्ययन शुरू किया। असम और ओडिशा राज्यों ( साथ ही AGB मानचित्र) के परिणाम पहले ISFR 2019 में प्रस्तुत किए गए थे।
- FSI ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स) पिलानी के गोवा कैंपस के सहयोग से 'भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की मैपिंग' पर आधारित एक अध्ययन किया है।
- यह सहयोगात्मक अध्ययन भविष्य की तीन समय अवधियों यानी वर्ष 2030, 2050 और 2085 के लिए तापमान और वर्षा डेटा पर कंप्यूटर मॉडल-आधारित अनुमान का उपयोग करते हुए भारत में वनावरण पर जलवायु हॉटस्पॉट का मानचित्रण करने के उद्देश्य से सहयोगात्मक अध्ययन किया गया था।
- रिपोर्ट में राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के अनुसार विभिन्न मापदंडों पर भी जानकारी शामिल है। रिपोर्ट में पहाड़ी, आदिवासी जिलों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वनावरण पर विशेष विषयगत जानकारी भी अलग से दी गई है।
धरातल
भू-भाग
भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भू-भाग पर, जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिन में वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है।
विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा । क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ शंकु धारी वन पाए जाते हैं।
जलवायु
तापमान
वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएँ तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मी० की ऊँचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों परिवर्तित करती है।
किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, उस स्थान के अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं।
वर्षण
भारत में लगभग सम्पूर्ण वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून (जून से सितंबर तक) एवं उत्तर-पूर्वी मानसून (लौटता हुआ मानसून) से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं।
वन नवीकरण योग्य संसाधन हैं और वातारण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय ।
भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की माँग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएँ और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है।
भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है।
कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग मरुस्थल, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है।
किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर्संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है।
| वनस्पति खंड | औसत वार्षिक तापमान | जनवरी में औसत तापमान | टिप्पणी |
| उष्ण | 24° से० से अधिक | 18° से० से अधिक | कोई पाला नहीं |
| उपोष्ण | 17° से० से 24° से० | 10° से० से 18° से० | पाला कभी-कभी |
| शीतोष्ण | 7° से० से 17° से० | - 1° से० से ( -10 )° से० | कभी पाला कभी बर्फ |
| अल्पाइन | 7° से० से कम | - 1° से० से कम | बर्फ |
धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को 'जीवोम' (Biome) कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है।
भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं।
डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध-मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है।
मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ पाई जाती हैं।
प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बाँटा जा सकता है:
वनों के प्रकार
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध-सदाबहार वन
ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।
ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22° सेल्सियस से अधिक रहता है ।
उष्ण कटिबंधीय वन सघन और पर्तों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नजदीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं, इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है।
चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग-अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे-भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ रोजवुड, महोगनी, ऐनी और एबनी हैं।
इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे, असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं।
अर्ध-सदाबहार वन, इन्हीं क्षेत्रों में, अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ साइडर, होलक और कैल हैं।
भारतवर्ष में, ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है।
जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है।
आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरीपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं।
सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आँवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं।
इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय: सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, साँप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं।
शुष्क पर्णपाती वन, देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं, जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर काँटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं।
अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये. वन पार्कनुमा भू-दृश्य बनाते हैं, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी-भरी घास होती है।
शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदुए पलास, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवूड (Axlewood) इत्यादि हैं।
राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशु चारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है।
उष्ण कटिबंधीय काँटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं।
इसमें दक्षिण-पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध-शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं।
इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है।
जंगलों में प्राय: चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई के साथ तापमान घटने के साथ-साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है ।
इन वनों को दो भागों में बाँटा जा सकता है - उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन ।
ऊँचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वतश्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों से टुण्ड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पायी जाती है।
हिमालय के गिरीपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1,000 से 2,000 मीटर की ऊँचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं।
उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं ।
इस क्षेत्र में 1,500 से 1, 750 मीटर की ऊँचाई पर व्यापारिक महत्त्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं।
हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है।
इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बल्यूपाइन और स्प्रूस 2, 225 से 3,048 मीटर की ऊँचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊँचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है।
इससे अधिक ऊँचाई पर एल्पाईन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3,000 से 4,000 मीटर की ऊँचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेन्ड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं।
ऋतु - प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्ढी और भुटिया, इन चरागाहों का पशु चारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊँचाई वाले भागों में टुण्ड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकेन आदि पाई जाती है।
इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं-कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियाँ पाई जाती हैं।
दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के तीन भागों में मिलते हैं : पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएँ। चूँकि, ये शृंखलाएँ उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 1, 500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊँचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है।
नीलगिरी, अनामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 'शोलास' के नाम से जाना जाता है। इन बनों में पाए जाने वाले वृक्षों मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और बैटल का आधिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं।
भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2,000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं।
'विश्व संरक्षण संघ' ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है।
भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं-
सर्पगंधा यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है।
जामुन : पके हुए फल से सिरका बनाया जाता जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह (Diabetes) रोग में सहायता करता है।
अर्जुन: ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमिता के लिए भी लाभदायक है।
बबूल इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है।
नीम : जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है।
तुलसी पावप: जुकाम और खाँसी की दवा में इसका प्रयोग होता है।
कचनार फोड़ा (अल्सर) व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है।
भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70 प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है।
ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन (रामसर अधिवेशन) के अंतर्गत रक्षित जलकुक्कुट आवास हैं।
हमारे देश की आर्द्र भूमि को आठ वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार हैं:
दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण-पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व पर्वतीय वन अन्य आर्द्र भूमि;
राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि;
गुजरात-राजस्थान से पूर्व (केवलादेव राष्ट्रीय पार्क) और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें व जलाशय;
भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून ( चिलका झील आदि);
गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र;
ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरीपद के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र;
कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ
(viii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र।
मैग्रोव लवण कच्छ, ज्वारीय सँकरी खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़-पौधे होते हैं।
बंधे जल व ज्वारीय प्रवाह की सँकरी खाड़ियों से आड़े-तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं।
यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार-भाटा आते हैं, की सबसे महत्त्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है।
असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी-रोटी और अस्तित्त्व है।
ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी की वस्तुएँ देते हैं।
जनजातीय समुदायों के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार हैं।
भारत के 593 जिलों में से 188 जनजातीय जिलें हैं। ये जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33. 63 प्रतिशत हिस्सा है, परन्तु देश का 59.61 प्रतिशत वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के धनी हैं।
वनों और जनजाति समुदायों में घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है।
वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यावहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है।
जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रह करने वाले न समझ कर उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाया जाना चाहिए।
घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है।
गंगा - ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताडु, क्योड़ा एवं ऐंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं।
इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के साँप भी इन जंगलों में मिलते हैं।
भारत में मैंग्रोव वन 6, 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7 प्रतिशत है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदर वन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है।
वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुँचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की जिसे 1988 में संशोधित किया गया।
इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत् पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।
इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :
देश में 33 प्रतिशत भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6 प्रतिशत अधिक है।
पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना;
देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण;
मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण;
निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार;
वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना;
पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हों, ताकि वनों पर दबाव कम हो ।
इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं:
सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनरोपण |
राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976-79) ने सामाजिक वानिकी को तीन वर्गों में बाँटा है शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी।
शहरों और उनके इर्द-गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि, जैसे- हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है।
ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है।
कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए।
समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि, जैसे- गाँव-चरागाह, मंदिर-भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है।
इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुँचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य, भूमिविहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुँचाना जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं।
फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्त्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग, इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है।
इस योजना के तहत कई तरह की भूमि, जैसे खेतों की मेड़ें, चरागाह, घासस्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। -
भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4-5 प्रतिशत किस्में भारत में पाई जाती हैं।
हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा है।
वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :
औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई;
खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया गया;
स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया;
पालतू पशुओं के लिए नए चरागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया;
जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियाँ नष्ट हुई।
राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और पारिस्थितिक पर्यटन (Eco-tourism) को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण है।
भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इनका युवाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव है।
वन्य प्राणी अधिनियम, 1972 में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना ।
इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित कर दिया गया जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 102 नेशनल पार्क और 515 वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं और ये 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं।
वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफी बड़ा है और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएँ निहित हैं। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब हर व्यक्ति इसका महत्त्व समझे और अपना योगदान दे।
यूनेस्को के 'मानव और जीवमंडल योजना' (Man and Biosphere Programme) के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणि जात के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
प्रोजेक्ट टाईगर (1973) इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की • जनसंख्या का स्तर बनाए रखना है, जिससे वैज्ञानिक, सौन्दर्यात्मक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सकें। जिससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा।
शुरू में यह योजना नौ बाघ निचयों (आरक्षित क्षेत्रों) में शुरू की गई थी और ये 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब यह योजना क्रोड बाघ निचयों में चल रही है और इनका क्षेत्रफल 36,988.28 वर्ग किलोमीटर है और 17 राज्यों में व्याप्त है। किन्तु वर्ष 2014 की गणना के अनुसार देश में कुल बाघों की संख्या, 2, 226 है।
यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परन्तु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएँ, जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हगुंल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही है।
भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं।
इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रन है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगो, हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है।
जीव मंडल निचय (आरक्षित क्षेत्र) विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम (MAB) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। भारत में 14 जीव मंडल निचय हैं।
इनमें से 4 जीव मंडल निचय - नीलगिरी; नंदादेवी; सुंदर वन और मन्नार की खाड़ी ।
यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं।
इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह भारत का पहला जीव मंडल निचय है। इस निचय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मदुमलाई, ऊपरी नीलगिरी पठार, सायलेंट वैली और सिदुवानी पहाड़ियां शामिल हैं। इस जीव मंडल निचय का कुल क्षेत्र 5520 वर्ग किलोमीटर है।
नीलगिरी जीव मंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति व सूखी झाड़ियां, जैसेशुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध-सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार शोलास, घास के मैदान और दलदल शामिल हैं।
यहां दो संकटापन्न प्राणी प्रजातियों, नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है।
नीलगिरी निचय में हाथी, बाघ, सांभर और चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संख्या तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित हैं, जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात हैं।
इस जीव मंडल की स्थलाकृति उबड़-खाबड़ है और समुद्र तल की ऊँचाई 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। पश्चिम घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी निचय में मिलते हैं।
नंदा देवी जीव मंडल निचय उत्तराखण्ड में स्थित है जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौड़ागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग शामिल हैं। यहां पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
यहां पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर वुड तथा लैटीफोली जैसे ओरचिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं।
इस जीव मंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव, जैसे- हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम- मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं।
यहां पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्य खतरा संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावानल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है।
यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित हैं। यह एक विशाल क्षेत्र (9630 वर्ग किलोमीटर) पर फैला हुआ है और यहां मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं।
मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक को आश्रय प्रदान करती है।
इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। स्वयं को लवणीय और ताजा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए, बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहां तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं।
सुंदर वन के मैंग्रोव वनों में हेरिशिएरा फोमीज, जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है, भी पाई जाती है।
मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निचय लगभग एक लाख पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है।
समुद्रीय जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे ध नी क्षेत्रों में से एक है।
इस जीवमंडल निचय में 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप और मैंग्रोव पाए जाते हैं।
यहां पर लगभग 3600 पौधों और जीवों की संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे- समुद्री गाय इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी संकटापन्न हैं।
Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
Facebook पर फॉलो करे – Click Here
Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
Google News ज्वाइन करे – Click Here







