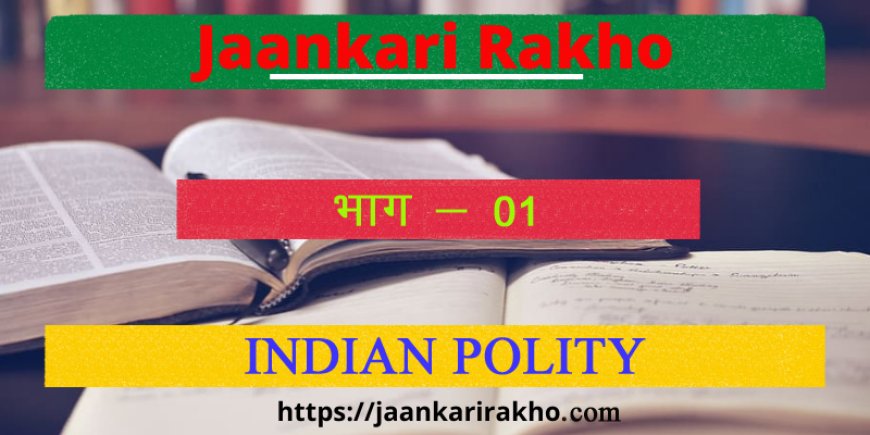General Competition | Indian Polity | संविधान का स्त्रोत
भारतीय संविधान के दो प्रकार के स्त्रोत हैं-
(1) आंतरिक स्त्रोत (2) बाह्य स्त्रोत
(1) आंतरिक स्त्रोत:-
1773 के रेगूलेटिंग एक्ट से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो अधिनियम पारित हुए हैं इनमें से जिस प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया वे भारतीय संविधान के आंतरिक स्त्रोत के अंतर्गत शामिल होते हैं। आंतरिक स्त्रोत के अंतर्गत भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है। जिस भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी भी जाता है। 1935 के अधिनियम से दो तिहाई प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किया गया है।
(2) बाह्य स्त्रोतः-
विश्व के अलग-अलग देशों से जो प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किये गयें हैं उसे ही बाह्य स्त्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। जो निम्न है-
(1) अमेरिका: - मौलिक अधिकार, संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्नाविलोकन, दबाब समूह, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा, जनहितवाद न्यायिक सर्कियता, इत्यादि........ ।
(2) आयरलैंडः- राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज़ सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली ।
नोटः- आयरलैंड के संविधान (1937) में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान स्पेन के संविधान से लिया गया है।
(3) दक्षिण अफ्रीका:- संविधान संसोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान
(4) ऑस्ट्रेलिया:- प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार - वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान
(5) रूस:- मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान
(6) फ्रांस:- गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी प्रावधान
(7) जापान:- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(8) कनाडा:- संघात्मक शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति
(9) जर्मनी:- आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी प्रावधान
नोटः- (क) जर्मनी के संविधान को वाइमर का संविधान कहा जाता है।
(ख) मूल तौर पर भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए है।
(10) ब्रिटेन:- विधि का शासन, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, प्रमाधिकार लेख, एकल नागरिकता
- मूल तौर पर भारतीय संविधान को 22 भागों में बाँटा गया है परंतू वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है तथा 395 अनुच्छेद है। जो निम्न है -
| भाग |
संबंध |
अनुच्छेद |
| भाग-1 |
संघ और राज्य क्षेत्र |
1-4 |
| भाग-2 |
नागरिकता |
5-11 |
| भाग-3 |
मौलिक अधिकार |
12-35 |
| भाग-4 |
राज्य के नीति निर्देशक तत्व |
36-51 |
| भाग-4 (क) |
मौलिक कर्तव्य |
51 (क) |
| भाग-5 |
संघ का शासन |
52-151 |
| भाग-6 |
राज्य का शासन |
152-237 |
| भाग-7 |
निरस्त |
238 |
| भाग-8 |
केंद्रशासित प्रदेश |
239-242 |
| भाग-9 |
पंचायत |
243 |
| भाग-9 (क) |
नगर पालिका |
243 |
| भाग-9 (ख) |
सहकारी |
243 |
| भाग-10 |
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में शासन |
244 |
| भाग-11 |
केंद्र और राज्य संबंध |
245-263 |
| भाग-12 |
वित्त, संपत्ति और संविदा |
264-300 (क) |
| भाग-13 |
व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता |
301-307 |
| भाग-14 |
लोक सेवा आयोग |
308-323 |
| भाग-14 (क) |
अधिकरण |
323 (क) |
| भाग-15 |
निर्वाचन आयोग |
324-329 |
| भाग-16 |
कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान |
330-342 |
| भाग-17 |
राजभाषा |
343-351 |
| भाग-18 |
आपात उपबंध |
352-360 |
| भाग-19 |
प्रकीर्ण |
361-367 |
| भाग-20 |
संविधान संसोधन |
368 |
| भाग-21 |
अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान |
369-392 |
| भाग-22 |
संविधान के लागू होने, संविधान का नाम और संविधान का हिन्दी पाठ्यक्रम |
393-395 |
नोट:- (1) भारतीय संविधान का भाग-2 को दो अध्याय में बाँटा गया है जिसमें अध्याय-1 हमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255) के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तथा अध्याय-2 हमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध ( अनुच्छेद 256-263) के विषय में जानकारी प्रदान करता है।
(2) 7वाँ संविधान संसोधन 1956 के तहत भारतीय संविधान का भाग-7 को निरस्त कर दिया गया।
(3) 42वाँ संविधान संसोधन 1976 के तहत् भाग - 4 - 4 (क) और 14 (क) जोड़ा गया, 74वाँ संविधान संसोधन 1992 के तहत् 9 (क) जोड़ा गया तथा 97वाँ संविधान संसोधन 2011 के तहत् 9 (ख) जोड़ा गया।
- मूल संविधान में 8 अनुसूची था नेकिन संविधान संसोधन के माध्यम से और अनुसूची नवमीं, दशर्मी, ग्यारहवीं तथा बारहवीं जोड़ी गई। तत्पश्चात् अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई।
नवम अनुसूची:-
प्रथम संविधान संसोधनं 1951 के तहत् इसे शामिल किया गया। इसमें भूमि सुधार की चर्चा है। इस अनुसूची के शामिल होने के समय हमारे देश का प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू थें। इस अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी 2007 को यह फैसला दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
दशर्मी अनुसूची:-
इसे 52वाँ. संविधान संसोधन 1985 के तहत् शामिल किया गया। इसमें दल-बदल अधिनियम की चर्चा है। इस अनुसूची के शामिल होने के समय हमारे देश का प्रधानमंत्री राजीव गाँधी थें।
ग्यारहवीं अनुसूची:-
इसे 73वाँ संविधान संसोधन 1992 के तहत् शामिल किया गया। इसमें पंचायती व्यवस्था की चर्चा है। पंचायती राजव्यवस्था को 29 विषय पर काम करने का अधिकार दिया गया।
बारहवीं अनुसूची:-
74वाँ संविधान संसोधन 1992 के तहत् इसे शामिल किया गया। इसमें नगर पालिका या नगर निगम को शामिल किया गया नगर निगम को 18 विषय पर काम करने का अधिकार दिया गया।
नोट:- ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची जब शामिल किया गया था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव थें ।
प्रथम अनुसूची:-
इस अनुसूची से हमें भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश ( नाम, क्षेत्रफल) के विषय में जानकारी प्राप्त होता है।
द्वितीय अनुसूची:-
इस अनुसूची से हमें भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी जैसे- राष्ट्रपति, राजसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इत्यादि के वेतन भत्ता और पेंसन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है।
नोट:- उच्च न्यायलय के न्यायधिशों को वेतन राज्य के संचित विधि से दिया जाता है, जबकि पेंसन भारत की संचित विधि से दिया जाता है।
तृतीय अनुसूची:-
इस अनुसूची से हमें भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारियों जैसे- संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधिश हाई कोर्ट के न्यायधिश, इत्यादि के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त होता है।
नोट:- तीसरी अनुसूची से हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होता है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद - 60, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद- 69 तथा राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद-159 में है।
- राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधिश दिलाते है ।
- उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं |
- प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
- राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधिश दिलाते हैं ।
- मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाते है ।
चौथी अनुसूची:-
इस अनुसूची में राज्यसभा सीटों के बटवारा के विषय में जानकारी प्राप्त होता है । जैसे- उत्तरप्रदेश को राज्यसभा में 31 सीट तथा बिहार को 16 सीट दिये गये हैं ।
पाँचवी अनुसूची:-
इस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्रों के शासन-प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में शासन प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है।
नोटः- जनजातीय सलाहाकार परिषद का गठन पाँचवी अनुसूची के तहत् किया जाता है।
छठी अनुसूची:-
इस अनुसूची से हमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के शासन-प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है ।
नोट:- स्वायतशासी जिला परिषद का गठन छठी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है।
सातवीं अनुसूची:-
इस अनुसूची से हमें तीन प्रकार के सूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्राप्त होता है ।
संघ सूची:-
इसमें मुलतः 97 विषय था जबकि वर्तमान समय में 100 विषय हैं। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून संसद बनाती है। भारत के भीतर कानून का निर्माण करनेवाली सबसे बड़ी संस्था संसद है।
जैसे - रक्षा, विदेश सेवा, जनगणना, संयुक्त राष्ट्र संघ, बड़े बंदरगाह, इत्यादि.......
राज्य सूची:-
इसमें मुलतः 66 विषय थें लेकिन 42वाँ संविधान संसोधन 1976 के तहत् राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तत्पश्चात राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 हो गई। इस सूची के विषय पर कानून राज्य विधान मंडल बनाती है।
जैसे - कृषि, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, इत्यादि.........
समवर्ती सूची:-
इस सूची में मुलतः 47 विषय था जबकि वर्तमान में 52 विषय है। इस सूची के विषयों पर कानून संसद या विधान में से कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर किसी विषय पा कानून संसद और विधानमंडल दोनों बनाती है तो इस स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा ।
जैसे - विवाह, तालाक, दंड प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, माप-तौल, न्याय प्रशासन, इत्यादि......
नोट:- शिक्षा, वन, वन्य जीवों का संरक्षण, माप-तौल, न्याय प्रशासन को 42वाँ संविधान संसोधन 1976 के तहत् राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया । 7वीं अनुसूची में हमें केंद्र और राज्य के बीच होने वाले शक्तियों के विभाजन के विषयों में जानकारी प्राप्त होता है ।
आठवीं अनुसूची:-
इस अनुसूची से हमें राज्य भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नर, तमिल, तेलगू, बंगाली, उड़िया, असमिया, राजस्थानी, मलयालम, उर्दू को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया । कलांतर में 8 और भाषा को संबंधित संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया, जिससे राज्य भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई ।
- 21वाँ संविधान संसोधन 1967 के तहत् सिन्धीं को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। सिंधी पंजाब तथा गुजरात में बोला जाता है।
- 71वाँ संविधान संसोधन 1992 के तहत् तीन भाषा को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है जो निम्न है-
(1) नेपाली - यह सिक्किम में बोला जाता है। न
(2) मणिपुरी - यह मणिपुर में बोला जाता है । म
(3) कोकनी - यह गोवा में बोला जाता है । क
- 92वाँ संविधान संसोधन 2003 के तहत् 4 भाषा को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है जो निम्न है-
(1) बोडो - यह असम में बोला जाता है।
(2) डोगरी - यह जम्मू-कश्मीर में बोला जाता है।
(3) मैथली - यह बिहार में बोला जाता है ।
(4) संथाली - यह झारखंड में बोला जाता है ।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..