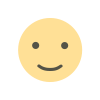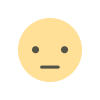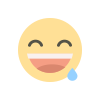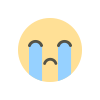संवैधानिक प्रक्रिया (विकास, संस्थाएं, विशेषताएं तथा संरचना की गाथा)
1. स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान ( विकास, संस्थाएं, विशेषताएं तथा संरचना )
भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार की कोशिश एक भविष्य का भारत बनाने की थी और इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक था कि ' भारतीय संविधान' के उन सभी प्रावधानों को रेखांकित किया जाए जिससे मानव का कल्याण हो सके। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ।
26 जनवरी 1950 को संविधान तो लागू हुआ लेकिन इसके बनने की शुरूआत कई दशक पहले ही हो चुकी थी। संविधान के लिए विभिन्न आधार के काम 'प्रतिनिधित्व' व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण बाते हैं। अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जाए तो हमें यह देखना होगा कि आंदोलन ने संसदीय जनतंत्र, गणतंत्रवाद, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय जैसे मुद्दे को पहले ही आधार बनाया था। 1920 के बाद कांग्रेस में भी चुनावी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था चलने लगी तथा अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक कांग्रेस में चुनाव के द्वारा चुने जाने लगे।
जब संविधान के बनने की शुरूआत हुई तो यह मानने में सर्वसम्मति थी कि इसका आधार जनतंत्र का आधार होना चाहिए। इसमें महिला उत्थान, तकनीकी उन्मूलन, शिक्षा का विकास इत्यादि को सर्वप्रमुखता देनी होगी। इन सबके बाद जो सबसे अधिक जरूरी था, वह था "जनता की भावना " ।
वैसे तो 1857 के बाद जब भारत में कंपनी की सरकार का स्थानांतरण 'ब्रिटिश सरकार की सरकार' से हो गया तो समय-समय पर कई 'भारत सरकार अधिनियम' आए जैसे 1861, 1882, 1919 तथा 1935 को भारत सरकार अधिनियम । लेकिन यह सुधार भारत की जनता की इच्छा के एक भाग को भी पूर्ण नहीं करता था।
अगर सर्वप्रमुखता दी जाए तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमारे गणतांत्रिक संविधान को एक सहायता मिली।
2. संविधान का विकास
अगर हम भारतीय नेतृत्व तथा आंदोलन कर्त्ताओं के द्वारा इस कोशिश को शुरूआत के तौर पर देखें तो कहीं न कहीं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की 'होम रूल लीग' से हमें शुरूआत करनी होगी। यह 1916 में आरम्भ हुआ तथा यह संयोग था कि 1916 में ही कांग्रेस-मुस्लिम लीग पैक्ट ने संवैधानिक सुधारों की कांग्रेस-मुस्लिम लीग स्कीम को जन्म दिया। इसमें मांग की गई कि प्रादेशिक विधायिकाओं के 5-4 सदस्य जनता द्वारा व्यापकतम संभव मताधिकार द्वारा चुने जाए। 1918 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में यह तय किया गया कि यह मांग आवश्यक है कि भारत की जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार मिले। 1919 में सुधार की स्थिति सिर्फ अंग्रेज ही बदल सकते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के हिस्से से ही स्वराज- पार्टी बनी तथा संवैधानिक संघर्षो को अपना मुख्य मुद्दा बनाया।
स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू ने भी वही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने केन्द्रीय सभा में 8 फरवरी 1924 को एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह कहा गया कि सरकार को एक प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन बुलाकर सभी के हितों एवम अधिकारों की रक्षा करना चाहिए तथा भारत के संविधान के लिए योजना पेश की जानी चाहिए। इस योजना का खाका भारत की नव निर्वाचित भारतीय संसद करे तथा ब्रिटिश संसद को इसका अनुमोदन करने दिया जाए। यह पहला अवसर था जब संविधान और उसके प्रावधान स्पष्ट रूप से पेश किए गए। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय मांग बन गया तथा यह केन्द्रीय असेंबली में 76 के मुकाबले 48 मतों के बड़े बहुमत से पास हुआ। अंग्रेजो की इस मांग पर जो प्रतिक्रिया थी वह टालने की थी तथा इसे एक 'नजर देने योग्य' जैसे विषय बनाने की थी। अंग्रेजों को फिर भी कुछ करना था तो उन्होंने 1927 में “साईमन कमीशन" की नियुक्ति कर दी जिसमें सिर्फ अंग्रेज ही सदस्य थे | इस कदम का भारत के सभी राजनीतिक इलाकों में जोरदार विरोध हुआ। इस विरोध से अंग्रेज इतना भड़क गए कि बर्केनहैड ने ब्रिटिश उच्च सदन में भारतीयों को चुनौति दे डाली कि “वे एक ऐसा संविधान बनाकर दिखा दे जो सभी भारतीयों को सर्वसम्मत कर सके।
कांग्रेस को बर्केनहेड की चुनौति स्वीकार थी तथा इस पहल पर कांग्रेस की तरफ से सर्वदलीय सम्मेलन समिति का गठन किया गया जो “भारत के संविधान" के सिद्धांत तय करे। 10 अगस्त 1928 को पेश नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव में भारत के संविधान का ढांचा सुझाया गया था। नेहरू रिपोर्ट में एक ऐसे संविधान की बात की गई जो संसदीय प्रणाली, जिम्मेदार सरकार, मतदान का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार सभी को प्रमुखता देता था। नेहरू रिपोर्ट ने भारत की जनता के लिए मूलभूत मानवाधिकार हासिल करने पर विशेष जोर दिया। इसके तथ्यों में धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा विचार की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, महिलाओं के समान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इत्यादि सभी शामिल थे।
नेहरू रिपोर्ट की सबसे अधिक मुख्य बात यह थी कि राज्य के धर्म निरपेक्ष चरित्र “मूलभूत अधिकारों" में शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट के 19 अधिकारों में दस संविधान में शामिल किए गए। नेहरू रिपोर्ट में प्रदेशों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की भी सलाह दी।
नेहरू रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई तो साइमन कमीशन के खिलाफ एक जनभावना बनी तथा बहुत सारे प्रदर्शन हुए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज' की मांग को प्रमुखता दी तथा अप्रैल 1930 में बापू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की हुंकार भरी। इस आंदोलन का प्रभाव ज्यादा व्यापक तौर पर हुआ तथा करीब लाख लोग जेल गए। यह बात धीरे-धीरे साबित हो गई की संविधान स्वयं तैयार करने से कम कोई भी बात स्वीकार नहीं की जाएगी। यह विचार सामने आया कि यह काम सम्मेलनों में नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि नेहरू रिपोर्ट के सिलसिले में किया गया था इस आधार पर यह मत बना कि संविधान के विकास के लिए “संविधान सभा " बननी चाहिए तथा सभी वर्गों को उसमें स्थान देना चाहिए।
जवाहर लाल नेहरू ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पहली बार औपचारिक रूप से 1933 में संविधान सभा का विचार पेश किया। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले 'एम. एन. रॉय' यह सुझाव देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जून 1934 में कांग्रेस कार्यसमिति ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेश 'श्वेत-पत्र' अस्वीकार कर दिया। साथ ही उसने यह तय किया कि श्वेत पत्र का एकमात्र संतोषजनक विकल्प वयस्क मताधिकार या इसकी निकटतम प्रणाली के आधार पर निर्मित संविधान सभा द्व द्वारा तैयार किया संविधान है। "
1933 के बाद कांग्रेस ने 'संविधान सभा' की मांग को जारी रखा। 1936-37 चुनावों के लिए तैयार कांग्रेस घोषणा-पत्र में संविधान सभा की मांग को प्रमुखता दी गई। कांग्रेस को इस चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिली। उसने मंत्रिमंडल भी बनाया। परंतु यह साफ कर दिया कि वर्तमान संवैधानिक ढांचा उसने स्वीकार नहीं किया है।
कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रदेशों को बहुमत से जीता था। मंत्रिमंडल बनाने के समय यह कहा गया कि सभी विधायक यह याद रखे उसे सदनों में संविधान सभा की मांग जल्द से जल्द रखनी है। विधायकों ऐसा 27-28 फरवरी 1937 के वर्धा कांग्रेस कार्य समिति में कहा गया।
नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में यह कहा कि "सभी कांग्रेस सदस्यों को पंचायती राज के लिए काम करना चाहिए जिसका निर्माण संविधान सभा करेगी जो हमारी जनता द्वारा चुनी गई उच्च पंचायत होगी। उन्होंने साफ कहा कि “इस संविधान को पूरी तरह त्याग करना होगा ताकि सभा का रास्ता पूरी तरह साफ हो । " धीरे-धीरे कांग्रेस और नेहरू की धैर्य की सीमा न रही। 1937 के अगस्त में सभी राज्यों में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पेश किया कि जल्द से जल्द संविधान सभा का निर्माण हो तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को खत्म किया जाए तथा इसकी जगह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत के लिए 'संविधान (एक) ' लागू किया जाए ।
1937 ई. में 17 सितम्बर को केन्द्रीय एसेम्बली में एक प्रस्ताव पास किया गया तथा यह कहा गया कि 1935 एक्ट के बदले संविधान सभा में निर्मित संविधान को लागू करना होगा। यह अनुरोध 'एस. सत्यमूर्ति' ने किया। इस अनुरोध में यह भी शामिल था कि अंग्रेजों को महात्मा गांधी से मित्रता बढ़ानी चाहिए तथा संविधान सभा की मांग स्वीकार कर भारतीयों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। 1938 के कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में भी यह मांग होती रही।
द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा उन्होंने ब्रिटेन द्वारा भारत को बिना उसकी जनता से पूछे युद्ध में सहभागी बना लेने के विरोध में किया। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेशों के मंत्रिमंडल ने असेम्बली में यह प्रस्ताव पास किया कि “भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए तथा इसका अपना संविधान हो । इसके बाद गांधी जी को भी संविधान सभा की मांग के समर्थन में लेख लिखने पड़े। गांधी ने कहा कि "हम नेहरू या किसी भी और नेता से 'संविधान सभा के लिए अधिक उत्साही हैं।" गांधी का विचार था कि असीमित मताधिकार पर आध कारित संस्था वे जिसमें स्त्री और पुरूष दोनों भाग लेंगे, विरोधी विचारों के प्रति न्याय कर पाएगी उन्होंने कहा कि "मुझे इसमें रास्ता दिखाई देता है जो जन राजनैतिक एवम अन्य शिक्षा के लिए जरिया बनने के अलावा सांप्रदायिक एवम अन्य विभाजनकारियों का उपाय भी है। "
15 से 19 अप्रैल 1940 के बीच गांधी-नेहरू के बीच वार्ताओं का दौर चला तथा वर्धा में यह दौर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बदल गया। इस बैठक में नेहरू ने भारत की आजादी की मांग को प्रमुखता से उठाया तथा गांधी जी ने कहा कि संविधान सभा के पहले एसेम्बली बुलानी चाहिए और उसे आजादी का सवाल तय करने के लिए मुक्त छोड़ देना चाहिए। जैसा कि हमेशा देखा गया था गांधी जी बहुत ही सावधानी से अंग्रेजों को संशय में डालते रहते थे, इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया।
1940 में उस समय के वायसराय 'लिनलियगो' ने 'अगस्त- प्रस्ताव' की बात कही। इस प्रस्ताव का एक मात्र उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पक्का करना था। इसमें पहली बार यह स्वीकार किया कि नए संविधान के निर्माण का कार्य पूरी तरह भारतीयों का होना चाहिए। हो सकता है कि यह स्वीकारोक्ति युद्ध के दबाव से ही निकली हो ।
अगस्त प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था बनायी जाएगी जो नये संविधान की रूपरेखा तैयार करेगी और इस संस्था में भारत के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। परंतु इसमें यह साफ तौर पर नहीं कहा गया कि इस संस्था का निमार्ण किस प्रकार हो । इसका अर्थ यह हुआ कि इसका रास्ता कैसा होगा जिससे प्रतिनिधि का चुनाव हो, या मनोनयन हो ।
संस्था के निर्माण की विधि पर चुप रहने के कारण भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने भारत से बिना मत लिए द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के कारण 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया। परंतु यहां एक बात और जानना आवश्यक है कि कांग्रेस ने युद्ध के कार्यों में कोई बाधा नहीं डाली क्योंकि इस युद्ध के उद्देश्य से कांग्रेस आंशिक सहमति रखती थी। सिर्फ कांग्रेस का विरोध इस बात पर था कि कांग्रेस को मत से यह फैसला लेना चाहिए था कि भारत भाग ले या न ले।
मार्च 1942 में दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटेन हार गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 'सर स्टैफोर्डक्रिप्स' को भारत भेजने की घोषणा की। युद्ध कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण लेबर पार्टी के सदस्य 'क्रिप्स' भारत के नेताओं के विशेषकर नेहरू के व्यक्तिगत मित्र थे । 'क्रिप्स प्रस्ताव मिशन' या 'क्रिप्स मिशन' ने संविधान सभा स्थापित करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है :-
युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद प्रादेशिक चुनाव होना आवश्यक होगा। इसके परिणाम के आधार पर निचले सदनों के सारे सदस्य एक चुनाव प्रकोष्ठ के सदस्य होंगे। वे समानुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एक संविधान बनाने वाली संस्था का निर्माण करेंगे। भारतीय रजवाड़ों के राज्य अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि तय करेंगे, वैसे ही जैसे ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि और उन्हीं अधिकारों के साथ।
क्रिप्स प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा था। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को इस स्तर पर स्वीकार किया कि यह प्रस्ताव भारतीयों को संविधान बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए सहमत था। संविधान सभा का विचार भी इस मिशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं थी। क्रिप्स प्रस्ताव के दूसरे जो भी प्रावधान थे वह कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे।
क्रिप्स मिशन की विफलता एक बहुत बड़ा प्रतिघाती रवैया साबित हुआ। अंग्रेजों और सारे राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के बीच टकराव बढ़ने लगे। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को 'भारत छोड़ो आंदोलन' का नारा दिया तथा साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि आजाद भारत की अस्थायी सरकार संविधान सभा की योजना तैयार करेगी। जन आंदोलनों ने अंग्रेजों के मन में कोई शक नहीं छोड़ा कि अंतिम बातचीत का समय पहुंच चुका है। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद मई 1945 में भारत संबंधी एक श्तेव - पत्र जारी किया गया। इसके बाद जून-जुलाई 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ जो असफल रहा।
1945 के जुलाई में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई। वायसराय लॉर्ड वैबर ने 19 सितंबर 1945 को भारत संबंधी नई नीति घोषित की। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन ने एक 'कैबिनेट मिशन' भारत भेजने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आजादी तथा संविधान निर्माण के प्रश्नों को हल करना था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और उसने भारतीय नेताओं के साथ विस्तार से बात की। बातचीत नहीं होने पर भी मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी योजना घोषित कर दी। उसने स्वीकार कर लिया कि संविधान बनाने की संस्था स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका वयस्क मताधिकार पर चुनाव होना चाहिए। परंतु इसके साथ इस मिशन ने यह भी कहा कि ऐसा कदम उठाना काफी जटिल होगा तथा संविधान बनने में देर होगी। इसलिए यह विदित हो गया कि प्रदेशों की नव निर्वाचित असेंबली दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करें। सिख तथा मुस्लिम विधायक अपने सम्प्रदायों की जनसंख्या के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुन लें। संघीय तथा प्रादेशिक अधिकारों संबंधी कई अन्य प्रावधन भी प्रस्तावित थे। इसमें विशेष महत्व के प्रावधान प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में थे।
प्रदेशों को तीन समूहों में बाँटा गया था:-
समूह 'ए':- मद्रास, बंबई, यू.पी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा । ('हिन्दू बहुल' प्रदेश )
समूह 'बी' : - पंजाब, उ.प्र., सीमांत प्रदेश, सिंध।
समूह 'सी' :- असम तथा बंगाल।
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव तथा अन्य औपचारिक कार्य करने के बाद अलग-अलग हिस्सों में बँटकर आगे का कार्य करें। प्रादेशिक प्रतिनिधि अपने-अपने कमीशनों में बैठकर पहले अपने प्रदेशों के या प्रदेशों के समूहों के संविधान तय करें। यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर प्रदेशों और रजवाड़ों (राज्यों) के प्रतिनिधि आपस में मिलकर संघीय संविधान तय करें। भारतीय संघ के पास विदेश प्रतिरक्षा एवम् संचार के विभाग होने चाहिए। कांग्रेस ने इस पर यह कहा कि संविधान सभा सार्वभौम होनी चाहिए। इसे विभिन्न मुद्दों पर कैबिनेट मिशन के सुझाव स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए। अंग्रेजों की ओर से इस संबंध में कोई वादा नहीं किया जा रहा था। फिर भी काफी विचार के बाद कांग्रेस ने योजना स्वीकार करना तय किया। उसे महसूस हो रहा था कि इसे मानने से सत्ता-हस्तांतरण में देरी हो सकती है। मुस्लिम लीग इसे स्वीकार न कर हर कदम पर बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। लीग हर मुद्दे पर संविधान सभा का विरोध कर रही थी, और इसके निर्माण के बाद भी विरोध करती रही।
3. संविधान सभा
अब यह तय हो गया था कि कैबिनेट मिशन की स्कीम को स्वीकार कर लिया गया तथा संविधान सभा के निमाण का रास्ता साफ हो गया था।
संविधान सभा के निर्माण के उद्देश्य सिर्फ संविधान बनाना नहीं था। यह तो सब जानते थे कि यह सभा संविधान बनाएगी। परंतु इस बात को अधिक महत्व का दिया कि संविधान क्यों बने? इसको केन्द्र में रखा जाए तथा इसके लिए कुछ केन्द्रित मुद्दे रखे गए जैसे:
1. संविधान भारत की आजादी के लिए
2. संविधान भूखमरी से लड़ने के लिए
3. संविधान गरीबों को अच्छी जिन्दगी देने के लिए।
4. संविधान भारत का विकास करने के लिए
5. संविधान भारतीयों को अपनी इच्छा से जिन्दगी जीने के लिए
संविधान सभा में प्रस्तावित रूप से 389 सदस्य थे। जिसमें 296 - ब्रिटिश तथा 93 भारतीयों रजवाड़े थे। इसमें यह बात कह देना साफ है कि आरम्भ में सिर्फ ब्रिटिश भारत के सदस्य संविधान सभा में थे। इसके लिए जुलाई से अगस्त 1946 के बीच चुनाव हुए। 210 सामान्य श्रेणी की सीटों में से कांग्रेस को 199 सीटें मिली। इसने पंजाब से 4 सिख सीटों में से 3 भी जीती। कांग्रेस को 78 मुस्लिम सीटों में से 3 सीटें मिली। इस प्रकार कांग्रेस को 208 सदस्य सीटें प्राप्त हुई वहीं मुस्लिम लीग को 78 मुस्लिम सीटों में से 73 सीटें मिली ।
संविधान सभा का चुनाव सर्वसम्मत से वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इसलिए कांग्रेस की इस मांग को सफल नहीं कह सकते कि इस प्रतिनिधित्व के आधार पर सभा को स्थापित किया जाए। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों और सिखों को ही विशेष प्रतिनिधित्व वाले 'अल्पसंख्यक' माना गया था। इन कारणों से सभा को सचमुच देश की विविधता का प्रतिनिधित्व बनाने के विशेष प्रयत्न किए गए। कांग्रेस कार्यसमिति ने जुलाई 1946 की शुरूआत में प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिया कि जनरल श्रेणी सूची में SC, पारसियों, एंग्लो इंडियनों, आदिवासियों और महिलाओं के प्रतिनिधि को शामिल करें।
असेंबली के चुनाव के लिए नाम तय करने में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संविधान तैयार करने के लिए अच्छे से सक्षम व्यक्तियों की खोज थी। गांधी जी ने स्वयं इसमें दिनचस्पी ली तथा उन्होंने अपनी तरफ से कांग्रेस की सूची में प्रमुख नामों का सुझाव दिया। इस प्रकार तीन ऐसे सदस्य कांग्रेस सूची में चुने गए जो इसके सदस्य नहीं थे। इससे असेंबली का वैचारिक स्वरूप स्वयं कांग्रेस सदस्यता के कारण अधिक व्यापक हो गया। संविधान सभा का चुनाव रोकने में मुस्लिम लीग पूरी तरह विफल हो गई तथा मुस्लिम लीग ने तब इस पर भाग लेने पर अपनी नीति को केन्द्रिन किया। कांग्रेस और जवाहर लाल नेहरू अपने स्तर से तथा अंतरिम सरकार की मुखिया की हैसियत से समझौते की कोशिश करते रहे तथा सरकार के अंतिम प्रयास तक भी कोई परिणाम नहीं निकला तथा 20 नवम्बर 1946 को संविधान सभा की बैठक जो प्रस्तावित थी उसे अब 9 दिसंबर 1946 को बुलाए जाने की घोषणा कर दी गई ।
9 दिसंबर को जब संविधान सभा को बुलाने की बात कर दी गई तो एक बात और सामने आई कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वैबेल इस सभा की बैठक रोक लेने के पक्ष में थे पर कांग्रेस अब इसमें देर करने के पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि किसी के कारण यानी मुस्लिम लीग के कारण हम रूके नहीं रह सकते। नेहरू को वायसराय की इच्छा का विरोध करना पड़ा। तब वायसराय ने सभा को बैठक के लिए मना किया। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सचिव की तरफ से सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेने को निमंत्रित किया गया तथा यह बात जोर देकर प्रदर्शित की गई कि यह संविधान सभा सार्वभौमिक रूप से भारतीय सभा हो तथा इसमें ब्रिटिश सरकार की किसी भी भूमिका का वर्णन इतिहास में लिखा न जाए।
भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को 11 बजे सुबह से आरंभ हो गया। वास्तव में भारतीय संसदीय इतिहास की आजादी की लौ यहीं से स्वतंत्रता पूर्वक जलनी शुरू हो गई। संविधान की रूपरेखा तय करने और इसके तहत जनता के अधिकार को सत्ता के साथ मिलाने के लिए एक नये स्तर से संविधान के निर्माण का काम आरंभ हो गया।
प्रथम अधिवेशन में 207 सदस्यों की भागीदारी थी। मुस्लिम लीग इसे न रोक सकी तो इसमें भाग ही नहीं लिया। मुस्लिम लीग के 76 सदस्य अलग रहे लेकिन कांग्रेस के 6 मुस्लिम सदस्यों ने इस अधिवेशन में भाग लिया।
11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। यह पद बाद में असेंबली का प्रेसिडेंट कहलाया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहर लाल नेहरू ने “उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव" पर अंतिम निर्णय को 'होल्ड' कर दिया ताकि इसमें मुस्लिम लीग तथा रजवाड़ो के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेकर अपना मत दे सके।
अगला अधिवेशन 20 से 22 जनवरी 1947 को हुआ जब यह देख- सुन लिया गया कि अब भी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लेने के इच्छुक हैं। अब 22 जनवरी 1947 को “ उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव " को पास कर दिया गया। तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को हुआ और इसमें भी लीग ने भाग नहीं लिया। 3 जून को अंततः “माउंट बैटन योजना " की घोषणा की गई। इसमें स्पष्ट किया गया कि भारत का विभाजन किया जाएगा। इसने संविधान सभा का परिप्रेक्ष्य ही पूरी तरह से बदल दिया। कैबिनेट मिशन योजना, जिसका सार था लीग के साथ समझौता अब प्रासंगिक नहीं रह गया।
जब हमारे देश ने 1947 को स्वतंत्र देश के रूप में जन्म लिया तो 'संविधान सभा ' एक सार्वभौम संस्था बन गई। यह संविधान सभा सर्वोच्च विधायिका के रूप में स्वीकार्य हो गई। इस पर संविधान बनाने तथा सामान्य कानून बनाने की भी जिम्मेदारी थी। विधायिका के रूप में इसका बड़ा आकार और विधायिका की इसकी जिम्मेदारी संविधान बनाने के काम में बाधा नहीं बने। इस कारण सदस्यों ने बड़ी जिम्मेदारी और सांगठनिक सूझ बूझ का परिचय देते हुए बड़ी तैयारियां की थी।
> संविधान सभा में विभिन्न कार्य को 5 चरणों में बाँटा गया था:
1. प्रथम कमिटी को मूल प्रश्नों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
2. संवैधानिक सलाहकार 'बी. ए. राऊ' ने विभिन्न काम काज-काजो का दस्तावेज तैयार किया।
3. डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया। इस कमिटि के बीच बहस और जनता की सहमति को जोड़ने की बात को सम्मिलित किया गया था।
4. मसविदे पर बहस हुई और संशोधन प्रस्तावित किए गए।
5. संविधान को स्वीकृत करने के लिए रखा जाना ।
संविधान सभा के लिए एक प्रस्ताव समिति का निर्माण किया गया। यह समिति जो 4 जुलाई 1946 को ही बनी थी (कांग्रेस के द्वारा) उसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी। इस समिति के सदस्य क्रमशः (1) आसफ अली (2) के. टी शाह (3) डी. आर. गागरिल (4 के. एम. मुंशी (5) हुमायुं कबीर (6) आर. संचानम् (7) एन. गोपाल स्वामी अय्यर थे। इस समिति ने नेहरू की अध्यक्षता में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव भी तैयार किया इसे कांग्रेस कार्यसमिति एवम् अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने 20 एवम 27 नवंबर 1946 को असेबंली के प्रथम अधिवेशन के पहले ही अनुमोदित कर दिया। संविधान की स्वीकृति तक यही तरीका अपनाया गया। जब भी किसी विशेष प्रस्ताव पर बहस होनी होती तो कांग्रेस के सदस्य पहले, पार्टी पर फिर सभा में बहस करते थे। कांग्रेस में किसी भी प्रस्ताव जो सभा में लाना होता वह पहले कांग्रेस के अन्दर के विचार के लिए पहले रखा जाता था।
यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद नहीं करना अन्याय होगा। पटेल ने रजवाड़ों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भाग लेने में निर्णायक भूमिका अदा की। पटेल ने इसके अलावा अलग मतदान अंग को समाप्त करने में एक महान भूमिका अदा की तथा जरूरी स्तर पर इसके लिए सफलतापूर्वक कोशिश की, कि धार्मिक स्तर पर अल्पसंख्यकों को सीटों का आरक्षण देने की कोशिश विफल हो जाए तथा पटेल इसमें सफल भी हुए ।
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सभा के अध्यक्ष के रूप में निस्पक्षता की मूर्ति कहा गया तथा मौलाना आजाद ने अपने स्वभाव से सुलझे हुए होने के कारण अपनी शान और दार्शनिक मस्तिष्क का प्रयोग किया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय भारत में एकमात्र पार्टी थी जो कांग्रेस थी, इसमें सरकार, पार्टी, देश सभी सरकारें तथा संस्थाएं कांग्रेस के द्वारा शासित थीं तथा संचालित थी फिर भी संविधान की प्रकृति में ऐसी कोई कठोरता तथा संकुचितता देखने को नहीं मिली जिससे हम यह कह सकें कि कांग्रेस ने सभा को अपनी सुविधा से पारित कर लिया।
सभा की पद्धति तथा प्रकृति उदार प्रजातांत्रिक तथा जनवादी थी । संविधान में यह सब रखने की कोशिश हुई कि विशेष की जगह पर बहुमत को तथा कुलीन तथा धनाढ्य की जगह गरीबी तथा सामान्य की आवश्यकता को अधिक महत्व दिया जाए।
4. संविधान के विभिन्न विशेष प्रावधान
यह तो पहले ही घोषणा कर ली गयी थी कि भारतीय संविधान को ऐसी जनतांत्रिक पद्धति के लिए बनाना है जिस पद्धति में मानव के विकास तथा सामान्यजनों के अधिकार दोनों की बात हो। इसलिए संविधान में विकास और मताधि कार के लिए किन-किन तंत्रों का निर्माण किया जाए उसकी रूपरेखा तैयार करनी थी बहुत सोच समझ कर संविधान में विभिन्न प्रावधानों को विशेष रूप से जोड़ा गया जो भारतीय संविधान की कहीं न कहीं विशेषता बन गई।
संविधान की विशेषता तथा विभिन्न प्रावधानों को लिए जाने के भी विभिन्न उद्देश्य थे जिसमें: संसदीय प्रणाली का निर्माण, पंचायती राज, सरकार कर विकेन्द्रीकरण, समाजवाद के प्रति भारतीय लोकतंत्र का झुकाव तथा सबसे बढ़कर भविष्य के प्रति भारत की चेतना विकसित करने जैसा उद्देश्य शामिल था।
इसलिए संविधान में निम्न प्रमुख प्रावधानों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया। इसके अलावा यह आवश्यक किया गया कि जनता के कल्याण पर कोई समझौता न किया जाए। विभिन्न प्रावधानों में निम्न प्रमुख बिन्दुओं को शामिल किया गया:
(1) मूल दर्शन (2) मूल अधिकार (3) नीति निदेशक सिद्धांत (4) वयस्क मताधिकार (5) धर्मनिरपेक्षता इत्यादि मूल दर्शन की स्थिति को हम संविधान की भूमिका के तौर पर निरूपित कर सकते है।
भूमिका को की प्रस्तावना भी कहा गया। यह एक दर्शन था जो संविधान के उद्देश्यों को एक साथ प्रदर्शित करता था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया तथा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया। इस प्रस्ताव में यह रखा गया कि 'प्रस्तावना' एक उद्देशिका के तौर पर संविधान के बनाए जाने के पीछे की भावना को हमेशा याद करवायगी । प्रस्ताव में महत्वपूर्ण बातें थीं उनमें:
1. न्याय
2. मूल अधिकार
मूल अधिकार भारतीय संविधान को एक रास्ता दिखाने के लिए सम्मिलित किया गया था। यह अधिकार महानता की परंपरा के साथ उन कमियों को भी दूर करने की एक कोशिश थी जो समाज, राजनीति, अर्थ तथा संस्कृति की विविधता के कारण उत्पन्न हुए थे।
मूल अधिकार जनता की सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों की गारंटी के तौर पर सामने आया। मूल अधिकारों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक समानता, अवसरों की समता तथा विचारों की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया था।
3. नीति निदेशक सिद्धांत
नीति निदेशक सिद्धांत की जहां तक बात है यह पूरी तरह भारतीय नागरिक के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार से जुड़े मुद्दे थे। इसमें सरकार को यह सलाह देने की बात की गयी थी कि वह विभिन्न ऐसे रास्ते खोजे जिससे जनता के विकास में सामाजिक, आर्थिक पक्ष को अधिक महत्व मिल सके। इसमें अधिकार की बात तो की गई थी पर यह साफ कर दिया गया था कि जनता के इन अधिकारों को पूर्ण करने का कार्य सरकारों का है और सरकार इसे अपने कर्त्तव्य तथा समर्थन के अनुसार पूर्ण करेगी। इसमें सामर्थ्य है, इसलिए जनता इसे पूर्ण करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकती क्योंकि नीति-निदेशक सिद्धांतों में वे चीजें भी शामिल थी जो संसाधन के उपलब्ध होने पर ही संभव होते।
निदेशक सिद्धांतो में धारा 38 में यह कहा गया है कि “राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रभावशाली ढंग से निर्मित करेगा और उसकी रक्षा करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवम राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का काम करेगा और इस प्रकार जनता का कल्याण कर पाएगा । " इस तरह देखा जाए तो यह राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह सभी नागरिकों को जीवन यापन के लिए उचित पार्टी मुहैया हो, संसाधनों का समान वितरण हो तथा संपत्ति का संकेन्द्रण न हो। समान काम तथा समान वेतन की अवधारणा तथा मजदूर, बच्चे, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की भी रक्षा को भी प्रमुखता प्रदान की गई।
इसके अलावा भारत के नागरिकों को शिक्षा, कार्य, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था की स्थिति में सरकार से सहायता लेने का अधिकार होगा।
नीति निदेशक सिद्धांतों में यह सम्मिलित किया गया था कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले तथा समान आचार संहिता के उद्देश्य हासिल करने के लिए प्रयास किये जाएं। इसके अलावा जीवन स्तर सुधारने के लिए विभिन्न अधिकारों को भी महत्व प्रदान किया गया था।
नीति निदेशक तत्व के बारे में जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा कि “राज्य नीति निदेशक तत्व" एक गतिशील तत्व है। मूलभूत सिद्धांत स्थायी पक्ष है जिन्हें बनाए रखना है। समय के साथ मुद्दे बदल जाए लेकिन उद्देश्य एक ही रहेंगे। मूलभूत सुधार में मौलिक अधिकार की विशेषताओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है। मौलिक अधिकार को उस समय 7 भागों में रखा गया।
1. समानता का अधिकार
2. आजादी का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धर्म संबंधी अधिकार
5. सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार
6. संपत्ति संबंधी अधिकार
7. संवैधानिक उपचार संबंधी अधिकार
मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12-35 के बीच रखा गया था।
यह सही है कि 1971 तक आते-आते मूल अधिकारों की प्रधानता न्यायपालिका के हाथ अधिक दे दी गयी थी इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में 25वें संशोधन तथा 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्वों की प्रधानता लाने में महत्वपूर्ण कोशिश की।
इसी बीच 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मुकदमें में एक फैसला किया। इनके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मूलभूत अधिकार तथा निर्देशक तत्व दोनों समान महत्व के हैं और एक की बिनाह पर दूसरे को छोड़ा नहीं जा सकता।
4. राष्ट्रीय एकता तथा मानविकी बराबरी का संकल्प लेने की पद्धति ।
प्रस्तावना में 'सामाजिक' और 'आर्थिक न्याय' की बात को बहुत ही सोच समझकर प्रस्तुत किया गया था क्योंकि हमारा समाज प्रिज्मेटिक है तथा गरीबी को हराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही थी ।
5. वयस्क मताधिकार
इसकी मांग तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही कांग्रेस की प्रमुख मांगों में शामिल थी। इसे अब लागू करने की स्थिति सही थी। कुछ लोगों का यह मत था कि वयस्क मताधिकार को ग्राम पंचायतों के स्तर तक ही सीमित रखा जाए तथा उच्च स्तर पर अप्रत्यक्ष तरीके से हो । परंतु बहुत बड़े बहुमत का यह मानना था कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे हों, यह ब्राह्ममणवादी उच्च जाति के प्रमुख लागों, गरीबों, निरक्षर समाज के लिए काफी महत्व रखता था।
इसके बारे में के. एम. पारिकर ने यह कहा था कि, वयस्क मताधिकार का सामाजिक प्रभाव इसके राजनीतिक महत्व से कहीं आगे जाता है। कई सामाजिक समूह पहले अपनी शक्ति के प्रति सचेत नहीं थे और राजनीति परिवर्तनों से अछूते थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं।
वयस्क मताधिकार भारतीय जनतंत्र को एक महान नींव देने के लिए एक सबसे बड़ा कदम था। यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि सरकार के निर्माण में प्रत्येक नागरिक के योगदान की बात वयस्क मताधिकार में समाहित है।
6. धर्मनिरपेक्ष राज्य
वैसे तो धर्मनिरपेक्षता को 'पंथनिरपेक्षता' के तौर पर तब्दील कर इसे और प्रभावी बना दिया गया। फिर भी संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश तथा राज्य के रूप में निरूपित करता है। हालांकि 1976 में एक यह शब्द 42वें संशोधन में समाजवादी शब्द के साथ जोड़े गए थे। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का मूल लक्षण बताया। यह पंथ. निरपेक्षता किसी भी एक धर्म को विशेष अधिकार देने से वंचित करती है। यह शब्द धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास तथा धार्मिक स्तर पर कोई कार्य आयोजित करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत की विविधताओं की नींव इसी पर टिकी है।
5. संविधान की संरचना
संविधान की संरचना को समझने के लिए इसकी विशेषताएं जो मूल थी तथा संस्थाएं जो इसे संरक्षण प्रदान करता था उसकी व्याख्या करना काफी उचित होगा। इसलिए संविधान की संरचना की व्याख्या करने से पहले इनकी विशेषताएं तथा संस्थाओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
संविधान की मुख्य विशेषताएं कहीं न कहीं भारतीय जनता के प्रति संवेदनशीलता तथा लोकतांत्रिक अधिकारों में प्रदर्शित है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी मूल रचना जो बदली नहीं जा सकती। यह बात 1973 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण बेंच ने केशवानंद भारती केस में स्पष्ट की गई। यह जरूरी तौर पर कहा गया कि संविधान की संरचना में मूल विशेषताओं को रेखांकित किया गया जिसमें निम्न मील के पत्थर सम्मिलित हैं:
1. सरकार का गणतंत्रीय एवम जनतांत्रिक रूप
2. संविधान का वर्चस्व
3. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
4. विधायिका, कार्यकारिणी, न्यायपालिका
5. संघीय ढांचा
6. मुक्त और न्यायपूर्ण चुनाव
7. भूमिका में वर्जित उद्देश्य
8. न्यायिक समीक्षा
9. व्यक्ति की आजादी और सम्मान
10. राष्ट्र की अखण्डता एवम एकता
11. समानता का सिद्धांत
12. सामाजिक एवम आर्थिक न्याय का विचार
13. मूलभूत अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य
14. न्यायपालिका की आजादी
15. न्याय आसानी से कर सकने का अधिकार
इंदिरा गांधी के शासन में अपातकाल के दौरान 42वें संशोधन (1976) में घोषणा की गई कि संसद द्वारा संशोधन करने के अधिकार में कोई 'लेकिन, परंतु' सीमा नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा गया कि संशोधन को किसी भी आध. र पर न्यायालय में जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल चरित्र बरकरार रखने पर पुनः जोर दिया। इसके विचार में न्यायिक समीक्षा एक ऐसा मूल पक्ष है जो “संविधान के संशोधन के जरिए भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि यदि कोर्ट को यह विश्वास हो जाए कि संविधान संशोधन के मूल चरित्र को प्रभावित करेगा तो यह खारिज कर दिया जाएगा।" इस प्रकार ‘मूल लक्षणों' के सिद्धांत के आधार पर न्यायिक सुधार की दृष्टि में हमारे संविधान में ठोस सीमाएं लागू करी गई हैं।
जजों के बीच मूल पहलुओं के बारे में कुछ मतभेद रहे है। लेकिन मूल रचना इन लक्षणों के सिद्धांत पर सहमति है। संसदीय बहुमत का प्रयोग करके संविधान नष्ट करने की कोशिश को रोका जा सकता है।
भारतीय संविधान का ढांचा मतलब 'संघीय ढांचा' और 'केन्द्रीय ढांचा'
संविधान के ढांचे को सबसे अधिक साकार केन्द्रीय या संघीय ढांचे में ही देखा जा सकता हैं। सही तौर पर देखें तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में संघीय ढांचे की मुख्यता को लेकर आरंभ में संदेह रहा । विपिन चन्द्रा की पुस्तक में इस मामले में ऑस्टिन की बातों को इस तरह निरूपित किया गया है :
“भारतीय संविधान इतना असाधारण है कि इसका संक्षेप में वर्णन करना कठिन है। अर्द्ध संघीय और 'स्थायी विकेन्द श्रीकरण' जैसे शब्द दिलचस्प है, लेकिन उनसे कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है । " असेंबली के सदस्यों ने खुद ही किसी संघीय विचार सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। उनका विचार था कि भारत की समस्याएं विशिष्ट थी, ऐसी समस्याएं जिनका सामना इतिहास में दूसरे संघों को नहीं करना पड़ा था। इनका हल सिद्धांत का सहारा लेकर नहीं किया जा सकता था क्योंकि संघवाद कोई विशेष विचार नहीं था और इसका अर्थ स्पष्ट भी नहीं था। इसलिए असेंबली के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण संघों के अनुभवों का अध्ययन किया। उन्होनें “उनमें क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, क्या राष्ट्र के चरित्र के हित के सबसे अनुकूल है, यह चुनने का रास्ता अख्तियार किया।'' इस प्रक्रिया से एक नए प्रकार का संघवाद उभरा जो भारत की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल था।
ऑस्टिन के शब्दों से अब यह सार मिल गया कि संविधान सभा में सदस्यों को 'भारतीय संघवाद' के लिए 'खाद-प. ानी' मिल गया जो न किसी दूसरे देश की नकल था न किसी देश की चुरायी चीज थी । बल्कि दूसरे देश के संघीय तंत्र और अपने देश की विवधता में कैसा संघ हो इस पर तुलना करके हमारी अपनी 'संघीय व्यवस्था' को सामने लाया गया था। इस संविधान सभा ने जो संघवाद अपनाने की काशिश की वह 'सहयोगी संघवाद' कहलाया । इस सहयोगी संघवाद का आकार तथा अर्थ “संघीय सरकार तथा राज्य की सरकार में आपसी निर्भरता के साथ संघीय तत्व को आदर देने की प्रवृत्ति था । ''
संविधान सभा एक ऐसी सहयोगी संघवाद की अवधारणा के लिए कार्य कर रही थी जिसमें केंद्र मजबूत हो तथा इस मजबूत केन्द्र के कारण राष्ट्रीय समस्या जैसे :- गरीबी, शरणार्थी, विभाजन से उपजी समस्या, आर्थिक पिछड़ेपन का एक भारत के लक्ष्य से समाधान किया जाए। लेकिन यह कहना उचित होगा कि विभाजन से पहले संविधान सभा ने अपने अस्तित्व के शुरूआती महीने में मजबूत केन्द्रीय सरकार का पक्ष नहीं लिया था। सभा की 'संघीय सत्ता समिति' ने नेहरू के नेतृत्व में अपनी पहली रिपोर्ट में बहुत ही कमजोर केन्द्रीय सरकार की सिफारिश की थी। परंतु जब 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा हुई तो संविधान सभा ने खुद को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना से मुक्त समझा और अपने स्तर से एक मजबूत केन्द्र सरकार का पक्ष लेना आरंभ कर दिया।
अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने यह कहा कि “राज्यों का संघ" के बदले “राज्यों का केन्द्र " शब्द प्रयोग किए जाएं।
अम्बेडकर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रारूप समिति का यह मत है कि भारत को एक संघ के रूप में देखा जाना चाहिए था। यह संघ राज्यों द्वारा इसमें शामिल होने की सहमति पर आधारित नहीं था, और चूँकि संघ किसी समझौते का नतीजा नहीं था, इसलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं था। यह संघ एक केन्द्र है क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि देश और जनता प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किए जा सकते हैं फिर भी देश एक ही है, इसकी जनता एक है जो एक ही स्त्रोत से निकाली सत्ता के तहत रहती है । "
उपरोक्त रिपोर्ट का अर्थ यह है कि संघ किसी समझौते का एहसास नहीं बल्कि एक केन्द्र है जिसमें प्रशासनिक सहूलियत के कारण राज्यों की सीमा में परिवर्तन तो हो सकता है पर शक्ति का स्त्रोत केन्द्र ही रहेगा।
भारतीय संघवाद की विशेषताएं हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि भारत का नागरिक सिर्फ भारतीय नागरिक होगा न कि दोहरी नागरिकता उसके राज्य की अलग से होगी।
दूसरी विशेष शक्ति का वैधानिक विभाजन है जो स्पष्टतः टकराव कम करने के कारण बनाए गए है। इनमें तीन सूचियों को रेखांकित किया गया है :- (1) संघीय सूची (2) राज्य सूची (3) समवर्ती सूची
इन सूचियों में उन सभी विषयों को शामिल किया गया जो प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक थे। इसके अलावा जहां तक अधिकारियों की बात है केन्द्र के पास अधिकार अधिक हैं जिसमें वित्तीय अधिकार को प्रमुखता दी जा सकती है। राज्यों को केन्द्र से अधिक मदद लेने के लिए हमेशा इंतजार करना इसमें एक नकारात्मक बिन्दू हो सकता है लेकिन इसके भी अपने ही मायने हैं।
संघीय व्यवस्था की भारत में सबसे प्रगतिशील तस्वीर इस बात से सामने आयी कि अलग-अलग राज्यों में अलग. -अलग पार्टी की तस्वीरों को देखा जा सकता है और फिर भी यह केन्द्र सरकार के साथ काम कर रही है। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ।
संविधान के कार्य संचालन का भार राष्ट्रपति के हाथ में दिया गया। लेकिन प्रारूप समिति ने इसकी ब्रिटेन के राजा से तुलना की। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख तो है लेकिन कार्यकारिणी के नहीं है। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि वे राष्ट्र के प्रतिनिधि तो है लेकिन शासक नहीं है। यह कार्य मतलब शासन का कार्य तथा कार्यकारिणी के नेतृत्व करने की जिम्मेवारी तो प्रधानमंत्री को दी गयी थी। लेकिन राजा से तुलना करना यहां बेईमानी होगी क्योंकि ब्रिटेन में राजा को चुना नही जाता पर यहां राष्ट्रपति को चुना जाता है। फिर भी राष्ट्रपति सांकेतिक रूप से ही सही भारत का प्रधान मुखिया होता है।
परंतु राष्ट्रपति का संविधान में भारत के परिप्रेक्ष्य में एक अहम अधिकार है। लेकिन यह भी यहां जोड़ देना आवश्यक है कि राष्ट्रपति के कार्य मंत्रिमंडल की सलाह से ही किये जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति का भी वर्णन संविधान में किया गया है जब राष्ट्रपति को सक्रिय होना पड़ता है। उनके औपचारिक और वास्तविक अधिकारों के बीच आरंभ से ही राष्ट्रपति के विवेक को न्याय के तराजू पर तौला जाता है। जब राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो यह शंका जताई गयी थी कि राजेन्द्र बाबु इतने सक्रिय नेता रहे है। इसके कारण सरकार के कार्यकारी प्रमुख से इनको घर्षण हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि राजेन्द्र प्रसाद जी को यह मौका मिला भी था जब 'हिन्दु कोड बिल' पर उन्हें काफी आपत्तियां थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कह भी दिया कि 'राष्ट्रपति की भूमिका' काफी अहम होती है फिर नेहरू ने संविधान विशेषज्ञों से इस पर चर्चा की तथा राजेन्द्र बाबू को संविधान सभा के उनके ही भाषण की प्रति दिखायी गयी जिसमें उन्होंने कहा थी कि “भारत में भी वही परंपरा पाली जाएगी जिसके तहत इंग्लैंड में राजा हमेशा ही अपने मंत्रियों की सलाह पर ही काम करता है तथा भारत के राष्ट्रपति को हरेक विषय में संवैधानिक राष्ट्रपति ही होना चाहिए।”
उपरोक्त कथन को राजेन्द्र बाबू के मन को बदलने वाला कहा जा सकता है तथा यह कहा जा सकता है कि संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति को सारगर्भित तरीके से पेश किया गया है।
संविधान के अलावा अगर व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति की महत्ता को बहुमत वाली सरकार जो एक पार्टी से बनी हो के काल में अधिक सारगर्भित कहा जा सकता है। परंतु जब गठबंधन या कमजोर सरकार जो मिली-जुली रहती है उस काल में राष्ट्रपति के द्वारा हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। नीलम संजीव रेड्डी से लेकर शंकर दयाल शर्मा जी को ऐसी परिस्थिति में विवेक सम्मत निर्णय लेने को राजी किया गया था।
उपरोक्त तथ्यों को अगर उदाहरणस्वरूप में देखना चाहेंगे तो हमें यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि ज्ञानी. जैल सिंह जी को एक बड़े उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। इन्होंने 'भारतीय डाक अधिनियम' विधेयक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की थी। बात तो यहां तक पहुंच गयी थी कि राजीव गांधी सरकार को वो बर्खास्त भी कर सकते है। किंतु हमें यह एहसास होना चाहिए कि राष्ट्रपति की शक्ति संविधान में इतने बड़े स्तर पर निहित है।
राष्ट्रपति की चर्चा एक मामले में और अधिक होती है जब धारा 356 लागू करने की बात होती है क्योंकि इस प्रकरण में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर मंत्रिमंडल के इस फैसले को लौटा भी सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, गोवा इसके बड़े उदाहरण रहे हैं 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद् से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध करे। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद अपने निर्णय पर कायम रहे तो राष्ट्रपति को वह स्वीकार करना होगा। यह एक बड़ा इशारा होता है जब राष्ट्रपति केन्द्र को किसी मंत्रिमंडल के फैसले को पुनः विचार के लिए भेजता है।
अनुच्छेद 111 में जब कोई बिल राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, तो उन्हें इससे असहमति जताने का अधिकार है, और यदि वे चाहें तो संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 1978 में किए गए 44वें संशोधन के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही अपातकाल की घोषणा कर सकता है। निस्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति कोई भी निर्णय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कर सकता है।
लोकसभा - यह निचला सदन होता है। मंत्रिमंडल इसी सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। इस सदन का चुनाव जनता के द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। इसे इसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही समाप्त किया जा सकता है। अठारह वर्ष की आयु के बाद इसमें मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद लोकसभा का चुनाव भारतीय नागरिक लड़ सकता है।
राज्यसभा - यह ऊपरी सदन होता है। यह सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 का चुनाव तथा 12 सदस्यों का मनोयन राष्ट्रपति करता है।
उपराष्ट्रपति - एक तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति ही होते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होते हैं। धारा:- 65 में यह प्रावधान किया किया गया था उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं।
मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री - संविधान में यह वर्णन है कि वास्तविक कार्यकारिणी का अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में होता है तथा यह कार्य प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद् के द्वारा पूरा करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। नेहरू ने प्रधानमंत्री को “ सरकार का केन्द्र बिन्दु" कहा है वहीं हमारे संविधान में एक तरह से प्रधानमंत्री को सरकार का इंजन कहा गया है। सही तौर पर भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है जो राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु के रूप में होती है क्योंकि संसद का एक अंग राष्ट्रपति के होने के बावजूद संसद में विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास ही जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की नीतियों को सर्वोच्च स्तर पर संसद में पेश होने से पहले मंत्रिमंडन से ही पास किया जाता है। "
राज्य सरकारें
> पूर्ण राज्य
> केंद्र शासित राज्य
पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री राज्य कार्यकारिणी के कार्य सभी कार्य संचालित करते हैं। राज्य का राज्यपाल केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि होता है वहीं मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही नियुक्त करता है। धारा 356 को आरोपित करने में राज्यपाल की भूमिका अहम होती है और कहीं-न-कहीं राष्ट्रपति, राज्यपाल के रूप में अपने प्रतिनिधि को राज्य में भेजता है।
राज्यपालों की भूमिका अधिकतर विवादों में रही है परंतु यह मान कर चलने में सही लगता है कि यह केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि होने के कारण केंद्र सरकार में जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी नुमाइंदगी करता है। राज्यपाल टिप्पणी तथा कदम न्यायालय से सुनवाई का आधार भी बन जाता है। राज्यपाल से जुड़े विवाद अधिकतर उसी समय सामने आते हैं जब केन्द्र और राज्य में अलग-अलग पार्टी की सरकार होती है।
राज्य सरकारें विधानसभा में बहुमत के आधार पर बनती हैं। विधानसभा की अधिकतर सीटें 500 तक तथा न्यूनतम 60 तक होती हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होता है।
केन्द्र शासित प्रदेशों में शासन केन्द्र के द्वारा संचालित होता है जिसमें उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति होती है। ये प्रदेश पूरी तरह केन्द्र की सरकार के द्वारा ही संचालित होते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी को संविधान के संशोधन के तहत अलग से अधिकार दिए गए। हैं।
6. स्थानीय प्रशासन
संविधान में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया गया था। परंतु नीति-निर्देशक तत्व में अनुच्छेद '40' के तहत 'पंचायती राज' की चर्चा की गई थी। लेकिन यह कहना आवश्यक है कि नीति-निर्देशक तत्व के बारे में सरकार को सिर्फ सलाह के तौर पर ही कहा जा सकता था। इसके अलावा पंचायती राज की अवधारणा की बात अगर नींव के तौर पर चर्चा की जा सकती है तो गांधी जी के 1920-22 यानी असहयोग आंदोलन के हल से अपने कार्यक्रम में पंचायती राज को शामिल करना महत्वपूर्ण है।
उपरोक्त तथ्यों की प्रगति ही स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज को एक महान विकास की ओर प्रेरित किया। सरकार ने आरंभ में ‘सामूदायिक विकास कार्यक्रम' के तौर पर इसकी नींव रखी।
1956 में सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन इस प्रणाली में सुधारों का सुझाव देने के लिए किया। बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तरों वाली प्रतिनिधि इकाईयों वाले पंचायती राज की स्थापना की सलाह दी थी। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, प्रखण्ड स्तर पर तथा जिला परिषद् जिला स्तर पर कार्य करें, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति का मत था।
1959-1960 के बीच सारे राज्य सरकारों ने पंचायती राज कानून लागू कर दिए। लेकिन यह कहना आवश्यक है कि उस काल में पंचायती राज के कार्य संतोषजनक नहीं रहे। सरकार ने बाद में चलकर पंचायती राज से संबंधित वि. भन्न समितियों जैसे- अशोक मेहता समिति 1978, जी.वी. के समिति 1985 तथा एल. एम. समिति 1986 ने इस मामले में काफी कुछ कहा।
1988 में पी.के. थुंगन समिति के नेतृतव में गठित समिति ने यह सुझाव दिया कि पंचायती राज से संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए। 1989 में संविधान में 64वाँ संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया गया पर यह राज्यसभा में गिर गया। 1993 में 73वें एवम 74वें संशोधन बिलों को 1993 में में पास करवाने में सरकार सफल हो गयी।
73वें संशोधन में ग्राम पंचायत तथा 74वें संशोधन में नगर निकाय के प्रावधान को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। पंचायत स्तर पर 29 विषयों को रखा गया था।
7. न्यायपालिका
संविधान सभा एक ऐसे लोकतंत्र की बुनियाद रख रही थी जिनमें आम नागरिक को सस्ता एवम सुलभ न्याय मुहैया हो। आज यह कितना फलीभूत हुआ, इस पर बहस हो सकती है लेकिन संविधान सभा ने भारत देश के लिए एक वृहत न्यायपालिका की नींव रखी तथा सही रूप में इसे 'संविधान का रक्षक' बताया । संविधान में न्यायपालिका में जुड़े प्रावधानों को धारा 124-127 तथा 214-231 के बीच रखा गया है।
संविधान में न्याय-पालिका सही तौर पर एक सर्वोच्च कानूनी संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रास्ता बनाने का जिक्र है जो संसद की नीति बनाने की सर्वोच्च शक्ति तथा उसके द्वारा बनायी गयी नीतियों की संवैधानिकता को परखती है। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थापना हुई तथा इसके पहले इसे फेडरल कोर्ट के तौर पर जाना जाता था। परंतु इस फेडरल कोर्ट को सर्वोच्च कहना गलत होगा क्योंकि इसका फैसला ब्रिटेन में प्रिनी काउंसिल की न्यायिक समिति के समक्ष किया जा सकता था। प्रिवी काउंसिल का अधिकार अक्टूबर 1949 में खत्म कर तथा फेडरल कोर्ट की जगह 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने ले ली। 1950 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 7 थी और 1986 में 25 थी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को (25:1) के अनुपात में रखा गया था। मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 25 न्यायाधीश। 64 वर्ष के अवकाश की अवधि अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए तथा 62 वर्ष के अवकाश की अवधि अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए रखी गई है। राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यन्यायाधीश तथा अन्य जजों की सलाह से न्यायधीश की नियुक्ति होती है। धारा 124 में यह कहा गया है कि न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाएगी। न्यायपालिका के इस सलाहकारी रवैये को हम अधिक स्वीकार्य रूप में ले सकते हैं। यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे वरिष्ठ (सीनियर) न्यायाधीश होते हैं, वहीं बनते हैं, लेकिन कभी-कभी सरकार के द्वारा इसे उल्लंधित भी किया गया है। जैसे इंदिरा गांधी ने दो बार इसका उल्लंघन किया था। इस बात का बहुत बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का रास्ता महाभियोग है जिसमें संसद के दोनों सदनों से बहुमत तथा उप. स्थित सदस्यों के दो-तिहाई सदस्य एक ही अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति को भेजने का प्रावधान किया गया है।
मौलिक अधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय को अपील या रिट संबंधी मूल अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना अन्य न्यायालय में गए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को केन्द्र तथा राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच मामलों के निपटारे संबंधी मूल अधिकार भी हैं। वह निचले न्यायालय से अपने पास केस मंगवा सकते हैं। संवैधानिक, नागरिक एवम अपराधिक मुकदमों में इसके पास अपील की सुनावाई के अधिकार भी हैं। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता भी अहम है।
संविधान की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका सर्वोच्च है। लेकिन यह साफ कह देना आवश्यक है कि यह सिर्फ मूल ढांचे को सुरक्षित करने के आधार पर किसी संशोधन को अवैध घोषित करने की परंपरा है। लेकिन सबसे अधिक आवश्यक है कि यह माना जाए कि सर्वोच्च न्यायलय के कार्य में 'संविधान की व्याख्या' के मायने संविधान के संरक्षण से है और इससे भी बढ़कर 'संविधान के मूल ढांचे' के संरक्षण से है।
उच्च न्यायालय के अपने अधिकार होते हैं। रिट का आदेश देने की शक्ति हाई कोर्ट थी, यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक है। इनका कार्य मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के उच्चतम पदाधिकारी होते हैं साथ ही दूसरे जज भी होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तरह ही होता है। हाई कोर्ट के कानून राज्य की सभी अदालतों पर एक समान लागू होते हैं।
राज्य के सभी न्यायालय उच्च न्यायालय के ही अधीन होते हैं। जिला न्यायाधीश कि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट से सलाह करके होती है। निचली न्यायालय में जटिलता, भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद के रूप में एक विचार देखा जाता रहा है।
प्रशासनिक सेवा तथा इससे जुड़ी हुई सुविधाएं तथा नियम:
स्वतंत्रता के बाद भारत के तंत्र को चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता थी। उस समय में भारतीय प्रशासनिक तंत्र में (आजादी के तत्काल बाद) रजवाड़ो तथा जमींदार परिवारों के ही लोग शामिल थे जिसमें अंग्रेजी सरकार के आई.सी.एस. ने परीक्षा में भाग लिया था। यह तंत्र के उस काल का प्रतिनिधित्व करते थे जो नौकरशाही के तौर जर जाना जाता था।
आई.सी.एस. अफसर का मतलब था वह अंग्रेजी अफसर जिसे विशेषाधिकार प्राप्त था । स्वतंत्रता के बाद इसमें परिवर्तन आया तथा राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर लोग अपने देश में सेवा अपने देश के लिए करने की प्रेरणा में जीने लगे। आईसी. ए स. की जगह पै ने ली । अखिल भारतीय सेवा प्रादेशिक सेवा तथा केन्द्रीय या संघीय सेवा का मूल ढांचा बरकरार था।
संविधान में भाग 14 जोड़ा गया तथा 'संघ तथा राज्यों के तहत सेवाएं' में कहा गया है कि केंन्द्रीय तथा राज्य विधनों में केन्द्र एवम राज्य की सेवाओं संबंधी भर्ती एवम कार्य नियम बनाए जाएंगे। धारा 315 में संविधान स्वतंत्र जन के द्वारा भर्ती का प्रावधान रखकर न्यायपूर्ण रुख अपनाने का प्रयत्न किया गया है।
संविधान के आरंभ में IAS और IPS की सेवाओं का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने के लिए राज्यसभा को दो तिहाई बहुमत से तय करने के अधिकार दिए गए।
प्रशासनिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने तथा लोकतंत्र में जनता की भावना का ख्याल रखने में प्रशासनिक अधि कारी का अहम योगदान होता है तथा नीतियों के मानचित्रण में सर्वोच्च हाथ इसी समूह का होता है।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..