BPSC TRE 2.0 SOCIAL SCIENCE CLASS 10TH HISTORY NOTES | यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भू-भाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था।
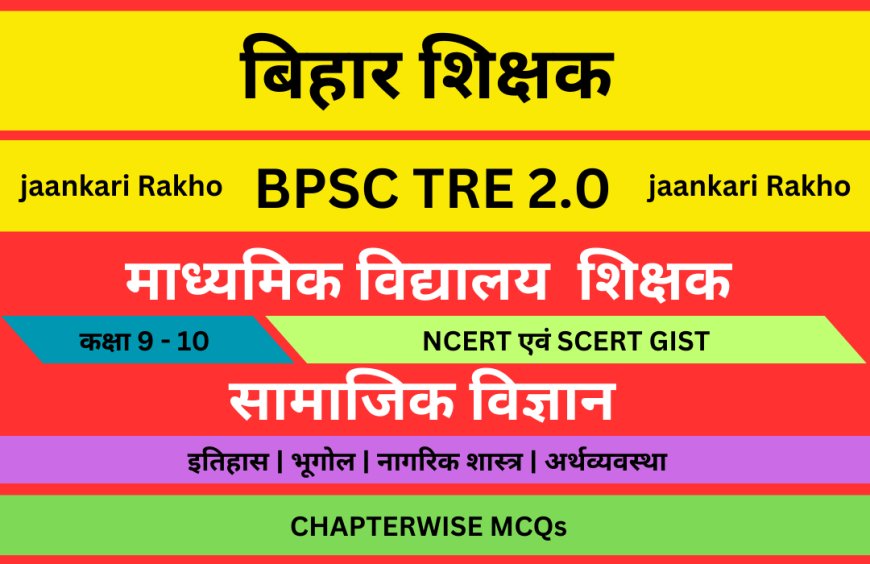
BPSC TRE 2.0 SOCIAL SCIENCE CLASS 10TH HISTORY NOTES | यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
- राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ई. में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई।
- 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भू-भाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था।
- फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक क़दम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी।
- पितृभूमि (la patrie) और नागरिक (le citoyen) जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा-तिरंगा ( the tricolour) चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली।
- इस्टेट जेनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल कर 'नेशनल एसेंबली' कर दिया गया।
- एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भू-भाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए ।
- आंतरिक आयात-निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एकसमान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को 'हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई।
- क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ़्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा।
- फ्रांस की घटनाओं की ख़बर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुँची तो छात्र तथा • शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे।
- क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएँ राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगीं।
- नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ़्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था।
- फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने नि:संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके।
- 1804 ई. की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसने क़ानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया।

- डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर किसानों को भू-दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई।
- शहरों में कारीगरों के श्रेणी-संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया।
- निरंकुश शासन का अंत कर प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव डाली गई।
- प्रशासन के साथ-साथ सामजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।
- फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश शासन का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
- क्रांति के पूर्व फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के शासक निरंकुश थे। उनपर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश नहीं था ।
- क्रांति ने राजा के विशेषाधिकारों और दैवी अधिकार सिद्धांत पर आघात किया। इस क्रांति के फलस्वरूप सामंती प्रथा (Feudal System) का अंत हो गया।
- कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। किसानों को सामंती कर से मुक्त कर दिया गया। कुलीनों और पादरियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गये।
- लोगों को भाषण-लेखन तथा विचार-अभीव्यक्ति का अधिकार दिया गया। फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर प्रणाली ( tax system) सुधार लाया गया।
- कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक-दूसरे से पृथक् कर दिया गया। अब राजा को संसद के परामर्श से काम करना पड़ता था।
- न्याय को सुलभ बनाने के लिए न्यायालय का पुनर्गठन किया गया। सरकार के द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की स्था की। गई। फ्रांस में एक एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, एक प्रकार के आर्थिक नियम बने और नाप-तौल की नयी व्यवस्था चालू की गई।
- लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। उन्हें किसी भी धर्म के पालन और प्रचार का अधिकार मिला। पादरियों को संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी । French Revolution ने लोगों को विश्वास दिलाया कि राजा एक अनुबंध के अंतर्गत प्रजा के प्रति उत्तरदायी है।
- यदि राजा अनुबंध को भंग करता है तो प्रजा का अधिकार है कि वह राजा को पदच्युत कर दे। यूरोप के अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की गयी।
| 1797 | नेपोलियन का इटली पर हमला; नेपोलियाई युद्धों की शुरूआत |
| 1814-1815 | नेपोलियन का पतन; वियना शांति संधि |
| 1821 | यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ |
| 1848 | फ्रांस में क्रांति; आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत; मध्यवर्ग संविधान और प्रतिनिध्यात्मक सरकार के गठन की माँग; इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि के द्वारा राष्ट्र राज्यों की मांग। |
| 1859-1870 | इटली का एकीकरण |
| 1866-1871 | जर्मनी का एकीकरण |
| 1905 | हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मज़बूत हुआ |
- जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड पहले राजशाहियों, डचियों (duchies) और कैंटनों (cantons) में बँटे हुए थे, जिनमें शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे।
- पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह-तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे।
- अकसर वे अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर, ऑस्ट्रिया-हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग-अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को मिलाकर बना था। ऐल्प्स के टिरॉल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ-साथ बोहेमिया भी शामिल था जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे।
- हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी-भाषी प्रांत भी शामिल थे।
- हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था।
- इन प्रभावशाली समूहों के अलावा, हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा में भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे- जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निओला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ़ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग।
- वस्तुत: "राष्ट्र" शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी भाषा के शब्द “नेशन" के पर्यायवाची के रूप में किया जाता रहा है लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है।
- 'राष्ट्र' से हमारा अभिप्राय किसी विशेष भूभाग, क्षेत्र या इलाके से रहा है लेकिन 'नेशन' से हमारा अभिप्राय किसी भूभाग से न होकर किसी समुदाय या मानव - सामूहिकता से है।
- भूभाग या मानव समुदाय का फर्क राष्ट्र और राष्ट्रवाद की परिभाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रवाद का उदय
- यूरोप में राजनीतिक इकाइयों और सांस्कृतिक इकाइयों का आगमन तो विकसित कृषक दौर तक हो चुका था लेकिन इनके बीच का संबंध वह नहीं था जो राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार होना था।
- अक्सर एक राजनीतिक इकाई राज्य के अन्तर्गत कई सांस्कृतिक इकाइयाँ संभावित राष्ट्र में मौजूद रहती थीं, या फिर एक विशाल सांस्कृतिक इकाई कई राज्यों में बिखरी हुई थी ।
- यह एक राज्य और एक राष्ट्र वाले राष्ट्रवादी सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन था। इन राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाइयों का राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार एक-दूसरे के साथ समेकित होने का कार्य मानव इतिहास के औद्योगिक दौर में हुआ।
- व्यापक साक्षरता के बगैर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का चल पाना संभव नहीं। अपने संचालन के लिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था 41888 को ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है जो परस्पर अजनबी और दूर-दूर होते हुए भी एक-दूसरे के साथ सम्प्रेषण • और संवाद जारी रख सकें। ऐसे संवाद के लिए उन्हें एक साझे भाषायी माधयम की आवश्यकता पड़ती है।
- परस्पर संवाद की इस आवयकता को न तो पुरानी क्लासिकी भाषाएँ लैटिन और ग्रीक पूरा कर सकती है और न ही सांस्कृतिक समूहों की अपनी स्थानीय बोलियाँ।
- औद्योगिक अर्थव्यवस्था की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी भाषाओं की जरूरत थी जो स्थानीय बोलियों के ऊपर तथा क्लासिकीय भाषाओं के नीचे पैदा हुए रिक्त स्थान को भर सकें।
- इस आवश्यकता को पूरा किया विभिन्न यूरोपीय समाजों में अंग्रेजी, पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, हंगेरियन इत्यादि भाषाओं ने।
- इन भाषाओं का विकास और मानकीकरण तो औद्योगिक क्रांति से पहले पुनर्जारण के बाद से ही शुरू हो गया था लेकिन 18वीं - 19वीं शताब्दियों में इनका अधिक प्रसार हुआ और अपने समाजों में ये राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्थापित और प्रतिष्ठित हुई।
- विशाल और संस्कृतिक रूप से समरूपी राष्ट्रीय इकाइयों को राष्ट्र ही सुरक्षित और संरक्षित नहीं रख सकता। महज राष्ट्र ही अपनी अस्मिता के संरक्षण के लिए काफी नहीं है। इन इकाइयों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक छत्रछाया की जरूरत पड़ती है।
- राष्ट्रवादी विचारधारा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के नागरिक राज्य के निर्देशों के अनुसार ही समाज को चलाने में राज्य की मदद करें। इस तरह से हम आधुनिक परिस्थितियों के अन्तर्गत राष्ट्रवाद को एक अपरिहार्य तत्व के रूप में पाते हैं।
- अपनी रक्षा के लिए यह राज्य पर निर्भर होता है (या कहें कि सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी के लिए इसे राज्य की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि राष्ट्र और राज्य एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनकी यह परस्पर निर्भरता ही राष्ट्रवाद के उदय का मूल सार है। जर्मनी और इटली का एकीकरण इन्हीं संदर्भों की देन रहे ।
- यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी liberalism शब्द लातिन भाषा के मूल liber पर आधारित है जिसका अर्थ है 'आज़ाद'।
- नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था 'व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी'।
- राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो ।
- फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरीवर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था।
- 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था।
- संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति-विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की माँग करते हुए विरोध-आंदोलन चलाए।
- महिलाएँ एवं संपत्ति विहिह्न पुरूष आर्थिक क्षेत्र में, उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूँजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में थे। 19वीं सदी के दौरान, उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार माँग थी ।
- नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप-तौल प्रणाली थी।
- 1833 ई. में हैम्बर्ग से न्यूरेम्बर्ग जा कर अपना माल बेचने वाले किसी व्यापारी को ग्यारह सीमाशुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था।
- नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तुओं, लोग और पूँजी का आवागमन बाधारहित हो ।
- 1834 ई. में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन (Zollverein) स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए।
- 1815 ई. में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएँ जैसे- राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊँच-नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे।
- नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था।
- एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था. सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति-यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे।
- 1815 में. ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले।
- सम्मेलन (Congress) की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि (Treaty of Vienna) तैयार की जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे।
- फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूब वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था।
- फ़्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके।
- उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया। जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पीडमॉण्ट में जेनोआ जोड़ दिया गया।
- प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्त्वपूर्ण नए इलाके दिए गए जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया।
- पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नयी रूढ़िवादी व्यवस्था क़ायम करने का लक्ष्य भी था।
- 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएँ निरंकुश थीं। वे आलोचना और असहमति बरदाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं।
- ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे।
- फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नयी रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था- प्रेस की आजादी।
- नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी विजयों के द्वारा यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन किए थे, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के प्रमुख राजनीतिज्ञों एवं प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन को वियना कांग्रेस कहा जाता है।
- वियना कांग्रेस सितम्बर, 1814 में प्रारम्भ हुई थी, किन्तु इससे पूर्व कि इसमें कुछ निर्णय लिए जाते, नेपोलियन बोनापार्ट एल्बा द्वीप से भाग निकलने में सफल हो गया।
- कुछ समय के लिए इस सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा। यह कांग्रेस पुनः नवम्बर, 1814 में प्रारम्भ हुई।
- 18 जून, 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात् नेपोलियन बोनापार्ट को बन्दी बनाकर सेण्ट हेलेना द्वीप भेज दिया गया।
- नेपोलियन बोनापार्ट के वाटरलू के युद्ध में परास्त होने के कुछ दिन पूर्व ही (9 जून, 1815 को) इस सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने अन्तिम निर्णयों पर हस्ताक्षर किए।
- नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो जाने से फ्रांस का सैनिक महत्त्व नष्ट हो गया था, किन्तु फ्रांस की राज्यक्रान्ति (1789 ई.) का प्रभाव सम्पूर्ण महाद्वीप में फैल चुका था। मित्र राष्ट्र इन क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों को नष्ट करके यूरोप में पुरातन व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहते थे।
- नेपोलियन बोनापार्ट ने स्पेन, हॉलैण्ड, इटली, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल तथा अन्य देशों को पराजित करके यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के पश्चात् इन सभी राज्यों की राजनीतिक स्थिति को ठीक करने के साथ-साथ यूरोप के मानचित्र को बनाने की समस्या भी उपस्थित हो गई थी।
- क्रान्ति काल में क्रान्तिकारियों ने रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारों और उसकी सम्पत्ति पर अधिकार करके उसके महत्त्व को समाप्त कर दिया था। मित्र राष्ट्र चर्च की प्राचीन महत्ता को पुनर्स्थापित करना चाहते थे।
- लगभग सभी देश नेपोलियन बोनापार्ट के युद्धों से प्रभावित हो चुके थे। इन युद्धों में अपार जन-धन की क्षति हुई थी। अब वह शान्ति चाहते थे। इस सम्मेलन में उन उपायों पर विचार-विमर्श होना था जिनके द्वारा यूरोप में स्थायी शान्ति स्थापित हो सके।
- ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिख इस सम्मेलन का संचालक था। मैटरनिख पुरातन एवं प्रतिक्रियावादी व्यवस्था का समर्थक तथा क्रान्तिकारी विचारों का कट्टर शत्रु था। नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
- वियना सम्मेलन के निर्णयों पर मैटरनिख के विचारों का पूरा प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में रूस के जार अलेक्जेण्डर प्रथम, इंग्लैण्ड के विदेश मन्त्री कैसलरे, फ्रांस के विदेश मन्त्री तैलीरौं तथा प्रशा के सम्राट् फ्रेड्रिक विलियम तृतीय की उपस्थिति ने सम्मेलन को आकर्षक बना दिया था।
- सम्मेलन के प्रतिनिधियों के पारस्परिक मतभेदों के कारण सम्मेलन की असफलता की सम्भावनाएँ बढ़ गई थीं, फिर भी समस्याओं के समाधान हेतु अग्रलिखित सिद्धान्त पारित किए गए थे
- सभी सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि पिछले 25 वर्षों में राजनीतिक उथल-पुथल का कारण 1789 ई. की क्रान्ति का विस्फोट था।
- यह निश्चित किया गया कि 1789 ई. की क्रान्ति से पूर्व सभी देशों में प्रचलित शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए अर्थात् उन प्राचीन राजवंशों को शासन करने का अधि कार पुनः प्रदान कर दिया जाए जो 1789 ई. की क्रान्ति से पूर्व सत्तारूढ़ थे।
- निर्णय लिया गया कि यूरोप का मानचित्र बनाते समय सभी देशों में शक्ति सन्तुलन स्थापित किया जाए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि फ्रांस तथा अन्य ऐसे देशों की सीमा पर शक्तिशाली राज्य स्थापित किए जाएँ, जहाँ पर क्रान्तिकारी विचारों के पुनः फैलने का भय था।
- सभी सदस्यों ने यह निश्चित किया कि नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित करने में जिन देशों ने मित्र राष्ट्रों की सहायता की थी, उन्हें पुरस्कार स्वरूप राजनीतिक सीमा बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए।
- इसके विपरीत नेपोलियन बोनापार्ट का साथ देने वाले देशों को दण्डित करने के उद्देश्य से उनकी राजनीतिक सीमा में | कटौती की जाए
- न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धान्त के आधार पर फ्रांस में बूब राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। सम्राट् लुई सोलहवें के छोटे भाई लुई अठारहवें को फ्रांस का राजा बनाया गया। पिछले युद्धों के लिए फ्रांस को जिम्मेदार ठहराते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में 70 करोड़ फ्रैंक की धनराशि फ्रांस पर लाद दी गई । इस रकम का भुगतान होने तक फ्रांस के खर्चे पर फ्रांस की सीमा पर मित्र राष्ट्रों के 15 लाख सैनिक नियुक्त कर दिए गए। फ्रांस की राजनीतिक सीमा को 1791 ई. की स्थिति में स्वीकार कर लिया गया।
- फ्रांस के पड़ोसी देश हॉलैण्ड को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से बेल्जियम का प्रदेश ऑस्ट्रिया से लेकर हॉलैण्ड को दे दिया गया।
- इटली की राष्ट्रीय एकता को समाप्त करके उसको आठ भागों में विभक्त कर दिया। रोम में पोप का शासन पुनः स्थापित कर दिया गया।
- जर्मनी के छोटे-छोटे 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन परिसंघ बनाया गया, जिसके अध्यक्ष पद पर ऑस्ट्रिया के सम्राट को नियुक्त किया गया। परन्तु परिसंघ को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। इस प्रकार राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध बड़े शिथिल रहे।
- ऑस्ट्रिया को बेल्जियम के बदले में इटली के लोम्बार्डी तथा वेनेशिया के प्रदेश दिए गए।
- सबसे अधिक लाभ ग्रेट ब्रिटेन को हुआ। उसे हेलिगोलैण्ड, माल्टा, आयोनियन द्वीप समूह, केप कॉलोनी, टोबैगो, सेण्ट लूसिया, त्रिनिदाद आदि क्षेत्र प्राप्त हो गए, जो औद्योगिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे।
- नार्वे तथा स्वीडन को मिला दिया गया। स्वीडन से फिनलैण्ड का प्रदेश लेकर रूस को दे दिया गया।
- प्रशा को शक्तिशाली बनाने के लिए उसे सेक्सनी राज्य का 40% भाग प्रदान किया गया।
- पोलैण्ड को तीन भागों में विभक्त करके अधिकांश भाग रूस को दे दिया गया।
- भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय जहाजों के आवागमन, समुद्रों के उपयोग तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार व वाणिज्य के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया।
- वियना समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा महाद्वीप में शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से इंग्लैण्ड, रूस, प्रशा व ऑस्ट्रिया ने यूरोप की संयुक्त व्यवस्था (Concert of Europe) की स्थापना की।
- इस सम्मेलन में किसी भी देश की जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया था। वस्तुतः यह शासकों का सम्मेलन था. जनता का नहीं। इसमें सभी अधिकार शासकों को सौंप दिए। गए। किसी ने जनता की भावनाओं को जानने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि जनता ने वियना व्यवस्था को कभी हृदय से स्वीकार नहीं किया । इतिहासकार हेजन ने लिखा है 'इस सम्मेलन में राजनीतिज्ञों द्वारा जनता की भावनाओं की अवहेलना करते हुए यूरोप का मानचित्र बनाया गया, जिसके कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका।'
- राष्ट्रीयता एवं प्रजातन्त्र तत्कालीन इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ थीं, किन्तु वियना सम्मेलन में इन प्रवृत्तियों की अवहेलना की गई। केवल शक्ति सन्तुलन का ध्यान रखते हुए यूरोपीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। इस महान् गलती के कारण 1815 ई. के बाद के वर्षों में निरन्तर आन्दोलन व क्रान्तियाँ होती रहीं। इसीलिए एक इतिहासकार ने कहा है, '1815 ई. के बाद के यूरोप का इतिहास वियना व्यवस्था की त्रुटियों को सुधारने का इतिहास है। '
- क्रान्ति के सिद्धान्तों का उस समय इतना व्यापक प्रभाव था कि इन सिद्धान्तों के विपरीत कोई भी व्यवस्था सफल नहीं | हो सकती थी। वियना सम्मेलन में भी क्रान्ति के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई तथा सभी देशों में शासन के अधिकार प्राचीन राजवंशों को प्रदान करके पुरातन व्यवस्था को पुनः . लागू कर दिया गया। इसलिए सभी देशों की जनता ने इसके निर्णयों को ठुकराना प्रारम्भ कर दिया।
- उस समय मित्र राष्ट्रों के सामने शान्ति की स्थापना एक मुख्य समस्या थी। उनके कन्धों पर महाद्वीप को युद्ध के ताण्डव से बचाने की जिम्मेदारी थी। निःसन्देह उन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। उन्होंने वियना व्यवस्था के माध्यम से लगभग 40 वर्षों तक महाद्वीप को युद्ध की आग से सुरक्षित रखा।
- यद्यपि सम्मेलन के निर्णयों में राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई थी, तथापि पीडमॉण्ट, प्रशा आदि राज्यों को शक्तिशाली बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से इटली व जर्मनी के राष्ट्रीय आन्दोलनों की सशक्त पृष्ठभूमि का निर्माण भी किया था।
- इस सम्मेलन ने भविष्य में परस्पर बातचीत के द्वारा समस्याओं को हल करने की नवीन परिपाटी को जन्म दिया। इस सम्मेलन को भविष्य के यूरोप का आधार माना जाता है। एक इतिहासकार ने लिखा है, 'वियना सम्मेलन के प्रतिनिधि ईश्वर के अवतार नहीं थे। अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने शान्ति स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था ।'
- सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था।
- इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बँधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर-पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद भूसंपत्तियों और शहरी - हवेलियों के मालिक थे।
- राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अकसर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे।
- मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज़ से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के दृष्टि अधिकांश लोग कृषक थे।
- पश्चिम में ज्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बँटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे।
- पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाज़ार के लिए उत्पादन पर टिका था।
- इंग्लैंड में औद्योगीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ लेकिन फ़्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ।
- नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने।
- मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए।
- 1815 ई. के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादीराष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए ।
- उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थीं।
- साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र-राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे।
- ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी 'जोसेफ मेजिनी' उनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया।
- चौबीस साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की।
- भूमिगत संगठनों में पहला था मार्सेई में यंग इटली दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे ।
- मेजिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था।
- उसे जोड़ कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था । यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था।
- इस मॉडल की देखा-देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया।
- मैटरनिख ने उसे 'हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन' बताया। मैटर्रानस्त्र प्रतिक्रियावादी विचाराधारा का सूत्र वाक्य था - " शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो । "
- 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मैटरनिख यूरोप की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का नेतृत्वकर्ता था। 1815 से 1848 ई. तक ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में वह यूरोप का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। 34 वर्ष की इस अवधि को यूरोप के इतिहास में 'मैटरनिख युग' कहा जाता है।
- मैटरनिख का जन्म 15 मई, 1773 को कॉब्लेंज नामक नगर में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने उसके पिता की जागीर को जर्मनी के पुनर्गठन के समय जब्त कर लिया था।
- कुलीनों एवं सामन्तों पर क्रान्तिकारियों के अत्याचारों की कहानी सुनकर मैटरनिख का हृदय सदैव के लिए क्रान्ति विरोधी हो गया था। 1795 ई. में उसकी शादी ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर कानिज की पौत्री के साथ हुई। इस घटना के पश्चात् उसके राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ हुआ।
- 1801 से 1806 तक वह यूरोप के अनेक देशों में राजदूत के पद पर नियुक्त हुआ। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर ऑस्ट्रिया के सम्राट् फ्रांसिस प्रथम ने 1809 ई. में उसे ऑस्ट्रिया का चांसलर नियुक्त किया तथा 1848 ई. तक वह निरन्तर इस पद पर बना रहा।
- मैटरनिख को अपनी शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था । वह समझता था कि उसका जन्म यूरोप महाद्वीप के बिगड़े हुए राजनीतिक ढाँचे को ठीक करने के लिए हुआ है।
- मैटरनिख क्रान्ति का कट्टर शत्रु था । वह क्रान्ति को सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा, संक्रामक रोग, ज्वालामुखी आदि नामों से पुकारता था।
- वह सुधारों का विरोधी तथा यथास्थिति का समर्थक था।
मैटरनिख की गृह नीति
- मैटरनिख कार्यकाल में ऑस्ट्रिया साम्राज्य में विभिन्न जातियों का निवास था, देश का सामाजिक ढाँचा सामन्तवादी था |
- देश की अधिकांश भूमि व सम्पत्ति पर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अधिकार था। दूसरी ओर साधारण वर्ग की दशा अत्यन्त दयनीय थी। उन्हें कृषि उपज का अधिकांश भाग कर के रूप में देना पड़ता था।
- साम्राज्य को कई प्रान्तों में बाँट दिया गया। प्रत्येक प्रान्त पर एक गवर्नर नियुक्त किया गया।
- विद्यालयों पर कठोर सरकारी नियन्त्रण स्थापित किया गया। सभी पाठ्यक्रमों को बदल दिया गया। इतिहास व दर्शन के अध्ययन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।
- अभिव्यक्ति, लेखन आदि पर नियन्त्रण के लिए समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिए गए।
- साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया।
- विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी गई।
- ऑस्ट्रिया की सीमा पर निरीक्षकों को नियुक्त किया गया। उनका कार्य राष्ट्रीयता के समर्थक व्यक्तियों एवं साहित्य के प्रवेश पर रोक लगाना था।
- व्यापारिक क्षेत्र में मैटरनिख ने संरक्षित शुल्क व्यवस्था को अपनाया, ताकि विदेशों में व्यापारिक सम्पर्क न बढ़ सके।
वैदेशिक नीति के क्षेत्र में मैटरनिख के महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित थे
1. वियना समझौता (1815 ई.)
- वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के पतन के पश्चात् 1815 ई. में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के सभी देशों के राजनीतिज्ञों का सम्मेलन बुलाया गया।
- मैटरनिख इस सम्मेलन का संयोजक था। इस सम्मेलन में हुए समझौते की शर्तों पर मैटरनिख के विचारों को स्पष्ट प्रभाव पड़ा।
- ऑस्ट्रिया साम्राज्य की सीमा में वृद्धि करने के साथ-साथ इटली व जर्मनी में भी अपना प्रभाव स्थापित करने में मैटरनिख को सफलता प्राप्त हुई थी।
- रूस के जार अलेक्जेण्डर प्रथम ने यूरोप महाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए ईसाई धर्म पर आधारित 'पवित्र संघ' की योजना को प्रस्तुत किया।
- मैटरनिख ने इस योजना का कड़ा विरोध किया और इसे 'ढोल की पोल' तथा 'नैतिकता का कोरा प्रदर्शन बतया । उसके विरोध के कारण यह योजना असफल हो गई।
- मित्र राष्ट्रों ने वियना समझौते को स्थायी बनाने के लिए चतुर्मुख संघ की स्थापना की थी।
- ऑस्ट्रिया भी इस संघ का सदस्य था, किन्तु शीघ्र ही हस्तक्षेप के प्रश्न पर मैटरनिख का इंग्लैण्ड से मतभेद हो गया।
- मैटरनिख संयुक्त व्यवस्था का प्रयोग यूरा में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद के दमन के लिए करना चाहता था, जबकि इंग्लैण्ड के विदेश मन्त्री कैसलरे तथा कैनिंग ने इस हस्तक्षेप को अनुचित बतलाते हुए मैटरनिख की नीति का कड़ा विरोध किया। इस पारस्परिक फूट के कारण यह व्यवस्था 1825 ई. में समाप्त हो गई।
- वियना समझौते के अनुसार जर्मनी को 39 राज्यों का एक संघ बनाकर ऑस्ट्रिया को इस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था।
- मैटरनिख का उद्देश्य जर्मनी में राष्ट्रवादी व क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना था, किन्तु जर्मनी की जनता ने इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
- मैटरनिख ने 1819 ई. में 'कार्ल्सबाद अध्यादेश' (Carlsbad | Decrees) पारित करके जर्मनी के विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, समाचार पत्रों एवं पत्रकारों पर कठोर नियन्त्रण लगा दिया। यह व्यवस्था 1848 ई. तक चलती रही।
- इटली को छोटे-छोटे राज्यों में बाँटकर वहाँ पर पुनः निरंकुश शासकों को सत्तारूढ़ करने में मैटरनिख की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
- इस व्यवस्था के विरुद्ध नेपल्स व पीडमॉण्ट राज्यों की जनता ने विद्रोह कर दिया।
- मैटरनिख ने ट्रोपो (1820 ई.) तथा लाईबेख (1821 ई.) की कॉन्फ्रेंस द्वारा अधिकार प्राप्त करके अपनी सेना भेजकर इन दोनों राज्यों के विद्रोहों का दमन कर दिया। इस प्रकार 1848 ई. तक इटली में भी यथास्थिति बनी रहीं।
- शक्ति सन्तुलन बनाए रखने के लिए उसने यूरोप और ऑस्ट्रिया में पाए जाने वाले विरोधों एवं मतभेदों को बनाए रखा।
- इटली और जर्मनी को विभाजित रखा तथा ऑस्ट्रिया में बसने वाली विभिन्न जातियों का एक-दूसरे के विरुद्ध उपयोग किया।
- मैटरनिख की असफलता के कारण तथा मैटरनिख का पतन
- 1848 ई. में फ्रांस की जनता ने सम्राट् लुई फिलिप के विरुद्ध क्रान्ति कर दी । लुई फिलिप भाग गया और फ्रांस में गणतन्त्र की घोषणा कर दी गई। इस समाचार को सुनकर ऑस्ट्रिया की जनता का उत्साह बढ़ गया।
- 13 मार्च, 1848 को मैटरनिख के विरुद्ध वियना में क्रान्ति हो गई। क्रान्तिकारियों ने मैटरनिख के महल को घेर लिया। भीड़ नारे लगा रही थी, 'मैटरनिख त्याग-पत्र दो, मैटरनिख का नाश हो' मैटरनिख ने परिस्थितियों की नाजुकता को पहचान लिया और कहा, 'मैं एक बूढ़ा हकीम हूँ, मैं साध्य और असाध्य बीमारियों के अन्तर को जानता हूँ, यह बीमारी प्राणघातक है।' उसने तुरन्त चांसलर पद से त्याग-पत्र दे दिया और इंग्लैण्ड भाग गया।
- मैटरनिख की शासन प्रणाली पूर्णतया प्रतिक्रियावादी और क्रान्तिजनित विचारों की विरोधी थी। परिणामस्वरूप उसका शासन विचारशील लोगों और देशभक्तों के लिए असहनीय हो गया।
- मैटरनिख की दमनकारी नीति के कारण समस्त यूरोप में आतंक छा गया। मैटरनिख को जो भी सहयोग मिला, | वह भय के कारण मिला, स्वेच्छा से नहीं। ऐसी स्थिति में उसका पतन अवश्यम्भावी था।
- यूरोप में समाजवाद की भावना का जन्म होने से श्रमिकों एवं पूँजीपतियों का विरोध बढ़ गया और उसका भी मैटरनिख के शासन पर व्यापक प्रभाव पड़ा।
- मैटरनिख शासन प्रगति का विरोधी था । वह यथास्थिति बनाए रखने का पक्षपाती था। उसने समाजवादी, उदारवादी और राष्ट्रवादी- इन तीनों आन्दोलनों को कुचलने का प्रयास किया और इसलिए उसे प्रबल जनमत का विरोध सहन करना पड़ा।
- शिक्षा के क्षेत्र में कठोर प्रतिबन्धों के लगने के फलस्वरूप शिक्षक और बौद्धिक वर्ग मैटरनिख का विरोधी बन गया।
- औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी आदि में इंग्लैण्ड की भाँति कल-कारखाने स्थापित हुए। फलस्वरूप यूरोप के अनेक राज्यों में नवयुग का प्रादुर्भाव हुआ। पुरातन व्यवस्था को अव्यावहारिक माना जाने लगा और इस स्थिति में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का पतन होना स्वाभाविक था।
- मैटरनिख तत्कालीन यूरोप का महानतम राजनीतिज्ञ था। उसने नेपोलियन के युद्धों से लहूलुहान यूरोप में काफी समय तक शान्ति बनाए रखी और उसने ऑस्ट्रिया के गौरव को बढ़ाया।
- अपने प्रतिक्रियावाद में मैटरनिख एक लम्बे समय तक सफल रहा। वह कहता था, 'यूरोप में शान्ति की स्थापना के लिए मेरी नीति आवश्यक और अनिवार्य साधन है। '
- यह ठीक है कि नेपोलियन के युद्धों से जर्जर अवस्था में यूरोप में शान्ति की स्थापना में मैटरनिख को सफलता मिली, परन्तु फिर भी मैटरनिख लगभग सभी इतिहासकारों की आलोचना का पात्र रहा। इसका कारण यह था कि वह अपने युग का महान् प्रतिक्रियावादी नेता था।
- वह क्रान्ति, राष्ट्रीयता, उदारवाद, प्रजातन्त्र आदि विचारों का कट्टर विरोधी तथा यथास्थितिवाद व पुरातनवाद का सफल पुजारी था। उसके चरित्र का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें समय के अनुसार समायोजित होने की योग्यता का अभाव था। वह प्रायः कहता था 'मैं इस संसार में या बहुत जल्दी आया हूँ अथवा देर से आया हूँ। पहले आने पर युग का आनन्द लेता और बाद में आने पर युग की पुनर्रचना में सहायता करता । किन्तु इस समय मुझे अपना जीवन बिगड़े हुए समाज को ठीक करने में लगाना पड़ा है।'
- इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी-राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली - अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे।
- प्रथम विद्रोह फ़्रांस में जुलाई, 1830 में हुआ। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फ़िलिप था।
- मैटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि 'जब फ़्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी-जुकाम हो जाता है।' जुलाई क्रांति से ब्रूसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया।
- एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम | पंद्रहवीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था।
- यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया।
- यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति (Hellenism) के प्रति सहानुभूति रखते थे।
- कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बता कर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी ।
- 1830 ई. में फ्रांस की जनता ने बूर्बो वंश के सम्राट् चार्ल्स Xth के विरुद्ध एक सफल क्रान्ति की थी। चार्ल्स Xth सिंहासन छोड़कर भाग गया। यूरोप के इतिहास में इसे 'जुलाई क्रान्ति' के नाम से जाना जाता है।
- 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रान्ति बूर्बो वंश के सम्राट् लुई सोलहवें के निरंकुश शासन के विरुद्ध की थी।
- फ्रांस की जनता बूर्बो वंश की निरंकुशता से घृणा करती थी। किन्तु वियना सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने उसी वंश को 1815 ई. में पुनः सत्तारूढ़ करके जन- असन्तोष को जन्म दिया।
- फ्रांस में एक वर्ग ऐसा भी था जो किसी भी दशा में बूब | वंश की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था।
- लुई 18वें द्वारा लागू किया गया संवैधानिक चार्टर दोषपूर्ण तथा जनता के लिए अहितकर था। मताधिकार योग्यता सम्पत्ति पर आधारित थी। सामन्तों की सभा (Chamber of Peers) के सदस्यों का मनोनयन केवल राजा द्वारा किया जाता था।
- राजा के अधिकार असीमित थे। मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इस प्रकार संविधान जन-भावनाओं के प्रतिकूल व अहितकर था।
- यद्यपि फ्रांस के विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों में विभिन्नता थी, तथापि बूर्बो वंश की निरंकुश नीति के विरोध में वे सभी एकमत थे। उन्होंने सामूहिक रूप से चार्ल्स दशम को हटाने का संकल्प लिया था। राजनीतिक दलों की एकता की भावना ने बूब वंश की जड़ों को कमजोर बना दिया। ने
- चार्ल्स Xth महान् प्रतिक्रियावादी शासक तथा कट्टर राजसत्तावादी दल का नेता था। सम्राट् बनने के पश्चात् उसने लोगों के भाषण, लेखन व प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
- मताधिकार योग्यता को अत्यधिक कठोर बना दिया। उसने चर्च को विशेष महत्त्व दिया।
- प्रधानमन्त्री पद पर प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को नियुक्त किया। इनमें पॉलिगनेक (Polignac) का नाम उल्लेखनीय है ।
- जब प्रतिनिधि सभा ने पॉलिगनेक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, तो चार्ल्स Xth ने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। इस प्रकार चार्ल्स Xth की प्रतिक्रियावादी व दमन नीति को फ्रांस की जनता ने स्वीकार नहीं किया।
- 1830 ई. की फ्रांसीसी क्रान्ति का मुख्य कारण चार्ल्स दसम के 'सेण्ट क्लाउड के अध्यादेश' (Ordinances of St-Cloud) थे।
- चार्ल्स दसम की दमन नीति उस समय पराकाष्ठा पर पहुँच गई जब 26 जुलाई, 1830 को उसने अध्यादेश पारित करके प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
- एक नये निर्वाचन कानून की घोषणा की गई, जिसके द्वारा मतदाताओं की संख्या को सीमित कर दिया गया। नवीन चुनावों की घोषणा कर दी गई।
- जुलाई अध्यादेशों की घोषणा के विरोध में 27 जुलाई को पेरिस में चार्ल्स दसम के विरुद्ध जुलूस निकाला गया। तीन दिन तक सेना तथा क्रान्तिकारियों में भयंकर युद्ध हुआ।
- अन्त में क्रान्तिकारियों की विजय हुई। स्थिति बिगड़ जाने पर चार्ल्स दसम ने जुलाई अध्यादेशों को वापस लेने की घोषणा की, किन्तु क्रान्तिकारियों को सन्तोष नहीं हुआ । अन्ततः 31 जुलाई, 1830 को चार्ल्स दशम सिंहासन छोड़कर भाग गया।
- इसके फलस्वरूप न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया गया। बूर्बो वंश की निरंकुश सत्ता के स्थान पर लुई फिलिप के नेतृत्व में संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना की गई।
- 1789 ई. की क्रान्ति के अधूरे कार्य को इस क्रान्ति ने पूरा कर दिया।
- इस क्रान्ति के फलस्वरूप सामन्तों, पादरियों व कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।
- यह क्रान्ति मैटरनिख व्यवस्था के पतन का संकेत थी।
- इस क्रान्ति से बेल्जियम पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गया।
- इस क्रान्ति का प्रभाव लगभग सम्पूर्ण यूरोप पर पड़ा ।
- स्पेन की जनता ने फर्डिनेण्ड सप्तम के निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
- यह विद्रोह कुचल दिया गया, तथापि 1834 ई. के चुनावों में राष्ट्रवादियों को सफलता मिल जाने के कारण राजा को 1837 ई. में उदार संविधान स्वीकार करना पड़ा।
- इसके फलस्वरूप स्पेन में वैध राजसत्ता की स्थापना हुई और लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल का गठन किया गया।
- पुर्तगाल की शासिका डोना मारिया के चाचा डॉन मिगुएल ने. डोना मारिया से सिंहासन छीनकर अपना निरंकुश शासन स्थापित कर लिया था।
- राष्ट्रवादियों ने फ्रांस की क्रान्ति से प्रेरणा पाकर क्रान्ति कर दी । फलस्वरूप डोना मारिया की सरकार पुनः सत्तारूढ़ हो गई।
- बेल्जियम की जनता ने हॉलैण्ड की सरकार के विरुद्ध क्रान्ति कर दी। ब्रुसेल्स में हॉलैण्ड की सेना तथा बेल्जियम की जनता में युद्ध हुआ। सेना बुरी तरह पराजित हो गई।
- इंग्लैण्ड, रूस व ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम की स्वतन्त्रता को मान्यता दे दी। राजकुमार लियोपोल्ड को वहाँ का राजा बनाया गया।
- जुलाई क्रान्ति से प्रेरित होकर स्विट्जरलैण्ड की जनता ने सरकार के समक्ष संविधान में संशोधन तथा प्रशासनिक सुधारों माँग प्रस्तुत की। सरकार ने जनता की प्रायः सभी माँगों को स्वीकार कर लिया।
- इंग्लैण्ड में टोरी दल की सरकार कार्य कर रही थी। 1820 ई. के आम चुनावों में जनता ने संसदीय सुधारों के समर्थन में बिग ( उदार) दल को अपना समर्थन दिया। फलस्वरूप बिग दल सत्तारूढ़ हो गया।
- 1832 ई. में प्रथम संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप जनता के संवैधानिक अधिकारों में वृद्धि हो गई।
- 1830 ई. में जर्मनी के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों से कई जर्मन राज्यों में विद्रोह किए।
- मैटरनिख ने हस्तक्षेप करके इन विद्रोहों का दमन कर दिया तथा यथास्थिति को कायम कर दिया। फिर भी राष्ट्रीयता की भावना को समूल नष्ट नहीं किया जा सका।
- 1815 ई. में जर्मनी की भाँति इटली को भी छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित करके उसकी राष्ट्रीय एकता को समाप्त कर दिया गया।
- अतः असन्तुष्ट राष्ट्रवादियों ने जुलाई क्रान्ति की सफलता से प्रेरित होकर इटली के राज्यों में भी आन्दोलन प्रारम्भ कर दिए।
- कई स्थानों पर क्रान्तियाँ सफल रहीं, किन्तु मैटरनिख ने तुरन्त हस्तक्षेप करके उन क्रान्तियों का दमन कर दिया। →
- 1830 ई. में पोलैण्ड की जनता ने रूस की अधीनता के विरुद्ध क्रान्ति कर दी।
- क्रान्तिकारियों ने इंग्लैण्ड, फ्रांस व जर्मनी के राष्ट्रवादियों से सहायता माँगी, किन्तु उन्हें सहायता नहीं मिली। फलस्वरूप रूस की सेना ने पोलैण्ड की क्रान्ति का दमन कर दिया।
- इस प्रकार 1830 ई. की जुलाई क्रान्ति का यूरोप के प्रत्येक देश पर प्रभाव पड़ा । यद्यपि कुछ देशों की क्रान्तियाँ असफल हो गई, तथापि प्रतिक्रियावादी व निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की यह प्रथम विजय थी।
- लिप्सन के अनुसार, 61688 तथा 1830 ई. की क्रान्ति में भी प्रजातन्त्र की दिशा में विशेष उन्नति नहीं की गई थी। लेकिन इंग्लैण्ड और फ्रांस, दोनों देशों में राजा के दैवी अधिकार के सिद्धान्त की स्थापना हुई।
- राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ । राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई।
- कला, काव्य, कहानियों-क़िस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया।
- रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क-वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर ज़ोर दिया।
- उनका प्रयास था कि एक साझा - सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए।
- जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी ।
- राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन-काव्य और लोकनृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था।
- स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक-साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुँचाना था जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे।
- यह पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों (Great Powers) ने विभाजन कर दिया था।
- पोलैंड अब स्वतंत्र भू-क्षेत्र नहीं था किंतु संगीत और भाषा के ज़रिये राष्ट्रीय भावना जीवित रखी। मसलन, कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजुरका जैसे लोकनृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया।
- भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्ज़े बाद, पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा कर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया।
- 1831 में, रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया।
- चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया।
- रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी।
- 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोज़गारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान-मजदूर विद्रोह कर रहे थे तब उसके समानांतर पढ़े-लिखे मध्यवर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी।
- फरवरी, 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्विक मताधिकार पर आधारित था।
- यूरोप के अन्य भागों में, जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे- जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य- वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री-पुरुषों ने संविधानवाद की माँग को राष्ट्रीय एकीकरण की माँग से जोड़ दिया।
- बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की माँगों को आगे बढ़ाया।
- यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था।
- जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिल कर एक सर्व-जर्मन नेशनल एसेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया।
- 18 मई, 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे-धजे जुलूस में जा कर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया।
- यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था ।
- जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरीख विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया।
- संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की माँगों का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे।
- उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था हालाँकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था।
- महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की।
- एसेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ़्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक-दीर्घा में खड़े होने दिया गया।
- रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुईं किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाईं।
- 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई।
- हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की हालाँकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ़ हुआ।
- 1848 ई. की क्रान्ति का मुख्य कारण लुई फिलिप की | आन्तरिक और बाह्य नीतियाँ थीं, जिनके कारण फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया।
- 1848 ई. में फ्रांस में जो क्रान्ति हुई, वह केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, वरन् इस क्रान्ति की चपेट में सम्पूर्ण यूरोप आ गया।
- इस प्रकार क्रान्ति को नष्ट कर पुरातन व्यवस्था को लादने का मैटरनिख का स्वप्न चकनाचूर हो गया और हर जगह नवीन शासन की स्थापना हुई।
1848 ई. की क्रान्ति के कारण
1. 1830-1848 ई. के बीच हुए आर्थिक परिवर्तन
- इस काल में औद्योगीकरण तीव्रता से हो रहा था। यातायात के साधनों के विस्तार ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा दिया था और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक नवीन पूँजीवादी व्यवस्था को जन्म दे चुका था।
- मजदूरों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उनकी समस्याएँ और आवश्यकताएँ भी बढ़ती जा रही थीं। 1838-1839 ई. तथा 1846-47 ई. में यूरोप में आर्थिक संकट आए, जिनसे जनता के कष्टों में मूल्य वृद्धि के कारण और अधिक बढ़ोत्तरी होती रही।
- औद्योगीकरण ने समाज के नये प्रभावशाली तत्त्वों, बुद्धिजीवियों व श्रमिक वर्ग को और अधिक विकसित किया प्रथम वर्ग ने उदारवादी शक्तियों को आत्मबल प्रदान किया, तो दूसरे वर्ग के आर्थिक शोषण के कारण सामाजिक एवं आर्थिक असन्तोष को तीव्रता मिली। परिणामस्वरूप 1848.ई. की क्रान्ति का विस्फोट हुआ।
- 1848 ई. की क्रान्ति का एक अन्य प्रमुख कारण इस समय तक समाजवाद का व्यापक प्रसार था।
- औद्योगीकरण ने पूँजीवाद को जन्म दिया और पूँजीवाद के परिणामस्वरूप समाजवाद नामक विचारधारा ने जन्म लिया। श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए आन्दोलन होने लगे।
- समाजवादियों ने देश के कल-कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने की जबरदस्त माँग करनी प्रारम्भ कर दी। जगह-जगह मजदूर संघों की स्थापना होने लगी। श्रमिक नेता मताधिकार विस्तृत करने की मांग करने लगे।
- लुई फिलिप का मन्त्री खिजों भी रूढ़िवादी और अपरिवर्तनशील विचारधारा का कट्टर समर्थक था । वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन एवं सुधार को खतरनाक समझता था।
- फ्रांस के प्रत्येक आन्दोलन को स्वार्थ का साधन बताकर उसकी अवहेलना ही नहीं की, बल्कि दमन भी किया। उसकी इन अपरिवर्तनशील निषेधात्मक नीतियों से फ्रांस के क्रान्तिकारी बड़े असन्तुष्ट हुए।
- लुई फिलिप की आन्तरिक और बाह्य, दोनों ही नीतियाँ क्रान्ति का महत्त्वपूर्ण कारण बनीं। उसने केवल मध्यम वर्ग को महत्त्व दिया और अन्य वर्गों की पूर्ण उपेक्षा की।
- इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक शान्तिप्रिय विदेश नीति ने उसे फ्रांस में दब्बू शासक के रूप में स्थापित किया, जिसे फ्रांसीसी कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे।
- बेल्जियम के मामले में तो वह बहुत अधिक झुका ही नहीं, बल्कि दब गया था।
- नेपोलियन के गौरवपूर्ण काल को देखने के पश्चात् फ्रांस की जनता दुर्बल शासक को अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर सकी और उसने शासन को उखाड़ फेंका।
- फ्रांसीसी गौरव से सदा पूर्ण रहे हैं। उन्हें लुई फिलिप की तुष्टीकरण और शान्ति की विदेश नीति बिल्कुल पसन्द नहीं आई।
- फ्रांस के क्रान्तिकारी चाहते थे कि फ्रांस विदेशों के क्रान्तिकारियों की मदद करे। परन्तु लुई फिलिप ने यूरोप के क्रान्तिकारियों की मदद तो की ही नहीं, बल्कि अपने देश तक में क्रान्तिकारियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया।
- लुई फिलिप के शासन पर मध्यम वर्ग का ही विशेष प्रभाव था और यह भी लुई फिलिप के भाग्य की विडम्बना थी कि इसी प्रभावशाली वर्ग ने उसे सत्ता से अलग कर दिया।
- मतदान की प्रणाली इस प्रकार रखी गई थी कि राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा में मध्यम वर्ग के धनवान व्यक्तियों का ही बहुमत रहा। फलत: अन्य वर्गों की उपेक्षा होती रही, जिसका परिणाम क्रान्ति के रूप में सामने आया।
1848 ई. क्रान्ति का अन्य देशों पर प्रभाव-
1. ऑस्ट्रिया पर प्रभाव
- 1848 ई. की क्रान्ति की सफलता का समाचार जब ऑस्ट्रिया की राजधानी पहुंचा, तो वहाँ के देशभक्त नवीन उत्साह से भर गए ।
- 18 मार्च को उन्होंने संगठित होकर एक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक, कारीगर, दुकानदार तथा मजदूर आदि सभी सम्मिलित थे।
- जुलूस की भीड़ ने मैटरनिख के घर को घेर लिया और उसके विरुद्ध नारे लगाए।
- मैटरनिख ने विवश होकर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और इंग्लैण्ड भाग गया । वास्तव में 1848 ई. की क्रान्ति ने मैटरनिख के प्रतिक्रियावादी शासन का अन्त कर दिया।
- बोहमिया ऑस्ट्रिया का एक अंग था। वहाँ पर भी क्रान्ति का प्रभाव पड़ा। राजा ने क्रान्तिकारियों की माँगें स्वीकार कर लीं, परन्तु बाद में क्रान्ति का दमन कर दिया गया।
- हंगरी की अधिकांश जनता मग्यार जाति की थी। वे ऑस्ट्रिया की अधीनता से मुक्त होना चाहते थे। जब उन्हें वियना की क्रान्ति का समाचार मिला, तो उन्होंने भी क्रान्ति का झण्डा खड़ा कर दिया।
- सम्राट को भयभीत होकर क्रान्तिकारियों से समझौता करना पड़ा। परन्तु आगे चलकर ऑस्ट्रिया ने रूस का सहारा लेकर क्रान्ति को विफल कर दिया।
- जब जर्मनवासियों को मैटरनिख के पतन का ज्ञान हुआ, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। क्रान्तिकारियों ने जुलूस निकालकर राजा के महल को घेर लिया।
- अंगरक्षकों द्वारा गोलियाँ चलाने पर क्रान्तिकारी भड़क उठे। राजा को विवश होकर संविधान सभा बुलानी पड़ी और नया लोकतान्त्रिक संविधान बनाया गया।
- फ्रांस की क्रान्ति से प्रेरित होकर स्विस लोगों ने धनवानों की प्रभुता के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने संगठित होकर प्रतिक्रियावादी कैथोलिक संघ पर आक्रमण कर उसे परास्त किया एवं स्विट्जरलैण्ड के लिए नया संविधान बनाकर उदारवादी शासन की स्थापना की।
- फ्रांस की 1848 ई. की क्रान्ति के प्रभाव से इंग्लैण्ड भी अछूता नहीं रहा।
- 1832 ई. का सुधार अधिनियम केवल मध्यम वर्ग के लोगों को ही सन्तुष्ट कर सका था, मजदूर किसानों को नहीं।
- 1848 ई. की क्रान्ति के फलस्वरूप इंग्लैण्ड में चार्टिस्ट आन्दोलन ने जोर पकड़ा।
- फ्रांस की क्रान्ति से प्रेरणा लेकर आयरलैण्ड की जनता ने इंग्लैण्ड के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। यद्यपि यह आन्दोलन सफल नहीं हो सका, क्योंकि आयरलैण्ड की जनता को फ्रांस की सहायता की उम्मीद थी, जो नहीं मिल सकी।
- मध्य यूरोप में क्रान्ति, जिसका प्रारम्भ बड़े उत्साहपूर्ण एवं | आशाजनक ढंग से हुआ था, थोड़े ही दिनों में शान्त हो गई। किन्तु यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि क्रान्ति मुख्यतः नगरों तथा मध्यम वर्ग तक ही सीमित थी।
- गाँवों की जनता अमूर्त भावात्मक स्वतन्त्रता की अपेक्षा अपने परम्परागत रीति-रिवाजों के प्रति अधिक आसक्त थी। 1850 ई. में उदारवाद तथा राष्ट्रीयता की प्रगतिशील शक्तियाँ मध्य यूरोप में प्रतिक्रिया की शक्ति के सामने पराजित हुई और प्रतिक्रिया की पूर्ण रूप से विजय हुई।
- स्लाव मैटरनिख के स्थान पर वार्जेनबर्ग चांसलर बना| ऑस्ट्रिया का संविधान रद्द हो गया, हंगरी का गणतन्त्र नष्ट हो गया, राष्ट्रीयता कुचल दी गई और समस्त साम्राज्य पर फिर से हात्सबुर्ग वंश का एकछत्र निरंकुश शासन स्थापित हो गया • तथा लोम्बार्डी एवं वेनेशिया फिर से ऑस्ट्रिया की अधीनता में पहुँच गए।
- सार्जीनिया के राजा के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयत्न निष्फल हुए और फ्रांसीसी तलवार के बल पर पोप फिर निरंकुश हो गया। जर्मनी फिर 1815 ई. की स्थिति में पहुँच गया।
- फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि क्रान्ति पूर्णतया असफल रही। प्रतिक्रियावादियों की अनेक सफलताओं के बीच भी कुछ लाभ बचे रहे।
- ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में अर्द्ध-दास व्यवस्था, जिसे क्रान्ति ने नष्ट कर दिया था, पुनः जीवित नहीं की गई।
- सार्जीनिया, स्विट्जरलैण्ड, हॉलैण्ड, डेनमार्क तथा प्रशा में किसी-न-किसी रूप में संवैधानिक शासन बना रहा। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि उदारवाद एवं राष्ट्रीयता की जिन भावनाओं का परिणाम यह क्रान्ति थी, उनका अस्तित्व नष्ट नहीं किया जा सका था।
- राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है, जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास परम्परा भाषा जातियता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते है ।
- 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी-जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया।
- इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक-दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया।
- 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गा, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टिनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था।
- बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई।
- 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के ज़रिए मज़बूत बनना चाहा था किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली।
- बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया।
- बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे-जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बनता गया।
- बाल्कन राज्य एक-दूसरे से ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गईं क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी।
- इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएँ खुल कर सामने आईं।
- रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थीं। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) हुआ।
- साम्राज्यवाद से जुड़ कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे।
- वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया।
- ब्रिटेन में राष्ट्र-राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल-पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था।
- 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीपसमूह में रहने वाले लोगों - अंग्रेज़, वेल्श, स्कॉट या आयरिश - की मुख्य पहचान नृजातीय (Ethnic ) थी ।
- सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएँ थीं। जैसे-जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन-दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई वह द्वीपसमूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताक़त छीन ली थी।
- संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ऐक्ट ऑफ़ यूनियन (1707) से 'यूनाइटेड किंग्डम ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन' का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड, व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया।
- ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी . पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया।
- स्कॉटिश हाइलैंड्स के निवासी जिन कैथलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा।
- स्कॉटिश हाइलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत . सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया।
- आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह देश कैथलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बँटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की।
- ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ़ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमेन (1798) की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंग्डम में शामिल कर लिया गया।
- एक नए 'ब्रितानी राष्ट्र' का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिह्नों, ब्रितानी झंडा (यूनियन जैक) और राष्ट्रीय गान (गॉड सेव अवर नोबल किंग) को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए।
- ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है।
- यह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं। संसद के उच्च सदन को लॉर्ड सभा तथा निचले सदन को कॉमन सभा कहते हैं।
- लॉर्ड सभा के सदस्य धनी तथा उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। यह एक प्रकार का वंशानुगत सदन है। इसे ब्रिटेन के निवासियों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का प्रतीक कहा जाता है।
- इस श्रेणी में 26 सदस्य होते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड बड़े गिरजाघरों के पादरी तथा बिशप होते हैं। ये सभा की कार्यवाही में प्रायः कम ही भाग लेते हैं।
- इस श्रेणी के पीयर सन् 1958 के 'आजीवन पीयरेज अधि नियम' के अन्तर्गत बनाए जाते हैं।
- ये सदस्य ख्याति प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों को आजीवन सदस्य बनाया जाता है। इस श्रेणी में स्त्रियाँ भी सदस्य बन सकती हैं।
- वर्ष 2005 तक इंग्लैण्ड में यह व्यवस्था थी कि सम्राट् द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता था। लेकिन A Constitutional Reform Act, 2005 के अनुसार अब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता।
- लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए अब स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है। कॉमन सभा के अध्यक्ष समान ही लॉर्ड सभा का अध्यक्ष (स्पीकर) निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं।
- Constitutional Reform Act, 2005 के बाद भी लॉर्ड चांसलर का पद बना हुआ है, लेकिन अब वह ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य मात्र है। अब वह लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता।
- सन् 1911 से पूर्व लॉर्ड सभा को अवित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थीं। किसी भी साधारण विधेयक के लिए यह आवश्यक था कि वह दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाए। परन्तु सन् 1911 तथा सन् 1949 के अधिनियमों ने इस स्थिति को बदल दिया है।
- सन् 1911 के अधिनियम के अनुसार कॉमन सभा के द्वारा पारित साधारण विधेयकों को लॉर्ड सभा केवल 2 वर्ष की देरी लगा सकती है।
- सन् 1949 अधिनियम के द्वारा यह अवधि 1 वर्ष कर दी गई है। एक वर्ष की अवधि के पश्चात् लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक पारित माना जाएगा।
- 18वीं शताब्दी से पूर्व लॉर्ड सभा राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी। परन्तु अब राजा कैविनेट के परामर्श के अनुसार कार्य करता है।
- जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है तथा कैबिनेट अपना त्याग-पत्र दे देती है, तो राजा को परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है, तो राजा लॉर्ड सभा से परामर्श ले सकता है।
- धन विधेयक पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। कॉमन सभा से पारित हो जाने के पश्चात् उनको लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्तियाँ नहीं के समान हैं।
- लॉर्ड सभा में न तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और न ही उसमें संशोधन किया जा सकता है।
- एक माह की अवधि समाप्त हो जाने पर विधेयक कानून बन जाता है। एक माह से अधिक देरी करने पर विधेयक को राजा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।
- लॉर्ड सभा मन्त्रिमण्डल को भंग नहीं कर सकती है। मन्त्रिमण डल को केवल कॉमन सभा ही अपदस्थ कर सकती है।
- मन्त्रिमण्डल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, परन्तु लॉर्ड सभा के सदस्यों को मन्त्रियों में प्रश्न पूछने का अधि कार है।
- इस क्षेत्र में लॉर्ड सभा को महत्त्वपूर्ण शक्तियां मिली हुई हैं। ये शक्तियाँ कॉमन सभा को प्राप्त नहीं हैं।
- लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, परन्तु समस्त लॉर्ड यह कार्य नहीं करते।
- यह कार्य केवल 9 न्यायिक लॉर्ड द्वारा किया जाता है। जब लॉर्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करती है, तो इसका अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर होता है।
- प्रजातन्त्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवस्थापिका पर किसी एक संस्था का एकाधिकार न होने पाए। वह मनमाने ढंग से या निरंकुश होकर कार्य न करे।
- अतः प्रथम सदन की निरंकुशता पर नियन्त्रण रखने के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। वास्तव में ब्रिटेन की लॉर्ड सभा इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है।
- आज विश्व के अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। यही कारण है कि ब्रिटेन में लॉर्ड सभा को बनाए रखने की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है।
- लॉर्ड सभा कॉमन सभा के द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है। ऐसा किए जाने के पीछे कारण यह है कि कॉमन सभा के पास काम अधिक रहता है और समय कम।
- लॉर्ड सभा की इस उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लॉर्ड सैलिसबरी का कथन है. “आज तक जब भी कोई विधेयक पिछले तीन वर्षों में इस सदन में विचारार्थ आया है, तो हमने सदैव ही उसको सुधारा है और उस पर पुनर्विचार किया है । "
- विवाद- लॉर्ड सभा में उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस सभा के लिए जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वे योग्य तथा विद्वान व्यक्ति होते हैं।
- लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को राजनीति में विशेष रुचि होती है। उनको जिस विषय पर बोलना होता है, वे उस विषय पर पूरी तैयारी करके बोलते हैं।
- इसी कारण वे अपने प्रामाणिक तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस सभा के सदस्य प्रशासक, राजदूत, व्यापारी, मन्त्री तथा किसी विशेष क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति होते हैं।
- इस तथ्य को फाइनर ने अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है, 'लॉर्ड सभा सार्वजनिक वाद-विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है। '
- भार को कम करना वर्तमान समय में कॉमन सभा का कार्य-भार अत्यधिक बढ़ गया है। इसी कारण अकेले कॉमन सभा के लिए समस्त कार्य करना सम्भव नहीं है।
- प्रतिवर्ष अनेक ऐसे विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं होता।
- कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जो लॉर्ड सभा में विरोधी दलों के लिए किसी प्रकार की चुनौती नहीं होते।
- लॉर्ड सभा में ऐसे विधेयकों को आसानी से पारित किया। जा सकता है।
- स्पष्ट है कि लॉर्ड सभा के कारण कॉमन सभा का बहुमूल्य समय बच जाता है।
- लॉर्ड सभा में जिन सदस्यों का चयन किया जाता है, वे ख्यातिप्राप्त राजनीतिज्ञ, व्यापारी, वकील, न्यायवेत्ता, समाजसेवी तथा धर्माधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी सेवाओं से देश को विशेष लाभ पहुँचाते हैं। यही कारण है कि लॉर्ड सभा को श्योग्यता का भण्डारश कहा जाता है।
- लॉर्ड सभा गम्भीर विषयों पर निष्पक्ष होकर विचार करती है। इसके फलस्वरूप जनमत प्रभावित होता है । ऐपड़े मैथिओट का कथन है, लॉर्ड सभा जनमत को निर्धारित करने में प्रभाव रखती है।
- लॉर्ड सभा ब्रिटिश रूढ़िवादी प्रवृत्ति की परिचायक है। ब्रिटिश जनता परम्परागत संस्थाओं के प्रति आस्था रखती है। इसी कारण वहाँ की जनता लॉर्ड सभा को बनाए रखने के पक्ष में है।
- लॉर्ड सभा के सदस्य किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होते हैं। चूँकि उन पर किसी दल का अंकुश नहीं रहता है, अतः वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट करते हैं।
- लॉर्ड सभा 'विलम्बकारी सदन' के रूप में विख्यात है। राजनीतिज्ञों का यह विश्वास है कि द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी विधेयक के पारित होने में विलम्ब कर सके। ऐसा इसलिए कि कोई सदन जल्दबाजी में कोई विधेयक पास न कर दे।
- सैलिसबरी का कथन है, 'लॉर्ड सभा द्वारा विलम्ब से विधेयक पारित करने में सदस्यों को किसी विधेयक पर ठण्डे दिल और मस्तिष्क से सोचने का समय मिल सकेगा।'
- 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अकसर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया।
- इस प्रक्रिया से जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। राष्ट्रवादी भावनाएँ मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थीं और 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था।
- राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फ़ौज की ताक़त ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों (Junkers) ने भी समर्थन किया।
- प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व सँभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री, ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली।
- सात वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीन युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई ।
- जनवरी 1871 में, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया।
- 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटोवॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्त्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल शीशमहल (हॉल ऑफ़ मिरर्स) में हुई।
- सभा ने प्रशा के काइज़र विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था।
- नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी ज़ोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए क़दम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अकसर एक मॉडल बना।
- 1870 ई. में सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट् नेपोलियन तृतीय की पराजय हुई। उसे प्रशा की सेना के समक्ष आत्म-समर्पण करना पड़ा।
- युद्ध के बाद 1871 ई. में फ्रांस व जर्मनी के मध्य फ्रैंकफर्ट की सन्धि हुई। सन्धि के अनुसार फ्रांस से अल्सास व लोरेन के प्रदेश छीन लिए गए।
- युद्ध के हर्जाने के रूप में 20 करोड़ पौण्ड की धनराशि के भुगतान का भार फ्रांस पर लाद दिया गया तथा इस धनराशि | का भुगतान न होने तक जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में तैनात कर दी गई, जिसका खर्च वहन करने का दायित्व फ्रांस को सौंपा गया।
- इस प्रकार फ्रैंकफर्ट की सन्धि की सभी शर्ते फ्रांस के लिए अपमानजनक थीं। यह सन्धि 1871 ई. के पश्चात् जर्मनी की विदेश नीति का आधार बनी।
1871 से 1890 ई. तक बिस्मार्क की विदेश नीति निम्नलिखित विचारों पर आधारित थी-
- जर्मनी का एकीकरण हो जाने के बाद बिस्मार्क यूरोप महाद्वीप में शान्ति चाहता था। अतः उसने सीमा विस्तार की नीति को छोड़कर घोषणा की कि जर्मनी एक सन्तुष्ट राष्ट्र है।
- बिस्मार्क महाद्वीपीय दृष्टिकोण का समर्थक था। वह जर्मनी को साम्राज्यवादी नीति से दूर रखना चाहता था । वह इंग्लैण्ड, ऑस्ट्रिया, रूस और इटली, इन प्रमुख राज्यों से घनिष्ठता स्थापित करना चाहता था, ताकि यूरोप में शान्ति स्थापित हो सके।
- बिस्मार्क को सबसे बड़ा खतरा फ्रांस से था। अतः वह फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्रहीन व एकाकी बनाना चाहता था । फ्रांस को आन्तरिक रूप से भी निर्बल बनाए रखा जाए, इस दृष्टि से भी फ्रांस में गणतन्त्रीय व्यवस्था का समर्थन किया जाए, ताकि इस व्यवस्था के अन्तर्गत फ्रांस अपने मतभेदों का शिकार बना रहे।
- बिस्मार्क की दृष्टि में रूस का सर्वाधिक महत्त्व था। उसने ' कहा था, 'रूस मेरी विदेश नीति की धुरी है।
- उस समय इंग्लैण्ड शानदार अलगाव की नीति का पालन कर रहा था। बिस्मार्क ने ऐसी विदेश नीति का पालन करना उचित समझा जिसका इंग्लैण्ड की विदेश नीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अतः उसने जर्मनी की जल सेना का विस्तार करने का विचार छोड़कर थल सेना का ही विस्तार किया। उसने कहा था, 'जर्मनी स्थल चूहा है, जबकि इंग्लैण्ड जल चूहा है। स्थल चूहा व जल चूहा में संघर्ष नहीं हो सकता।'
- पूर्वी समस्या में बिस्मार्क की कोई रुचि नहीं थी। वह इसे तनावपूर्ण समस्या मानता था। इसलिए वह कहता था- 'कुस्तुन तुनिया से आने वाली डाक को मैं कभी नहीं खोलता।'
बिस्मार्क की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित थे
- अपनी विजयों को सुरक्षित रखना,
- यूरोप महाद्वीप में शान्ति स्थापित करना;
- फ्रांस को मित्रहीन बनाना, तथा
- फ्रांस के विरुद्ध व जर्मनी के पक्ष में गुटबन्दी करना ।
- एक इतिहासकार ने लिखा है, 'बिस्मार्क यूरोप महाद्वीप में जर्मनी को सन्तुष्ट साम्राज्य बनाना चाहता था।
- उसकी विशेष इच्छा थी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन यूरोप की राजधानी का केन्द्र बने।'
उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर बिस्मार्क ने अपने बीस वर्ष के कार्यकाल में वैदेशिक क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए
- रूस व ऑस्ट्रिया की मित्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने इन राष्ट्रों को 1872 ई. में बर्लिन में आमन्त्रित किया। तीनों देशों के सम्राटों ने एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
- इसके आधार पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी व रूस के मध्य 1872 ई. में 'त्रिसम्राट् संघ' की स्थापना हुई। तीन राष्ट्रों के संघ के द्वारा यह निश्चय किया गया
- 1871 ई. की प्रादेशिक व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा।
- बाल्कन समस्या का तीनों के लिए मान्य हल निकाला जाएगा।
- अपने-अपने देश में क्रान्तिकारी भावनाओं का दमन किया जाएगा।
- तीन सम्राटों की यह मित्रता आगे चलकर और भी मजबूत हो गई।
- 1878 ई. की बर्लिन सन्धि के फलस्वरूप रूस व जर्मनी के सम्बन्ध खराब हो गए। अतः बिस्मार्क को रूस व फ्रांस की मित्रता के प्रति आशंका प्रतीत हुई।
- इस संकट को टालने तथा उसका मुकाबला करने के लिए बिस्मार्क ने 1879 ई. में ऑस्ट्रिया व जर्मनी के मध्य द्विराज्य सन्धि को सम्पन्न किया।
- सन्धि के फलस्वरूप रूस व फ्रांस के संयुक्त आक्रमण के विरुद्ध जर्मनी व ऑस्ट्रिया द्वारा मिलकर प्रतिरोध करने का निश्चय किया गया।
- बिस्मार्क यूरोप की राजनीति में जर्मनी की स्थिति को त्रिकोणात्मक बनाना चाहता था। त्रिसम्राट् संघ के भंग हो जाने के कारण बिस्मार्क की विदेश नीति का सन्तुलन बिगड़ गया था।
- वह हरसम्भव तरीके से जर्मनी के पक्ष में तीन राष्ट्रों की मित्रता को आवश्यक समझता था।
- 1882 ई. में उसने द्विराज्य सन्धि में इटली को सम्मिलित करके त्रिराज्य संघ की स्थापना की और जर्मनी की स्थिति को मजबूत कर लिया। इस त्रिगुट या त्रिराष्ट्र समझौते के अनुसार यह तय किया गया
- इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं करेगा।
- फ्रांस के आक्रमण से इटली की रक्षा की जाएगी।
- इटली भी अन्य देशों की ऐसे अवसर पर सहायता करेगा।
- यदि दोनों देशों पर कोई भी देश आक्रमण करेगा, तो तीनों देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।
- यह सन्धि भी गुप्त और रक्षात्मक थी और 5 वर्ष के लिए की गई थी।
- सर्वाधिक महत्त्व बिस्मार्क अपनी विदेश नीति में रूस देता था।
- 1878 ई. में रूस जर्मनी से नाराज हो गया था, फिर भी विस्मार्क रूस की मित्रता को जर्मनी के हित में आवश्यक समझता था।
- अतः उसने 1887 ई. में रूस के साथ गोपनीय ढंग से पुनराश्वासन सन्धि की, जिसकी शर्त गुप्त रखी गई। इन शर्तों। का नवीनीकरण प्रति तीन वर्ष बाद होना था।
- बिस्मार्क ने अपने बीस वर्ष के कार्यकाल में जर्मनी की सुरक्षा व यूरोपीय शान्ति के लिए गुटबन्दी का सहारा लिया। उसकी विदेश नीति मुख्य रूप से रूस के क्रियाकलापों तथा फ्रांस की मित्रहीनता पर आधारित थी।
- अपनी कूटनीतिक योग्यता के द्वारा बिस्मार्क ने रूस व ऑस्ट्रिया तथा इटली व ऑस्ट्रिया जैसे प्रतिद्वन्द्वी देशों को जर्मनी का मित्र बनाने में सफलता प्राप्त की।
- ऑस्ट्रिया के आक्रमण के विरुद्ध रूस की तटस्थता, रूस के आक्रमण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की तटस्थता, फ्रांस के आक्रमण के विरुद्ध इटली की सहायता तथा रूस व फ्रांस के संयुक्त आक्रमण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया व इटली की सहायता के रूप में बिस्मार्क ने ऐसा कूटनीतिक जाल बिछाया, जिसे बिस्मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ सका। इन्हीं विशेषताओं के कारण बिस्मार्क को 'पाँच गेंदों से खेलने वाले कुशल बाजीगर' की संज्ञा दी गई हैं।
- जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहु-राष्ट्रीय 'हैव्सवर्ग साम्राज्य' में बिखरा हुआ था।
- 19वीं सदी के मध्य में इटली सात राज्यों में बँटा हुआ था जिनमें से केवल एक सार्डिनिया-पीडमॉण्ट में एक इतालवी राजघराने का शासन था।
- उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैव्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोष का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूब राजाओं के अधीन थे।
- 1830 के दशक में ज्युसेपे मेत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी।
- ज्युसेपे मेत्सिनी ने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए 'यंग इटली' नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था।
- 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के ज़रिये इतालवी राज्यों को जोड़ने की ज़िम्मेदारी सार्डिनिया-पीडमॉण्ट के शासक विक्टर इमेनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएँ उत्पन्न करता था।
- कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला।
- इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया-पीडमॉण्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से सार्डिनिया-पीडमॉण्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ।
- नियमित सैनिकों के अलावा ज्युसेपे गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया।
- 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे।
- 1861 में इमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। मगर, इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊँची थी, अभी भी उदारवादी - राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे।
- दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबॉल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया (Italia) के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया (La Talia) विक्टर इमेनुएल की पत्नी थी।
- इटली की स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीय एकीकरण के पावन यज्ञ में असंख्य देशभक्तों ने अपने अमूल्य जीवन की आहुति दी थी।
- इटालियन देशभक्तों में चार महान् विभूतियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनके महत्त्व का दिग्दर्शन इस वाक्य में भलीभाँति हो जाता है, ‘मेजिनी ने इटली की आत्मा, कैवूर ने मस्तिष्क, गैरीबाल्डी तथा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने शरीर बनकर अपनी मातृभूमि इटली की पराधीनता की जंजीरें काट डाली और देश के एकीकरण के कार्य को सम्पूर्ण किया। '
- इटली के एकीकरण का कार्य अनेक प्रयासों के माध्यम से पूरा हुआ था। इटली के राष्ट्रवादियों ने स्थान-स्थान पर 'कार्बोनरी ' नामक गुप्त समितियाँ स्थापित की थीं।
- समितियों की बैठक रात में होती थी। देश के सभी मुख्य नेता इन समितियों के सदस्य बन गए थे।
- कार्बोनरी का मुख्य उद्देश्य विदेशियों को इटली से बाहर निकालना तथा वैधानिक स्वतन्त्रता की स्थापना करना था। इटली के एकीकरण के इतिहास में किए गए प्रारम्भिक प्रयासों में कार्बोनरी का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था।
- जिस समय कार्बोनरी समितियाँ राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में प्रयासरत थीं, उसी समय इटली की राजनीति में मेजिनी नामक देशभक्त का उदय हुआ, जिसने इटली के एकीकरण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया।
- वह कार्बोनरी का सदस्य रह चुका था। 1830 ई. में उसने इटली के राज्यों में होने वाली क्रान्तियों का नेतृत्व किया। उसने इटली की जनता को सन्देश दिया तथा राष्ट्रीय जीवन में चेतना जाग्रत की।
- 1830 ई. तक की असफलताओं से मेजिनी ने दो निष्कर्ष निकाले
- इटली का सबसे प्रबल शत्रु ऑस्ट्रिया है।
- एकीकरण को पूरा करने के लिए कार्बोनरी अपर्याप्त है।
- इस आधार पर मेजिनी ने 'युवा इटली' नामक दल का गठन किया। इसकी सहायता से उसने देश में जन-जागरण का कार्य प्रारम्भ किया और इटली की जनता को समझाया कि बनावटी राजनीतिक सीमाओं के द्वारा हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए हैं, किन्तु इटली एक राष्ट्र है और उसमें एकता है। उस एकता को जीवित रखना इटली के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
- मेजिनी का कथन था, जब तक कार्य और उद्देश्य अलग-अलग हैं, तब तक सफलता अनिश्चित है।'
- 1848 ई. की प्रसिद्ध क्रान्ति से सम्पूर्ण यूरोप महाद्वीप प्रभावित हुआ था। मैटरनिख के पतन का समाचार सुनकर मार्च, 1848 में इटलीवासियों ने मेजिनी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी।
- मेजिनी ने पोप की राजधानी रोम में गणतन्त्र की घोषणा कर दी, किन्तु फ्रांस के राष्ट्रपति लुई नेपोलियन ने सेना भेजकर पोप की सहायता की।
- मेजिनी पराजित हो गया और पोप को पुनः सत्तारूढ़ कर दिया गया। मेजिनी पराजित होकर स्विट्जरलैण्ड भाग गया।
इटली के राज्य पीडमॉण्ट के शासक विक्टर इमैनुअल काण्ट की यह इच्छा थी कि इटली का एकीकरण पीडमॉण्ट के नेतृत्व में पूरा होना चाहिए। उसके प्रधानमन्त्री कावूर का भी यही विचार था।
कावूर राजतन्त्र का समर्थक, कूटनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी नेता था । इटली के एकीकरण की दिशा में उसने निम्नलिखित कार्य किए थे
- सर्वप्रथम कैवूर का ध्यान इटली की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए आकर्षित हुआ। क्रीमिया के युद्ध में उसे यह अवसर प्राप्त हो गया। क्रीमिया का युद्ध टर्की की समस्या और चर्च के प्रश्न से सम्बन्धित था । इटली न तो रूस का शत्रु था और न ही इंग्लैण्ड व फ्रांस का । फिर भी कैवूर ने इस युद्ध में इंग्लैण्ड, फ्रांस व टर्की के समर्थन में अपनी सेना भेजकर महान् दूरदर्शिता का परिचय दिया। इससे कैवर को इटली की समस्या के प्रति इंग्लैण्ड व फ्रांस जैसे बड़े देशों की सहानुभूति प्राप्त हो गई। यही कैवूर का उद्देश्य था।
- कावूर ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 31 जुलाई, 1858 को फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ एक समझौता किया, जिसमें नेपोलियन तृतीय ने इटली को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैनिक सहयोग का वचन दिया । कैवूर की यह महान् सफलता थी।
- सन् 1858 में ऑस्ट्रिया व पीडमॉण्ट के मध्य युद्ध प्रारम्भ हुआ। नेपोलियन तृतीय ने अपनी सेना को पीडमॉण्ट की सहायता के लिए भेज दिया। युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और लोम्बार्डी का प्रदेश ऑस्ट्रिया से छीन लिया गया।
- मध्य इटली के परमा, मोडिना, टुस्कने राज्यों की जनता ने पीडमॉण्ट के साथ रहने की इच्छा प्रकट की । कैवूर के प्रयासों | के फलस्वरूप मार्च, 1860 में इन प्रदेशों में जनमत कराया गया। बहुमत के आधार पर राज्यों का एकीकरण करके उत्तर- मध्य इटली का निर्माण किया गया।
- दुर्भाग्यवश 6 जून, 1861 को कैवूर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय वेनेशिया और रोम को छोड़कर शेष सम्पूर्ण इटली का एकीकरण हो चुका था। मरते समय कैवूर ने कहा था, 'अब सब सुरक्षित है, इटली का निर्माण हो चुका है। '
- इटली, सिसली व नेपल्स राज्यों की जनता ने भी विद्रोह कर दिया। गैरीबाल्डी नामक नाविक योद्धा ने अपनी लालकुर्ती सेना के साथ वहाँ की जनता का पूरा सहयोग किया। फलस्वरूप उक्त दोनों राज्यों को भी इटली में मिला दिया गया।
- इटली का पूर्ण एकीकरण- इस समय बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का अभियान चल रहा था। 1866 ई. में सेडोवा के युद्ध में प्रशा तथा पीडमॉण्ट की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और वेनेशिया का प्रदेश पीडमॉण्ट को प्राप्त हो गया।
- 1870 ई. में फ्रांस व प्रशा का युद्ध प्रारम्भ हो गया। अवसर का लाभ उठाकर इटली की सेनाओं ने रोम पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही इटली का एकीकरण पूरा हो गया।
- रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। 1856 ई. में कावूर ने कहा था 'मुझे विश्वास है कि एक दिन इटली स्वतन्त्र राष्ट्र बनेगा और रोम उसकी राजधानी । '
- इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य निम्नलिखित चार चरणों में पूरा हो सका था। इनका विवरण निम्न प्रकार है
- मई, 1858 में कैवूर ने प्लोम्बियर्स समझौते के द्वारा फ्रांस के सम्राट् नेपोलियन तृतीय को नीस एवं सेवॉय के प्रदेश देने का आश्वासन प्रदान करके उससे लाखों फ्रांसीसी सैनिकों की सहायता प्राप्त की।
- इसके उपरान्त ऑस्ट्रिया के साथ पीडमॉण्ट के शासक विक्टर इमैनुअल का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी सैनिक सहायता के बल पर उसको ऑस्ट्रियन सेना को दो युद्धों में पराजित करने का अवसर प्राप्त हुआ।
- इस प्रकार लोम्बार्डी के प्रान्त से ऑस्ट्रिया का अधिकार जाता रहा और वह पीडमॉण्ट संघ में सम्मिलित कर लिया गया। लोम्बार्डी पर अधिकार किया जाना इटली के एकीकरण की प्रथम सीढ़ी थी ।
- मध्य इटली के छोटे-छोटे प्रान्तों पर्मा, मोडेना, टस्कनी तथा पोप के राज्य के रामागना एवं बोलोगना आदि प्रान्तों की जनता ने देशभक्ति एवं स्वतन्त्रता की भावनाओं के प्रवाह में बहकर अपने यहाँ के निरंकुश शासकों के अत्याचारपूर्ण शासन का अन्त कर दिया और पीडमॉण्ट संघ में सम्मिलित होने के लिए पीडमॉण्ट के शासक से निवेदन किया।
- ऑस्ट्रिया ने इसका भारी विरोध किया। परन्तु कैवूर की राजनीतिक पटुता के कारण नेपोलियन तृतीय की इस सम्बन्ध में सहमति प्राप्त कर ली गई ।
- जनता के मतदान से ज्ञात हुआ कि बहुमत उन राज्यों को पीडमॉण्ट संघ में मिलाए जाने का पक्षपाती है। अतः उत्तरी इटली के उन छोटे-छोटे राज्यों को भी पीडमॉण्ट संघ का सदस्य बना लिया गया। इस प्रकार इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का द्वितीय चरण पूर्ण हुआ।
- 1860 ई. में सिसली की जनता ने नेपल्स के निरंकुश शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
- प्रसिद्ध देशभक्त गैरीबाल्डी अपने लालकुर्ती दल के लगभग सहस्त्र सैनिकों सहित जन-आन्दोलन की सहायतार्थ सिसली पहुँच गया। उसने नेपल्स के राजा को दो युद्धों में बुरी तरह पराजित करके सिसली पर अधिकार कर लिया।
- इसके उपरान्त उसने नेपल्स के राज्य पर आक्रमण कर दिया।
- राजा बिना युद्ध किए ही नेपल्स छोड़कर गेटा (Gaeta ) भाग गया। इस प्रकार सिसली और नेपल्स का विशाल राज्य गैरीबाल्डी के अधीन हो गया।
- 1866 ई. में प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें प्रशा को अपूर्व विजय प्राप्त हुई। इस विजय का प्रमुख कारण प्रशा के चांसलर बिस्मार्क के संकेत पर विक्टर इमैनुअल द्वितीय द्वारा वेनेशिया और टायरील पर किया आक्रमण था।
- इस आक्रमण के कारण ऑस्ट्रिया प्रशा के विरुद्ध युद्ध में अपना सम्पूर्ण सैन्य दल नहीं उतार सका। अतः उनकी सैनिक शक्ति प्रशा के समक्ष कमजोर पड़ गई और उसे पराजित होना पड़ा।
- अन्त में सन्धि की गई, जिसमें बिस्मार्क ने अपने वचन का पालन करते हुए ऑस्ट्रिया के अधीन वेनेशिया प्रदेश को पीडमॉण्ट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को अर्पित करने के लिए विवश किया।
- 1870 ई. में फ्रांस का प्रशा के साथ युद्ध छिड़ गया। अतः नेपोलियन तृतीय को रोम से फ्रांसीसी सेना वापस बुलानी पड़ी। इस प्रकार रोम की सुरक्षा जाती रही ।
- नेपोलियन का पतन होते ही विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने अपनी सेना भेजकर रोम पर अधिकार जमा लिया।
- इस प्रकार इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ और संगठित इटली राष्ट्र की राजधानी रोम को बनाया गया।
- यही इटली के राष्ट्रीय एकीकरण की अन्तिम सीढ़ी थी, जिसे पार करके इटली ने यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना की। मेजिनी ने लिखा भी था, 'इटली एक राष्ट्र होना चाहता है और कुछ भी हो, वह एक राष्ट्र अवश्य बन जाएगा।'
- यूनान के स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात् बाल्कन प्रायद्वीप में रूस का प्रभाव बढ़ गया, किन्तु रूस अपनी स्थिति से पूर्ण सन्तुष्ट नहीं था।
- रूस का जार निकोलस अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी था। उसकी प्रबल इच्छाओं ने पूर्वी समस्या के क्षेत्र में एक नये युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसे क्रीमिया का युद्ध कहते हैं।
1. फ्रांस का दृष्टिकोण
- फ्रांस का सम्राट् नेपोलियन तृतीय विदेशों में फ्रांस की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था । वह टर्की के मामलों में गहरी रुचि लेता था। उसके तथा रूस के जार के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे।
- इसके अलावा नेपोलियन तृतीय अपने देश की रोमन कैथोलिक जनता को खुश रखने के लिए सैनिक विजय प्राप्त करना चाहता था।
- इतिहासकार हेज ने लिखा है, 'रूस व फ्रांस की पुरानी शत्रुता का बदला लेने, नेपोलियन बोनापार्ट की मॉस्को पराजय का हिसाब चुकाने, वाटरलू की पराजय एवं वियना सन्धि का बदला लेने के लिए नेपोलियन तृतीय ने क्रोमियाँ युद्ध में भाग लिया था। '
- रूस आरम्भ से ही टर्की साम्राज्य का विघटन चाहता था । वह टर्की की आन्तरिक दुर्बलता का लाभ उठाकर उस पर अधि कार करना चाहता था।
- 1853 ई. में रूस के जार ने कहा था, 'हमारे सामने एक अत्यन्त बीमार आदमी है। उसकी मौत से पूर्व यदि हमने उसकी सम्पत्ति का बँटवारा नहीं किया, तो यह हमारा महान् दुर्भाग्य होगा।'
- वास्तव में रूस अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करने हेतु भूमध्य सागर तथा काला सागर पर अधिकार करना चाहता था।
- इंग्लैण्ड टर्की साम्राज्य के विघटन के पक्ष में नहीं था, क्योंकि भूमध्य सागर पर रूस का अधिकार हो जाने से इंग्लैण्ड के पूर्वी साम्राज्य को खतरा हो सकता था।
- इंग्लैण्ड की इच्छा थी कि पूर्वी समस्या का सम्बन्ध यूरोप के बड़े देशों से होने के कारण उसका समाधान भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए।
- टर्की साम्राज्य के अन्तर्गत जेरूसलम नामक स्थान ईसाइयों का पवित्र तीर्थस्थल था। वहाँ पर यूनानी व रोमन कैथोलिक, दोनों प्रकार के पादरी रहते थे। इनकी आपसी कटुता का लाभ रूस व फ्रांस ने उठाया।
- ये दोनों देश अपनी सैनिक महत्त्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते थे। जेरूसलम की समस्याओं का लाभ दोनों देशों ने एक-दूसरे के विरुद्ध उठाया।
- रूस ने विपत्ति के दिनों में टर्की की सहायता की थी। फलस्वरूप रूस के प्रस्ताव पर 1833 ई. में उनकियर स्केलेसी (Unkier Skellessi) की सन्धि पर टर्की ने हस्ताक्षर कर दिए और वह रूस के प्रभाव में आ गया। इससे इंग्लैण्ड को चिन्ता हुई।
- पामर्स्टन ने इस सन्धि को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने पूर्वी समस्या पर व्यापक समझौता करने के लिए 1840 ई. में यूरोपीय राज्यों का लन्दन में एक सम्मेलन बुलाया।
- इस सम्मेलन में बड़े राष्ट्रों द्वारा सन्धि पर हस्ताक्षर करने से टर्की साम्राज्य पर रूस का प्रभाव कम हो गया। सभी शक्तियों ने स्वीकार किया कि टर्की का अस्तित्व रहना चाहिए।
- इसके पश्चात् लगभग 10 वर्षों तक पूर्वी समस्या शान्त रही। इसी दौरान फ्रांस में लुई नेपोलियन का शासन आया, जिसने जेरूसलम के ईसाई पादरियों का पक्ष लेकर पूर्वी समस्या को उभारा। क्रीमिया युद्ध इसी का परिणाम था।
- क्रीमिया युद्ध 2 वर्षों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों की अपार जन-धन की हानि हुई।
- रूस अकेले फ्रांस; इंग्लैण्ड, टर्की और सार्जीनिया की सामूहिक शक्ति का सामना नहीं कर सकता था।
- उल्लेखनीय है कि पीडमॉण्ट- सार्डिनिया इटली का राज्य था, जिसके प्रधानमन्त्री कैवूर ने फ्रांस का साथ देने और उसकी सहानुभूति लेने के लिए रूस के विरुद्ध 15 हजार सैनिक भेजे थे। प्रशा इस युद्ध में तटस्थ रहा। ऑस्ट्रिया ने भी अपनी • तटस्थता की घोषणा की थी, परन्तु युद्ध के दौरान उसने रूस को धमकाया भी था।
- मार्च, 1855 में रूस के जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर अलेक्जेण्डर द्वितीय जार बना। इस नये सम्राट ने युद्ध को समाप्त करना ठीक समझा।
- ऑस्ट्रिया की मध्यस्थता से युद्ध समाप्त हो गया और सन्धि के लिए पेरिस में तैयारी होने लगी ।
क्रीमिय युद्ध का अन्त पेरिस की सन्धि से हुआ।
30 मार्च, 1856 को पेरिस की सन्धि हुई, जिसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार थीं
- टर्की की प्रादेशिक अखण्डता और राजनीतिक स्वतन्त्रता बनाए रखी जाए।
- टर्की का सुल्तान ईसाई प्रजा की स्थिति को सुधारेगा।
- रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया।
- मोल्डेविया और बेलेशिया पर से रूस का संरक्षण समाप्त हो गया।
- कार्स का प्रदेश टर्की को और क्रीमिया रूस को वापस मिल गया।
- सर्बिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया।
- डेन्यूब नदी व्यापार के लिए यूरोपीय राष्ट्रों के लिए खुल गई ।
- काला सागर को तटस्थ घोषित कर दिया गया।
- यूरोपीय इतिहास के दृष्टिकोण से वियना कांग्रेस के बाद क्रीमिया युद्ध एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध से रूस का प्रसार रुक गया और टर्की में एक नये जीवन का संचार हुआ।
- इस प्रकार यूरोपीय राज्यों ने पूर्वी समस्या को अकेले ही सुलझाने के रूसी दावे को ठुकरा दिया।
- रूस को कमजोर बना दिया गया और उसे अपमानित भी किया गया। यद्यपि रूस चुप नहीं बैठा और 14 वर्ष बाद उसने अपने अपमान का बदला लिया।
- युद्ध का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से इटली पर पड़ा तथा उसे फ्रांस का सहयोग प्राप्त हो गया।
- क्रीमिया युद्ध सामान्य अर्थ में यूरोपीय इतिहास का एक युगान्तकारी युद्ध था।
- क्रीमिया युद्ध के परोक्ष परिणाम बहुत ही दूरगामी और व्यापक निकले। इटली व जर्मनी के एकीकरण, रूस की राजनीति, बाल्कन प्रायद्वीप के पुनर्निर्माण और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा।
- 1852 ई. में कैवूर पीडमॉण्ट राज्य का प्रधानमन्त्री था। जब क्रीमिया युद्ध हुआ, तो उसने पीडमॉण्ट को इसमें सम्मिलित करने का निश्चय किया।
- युद्ध में वह इसलिए सम्मिलित हुआ था कि दिखा सके कि इटली के लोग व उसकी शक्ति किसी से कम नहीं और उसे भी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।
- क्रीमिया युद्ध में सम्मिलित होने से पीडमॉण्ट की प्रतिष्ठा बढ़ गई और युद्ध में शामिल राष्ट्र उसके ऋणी हो गए। इन राष्ट्रों की इटली के प्रति सहानुभूति जाग्रत हुई और वे इटली के एकीकरण के लिए प्रयत्नशील हुए।
- उल्लेखनीय है कि पेरिस के शान्ति सम्मेलन में कैवूर ही इटली का प्रतिनिधि बनकर आया था और वह ऑस्ट्रिया के साथ समानता के स्तर पर सम्मेलन में बैठा।
- इस सम्मेलन में कैवूर ने इटली की दुर्दशा का चित्रण प्रभावशाली ढंग से किया और ऑस्ट्रिया की नीति का विरोध किया।
- इसके फलस्वरूप कावूर को इंग्लैण्ड की सहानुभूति और नेपोलियन का सक्रिय समर्थन मिला, जिसके कारण इटली के एकीकरण को बल मिला। इन्हीं कारणो से कहा गया है कि ‘क्रीमिया की कीचड़ से नवीन इटली का जन्म हुआ।'
- इस युद्ध ने इटली के एकीकरण हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया। कैवूर ने इस युद्ध में अपनी सेना भेजकर बड़े देशों की सहानुभूति प्राप्त की।
- क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय के फलस्वरूप वहाँ की जनता जार के निरंकुश व एकतन्त्रात्मक शासन की कमजोरियों पर विचार करने लगी ।
- इस युद्ध की पराजय से निराश होकर रूस बाल्कन प्रायद्वीप से अपना ध्यान हटाकर चीन, जापान व पूर्वी एशिया में लगाने लगा।
- क्रीमिया युद्ध के महत्त्व के सम्बन्ध में डेविस थॉम्पसन ने लिखा है, 'युद्ध में पहली बार इंग्लैण्ड व फ्रांस साथ-साथ लड़े थे। इस युद्ध में स्त्रियों ने पहली बार फ्लोरेंस नाइटेंगिल के नेतृत्व में भाग लिया था तथा पहली बार विज्ञान के नये आविष्कारों का प्रयोग हुआ था। '
- अनेक विद्वानों ने क्रीमिया युद्ध की आलोचना करते हुए इसे 'बेकार का युद्ध' बताया है। उनका विचार है कि इस युद्ध में अपार जन-धन एवं समय का विनाश होने पर भी पूर्वी समस्या का स्थायी हल नहीं निकाला जा सका।
- पेरिस की सन्धि की धाराएँ स्थायी सिद्ध न हो सकी। इस युद्ध का उद्देश्य रूस की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना था, किन्तु इस उद्देश्य में भी सफलता न मिल सकी।
- रूस द्वारा पेरिस की सन्धि में हुए अपने अपमान को भुलाया नहीं जा सका। मित्र राष्ट्रों के लिए भी इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी सिद्ध हुए।
- क्रीमिया युद्ध ने यथास्थिति की जड़े शान्ति को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर रचनात्मक युद्धों के युग का प्रारम्भ किया। इस प्रकार शान्ति से युद्ध के क्षेत्र में तथा मध्ययुगीन से आधुनिक व्यवस्था में अवतरण का समय यदि किसी घटना द्वारा निर्धारित करना हो, तो यह घटना निःसन्देह रूप से क्रीमिया युद्ध ही है ।
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







