BPSC TRE 2.0 SOCIAL SCIENCE CLASS 10TH HISTORY NOTES | इंडो-चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन
वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में यानी भारत से भी पहले आज़ादी मिल गई थी लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहाँ के लोगों को तीस साल और संघर्ष करना पड़ा।
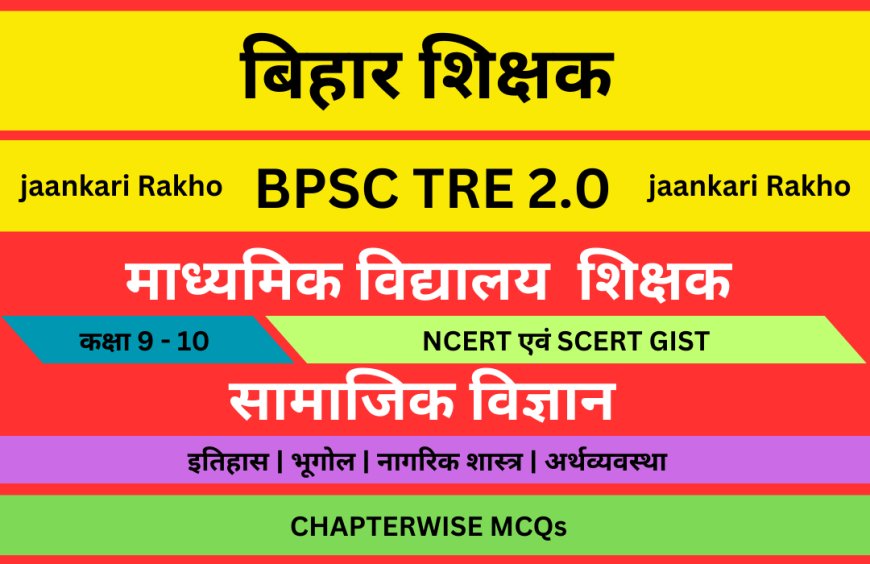
BPSC TRE 2.0 SOCIAL SCIENCE CLASS 10TH HISTORY NOTES | इंडो-चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन
- वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में यानी भारत से भी पहले आज़ादी मिल गई थी लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहाँ के लोगों को तीस साल और संघर्ष करना पड़ा।
- वियतनाम में राष्ट्रवाद का उदय उस प्रकार नहीं हुआ था जिस तरह यूरोप में हुआ था।
- वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। वियतनाम के विभिन्न समुदायों को मिला कर आधुनिक वियतनामी राष्ट्र की स्थापना में आशिक रूप से उपनिवेशवाद का योगदान रहा तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस राष्ट्र का रूप-स्वरूप औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ़ चले संघर्षों से ही तय हुआ था।

- पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों को ज्यादा बराबरी वाला दर्जा मिलता था, खासतौर से निचले तबके में। फिर भी औरतों की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर तो थी ही। वे अपने भविष्य के बारे में अहम फैसले नहीं ले सकती थीं। न ही सार्वजनिक जीवन में उनका कोई खास दखल होता था।
- वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन ज़ोर पकड़ने लगा समाज में महिलाओं की हैसियत व स्थिति पर भी सवाल उठने लगे और स्त्रीत्व की एक नयी छवि सामने आने लगी।
- साहित्यकार और राजनीतिक विचारक विद्रोहों में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करने लगे।
- 1913 में राष्ट्रवादी नेता फान बोई चाऊ ने 39-43 ईस्वी में चीनी कब्ज़े के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाली ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक लिखा। इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि इन बहनों ने वियतनामी राष्ट्र को चीनियों से मुक्त कराने लिए देशभक्ति के भाव से कैसे-कैसे कारनामे किए थे।
- वियतनामियों की अपराजेय इच्छाशक्ति और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पेंटिंग्स, नाटकों और उपन्यासों में उनका महिमामंडन होने लगा।
- ट्रंग बहनों ने 30,000 सैनिकों की फ़ौज जुटा ली थी, उन्होंने चीनियों का दो साल तक मुक़ाबला किया और अंत में जब उन्हें अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुदकुशी कर ली।
- अतीत की अन्य विद्रोहिणियाँ भी व्यापक राष्ट्रवादी आख्यान का हिस्सा थीं। इनमें त्रियू अयू सबसे महत्त्वपूर्ण और सम्मानित रही हैं।
- बड़ी होने पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों में चली गई। वहाँ रहकर उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी।
- इस संघर्ष के अंत में जब उनकी सेना हार गई तो उन्होंने पानी में डूब कर अपनी जान दे दी थी। वियतनामियों के लिए वह देश के मान की रक्षा करते हुए जान देने वाली शहीद ही नहीं बल्कि एक देवी बन गई थीं।
- न्यूयेन थी शुआन नामक महिला के बारे में बताया जाता था कि उसके पास केवल 20 गोलियाँ थीं लेकिन इन्हीं के सहारे उसने एक जेट विमान को मार गिराया था।
- औरतों को सिर्फ योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया जा रहा था।
- जब साठ के दशक में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने लगे तो औरतों से भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में सेना में भर्ती होने का आह्वान किया गया।
- बहुत सारी औरतों ने इस आह्वान को गंभीरता से लिया और वे प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गईं। वे घायलों की मरहम-पट्टी करने, भूमिगत कमरे व सुरंगें बनाने और दुश्मन से मोर्चा लेने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने लगीं।
- 1965 से 1975 के बीच हो ची चिन्ह मार्ग पर काम करने वाले युवाओं में से 70-80 प्रतिशत लड़कियाँ थीं। एक सैनिक इतिहासकार का कहना है कि वियतनाम की सेना मिलीशिया (नागरिक सेना), स्थानीय दस्तों और पेशेवर टोलियों में 15 लाख औरतें काम करती थीं।
- 70 के दशक तक आते-आते शांति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। युद्ध समाप्त होने के आसार दिखाई देने लगे थे। इसके बाद औरतों को योद्धाओं के रूप में पेश करने का चलन खत्म होने लगा। अब औरतों को मजदूरों के रूप में ही ज्यादा पेश किया जाने लगा। उन्हें सैनिकों के रूप में नहीं बल्कि कृषि कोऑपरेटिवों, कारखानों और उत्पादन इकाइयों में काम करते हुए दर्शाया जाने लगा।
- अमेरिका न तो वियतनामियों के प्रतिरोध को कुचल पाया था और न ही अमेरिकी कार्रवाई के लिए वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया। इस दौरान हज़ारों नौजवान अमेरिकी सिपाही अपनी जान गँवा चुके थे और असंख्य वियतनामी नागरिक मारे जा चुके थे।
- इस युद्ध को पहला टेलीविज़न युद्ध कहा जाता है। युद्ध के दृश्य हर रोज़ समाचार कार्याक्रमों में टेलीविज़न के पर्दे पर प्रसारित किए जाते थे।
- अमेरिकी कुकृत्यों को देखकर बहुत सारे लोगों का अमेरिका से मोहभंग हो चुका था। मैरी मैक्कार्थी जैसे लेखक या जेन फोंडा जैसे कलाकारों ने तो उत्तरी वियतनाम का दौरा भी किया और अपने देश की रक्षा के लिए वियतनामियों द्वारा दिए गए बलिदानों की प्रशंसा की।
- राजनीतिक सिद्धांतकार नोम चॉम्स्की ने इस युद्ध को 'शांति के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारी खतरा' बताया।
- सरकारी नीति के ख़िलाफ़ व्यापक प्रतिक्रियाओं ने युद्ध खत्म करने के प्रयासों को और बल प्रदान किया। जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- इस समझौते से अमेरिका के साथ चला आ रहा टकराव तो खत्म हो गया लेकिन साइगॉन शासन और एनएलएफ के बीच टकराव जारी रहा।
- आखिरकार 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिला कर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई।
- हिन्द-चीन दक्षिण-पूर्व एशिया में फैला एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग कि.मी. है, जिसमें आज का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं।
- वियतनाम के तोंकिन एवं अन्नाम कई शताब्दीयों तक चीन के कब्जे में रहा तथा दूसरी तरफ लाओस-कम्बोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था।
- चौथी शताब्दी में कम्बुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केन्द्र था। 12वीं शताब्दी में राजा सुर्यवर्मा द्वितीय (II) ने अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया था।
- हिन्द- चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पूर्तगाली थे। उसके बाद डच, इंगलैंड तथा फ्रांस आया।
- 20वीं शताब्दी तक सम्पूर्ण हिन्द-चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया।
- फ्रांस द्वारा हिन्द - चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था।
- एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। हिन्द - चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था।
- 1930 ई. में फान-बोई-चाऊ ने 'दुई-तान होई' नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसके नेता कुआंग दे थे।
- फान-बोई-चाऊ ने 'द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम' लिखकर हलचल पैदा कर दी।
- सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन के साथ हीं हिन्द-चीन के छात्रों ने प्रेरित होकर वियेतनाम कुवान फुक होई (वियतनाम मुक्ति एशोसिएशन) की स्थापना की।
- 1914 ई. में वियतनामी देशभक्तों ने 'वियतनामी राष्ट्रवादी दल' नामक संगठन बनाया, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला।
- 1917 में 'न्यूगन आई क्वोक' (हो- ची मिन्ह ) नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस मे ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया।
- हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गए और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में 'वियतनामी क्रांतिकारी दल' की गठन किया।
- 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया।
- दक्षिणी वियतनाम में एक गाँव था, जहाँ के लोगों को वियतनामी समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरूषों को मार दिया, औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मार कर पूरे गांव में आग लगा दिया।
- लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिन्दा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया।
- जून 1940 ई० में फ्रांस, जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गयी। उसके बाद जापान ने पूरे हिन्द - चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया।
- हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने 'वियतमिन्ह' (वियतनाम स्वतंत्रता लीग) की स्थापना कर पीड़ित किसानों, बुद्धिजीवियों, आतंकित व्यापारियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन (अपनाना) किया।
- 1944 में फ्रांस, जर्मनी के अधिपत्य से निकल गया तथा जापान पर परमाणु हमला के पश्चात् जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियतमिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना 2 सितम्बर 1945 ई. को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, इस सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह को बनाया गया।
- जापानी सेनाओ के हटते हीं, फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुँची वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रही।
- अंतत: 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना।
- फ्रांस ने कोचीन-चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया जिससे हनोई समझौता टूट गया।
- अब तक हो ची मिन्ह की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके। अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया।
- इसी क्रम में गुरिल्ला सैनिकों ने दिएन - विएन-फु पर भयंकर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। इस तरह दिएन - विएन-फु पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया।
- अमेरिका ने हिन्द - चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनायी। 1954 में हिन्द-चीन समस्या पर एक वार्ता बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है।
- जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बाँट दिया। हनोई नदी से सटे उत्तर के क्षेत्र उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह को और उससे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया।
- जेनेवा समझौता के तहत लाओस और कम्बोडिया को वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया।
- होआ-होआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, , जिसके नेता हुईन्ह फु-सो था । क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था।
- 25 दिसम्बर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन्न फूमा के नेतृत्व में सरकार बनीं।
- लाओस में तीन भाईयों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चालू हो गया तथा भयंकर गृह युद्ध शुरू हो गया।
- मई 1961 में इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमण्डल के गठन पर सहमति प्रदान की और मंत्रिमण्डल भी बना, परन्तु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गयी और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया।
- अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुवन्न फुमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुफन्न बोंग उप प्रधानमंत्री बना। इससे असंतुष्ट पाथेट लाओ ने सन् 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया।
- 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया उनके साथ अमेरिकी सैनिक भी थे। इनका उद्देश्य हो - ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था।
- लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना हीं एक मात्र विकल्प था। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथ के प्रसार को रोक नहीं पाया।
- सन् 1954 ई० में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कम्बोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक को शासक माना गया।
- मई 1965 में अमेरिका ने वियतनाम के साथ कम्बोडिया के . सीमावर्ती गांवो पर आक्रमण कर दिया।
- आगे चलकर सन् 1969 में अमेरिका ने कम्बोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40 हजार एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट हो गयी।
- सिहानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक सम्बंध बढ़ाने शुरू किये।
- तत्कालीन दो गुटिय विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कम्बोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखें।
- अमेरिकी षड्यंत्र के कारण नरोत्तम सिंहानुक को पद से हटा दिया गया तथा अमेरिका समर्थित जेनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बना।
- अप्रैल 1970 से सिंहानुक ने नयी सरकार के विरूद्ध युद्ध छेड़ दिया। नरोत्तम सिंहानुक की सेना विजयी होते हुए राजधानी नामपेन्ह की ओर बढ़ रही थी।
- अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कम्बोडिया में प्रवेश कर गयी और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया।
- कम्बोडियायी छापामारों, अमेरिकी सेना के बीच युद्धों, बमबारी नृशंश हत्याओं के इस दौर में 9 अक्टूबर, 1970 को कम्बोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। परन्तु सिंहानुक एव लोन नोल की सेनाओं में संघर्ष चलता रहा।
- पांच वर्ष बाद सिंहानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना विजयी होते हुए आगे बढ़ती गयी। अंततः लोन नोल को भागना पड़ा।
- अप्रैल 1975 में कम्बोडियायी गृह युद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सिंहानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने परन्तु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब कम्बोडिया का नाम बदल कर कम्पुचिया कर दिया गया।
- यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियाँ झुलस जाती थी तथा पेड़ मर जाते थे। इसका इस्तेमाल जंगलों को खत्म करने के लिए किया जाता था।
- जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम में बाँट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित हो ची मिन्ह और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित बाओदायी की सरकार थी।
- 1960 में 'वियतकांग (राष्ट्रीय मुक्ति सेना) का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष जारी हो गया।
- अमेरिका ने 1961 में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए 'शांति के खतरे' नाम से श्वेत पत्र जारी कर दिया और अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम में भेज दिया।
- अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर उसके सैनिक अड्डे को तबाह कर दिया। अमेरिका हो ची मिन्ह मार्ग पर सैकड़ों आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया।
- इस मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया पर भी आक्रमण किया।
- तीन तरफा युद्ध में पड़कर अमेरिका फंस गया और उसे वापस होना पड़ा।
- अमेरिका, शांति वार्ता चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर, जिसके कारण 1968 में पेरिस का शांति वार्ता सफल नहीं हो सका।
- अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन ने शांति के लिए पाँच सूत्री योजना की घोषणा की। परन्तु पाँच सूत्री शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने पुनः बमबारी शुरू कर दी ।
- 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उतरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परन्तु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया।
- अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ती के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया।
- इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल, 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया।
- समाजशास्त्रीयों के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है।
- तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई।
- पहला- औद्योगिक पूँजीवाद का उदय,
- दूसरा - विश्व के विशाल भू-भाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, और
- तीसरा- लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास।
- कस्बा - ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को माना जाता है। जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केन्द्र होता है।
- गंज- एक छोटे स्थायी बाजार को कहा जाता है। क़स्बा और गंज दोनों कपड़ा, फूल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबंधित था।
- महानगर- किसी प्रांत या देश का विशाल घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है। 10 लाख से ऊपर की आबादी को महानगर कहा जाता है।
- टेनमेंट्स- कामचलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान। ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते हैं।
- 3000 वर्ष पूर्व नदी घाटी की सभ्यताओं से शहर का विकास प्रारंभ हुआ। सिन्धु घाटी में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा प्रसिद्ध शहर थे।
- आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार हैं- (i) जनसंख्या का घनत्व तथा (ii) कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात ।
- किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है। ऐसी मान्यता का मुख्य कारण है पूँजी का असमान वितरण ।
- व्यावसायिक पूँजीवाद ने नगरों के उद्भव में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इनके कारण ही नगरों में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि का विकास हुआ। व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे।
- आधुनिक काल में औद्योगीकरण ने शहरीकरण स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया।
- शहरों में फैक्टरी प्रणाली की स्थापना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषक वर्ग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगा।
- मध्यम वर्ग एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा, जो विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए।
- रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण शहर में लोगों का स्तर ऊपर उठने लगा, जिससे क्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया।
- जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है ।
- औद्योगिक क्रांति इंगलैंड में सबसे पहले हुई इसलिए आधुनिक शहरों का विकास भी इंगलैंड में हीं शुरू हुआ ।
- 1815 में मैनचेस्टर में रहने वाले तीन चौथाई से अधिक लोग गाँव से आये प्रवासी मजदूर थे ।
- दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी, 1863 ई. को किया गया। यह रेल लाइन लंदन की पैडिंग्ल और कैरिंगटन के बीच स्थित थी।
- वे दो कानून ने इंगलैंड में बाल श्रमिकों को कारखानों में काम करने से रोक दिया था (I) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा (II) 1902 का फैक्ट्री कानून।
- घेटा सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में यह एक विशिष्ट धर्म, नृजाति, या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है ।
पेरिस का हॉस्मानीकरण
- 1852 में फ्रांस के सम्राट लुई तृतीय (नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे) ने फ्रांस की सत्ता संभालने के बाद अपनी राजधानी पेरिस शहर का पुनर्निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया।
- नये पेरिस के निर्माण कार्य बैरॉन हॉस्मान जो एक विख्यात और कुशल वास्तुकार तथा सियाँ का प्रिफेक्त था, उसे सौंपा गया।
- हॉस्मान ने 17 वर्ष में यह कार्य पूरा किया। यह काम हॉस्मान ने शहर को खूबसूरत बनाने तथा किसी प्रकार की विद्रोह की आशंका को दूर करने के उद्देश्य से पेरिस के मध्य से गरीबों की बस्तियों को साफ करवा दिया।
- पेरिस नगर सौंदर्य की दृष्टि से यूरोप के सभी नगरों से सर्वश्रेष्ठ बन गया। इससे पेरिस पूरे यूरोप के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया।
- सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है। 1965 तक सिंगापुर एक बन्दरगाह था। यहाँ अंग्रेजों का शासन था।
- यहाँ के ज्यादातर लोग भीड़ भरी गंदे मकानों और गंदगी में जीते थे।
- 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में सिंगापुर को आजादी मिली। उसने एक विशाल आवास एवं विकास कार्यक्रम शुरू किया। सरकार के द्वारा 86 प्रतिशत जनता को अच्छे मकान दिए गए।
- ऊंची आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार की सेवाओं का इंतजाम किया गया। बाहरी गलियारों के कारण अपराध कम हुए।
- भारतीय, चीनी और मलय समुदायों के बीच टकराव को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर भी लागातार सचेत रहने के उपाय किए गए।
- 17वीं शताब्दी में बंबई सात टापुओं का समूह था, उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था।
- 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय (II) का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरुप पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय (II) को दहेज में बंबई दे दिया।
- चार्ल्स द्वितीय (II) ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पश्चिमी भारत के अपने सबसे मुख्य बंदरगाह सूरत से अपना मुख्यालय बंबई में कायम कर लिया तथा इसका विकास कर इसे महानगर में परिवर्तित कर दिया।
- 1784 ई. में बंबई के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने विशाल तटीय दीवार का निर्माण समुद्रों के किनारे-किनारे बनवाया ताकि शहर के निचले इलाके को समुद्र के पानी की चपेट में आने से रोका जा सके।
- 1854 ई. में यहाँ पहला कपड़ा मिल खुला। 1921 ई० तक यहाँ 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थीं । 1931 तक बंबई के निवासी सिर्फ एक चौथाई हीं थे, बाकी निवासी बाहर से आकर यहाँ बसे थे।
- बम्बई के सुनियोजित विकास के लिए 1898 में सिटी ऑफ बंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गयी।
- चॉल- 1901 की जनगणना के अनुसार बम्बई की लगभग 80 प्रतिशत आबांदी चॉलों में रहती थी।
- 1918 में बम्बई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून पारित किया गया।
- बंबई की भूमि विकास योजना |
- 'बंबई पोर्ट ट्रस्ट' ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का भी निर्माण किया और खुदाई से निकली मिट्टी से 22 एकड़ का 'बांलार्ड एस्टेट' बनाया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में बंबई का मशहूर 'मरीन ड्राइव' बना।
- पाटलिपुत्र यानी पटना शहरीकरण की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण उदहारण है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर अथवा पुष्पपुर था। यह नगर चारों ओर से गंगा, गंडक, सोन तथा पुनपुन से घिरा हुआ था।
- पाटलिपुत्र नगर की स्थापना छठीं शताब्दी ई० पू० में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी। बाद में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बना।
- 457 ई० पू० में अजातशत्रु के पुत्र ने मगध की राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया।
- मेगास्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। गुप्त काल में भी इस नगर का वैभव बना रहा। इसके विशाल भवनों के वैभव और सौन्दर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा की गई है।
- पूर्व मध्यकाल में इस नगर का पतन हो गया। पुन: इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेरशाह सूरी ने स्थापित किया। उसने 1541 ई. के लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया क्योंकि उस स्थान के सैनिक महत्व को उसे आभास था।
- अकबर के शासनकाल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन चुका था।
- 1856 ई. में अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने इस नगर का भ्रमण किया। मुगलकाल में यहाँ अनेक सुंदर भवनों का निर्माण हुआ।
- इस नगर में 1666 ई० में सिखों के दसवें और अंतिम गुरु श्री गोविन्द सिंह जी का जन्म हुआ जिसके कारण सिख धर्म का तीर्थस्थल बन गया। वर्तमान में यह स्थल 'पटना साहिब' के नाम से जाना जाता है ।
- 18वीं सदी में पूर्वी भारत में जब ब्रिटिश शासन की स्थपाना हुई तो आधुनिक पटना नगर का विकास हुआ।
- 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नव निर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया।
- यहाँ से लगभग पाँच किलोमीटर की दूरी पर अनाज के भंडारण के लिए विशाल गोदाम का निर्माण 1786 ई० में किया गया जो आज गोलघर के नाम से जाना जाता है।
- 1774 ई. के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के प्रशासन के लिए कई व्यवस्थाएँ लागू की गई।
- 1911 में दिल्ली दरबार ने बिहार को बंगाल से अलग कर पृथक राज्य का दर्जा देने का निर्णय लिया गया।
- 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा मिला तथा पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया।
- इंडो-चाइना तीन देशों से मिल कर बना है। ये तीन देश हैं- वियतनाम, लाओस और कंबोडिया । इस पूरे इलाके के शुरुआती इतिहास को देखने पर पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते, थे और पूरे इलाक़े पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था।
- वियतनाम के एक स्वतंत्र देश की स्थापना करने के बाद भी वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा।
- वियतनाम उस रास्ते से भी जुड़ा रहा है जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता था। इस रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों की खूब आवाजाही चलती थी। व्यापार के अन्य रास्तों के माध्यम से वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से भी जुड़ा रहता था जहाँ गैर - वियतनामी समुदाय - जैसे खमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे।
- वियतनाम पर फ्रांसीसियों के क़ब्ज़े के बाद वियतनामियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जीवन के हर मोर्चे पर जनता का औपनिवेशिक शासकों के साथ टकराव होने लगा।
- फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में ही दिखाई देता था लेकिन वियतनामी संस्कृति को तहस-नहस करने के लिए भी उन्होंने सुनियोजित प्रयास किए।
- फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का अहसास कराने वाली हर चीज के खिलाफ वियतनामी समाज के हर तबके ने जमकर संघर्ष किया और यहीं से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े ।
- फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। के दशक के मध्य तक आते-आते उन्होंने देश के उत्तरी इलाक़े पर मज़बूती से कब्ज़ा जमा लिया। फ्रांस-चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोंकिन और अनाम पर भी कब्ज़ा कर लिया।
- 1887 में फ्रेंच इंडो-चाइना का गठन किया गया। बाद के दशकों में एक ओर फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना कब्ज़ा जमाते गए और दूसरी तरफ वियतनामियों को यह बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथों वे क्या-क्या गँवा चुके हैं।
- एक जमाने में प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और ज़रूरी साजो-सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना ज़रूरी माना जाता था। इसके अलावा, दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाजों तक सभ्यता की रोशनी पहुँचाना 'विकसित' यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है।
- फ्रांसीसियों ने वियतनाम के 'मेकांग डेल्टा' इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहाँ नहरें बनाईं और जल निकासी का प्रबंध शुरू किया।
- सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई । बहुत सारी नयी नहरें और भूमिगत जलधाराएँ बनाई गईं। ज्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगा कर निर्मित की गई इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई।
- 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। इसी दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फ़ौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया।
- पूरे इंडो-चाइना से गुजरने वाला एक विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया। इसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए।
- यह रेल नेटवर्क चीन में स्थित येनान प्रांत तक जाता था। यह नेटवर्क 1910 में बन कर पूरा हुआ। उसी समय एक और लाइन बिछाई गई जिसके ज़रिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के रास्ते होते हुए वियतनाम को स्याम देश ( उस समय थाईलैंड का यही नाम हुआ करता था) से जोड़ दिया गया।
- 1920 के दशक तक आते-आते फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे कि संरचनागत परियोजनाओं को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए।
- स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए ही उपनिवेश बनाए जाते थे। प्रभावशाली लेखक और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना ज़रूरी है। उनका कहना था कि उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी और लोगों का जीवनस्तर बेहतर होगा तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे जिससे बाज़ार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायों को फायदा होगा।
- बर्नार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली कई बातें गिनवाई हैं। जैसे, देश की आबादी ज्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर कम था और किसान भारी कर्जे में डूबे हुए थे।
- ग्रामीण गरीबी कम करने और खेतिहर उत्पादन बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी था कि वियतनाम में भी उसी तरह के भूमि सुधार किए जाएँ, जिस तरह के सुधार जापान में 1890 के दशक में किए गए थे। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए यह गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि सबको रोज़गार भी मिल जाएगा। जैसा कि जापान के अनुभवों से स्पष्ट हो चुका था, नए रोज़गार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण करना ज़रूरी था।
- वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के बागानों पर आश्रित थी। इन पर फ्रांस और वियतनाम के मुट्ठी भर धनी तबके का स्वामित्व था।
- वियतनाम के बागानों में इस तरह की मजदूरी व्यवस्था काफी प्रचलित थी।
- इस व्यवस्था में मजदूर ऐसे अनुबंधों के तहत काम करते थे जिनमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे जबकि मालिकों को बेहिसाब अधिकार मिलते थे।
- अगर मजदूर अनुबंध की शर्तों के हिसाब से अपना काम पूरा न कर पाएँ तो मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सज़ा देते थे, जेलों में डाल देते थे।
- फ्रांसीसी उपनिवेशवाद सिर्फ आर्थिक शोषण पर केंद्रित नहीं था। इसके पीछे 'सभ्य' बनाने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत में अंग्रेज़ दावा करते थे उसी तरह फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं।
- उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है। इसीलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृतियों, धर्मों व परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
- 'देशी' जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफी अहम माना जाता था। लेकिन वियतनाम में शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों को एक और दुविधा हल करनी थी। दुविधा इस बात को लेकर थी कि वियतनामियों को किस हद तक या कितनी शिक्षा दी जाए? फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की ज़रूरत तो थी लेकिन गुलामों को पढ़ाने-लिखाने से समस्याएँ, भी पैदा हो सकती थीं।
- शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे। इतना ही नहीं, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों (जिन्हें कोलोन कहा जाता था) को तो यह भी भय था कि स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम-धंधे और नौकरियाँ भी हाथ से न जाती रहें।
- शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। वियतनाम के धनी और अभिजात्य तबके के लोग चीनी संस्कृति से गहरे तौर पर प्रभावित थे। फ्रांसीसियों की सत्ता को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए इस प्रभाव को समाप्त करना ज़रूरी था।
- फलस्वरूप, पहले उन्होंने परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से तहस-नहस किया और फिर वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल दिए |
- अब तक समाज के खाते-पीते तबके के लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसे हटाना ज़रूरी था। लेकिन उसकी जगह लेने वाली भाषा कौन सी हो ? चीनी भाषा को हटा कर लोगों को वियतनामी भाषा पढ़ायी जाए या उन्हें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए?
- इस सवाल पर लोगों के बीच दो मत थे। कुछ नीति-निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।
- फ्रांसीसी भाषा सीखने से वियतनाम के लोग फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएँगे। इस प्रकार 'यूरोपीय फ्रांस के साथ मज़बूती से बँधे एक एशियाई फ्रांस' की रचना करने में मदद मिलेगी।
- वियतनाम के शिक्षा प्राप्त लोग फ्रांसीसी भावनाओं व आदर्शों का सम्मान करने लगेंगे, फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रभुत्व हो जायेगा और फ्रांसीसियों के लिए लगन से काम करने लगेंगे।
- बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ थे कि पढ़ाई के लिए केवल फ्रांसीसी भाषा को ही माध्यम बनाया जाए। उनका विचार था कि अगर छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।
- स्कूलों में दाखिला लेने की ताकत तो वियतनाम के धनी वर्ग के पास ही थी। यह देश की आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा था। जो स्कूल में दाखिला ले पाते थे उनमें से भी बहुत थोड़े से विद्यार्थी ही ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे।
- बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझ कर फेल कर दिया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त न कर सकें।
- आमतौर पर दो तिहाई विद्यार्थियों को इसी तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वालों की संख्या 400 से भी कम थी।
- पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल खोला गया था। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएँ भी शामिल थीं।
- स्कूल की नज़र में 'आधुनिक' के क्या मायने थे स्कूल की राय में, सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं था : आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा दिखना भी पड़ेगा।
- शिक्षकों और विद्यार्थियों ने इन पुस्तकों और पाठ्यक्रमों का आँख बंद कर अनुसरण नहीं किया। कहीं इनका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया।
- 1926 में साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। वियतनामी लड़की को स्कूल से निकाल दिया।
- हालात बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को वापस दाखिला तो दे दिया लेकिन साथ ही यह ऐलान भी कर दिया कि 'मैं सारे वियतनामियों को पाँव तले कुचल कर रख दूँगा।
- दूसरे इलाकों में भी छात्र-छात्राओं ने सरकार की इस चाल का जमकर विरोध किया कि वियतनामी बच्चों को सफ़ेदपोश नौकरियों के लायक योग्यता न मिले।
- ये विद्यार्थी देशभक्ति की भावानाओं से प्रेरित थे । उनको विश्वास था कि शिक्षितों को समाज के भले के लिए काम करना चाहिए।
- उनकी इसी सोच के कारण न केवल फ्रांसीसियों के साथ बल्कि स्थानीय अभिजात्य वर्ग के साथ भी उनका टकराव बढ़ने लगा क्योंकि दोनों को ही लगता था कि इस तरह तो उनकी हैसियत और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी।
- 1920 के दशक तक आते-आते छात्र-छात्राएँ राजनीतिक पार्टियों बनाने लगे थे। उन्होंने यंग अन्नान जैसी पार्टियों बना ली थीं और वे अन्नानीज स्टूडेंट (अन्नान के विद्यार्थी) जैसी पत्रिकाएँ निकालने लगे थे।
- पाठशालाएँ राजनीतिक सांस्कृतिक संघर्ष के अखाड़ों में तब्दील होने लगीं। शिक्षा पर नियंत्रण के माध्यम से फ्रांसीसी वियतनाम पर अपना कब्जा और मजबूत करने की फिराक में थे।
- वे जनता की मूल्य मान्यताओं, तौर-तरीकों और रवैयों को > बदलने का प्रयास करने लगे ताकि लोग फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामियों को कमतर मानने लगें।
- दूसरी तरफ़, वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगता था कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर अपना नियंत्रण खोता जा रहा है बल्कि अपनी पहचान भी गँवाता जा रहा है।
- उसकी संस्कृति और मूल्यों का अपमान किया जा रहा था और लोगों में राजा- वाल भाव पैदा हो रहा था। फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाले व्यापक संघर्ष का हिस्सा बन गया था।
| 1802 | न्यूयेन राजवंश के अंतर्गत राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतीक न्यूयेन आन्ह की सम्राट के रूप में ताजपोशी होती है। |
| 1867 | कोचिनचाइना (दक्षिण) फ्रांस का उपनिवेश बन जाता है। |
| 1887 | कोचिनचाइना, अन्नम, टोकिन, कंबोडिया और बाद में। लाओस को मिला कर इंडो-चाइना यूनियन की स्थापना की जाती है। |
| 1930 | हो ची मिन्ह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। |
| 1945 | वियेतमिन्ह जनविद्रोह शुरू करते हैं। बाओ दाई को गद्दी से हटा दिया जाता है। हो ची मिन्ह हनोई में स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं (23 सितम्बर ) । |
| 1954 | दिएन बिएन फू के मोर्चे पर फ्रांसीसी सेना घुटने टेक देती है। |
| 1961 | कैनेडी दक्षिणी वियतनाम के लिए अमेरिकी सैनिक सहायता बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। |
| 1974 | पेरिस शांति संधि | |
| 1975 | (30 अप्रैल) एन.एल.एफ. की सैनिक टुकड़ियाँ साइगॉन में दाखिल होती हैं। |
| 1976 | वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना होती है। |
- जब फ़्रांसीसियों ने एक आधुनिक वियतनाम की स्थापना का काम शुरू किया तो उन्होंने फैसला लिया कि वे हनोई का भी पुनर्निर्माण करेंगे।
- एक नए 'आधुनिक' शहर का निर्माण करने के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में सामने आ रहे नवीनतम विचारों और आधुनिक इंजीनियरिंग निपुणता का इस्तेमाल किया गया।
- 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में ब्यूबॉनिक प्लेग की महामारी फैल गई। बहुत सारे औपनिवेशिक देशों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जो क़दम उठाए गए उनके कारण भारी सामाजिक तनाव पैदा हुए। परंतु हनोई के हालात तो कुछ ख़ास ही थे।
- हनोई के फ़्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ़-सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें थीं और निकासी का बढ़िया इंतज़ाम था । 'देशी' बस्ती में ऐसी कोई आधुनिक सुविधाएँ नहीं थीं।
- पुराने शहर का सारा कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में बहा दिया जाता था। भारी बरसात या बाढ़ के समय तो सारी गंदगी सड़कों पर ही तैरने लगती थी।
- प्लेग की शुरुआत ही उन चीजों से हुई थी जिनको शहर के फ़्रांसीसी भाग में स्वच्छ परिवेश बनाए रखने के लिए लगाया गया था। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे। यही सीवर चूहों के पनपने के लिए भी आदर्श साबित हुए। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए भी उचित थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटके घूमते थे। और इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे फ़्रांसीसियों के चाक- -चौबंद घरों में घुसने लगे।
- इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 ई. में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। इस काम के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया और उन्हें हर चूहे के बदले ईनाम दिया जाने लगा।
- वियतनामियों को चूहों के शिकार की इस मुहिम के ज़रिए सामूहिक सौदेबाज़ी का महत्त्व समझ में आने लगा था।
- जो लोग सीवरों की गंदगी में घुस कर काम करते थे उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएँ तो बेहतर मेहनताने के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं।
- इस स्थिति से फायदा उठाने के एक से एक नायाब तरीक़े भी ढूँढ़ निकाले । मज़दूरों को पैसा तब मिलता था जब वे यह साबित कर देते थे कि उन्होंने चूहे को पकड़ कर मार डाला है। सबूत के तौर पर उन्हें चूहे की पूँछ लाकर दिखानी पड़ती थी। इस प्रावधान का फायदा उठाते हुए मज़दूर ज्यादा पैसा कमाने के लिए चूहे को पकड़ कर उसकी पूँछ तो काट लेते थे पर चूहे को जिंदा छोड़ देते थे ताकि वे कभी खत्म न हों और उनको पकड़ने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। कुछ लोगों ने तो पैसे कमाने के लिए बाकायदा चूहे पालना शुरू कर दिया था।
- निर्बलों के इस प्रतिरोध और असहयोग से तंग आकर आखिरकार फ्रांसीसियों ने चूहे के बदले पैसे देने की योजना ही बंद कर दी। लिहाजा, ब्यूबॉनिक प्लेग खत्म नहीं हुआ। न केवल 1903 में बल्कि अगले कुछ सालों तक यह बीमारी पूरे इलाके में फैल गई।
- चूहों के आतंक की यह कहानी कई मायनों में फ़्रांसीसी सत्ता की सीमा और सभ्यता प्रसार के उनके मिशन में निहित अंतर्विरोधों को सामने ला देती है।
- औपनिवेशिक वर्चस्व निजी और सार्वजनिक जीवन के तमाम पहलुओं पर नियंत्रण के रूप में सामने आता था। फ्रांसीसियों ने न केवल सैनिक ताक़त के सहारे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था बल्कि वे वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी पूरी तरह बदल देना चाहते थे।
- धर्म ने औपनिवेशिक शासन को मज़बूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की लेकिन दूसरी ओर उसने प्रतिरोध के नए-नए रास्ते भी खोल दिए थे।
- कन्फ्यूशियस ( 551-479 ईसा पूर्व) एक चीनी विचारक थे जिन्होंने सदाचार, व्यवहार बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी।
- उनके सिद्धांतों के आधार पर लोगों को बड़े-बुजुर्गों व माता-पिता का आदर करने और उनका कहना मानने का पाठ पढ़ाया जाता था।
- उन्हें सिखाया जाता था कि राजा और प्रजा का संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसा माता-पिता का अपने बच्चों के साथ होता है।
- वियतनामियों के धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति-रिवाजों पर आधारित थे। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें वियतनामियों के धर्मिक जीवन में इस तरह का घालमेल पसंद नहीं था।
- 18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे।
- 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट (विद्वानों का विद्रोह) फ्रांसीसी क़ब्ज़े और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलनों में से था।
- इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। ये अफ़सर कैथलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज़ थे। उन्होंने न्यू अन और हा तिएन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व किया और एक हज़ार से ज्यादा ईसाइयों का क़त्ल कर डाला।
- कैथोलिक मिशनरी 17वीं सदी की शुरुआत से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे और 18वीं सदी के अंत तक आते-आते उन्होंने लगभग 3,00,000 लोगों को ईसाई बना लिया था।
- फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलन को तो कुचल डाला लेकिन इस बग़ावत ने फ्रांसीसियों के खिलाफ अन्य देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर कर दिया।
- वियतनाम के अभिजात्य चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे। लेकिन किसानों के धार्मिक विश्वास बहुत सारी समन्वयवादी परंपराओं से जन्मे थे जिनमें बौद्ध धर्म और स्थानीय मूल्य-मान्यताओं, दोनों का सम्मिश्रण था।
- वियतनाम में बहुत सारे पंथ ऐसे लोगों के ज़रिए फैले थे जिनका दावा था कि उन्होंने ईश्वर की आभा देखी है। इनमें से कुछ धार्मिक आंदोलन फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे जबकि कुछ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों के पक्षधर थे।
- होआ हाओ ऐसा ही एक आंदोलन था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। हरे-भरे मेकांग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में उपजे विचारों से प्रेरित था।
- होआ हाओ आंदोलन के संस्थापक हुइन्ह फू सो थे। वह जादू-टोना और ग़रीबों की मदद किया करते थे। व्यर्थ खर्चे के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों में काफी असर था। वह बालिका वधुओं की खरीद-फरोख्त, शराब व अफीम के प्रखर विरोधी थे।
- फ्रांसीसियों ने हुइन्ह फू सो के विचारों पर आधारित आंदोलन को कुचलने का कई तरह से प्रयास किया। उन्होंने फू सो को पागल घोषित कर दिया।
- आखिरकार 1941 ई. में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने भी मान लिया कि वह पागल नहीं हैं। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लाओस भेज दिया। उनके बहुत सारे समर्थकों और अनुयायियों को यातना शिविर (Concentration Camp) में डाल दिया गया।
- इस तरह के आंदोलनों का राष्ट्रवाद की मुख्यधारा के साथ अंतर्विरोधी संबंध रहता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों से जुड़े जनसमर्थन का फ़ायदा उठाने की तो कोशिश करते थे लेकिन उनकी गतिविधियों से बेचैन भी रहते थे।
- राजनीतिक दलों को ऐसे समूहों पर नियंत्रण और अपना अनुशासन कायम करने में काफी परेशानी महसूस होती थी; न ही वे उनके रीति-रिवाजों और व्यवहारों का समर्थन कर पाते थे।
- 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसियों के विरोध का नेतृत्व प्रायः कन्फ्यूशियन विद्वानों कार्यकर्ताओं के हाथों में होता था जिन्हें अपनी दुनिया बिखरती दिखाई दे रही थी।
- कन्फ्यूशियन परंपरा में शिक्षित फान बोई चाऊ (1867-1940) · ऐसे ही एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने 'रेवोल्यूशनरी सोसायटी' (दुई तान होई) नामक पार्टी का गठन किया और तभी से वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के एक अहम नेता बन गए थे। राजकुमार कुआंग दे इस पार्टी के मुखिया थे।
- फान बोई चाऊ ने 1905 में चीनी सुधारक लियाँग किचाओ (1873-1929) से योकोहामा में भेंट की। फान की सबसे प्रभावशाली पुस्तक, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ़ वियतनाम, लियाँग की सलाह और प्रभाव में ही लिखी गई थी।
- यह किताब एक-दूसरे से जुड़े दो विचारों पर केंद्रित हैं : एक, देश की संप्रभुता का नाश, और दूसरा, दोनों देशों के अभिजात्य वर्ग को एक संस्कृति में बाँधने वाले वियतनाम - चीन संबंधों का टूटना।
- फान अपनी पुस्तक में इसी दोहरे नाश का विलाप करते हैं। उनके शोक का अंदाज़ वैसा ही था जैसा परंपरागत अभिजात्य तबके से निकले सुधारकों का दिखाई देता था।
- अन्य राष्ट्रवादी फान बोई चाऊ के विचारों से गहरे तौर पर असहमत थे। फान चू त्रिन्ह (1871-1926) ऐसे नेताओं में प्रमुख थे। वे राजशाही / राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे।
- पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित त्रिन्ह पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खारिज करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे लेकिन उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं।
- उनकी माँग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें और कृषि व उद्योगों का विकास करें।
- प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों के जापान और चीन के साथ काफी घनिष्ठ संबंध थे। जापान और चीन न केवल बदलाव का प्रतीक थे बल्कि फ्रांसीसी पुलिस से बच निकलने वालों के लिए शरणस्थली भी थे। इन देशों में एशियाई क्रांतिकारियों के नेटवर्क बने हुए थे।
- 20वीं सदी के पहले दशक में 'पूरब की ओर चलो' आंदोलन काफी तेज था। 1907-1908 में लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। उनमें से बहुतों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकाल बाहर किया जाए, कठपुतली सम्राट को गद्दी से हटा दिया जाए और फ्रांसीसियों द्वारा अपमानित करके गद्दी से हटा दिए गए न्यूयेन राजवंश को दोबारा गद्दी पर बिठाया जाए।
- इन राष्ट्रवादियों को विदेशी हथियार और मदद लेने से कोई परहेज़ नहीं था। इसके लिए उन्होंने एशियाई होने के नाते जापानियों से मदद माँगी। जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुका था।
- जापानियों ने पश्चिम द्वारा गुलाम बनाए जाने की कोशिशों का भी सफलतापूर्वक विरोध किया था। 1907 में रूस पर विजय प्राप्त करके जापान अपनी सैनिक ताक़त का भी लोहा मनवा चुका था।
- वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी 'रेस्टोरेशन सोसायटी' की स्थापना कर ली थी लेकिन 1908 में जापानी गृह मंत्रालय ने ऐसी गतिविधियों का दमन शुरू कर दिया ।
- फान बोई चाऊ सहित बहुत सारे लोगों को जापान से निकाला जाने लगा और उन्हें मजबूरन चीन व थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी।
- चीन के घटनाक्रम ने भी वियतनामी राष्ट्रवादियों के हौसले बढ़ा दिए थे। सुन यात सेन के नेतृत्व में चले आंदोलन के ज़रिए जनता ने लंबे समय से चीन पर शासन करते आ रहे राजवंश को 1911 में गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया और वहाँ गणराज्य की स्थापना की गई।
- इन घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने भी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन (वीयेत- नाम कुवान फुक होई) की स्थापना कर डाली । अब फ्रांस-विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदल चुका था।
- 1930 के दशक में आई महामंदी का वियतनाम पर भी गहरा असर पड़ा। रबड़ और चावल के दाम गिर गए और क़र्ज़ा बढ़ने लगा। चारों तरफ़ बेरोजगारी और ग्रामीण विद्रोहों का बोलबाला था। न्पे अन और हा तिन्ह प्रांतों में भी ऐसे ही आंदोलन हुए।
- फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादियों के अलग-थलग समूहों और गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट (वियतनाम काँग सान देंग) पार्टी की स्थापना की जिसे बाद में इंडो-चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। हो ची मिन्ह यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के उग्र आंदोलनों से काफी प्रभावित थे।
- 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्ज़ा कर लिया। जापान पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया पर कब्ज़ा करना चाहता था। ऐसे में अब राष्ट्रवादियों को फ्रांसीसियों के साथ-साथ जापानियों से भी लोहा लेना था। बाद में वियेतमिन्ह के नाम से जानी गई लीग फॉर द इंडिपेंडेस ऑफ वियतनाम (वियतनाम स्वतंत्रता लीग) ने जापानी कब्ज़े का मुँहतोड़ जवाब दिया और सितंबर 1945 में हनोई को आज़ाद करा लिया।
- इसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और हो ची मिन्ह को उसका अध्यक्ष चुना गया।
- नए गणराज्य के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे।
- फ्रांसीसी हमले को देखते हुए वियेतमिन्ह के सदस्यों को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। आठ साल तक चली लड़ाई में आखिरकार फ्रांसीसियों को दिएन बिएन फू के मोर्चे पर मुँह की खानी पड़ी।
- फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल हेनरी नावारे ने 1953 में ऐलान किया था कि उनकी सेना जल्दी ही विजयी होगी। लेकिन 7 मई 1954 को वियेतमिन्ह ने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनिरी कोर के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया और 16,000 से ज्यादा को क़ैद कर लिया।
- एक जनरल, 16 कर्नलों और 1,749 अफ़सरों सहित पूरे कमांडिंग दस्ते को पकड़ लिया गया।
- फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ताओं में वियतनामियों को देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया गया।
- उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, दो अलग-अलग देश बन गए। उत्तरी भाग में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हुई जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओ डाई की सत्ता बनी रही।
- इस बँटवारे से पूरा वियतनाम युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया। देश के अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही होने लगी। कुछ समय बाद दिएम के नेतृत्व में हुए तख्तापलट में बाओ डाई को गद्दी से हटा दिया गया।
- दिएम की अगुवाई में एक और दमनकारी व निरंकुश शासन की स्थापना हुई। उसका विरोध करने वालों को कम्युनिस्ट कहकर जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था।
- दिएम ने अध्यादेश 10 को भी नहीं हटाया जिसमें ईसाई धर्म को तो मान्यता दी गई थी लेकिन बौद्ध धर्म को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। उसके तानाशाही शासन के ख़िलाफ़ नेशनल लिबरेशन फ्रंट (एन.एल.एफ.) के नाम से एक व्यापक मोर्चा बनाया गया।
- उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से एन.एल.एफ. ने देश के एकीकरण के लिए आवाज उठाई। अमेरिका इस गठबंधन की बढ़ती ताकत और उसके प्रस्तावों से भयभीत था।
- पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्ज़ा होने के भय से अमेरिका ने अपनी फौजें और गोला-बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया। अमेरिका इस खतरे से सख्ती निपटना चाहता था।
- हो ची मिन्ह की शुरुआती जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारियाँ | उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह अपनी निजी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत बात नहीं करते थे। उन्होंने खुद को वियतनाम की आज़ादी के लिए झोंक दिया था।
- उनका जन्म मध्य वियतनाम में हुआ और उनका असली नाम संभवतः न्यूयेन वान थान्ह था। हो न भी उन्हीं फ्रांसीसी स्कूलों में शिक्षा पाई थी न्गो दिन्ह दिएम, वो न्यूयेन ग्याप, और फान वान देंग जैसे नेता निकले थे।
- 1910 में कुछ समय के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। 1911 में उन्होंने बेकिंग सीखी और साइगॉन से मार्सेई जाने वाले फ्रांसीसी जहाज़ पर नौकरी कर ली ।
- बाद में हो कॉमिन्टर्न के सक्रिय सदस्य बन गए और लेनिन व अन्य नेताओं से मिले। यूरोप, थाईलैंड और चीन में 30 साल बिताने के बाद मई 1941 में वह वियतनाम लौट आए। 1943 में उन्होंने अपना नाम बदल कर हो ची मिन्ह (पथप्रदर्शक) रख लिया।
- जब वियतनाम लोक गणराज्य की स्थापना हुई तो उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। 3 सितंबर 1969 को हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई। उन्होंने वियतनाम की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए 40 साल से भी ज्यादा समय तक पार्टी का नेतृत्व किया।
- अमेरिका के भी युद्ध में कूद पड़ने से वियतनाम में एक नया दौर शुरू हुआ। 1965 से 1972 के बीच अमेरिका के 34,03,100 सैनिकों ने वियतनाम में काम किया जिनमें से 7. .484 महिलाएँ थीं।
- अमेरिका के साथ संघर्ष का यह दौर काफी यातनापूर्ण और निर्मम रहा। इस युद्ध में बड़े-बड़े हथियारों और टैंकों से लैस हज़ारों अमेरिकी सैनिक वियतनाम में झोंक दिए गए थे। उनके पास बी 52 बमवर्षक विमान भी मौजूद थे जिन्हें उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धक विमान माना जाता था।
- चौतरफा हमलों और रासायनिक हथियारों के बेतहाशा इस्तेमाल से असंख्य गाँव नष्ट हो गए और विशाल जंगल तहस-नहस कर दिए गए।
- अमेरिकी फ़ौजों ने नापाम, एजेंट ऑरेंज और फ़ॉस्फोरस बम जैसे घातक रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। इन हमलों में असंख्य साधारण नागरिक मारे गए।
- एजेंट ऑरेंज एक ऐसा ज़हर है जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। उसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसे जिन ड्रमों में रखा जाता था उन पर नारंगी (यानी ऑरेंज) रंग की पट्टियाँ बनी होती थीं।
- 1961 से 1971 के बीच अमेरिकी फ़ौज़ों के मालवाही विमानों ने वियतनाम पर लगभग 1.1 करोड़ गैलन एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था।
- युद्ध का असर अमेरिका में भी साफ महसूस किया जा सकता था। वहाँ के बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौजों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता।
- अग्नि बमों के लिए गैसोलीन को फुलाने में इस्तेमाल होने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
- यह मिश्रण धीरे-धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है और जलता रहता है।
- अमेरिका में विकसित किए गए इस रसायन का दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था।
- भारी अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद इसका वियतनाम में भी। बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।
- वियतनाम युद्ध अमेरिकी सैनिकों के लिए मौत का फंदा बन चुका था। अमेरिका को इस युद्ध में अपने करीब 58,000सैनिकों को गंवाना पड़ा।
- अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं और कई जीती हैं लेकिन कुछ युद्ध उसके लिए गले की हड्डी बन गए थे, न निगलते बन रहा था और न उगलते बन रहा था। ऐसा ही एक युद्ध वियतनाम का युद्ध है।
- वियतनाम पर 19वीं सदी से फ्रांस का कब्जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर हमला किया। अब वियतनाम को एक साथ दो मोर्चे पर लड़ना था।
- एक तरफ उसे जापान की फौज से लड़ना था तो दूसरी तरफ उसे फ्रांस के औपनिवेशिक शासन को भी उखाड़ फेंकना था। दोनों काम को एक साथ अंजाम देने के लिए हो चो मिन्ह ने वियत मिन्ह या वियतनाम की आजादी के लिए लीग की स्थापना की।
- हो चो मिन्ह वियतनाम के राजनेता थे जो चीनी और सोवियत साम्यवाद से काफी प्रभावित थे। दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जापान की सेना वियतनाम से निकल गई।
- जापान के निकलने से वियतनाम पर सम्राट बाओ डाई का कब्जा हो गया जिन्होंने फ्रांस से पढ़ाई की थी और उनको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। यानी वियतनाम पर फ्रांस की कठपुतली सरकार का शासन था।
- हो को वियतनाम पर कब्जा करने का मौका दिखा। उनकी वियत मिन्ह सेना ने हनोई के उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया और उसे लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम (डीआरवी) करार दिया। हो चो मिन्ह को उसका राष्ट्रपति बनाया गया।
- फ्रांस की मदद से सम्राट बाओ ने उस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए मुहिम छेड़ा। जुलाई 1949 में उन्होंने वियतनाम राज्य का गठन किया।
- साइगोन को उसकी राजधानी बनाई गई। दोनों चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो। लेकिन सिस्टम को लेकर उनके बीच मतभेद था।
- हो और उनके समर्थक चाहते थे कि उनके देश को अन्य कम्यूनिस्ट देशों के मॉडल पर विकसित किया जाए। वहीं बाओ और अन्य लोगों की चाहत थी कि वियतनाम पश्चिमी देशों का मॉडल अपनाए।
- वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी 1954 में शुरू हुई। हो की साम्यवादी सेना का उत्तरी वियतनाम पर कब्जा होने के बाद उत्तरी और दक्षिणी भाग की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया।
- मई 1954 में उनके बीच निर्णायक युद्ध हुआ। उसमें वियत मिन्ह सेना जीत गई। युद्ध में फ्रांस की हार के साथ ही वियतनाम में फ्रांस के औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ।
- जुलाई 1954 में जेनेवा कॉन्फ्रेंस में एक संधि हुई जिसमें वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया।
- हो के कब्जे में उत्तरी वियतनाम रहा जबकि बाओ के कब्जे में दक्षिणी वियतनाम । संधि में प्रावधान था कि देश का फिर से एकीकरण के लिए 1956 में चुनाव होगा।
- 1955 में न्गो दिन्ह दिएम नाम के राजनीतिज्ञ ने सम्राट बाओ का तख्तापलट कर दिया।
- वह वियतनाम गणराज्य की सरकार (जीवीएन) के राष्ट्रपति बन गए। उस दौरान जीवीएन को दक्षिण वियतनाम के नाम से जाना जाता था।
- इसी बीच दुनिया भर में शीत युद्ध जोर पकड़ने लगा था। अमेरिका ने शीत युद्ध के मद्देनजर सोवियत संघ के सहयोगियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी को काफी सख्त कर दिया था।
- 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्विट डी. आइजन हावर ने डिएम और दक्षिण वियतनाम को पुरजोर सहायता करने की कसम खाई।
- दक्षिण वियतनाम की सरकार को अमेरिकी सेना और सीआईए ने हथियार मुहैया कराए। दक्षिण वियतनाम की सेना को भी प्रशिक्षण दिया गया।
- अमेरिका ने वहां अपने सैनिक भेज दिए। इसके बाद दिएम की सेना ने दक्षिण वियतनाम में वियत मिन्ह के समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू किया।
- करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कई को बुरी तरह टॉर्चर किया गया और प्रताड़ना दी गई ।
- दक्षिण वियतनाम की सरकार वियत मिन्ह के समर्थकों को वियत कॉन्ग या वियतनाम का कम्यूनिस्ट कहती थी। 1957 के बाद वियत कॉन्ग और दिएम के अन्य विरोधियों ने सरकारी अधिकारियों एवं अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1959 तक दक्षिणी वियतनाम की सेना के साथ उनकी सशस्त्र लड़ाई शुरू हो गई।
- दिसंबर 1960 में दिएम के विरोधियों ने उसके दमनकारी शासन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति मोर्च (एनएलएफ) का गठन किया। उसमें दिएम के विरोधी कम्यूनिस्ट और गैर कम्यूनिस्ट दोनों शामिल थे।
- एनएलएफ ने खुद को स्वायत्त घोषित किया लेकिन वॉशिंगटन को लगता था कि एनएलएफ उत्तरी वियतनाम की कठपुतली है। वॉशिंगटन ने इसके लिए दक्षिण वियतनाम का सर्वे कराया।
- रिपोर्ट में वियत कॉन्ग के खतरे से निपटने के लिए डिएम को सैन्य, आर्थिक और तकनीकी सहायता देने का सुझाव दिया गया। वैसे तो 1954 में ही अमेरिकी सैनिक वियतनम में पहुंच गए थे लेकिन उस समय उनकी तादाद 800 से कम ही थी। 1962 तक उनकी तादाद 9,000 हो गई ।
- नवंबर 1963 में दिएम के जनरलों ने बगावत कर दी। दिएम की सरकार गिरा दी गई। उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई। ऊधर उससे तीन हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी की हत्या कर दी गई ।
- दक्षिण वियतनाम में बदल रही परिस्थिति ने केनेडी के उत्तराधि कारी लिंडन बी. जॉनसन को वियतनम में अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई।
- अगस्त 1964 में अमेरिका के दो जहाजों पर टोंकिन की खाड़ी में हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में बदले की कार्रवाई के तौर पर बमबारी का आदेश दिया।
- अगले साल अमेरिकी जहाजों ने वियतनाम में बमबारी शुरू कर दी। वियतनाम में अमेरिका अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडर रखा।
- मार्च 1965 में जॉनसन ने वियतनाम के युद्ध में और सैनिकों को भेजने का फैसला लिया। जॉनसन ने वियतनाम में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर करीब 4.5 लाख कर दी।
- वियतनाम में अमेरिका की ओर से खूब बमबारी होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में जितने बम गिराए थे, उससे चार गुना ज्यादा वियतनाम में गिराए गए।
- जेनेवा संधि के समय अमेरिका ने वियतनाम में 1956 चुनाव का वादा किया था। लेकिन बाद में उससे मुकर गया जिससे जॉनसन की विश्वसनीयता घटी।
- ऊधर चीन और सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम की मदद नाटकीय तौर पर बढ़ा दी। वियतनाम के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े थे।
- वह देश के लिए मरने-मारने को तैयार थे। वियतनाम की सेना के साथ मिलकर वहां के नागरिक भी अमेरिकी सैनिकों को चुन-चुनकर मारने लगे।
- साल 1968 तक अमेरिकी सैनिकों का हौसला जवाब दे चुका था। वे जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। वे किसी तरह अपनी जान बचाने में जुट गए थे।
- अमेरिका ने उत्तरो वियतनाम के साथ बातचीत शुरू की लेकिन 1972 ई. तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कम्यूनिस्टों ने एक बार फिर जोरदार हमला किया। फिर अमेरिका ने मई और जून 1972 ई. में उत्तरी वियतनाम में खूब बमबारी की।
- उत्तरी वियतनाम की ओर से भी बराबर बदले की कार्रवाई की गई। अमेरिका ने भले ही खूब बमबारी की लेकिन जमीनी स्तर उनके सैनिकों का हौसला टूट चुका था।
- बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने से अमेरिका पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव था।
- आखिरकार जनवरी 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक शांति संधि हुई।
- इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध का अंत हो गया। लेकिन उत्तरी और दक्षिण वियतनाम के बीच लड़ाई जारी रहो।
- 30 अप्रैल, 1975 को डीआरवी सेना ने साइगोन पर कब्जा कर लिया और उसका नाम हो चो मिन्ह शहर कर दिया।
- 1976 में डीआरवी ने वियतनाम का एकीकरण किया और उसका नाम समाजवादी गणराज्य वियतनाम हो गया।
- युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वियतनाम के करीब 20 लाख लोगों को मारे जाने और 30 लाख के करीब लोगों को घायल होने का अनुमान है।
- करीब 1.2 करोड़ लोगों ने दूसरे देशों में शरण लिया। अमेरिका को अरबों डॉलर पैसा खर्च करना पड़ा और उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए।
- हो ची मिन्ह मार्ग को देखने पर इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया। इससे पता चलता है कि वियतनाम के लोग अपने सीमित संसाधनों का भी कितनी सूझबूझ से इस्तेमाल करना जानते थे।
- फुटपाथों और सड़कों के इस विशाल नेटवर्क जरिए देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद भेजी जाती थी।
- 50 के दशक के आखिर में इस मार्ग को काफी बेहतर बना दिया गया था और 1967 के बाद हर महीने लगभग 20, 000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इसी रास्ते से होते हुए दक्षिणी वियतनाम पहुँचने लगे थे।
- इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था और उसके कई सिरे दक्षिणी वियतनाम में पहुँच जाते थे।
- अमेरिकी टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए इस मार्ग पर कई बार बम बरसाए। पर बेहिसाब बमबारी के बावजूद वे इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाए।
- अमेरिकी इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि वहाँ के लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर लेते थे।
- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Facebook पर फॉलो करे – Click Here
- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
- Google News ज्वाइन करे – Click Here







