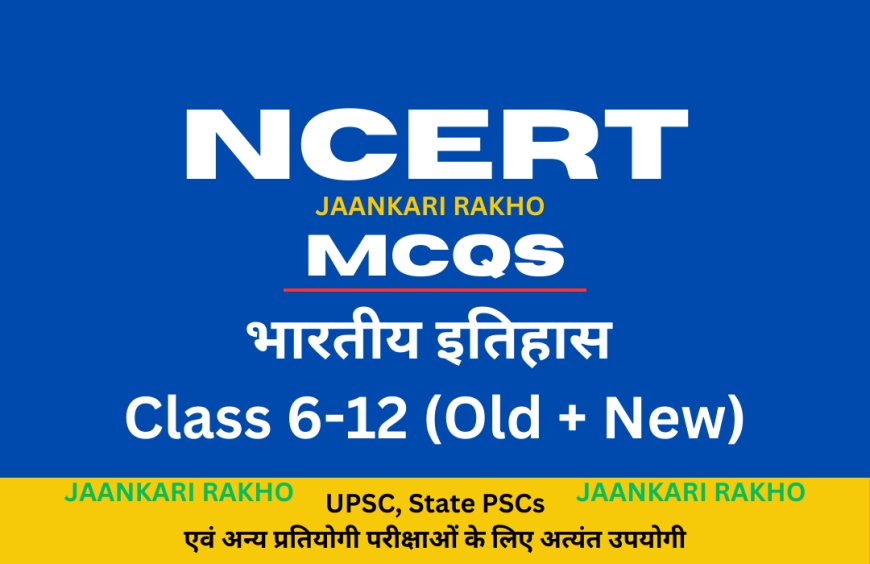NCERT MCQs | प्राचीन इतिहास | प्राचीन भारत के विविध पहलू
1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) भारतीय दर्शन को चार भागों में बाँटा गया है
(b) इसका मुख्य विषय मोक्ष रहा है
(c) मोक्ष का उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया था
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर - (a)
व्याख्या- दिए गए कथनों में से कथन (a) सत्य नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन में चार नहीं बल्कि छः मतवाद विकसित हो चुके थे, जिनमें शामिल हैं—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत । भारतीय दर्शन का केंद्रीय विषय मोक्ष है। मोक्ष की संकल्पना बौद्ध धर्म से प्रभावित है, जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने किया था।
2. सांख्य दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. यह सबसे प्राचीन दर्शन है।
2. इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं, अपितु प्रकृति से होती है।
3. प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से सृष्टि का निर्माण होता है।
उपर्युक्त 'कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3
(d) 1 और 3
उत्तर - (c)
व्याख्या- सांख्य दर्शन के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। यह सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है।
प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के लिए दैवी शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। अतएव यह एक तर्कमूलक प्राचीन मत था कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है ।
चौथी सदी के आस-पास सांख्य दर्शन में 'प्रकृति' के अतिरिक्त 'पुरुष' नामक एक और उपादान (उपहार) जुड़ा और दोनों को सृष्टि का कारण माना गया। इस नवीनतम मतानुसार 'प्रकृति' और 'पुरुष' दोनों के मेल से सृष्टि का निर्माण होता है।
3. योग दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है ।
2. ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह योगमार्ग का मूलाधार है ।
3. इसमें सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 3
(b) 2 और 3
(c) 1 और 2
(d) केवल 3
उत्तर - (c)
व्याख्या- योग दर्शन के संबंध में कथन (1) और (2) सत्य हैं। योग दर्शन के अनुसार, मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से प्राप्त होता है।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के आसन अर्थात् विभिन्न स्थिति में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम अर्थात् श्वास के व्यायाम बताए गए हैं। अतः ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह योगमार्ग का मूलाधार है।
कथन (3) असत्य है, क्योंकि योगदर्शन में सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
4. “जहाँ-जहाँ धुआँ रहता है, वहाँ-वहाँ आग रहती है" जैसी तर्कपूर्ण बातें किस दर्शन का हिस्सा हैं?
(a) योग दर्शन
(b) न्याय दर्शन
(c) सांख्य दर्शन
(d) वैशेषिक दर्शन
उत्तर - (b)
व्याख्या- “जहाँ-जहाँ धुआँ रहता है, वहाँ-वहाँ आग रहती है', जैसी तर्कपूर्ण बातें न्याय `का हिस्सा हैं। न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में ं हुआ है। इस दर्शन की विशेष बात यह है कि इसमें किसी प्रतिज्ञा या कथन की सत्यता की जाँच अनुमान, शब्द और उपमान द्वारा की जाती है।
5. वैशेषिक दर्शन के संबंध में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) यह सामान्य और विशेष के बीच कोई अंतर नहीं करता।
(b) पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएँ बनती हैं।
(c) वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की।
(d) वैशेषिक दर्शन ने भारत में भौतिकशास्त्र का आरंभ किया।
उत्तर - (a)
व्याख्या- वैशेषिक दर्शन के संबंध में कथन (a) सत्य नहीं है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन सामान्य और विशेष के बीच अंतर करता है। यह द्रव्य अर्थात् भौतिक तत्त्वों के विवेचन को महत्त्व देता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक थे और यह प्रकृतिवाद में अपनी अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। यह प्राकृतिक दर्शन में परमाणुवाद का एक रूप है।
6. मीमांसा दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. इसके अनुसार मोक्ष वेद-विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है।
2. वेद में कही गई बातें सदैव सत्य नहीं होती हैं।
3. मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर - (c)
व्याख्या- मीमांसा दर्शन के संबंध में कथन (1) और (3) सत्य हैं। मीमांसा का मूल अर्थ है- तर्क करने और अर्थ लगाने की कला, लेकिन इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने हेतु किया गया है। इस दर्शन के अनुसार, मोक्ष इन्हीं वेद - विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है।
मीमांसा दर्शन दृढ़तापूर्वक यह संकेत करता है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ आवश्यक है। ऐसे यज्ञों से पुरोहितों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता था और विविध वर्गों के बीच सामाजिक स्तरभेद को मान्यता मिलती थी।
कथन (2) असत्य है, क्योंकि मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद में कहीं गई बातें सर्वदा सत्य होती हैं।
7. वेदांत दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) बादरायण का 'ब्रह्मसूत्र' इस दर्शन का मूल ग्रंथ है।
(b) रामानुज ब्रह्म को निर्गुण बताते हैं।
(c) इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है।
(d) आत्मा और ब्रह्म अभेद है।
उत्तर - (b)
व्याख्या- वेदांत दर्शन के संबंध में कथन (b) सत्य नहीं है, क्योंकि वेदांत दर्शन में रामानुज ब्रह्म को सगुण बताते हैं, न कि निर्गुण | इस दर्शन में शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण बताते हैं। वेदांत का अर्थ है 'वेद का अंत' । ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में संकलित बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। वेदांत दर्शन का मूल आरंभिक उपनिषदों में पाया जाता है। इस दर्शन के अनुसार आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। अतः जो भी आत्मा को या स्वयं को पहचान लेता है, उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है।
8. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा भारतीय षड्दर्शन का हिस्सा नहीं है ?
(a) मीमांसा और वेदांत
(b) न्याय और वैशेषिक
(c) लोकायत और कापालिक
(d) सांख्य और योग
उत्तर - (c)
व्याख्या- लोकायत और कापालिक भारतीय षड्दर्शन का हिस्सा नहीं है । लोकायत को चार्वाक दर्शन भी कहते हैं, यह एक भौतिकवादी दर्शन है। अजित केशकंबली को इस दर्शन का अग्रदूत माना जाता है।
कापालिक एक संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लवकुलीश (लकुलीश) थे, यह शैव धर्म का अंग है।
1. निम्नलिखित में से कौन भारत के एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क को दर्शाता है ?
(a) श्रीलंका, बर्मा, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार
(b) ब्राह्मी अभिलेख का श्रीलंका में पाया जाना
(c) बर्मी लोगों द्वारा थेरवाद को विकसित करना
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर - (d)
व्याख्या- दिए गए सभी कथन भारत के एशियाई देशों के सांस्कृतिक संपर्क को दर्शाते हैं। भारत हड़प्पा युग से ही अपने एशियाई पड़ोसियों के साथ संपर्क में रहा था। भारतीय व्यापारी लोग मेसोपोटामिया के नगरों तक पहुँचे, जहाँ ईसा-पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 1700 के बीच उन व्यापारियों की मुहरें पाई गई हैं। धीरे-धीरे बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ भारत का संपर्क बढ़ा। अशोक के काल में श्रीलंका में धर्म प्रचारक के रूप में महेंद्र गया था।
यहीं से ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों के छोटे-छोटे ब्राह्मी अभिलेख श्रीलंका में पाए गए हैं। इसके पश्चात् ईसवी सन् की आरंभिक सदियों में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बर्मा अर्थात् आधुनिक म्यांमार की ओर हुआ।
बर्मी लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद को विकसित किया और बुद्ध की आराधना अनेक मंदिर और प्रतिमाएँ बनवाईं ।
2. निम्न कथनों पर विचार कीजिए
1. बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की रचना की।
2. श्रीलंका में समस्त पालि मूल ग्रंथ संगृहीत किए गए।
3. श्रीलंका से कालांतर में बौद्ध धर्म लुप्त हो गया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) 1, 2 और 3
उत्तर - (c)
व्याख्या- दिए गए कथनों में से कथन (1) और (2) सत्य हैं। भारत से बाहर धार्मिक प्रसार के क्रम में बर्मा और श्रीलंका के बौद्धों ने प्रचुर बौद्ध साहित्य की रचना की, जो भारत में दुर्लभ था। इस काल के दौरान श्रीलंका में समस्त पालि मूल ग्रंथ संगृहीत किए गए और उन पर टीकाएँ लिखी गईं ।
कथन (3) असत्य है, क्योंकि कालांतर में बौद्ध धर्म श्रीलंका में नहीं, बल्कि भारत में लुप्त हो गया। वर्तमान में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुतायत में में विद्यमान हैं।
3. अफगानिस्तान के किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति का निर्माण ईसवी सन् में हुआ था ?
(a) बेगराम
(b) बामियान
(c) हेरात
(d) काबुल
उत्तर - (b)
व्याख्या- अफगानिस्तान के बामियान नामक स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति का निर्माण ईसवी सन् में चट्टान को काटकर किया गया था।
यह स्थान अफगानिस्तान के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ से बुद्ध की बहुत-सी मूर्तियों और विहारों के पुरावशेष मिले हैं। इसके साथ का दूसरा स्थल बेगराम हाथीदाँत की दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कुषाण काल की भारतीय कलाकारी की झलक मिलती है।
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. बौद्ध धर्म के माध्यम से ही सभी क्षेत्रों से भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ।
2. बर्मा के पेगू और मोलमेन सुवर्ण भूमि कहलाते थे।
3. पांड्य राजाओं ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ स्थापित की।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 2
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1
उत्तर - (a)
व्याख्या- दिए गए कथनों में से कथन (2) सत्य है। बर्मा के पेगू और मोलमेन सुवर्ण भूमि कहलाते थे तथा भड़ौच, वाराणसी और भागलपुर के व्यापारी बर्मा के साथ व्यापार करते थे।
कथन (1) और (3) असत्य हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं पहुँची। बर्मा को छोड़कर अन्य देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतया ब्राह्मणीय धर्म के माध्यम से हुआ। ईसवी सन् की आरंभिक सदियों में पांड्य राजाओं ने नहीं, बल्कि पल्लव शासकों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ स्थापित की थीं।
5. प्राचीन भारत के लोगों के सुवर्णद्वीप के साथ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध थे। इसकी पहचान किससे की गई है?
(a) इंडोनेशिया (जावा)
(b) सुमात्रा
(c) फिलीपींस
(d) सिंहलद्वीप
उत्तर - (a)
व्याख्या- भारतीयों के ईसा की पहली सदी से ही इंडोनेशिया (जावा) के साथ, जिसे प्राचीन भारत के लोग सुवर्णद्वीप कहते थे, घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। यहाँ पर 56 ई. में सर्वप्रथम स्थापित की गई भारतीय बस्तियाँ इस तथ्य का प्रमाण देती हैं कि ईसा की दूसरी सदी में यहाँ कई छोटे-छोटे भारतीय राज्य भी स्थापित हुए।
6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) सौराष्ट्र से आने वाले व्यापारी प्राय: जैन होते थे।
(b) दक्षिण भारत से आने वाले व्यापारी शैव और वैष्णव होते थे।
(c) बंगाल से आने वाले व्यापारी बौद्ध होते थे।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं ।
उत्तर - (d)
व्याख्या- दिए गए सभी कथन सत्य है ।
ईसा की सातवीं शताब्दी तक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का संबंध काफी बढ़ गया था। धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों ने भारतीय संस्कृति की • कुछ बातें स्वीकार कर लीं। भारत के व्यापारी सौराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल आदि से दक्षिण-पूर्व एशिया जाते थे। सौराष्ट्र से आने वाले व्यापारी प्राय: जैन होते थे। दक्षिण भारत से आने वाले शैव और वैष्णव तथा बंगाल से आने वालों में बौद्धों की बहुतायत थी।
7. गुप्तोत्तर कालीन धार्मिक प्रवृत्तियों में आए परिवर्तन के संबंध में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) पंचदेवता में इंद्र का स्थान प्रमुख था
(b) मारुत पंचदेवता में शामिल नहीं थे
(c) वरुण लोकपाल की श्रेणी के देवता थे
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर - (a)
व्याख्या- गुप्तोत्तर कालीन धार्मिक प्रवृत्तियों के संबंध में कथन (a) सत्य नहीं है। गुप्तोत्तर काल में ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति और शिव पाँच देवताओं की पूजा प्रचलित रही, जिन्हें सम्मिलित रूप से 'पंचदेवता' कहा जाता था। इस काल में देवमाला में देवताओं का स्थान उनकी श्रेष्ठता के क्रम में दिया जाने लगा। विष्णु, शिव और दुर्गा ये तीनों मुख्य देवता के रूप में ग्रहण किए गए और कई अन्य देव और देवियाँ उनके अधीन या गौण देवता माने गए तथा परिचरों और अनुचरों के रूप में उनके नीचे रखे गए।
1. भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. ऐसी मान्यता थी कि वर्ण व्यवस्था दैवी शक्ति द्वारा निश्चित की गई थी।
2. प्रत्येक वर्ण की न केवल सामाजिक पहचान, बल्कि अनुष्ठानिक पहचान भी थी।
3. रामायण में वर्णित है कि दूसरे के धर्म को अपनाने के बदले अपने धर्म की रक्षा के लिए मर जाना अच्छा है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 2
उत्तर - (a)
व्याख्या- भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के संबंध में कथन ( 1 ) और (2) सत्य हैं ।
भारत में धर्म के प्रभाव से विशेष प्रकार के सामाजिक वर्गों का गठन हुआ। भारत में वर्ण संबंधी नियमों को राज्य और धर्म दोनों का समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन समाज में ऐसा विश्वास प्रचलित था कि वर्ण व्यवस्था दैवी शक्ति द्वारा निश्चित की गई है।
भारत में समाज चार वर्णों में विभक्त था - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । इन वर्णों की न केवल सामाजिक पहचान, बल्कि अनुष्ठानिक पहचान भी थी। कानून और धर्म ने वर्णों और जातियों को कर्ममूलक, से जन्ममूलक या आनुवंशिक बना दिया।
कथन (3) असत्य है, क्योंकि रामायण नहीं, बल्कि भगवद्गीता हमें यह सिखाती है कि दूसरे के धर्म को अपनाने के बदले अपने धर्म की रक्षा के लिए मर जाना अच्छा है, क्योंकि दूसरे धर्म को अपनाने का परिणाम संकटपूर्ण होता है।
2. प्राचीन भारत में हुए सामाजिक परिवर्तनों के अनुक्रम के संबंध में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) गाय की रक्षा के कारण राजा 'गोपति' कहलाता था ।
(b) बेटी को दुहितृ कहा जाता था।
(c) बैल को गोवाल कहा गया।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर - (c)
व्याख्या- दिए गए कथनों में से कथन (c) सत्य नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत में हुए सामाजिक परिवर्तनों के अनुक्रम में 'गोवाल' शब्द बैल के लिए नहीं, बल्कि भैंस के लिए प्रयोग किया गया। वैदिक आर्यों को गाय से इतनी घनिष्ठता थी कि जब उन्होंने भारत में भैंस को पहली बार देखा तो 'गोवाल' अर्थात् गाय जैसे बालों वाली कहने लगे।
3. प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. द्विजों को यज्ञोपवीत का अधिकार प्राप्त नहीं था।
2. शूद्रों को 'अनागरिक' की संज्ञा दी गई थी।
3. ब्राह्मणों को कर्ज पर ब्याज दो प्रतिशत मिलता था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर - (b)
व्याख्या- प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों में से कथन (2) और (3) सत्य हैं।
प्राचीन काल की सामाजिक वर्ण संरचना में शूद्रों का स्थान निम्न था। उन्हें अपने से ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी होती थी। कुछ स्मृतिकारों ने शूद्रों को दास के रूप में प्रयोग किया है। अतः इन्हें 'अनागरिक' की संज्ञा दी गई थी। प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के लिए भुगतान की दर और आर्थिक सुविधा अलग-अलग निश्चित की गई थी। ब्राह्मणों को कर्ज पर ब्याज दो प्रतिशत मिलता था, क्षत्रियों को तीन प्रतिशत, वैश्यों को चार प्रतिशत तथा शूद्रों के लिए पाँच प्रतिशत निर्धारित था।
कथन (1) असत्य है, क्योंकि प्राचीन काल में द्विज शब्द का प्रयोग संयुक्त रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए किया जाता था और उन्हें वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत संस्कार पाने का अधिकार था, परंतु शूद्र इससे वंचित थे।
4. कलियुग का लक्षण विभिन्न वर्गों या सामाजिक वर्गों के मिश्रण का होना बताया गया है, जिसे क्या कहते हैं?
(a) वर्ण संकर
(b) चांडाल
(c) शूद्र
(d) द्विज
उत्तर - (a)
व्याख्या- कलियुग का लक्षण विभिन्न वर्णों या सामाजिक वर्गों के मिश्रण का होना बताया गया है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। इसका यह आशय है कि वैश्यों और शूद्रों (किसानों, शिल्पियों और मजदूरों) ने अपने ऊपर सौंपे गए उत्पादन कार्य करने बंद कर दिए अर्थात् वैश्य किसानों ने कर चुकाना बंद कर दिया और शूद्रों ने मजदूरी करना छोड़ दिया। वे विवाह आदि सामाजिक संबंधों में वर्णसंबंधी प्रतिबंधों की उपेक्षा करने लगे, इन सभी कृत्यों ने एक नई पद्धति का विकास किया।
5. धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णित 'उचित जीविका' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. ब्राह्मणों का कार्य दान देना और लेना था।
2. क्षत्रियों का कार्य न्याय करना है।
3. गौ-पालन शूद्रों का कार्य था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?
(a) 1 और 3
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 3
उत्तर - (d)
व्याख्या- धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णित 'उचित जीविका' के संबंध में कथन (3) असत्य हैं, क्योंकि गौ-पालन का कार्य वैश्यों का था न कि शूद्रों का। वैश्यों को तीन कार्य करने होते थे, जिनमें शामिल हैं- कृषि, गौ-पालन तथा व्यापार कार्य, जबकि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका थी- तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना ।
6. जाति एवं सामाजिक गतिशीलता के संबंध में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) वर्ण की भाँति जाति भी जन्म पर आधारित थी।
(b) वर्ण की भाँति जातियों की संख्या भी निश्चित थी।
(c) जंगल में रहने वालों को निषाद कहा जाता था।
(d) सुवर्णकार जाति समूह का प्रतिनिधित्व करता था।
उत्तर - (b)
व्याख्या- जाति एवं सामाजिक गतिशीलता के संबंध में कथन (b) सत्य नहीं है। जाति एवं सामाजिक गतिशीलता के परंपरागत सिद्धांत में चार वर्ण बताए गए हैं, जबकि जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। हालाँकि वर्ण की भाँति जाति भी जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मणीय व्यवस्था में अनेक नए समुदायों का उदय हुआ, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में समाहित करना सरल नहीं था। अतः उन्हें जातियों में बाँट दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थीं, उन्हें कभी-कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था।
7. प्राचीन भारतीय समाज को मध्यकालीन समाज में बदलने के कारणों में कौन शामिल था?
(a) इसका मूल कारण भूमि अनुदान था।
(b) वर्णमूलक समाज का अत्यधिक कठोर होना।
(c) भूमि अनुदान के कारण भू-स्वामियों का उदित होना।
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर - (d)
व्याख्या- प्राचीन भारतीय समाज को मध्यकालीन समाज में बदलने में उपर्युक्त सभी कारण शामिल थे। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित हैं
प्राचीन भारतीय समाज, जो धीरे-धीरे मध्यकालीन समाज में परिणत हुआ, उसका मूल कारण भूमि अनुदान की प्रथा थी। भूमि अनुदान की प्रथा के फलस्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना हुई, जिसमें भोग-विलासी जीवन और नियत कर्मों से विमुख होना प्रमुख था।
वर्णमूलक समाज, जिसमें वैश्य और शूद्र सम्मिलित थे, इनके उत्पादनात्मक क्रियाकलापों पर संपूर्ण व्यवस्था निर्भर थी, लेकिन कलियुग संकट के फलस्वरूप यह व्यवस्था एक नया रूप लेने लगी।
भूमि अनुदान की प्रथा ने भूस्वामियों के उदय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप अनेक राजाओं का प्रभुत्व क्षेत्र कम होता गया।
8. छठी - सातवीं सदी में सांस्कृतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. सातवीं सदी में संस्कृत के गद्य और पद्य की अलंकृत शैलियों का प्रचलन बढ़ा।
2. गद्य में अलंकरण की पराकाष्ठा 'बाण' की कृतियों में मिलती है।
3. सातवीं सदी में देव प्रतिमाएँ केवल प्रस्तर की बनाई जाती थीं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) केवल 3
उत्तर - (a)
व्याख्या- छठी-सातवीं सदी में सांस्कृतिक विकास के संबंध में कथन (1) और (2) सत्य हैं ।
छठी-सातवीं शताब्दी संस्कृत साहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। शासक वर्ग द्वारा लगातार उपयोग में आने से संस्कृत भाषा का सातवीं सदी तक गद्य तथा पद्य • प्रचलन बढ़ता गया।
मध्यकाल के संस्कृत लेखकों द्वारा बाणभट्ट की रचनाओं का अनुसरण करना, बाण की गद्य में अलंकरण की पराकाष्ठा को दर्शाता है।
कथन (3) असत्य है, क्योंकि सातवीं सदी में देव प्रतिमाएँ केवल प्रस्तर की नहीं, बल्कि प्रस्तर तथा कांसा के मिश्रण से निर्मित की गई थीं।
9. भारत के सांस्कृतिक इतिहास में 'पंचायतन' शब्द किसे निर्दिष्ट करता है ?
(a) बुजुर्गों की आम सभा
(b) श्रमिकों का संघ
(c) एक मंदिर शैली
(d) राजा की परिषद्
उत्तर - (c)
व्याख्या- गुप्तोत्तर काल में प्रचलित 'पंचायतन' एक विशेष प्रकार के मंदिर को दर्शाता है। गुप्तोत्तर काल धार्मिक परिवर्तनों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है। इस समय पंचदेवता (ब्रह्मा, गणपति, विष्णु, शक्ति और शिव) प्रचलित हुए। मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देव या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों और बने चार गौण मंदिरों में चार अन्य देवता स्थापित किए जाते थे। ऐसे ही मंदिरों को 'पंचायतन' का दर्जा प्राप्त था।
10. प्राचीन कालीन कला और साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. उत्तरी काले पॉलिशदार मृद्भांड उन्नत अवस्था में थे।
2. बुद्ध की पहली मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई थी।
3. गुप्तकाल में मंदिरों का निर्माण प्रस्तर खंड में हुआ है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है /हैं?
(a) 1 और 3
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 3
उत्तर - (b)
व्याख्या- प्राचीन कालीन कला और साहित्य के संबंध में कथन (1) और (2) सत्य हैं।
प्राचीन भारत में शिल्पकार सुंदर कलाकृतियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध थे। अशोक द्वारा बनवाए गए अखंड प्रस्तर के स्तंभ अपनी चमकदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु उनकी तुलना उत्तरी काले पॉलिशदार मृद्धांड से की जाती है। अतः यह अवस्था दर्शाती है कि ये मृद्धांड अपनी उन्नत अवस्था में थे।
भारतीय कला और यूनानी कला के मिश्रण से जिस कला-शैली का जन्म हुआ, वह गांधार शैली कहलाती है। बुद्ध की पहली प्रतिमा गांधार शैली में ही निर्मित थी।
कथन (3) असत्य है, क्योंकि गुप्तकाल में मंदिरों का निर्माण ईंटों के प्रयोग द्वारा किया जाता था और इसका प्रारंभ गुप्तकाल में ही हुआ।
1. प्राचीन कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. उत्तर वैदिक काल में किसान शासकों और योद्धाओं को नजराना देते थे।
2. किसान लौहारों, रथकारों और बढ़इयों का पेट भरते थे ।
3. उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग 'बल' कहलाने लगे।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3
उत्तर - (d)
व्याख्या- प्राचीन कालीन कृषि के संबंध में सभी कथन सत्य हैं ।
उत्तर वैदिक काल में किसान और अन्य लोगों के द्वारा राजाओं और योद्धाओं को राजांश (नजराना) दिया जाता था, जिसका उपयोग राजा द्वारा यज्ञ और पुरोहितों के संपोषण हेतु किया जाता था।
किसान मुख्यत: योद्धा वर्ग के रूप में उभर रहे लौहारों, रथकारों और बढ़ई की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे तथा उनका पेट भरते थे ।
वैदिक काल में किसानों की सेना ने पशुचारक सेना का स्थान लिया और धीरे-धीरे सशस्त्र सेना के रूप में संगठित हुए। उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग 'बल' अर्थात् सैन्य शक्ति कहलाने लगे।
2. निम्नलिखित में किसके लिए वैदिक साहित्य में किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है?
(a) शिल्पियों के लिए
(b) मजदूरों के लिए
(c) गाय के लिए
(d) बढ़ई के लिए
उत्तर - (b)
व्याख्या- वैदिक साहित्य में मजदूरों के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदली और मौर्यकाल तक आते-आते दास और मजदूर बड़े-बड़े राजकीय कृषि क्षेत्रों में कार्य करने लगे, जिसकी जानकारी कौटिल्य की रचना 'अर्थशास्त्र' से मिलती है।
3. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(a) भूमि अनुदान से कृषि पंचांग का प्रचार हुआ।
(b) भूमि अनुदान से सुदूर दक्षिण और सुदूर पूर्व में सभ्यता का विस्तार हुआ।
(c) पूर्व मध्यकाल के ग्रंथों में शूद्रों को कृषक कहा जाने लगा।
(d) सामंती ढाँचे में भू-स्वामियों और योद्धाओं के वर्ग की स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ।
उत्तर - (d)
व्याख्या- दिए गए कथनों में से कथन (d) सत्य नहीं है, क्योंकि छठी सदी के आस-पास सामंती ढाँचे में भू-स्वामियों और योद्धाओं के वर्ग की स्त्रियों की दशा सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन बढ़ा, लेकिन निचले वर्ग की स्त्रियों को आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने और पुनर्विवाह करने में स्वायत्तता दी गई। सामंती ढाँचे का उदय भूमि अनुदान के परिणामस्वरूप उपजी एक व्यवस्था थी।
4. प्राचीन भारत की नई कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक बतलाया।
2. भू- स्वामी सामान्यतः सभी वर्गों के होते थे।
3. कृषक को गाँव अनुदान के रूप में दिया जाता था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 3
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1
उत्तर - (a)
व्याख्या- प्राचीन भारत की नई कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में कथन ( 1 ) और (3) सत्य हैं ।
प्राचीन भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसी क्रम में ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक बताया है। अतः इससे ज्ञात होता है कि शूद्र, कृषि-मजदूरों और दासों के रूप में कृषि कार्य करना छोड़ रहे थे।
पाँचवीं-छठी सदी में जनजातीय क्षेत्रों में सामान्यतः गाँव अनुदान में दिया जाता था। साथ ही उस क्षेत्र के कृषक भी इस व्यक्ति को सौंप दिए जाते थे, जिन्हें अनुदान में संपूर्ण गाँव दिया जाता था।
कथन (2) असत्य है, क्योंकि भू-स्वामी सामान्यतः ब्राह्मण होते थे न कि सभी वर्णों के।
5. गुप्तोत्तर कालीन कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. इस समय कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र में बँटाईदार या गैर-स्वामित्व प्राप्त किसान आ गए थे।
2. कृष्य भूमि अनुदान की पद्धति को समर्थन प्राप्त हुआ था।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर - (c)
व्याख्या- गुप्तोत्तर कालीन कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दोनों कथन सत्य हैं। गुप्तोत्तर काल में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब भू-स्वामी न तो स्वयं भूमि पर कृषि करते थे और न ही प्रत्यक्ष रूप से कर वसूलते थे। अब भूमि आबाद करने और कर वसूली का अधिकार बँटाईदारों अथवा गैर-स्वामित्व प्राप्त किसानों को दिया गया था।
कृष्य भूमि अनुदान की प्रथा को नवोदित शासकों का समर्थन था।
1. विश्व में इस्पात बनाने की कला सबसे पहले किस देश में विकसित में हुई थी?
(a) यूरोप
(b) भारत
(c) चीन
(d) अफ्रीका
उत्तर - (b)
व्याख्या- विश्व में सर्वप्रथम इस्पात बनाने की कला भारत में विकसित हुई। इस्पात बनाने की कला भारतीयों की भौतिक संस्कृति का द्योतक है । इस्पात निर्माण ने भारतीयों को निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया, जिससे भारत का व्यापार यूरोपीय देशों तक बढ़ा । प्राचीन काल में भारत से परिष्कृत लोहे के निर्यात व्यापार को 'उट्ज' कहा जाता था।
2. प्राचीन काल में प्रचलित विज्ञान एवं गणित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. भारतीयों ने अंकन पद्धति, दाशमिक पद्धति और शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ किया था।
2. अरबों के द्वारा भारतीय अंकन पद्धति को अपनाया गया।
3. ईरानियों ने स्वयं अपनी अंकमाला को हिंदसा कहा।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है / हैं?
(a) 1 और 3
(b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 2
उत्तर - (b)
व्याख्या- प्राचीन काल में प्रचलित विज्ञान एवं गणित के संबंध में से कथन (1) और (2) सत्य हैं ।
ईसा पूर्व तीसरी सदी गणित, खगोल - विद्या और आयुर्विज्ञान के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण थी । गणित के क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अंकन पद्धति, दाशमिक पद्धति और शून्य के प्रयोग का विकास किया गया। भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और उसका पश्चिमी देशों में प्रसार किया।
कथन (3) असत्य है, क्योंकि ईरानियों ने नहीं, बल्कि अरबों ने स्वयं अपनी अंकमाला को 'हिंदसा' कहा। पश्चिमी देशों में इस अंकमाला का प्रचार होने के सदियों पहले ही भारत में इसका प्रयोग किया जा चुका था।
3. ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के लिए उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए किसने व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की?
(a) ब्रह्मगुप्त
(b) आर्यभट्ट
(c) आपस्तंब
(d) वराहमिहिर
उत्तर - (c)
व्याख्या- ईसा-पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के लिए उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्तंब ने व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की। इस ज्यामिति में न्यूनकोण, अधिककोण और समकोण का वर्णन किया गया है।
4. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सत्य नहीं है?
(a) अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है।
(b) सुश्रुत संहिता में शल्य विधि का वर्णन है।
(c) चरक को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है।
(d) चरक संहिता में कुष्ठ और मिरगी का वर्णन है।
उत्तर - (c)
व्याख्या- दिए गए कथनों में से कथन (c) सत्य नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान (चिकित्सा विज्ञान) में सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, न कि चरक को। प्राचीन भारत में वैद्यों ने शरीर रचना विज्ञान, जिसे एनटॉमी कहते हैं, का अध्ययन किया और इन्होंने रोगों के उपचार हेतु नई विधियों की खोज की तथा औषधि भी बताई । औषधियों का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..